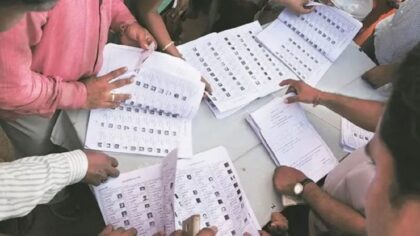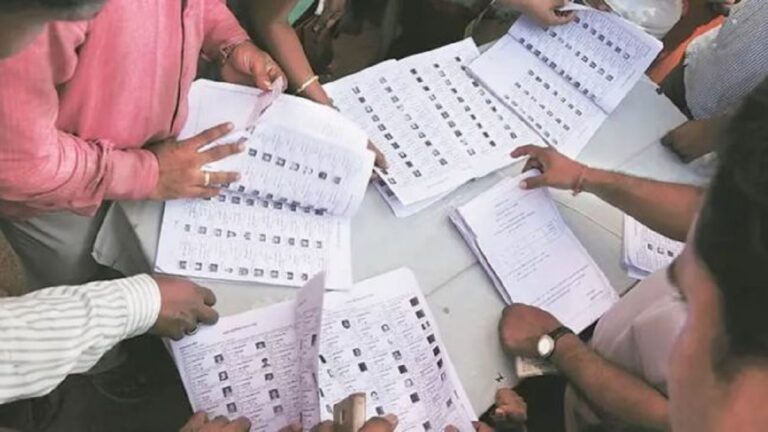अभी तक देश को यही बताया गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से निजी वाहनों की आवक और पंजाब-हरियाणा के किसानों के द्वारा जलाई जाने वाली पराली जिम्मेदार है। लेकिन 15 नवंबर 2024 को जारी Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) की रिपोर्ट कुछ ऐसे पहलुओं को उजागर करती है, जिसे देख सहसा यकीन नहीं होता कि इस सबके लिए खुद सरकार सबसे अधिक जिम्मेदार है।
पिछले एक दशक से वायु प्रदूषण की समस्या अब एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है, जिसके लिए अब केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी एक दूसरे को कोसना बंद कर दिया है। बीच-बीच में जरुर सुप्रीम कोर्ट की फटकार बजती है और शांत हो जाती है, मानो आम लोगों को संतुष्ट करने के लिए नक्कारखाने से कभी-कभी मुनादी करना और जागते रहो-जागते रहो से भरोसा कायम रहे।
हम एक ऐसी व्यवस्था से घिरे हुए हैं, जिसमें सिर्फ वायु प्रदूषण से सांसें ही नहीं घुट रही हैं, बल्कि आँख, नाक, कान और दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है। अर्थव्यवस्था का पहिया पहले से दलदल में बुरी तरह से धंस चुका है। मेक इन इंडिया और पीएलआई का चारा देकर कुछ विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है तो वे भी भारत को अपना बाजार बनाने में अधिक रूचि रखती हैं, और मोटी सब्सिडी का फायदा उठाते हुए भी देश में रोजगार सृजन में नगण्य योगदान कर रही हैं।
लेकिन इस सबके बीच में प्रदूषण दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कैसे देश की सरकार ही वायु प्रदूषण के लिए सबसे बड़ी दोषी है, इस बारे में पहली बार ध्यान दिलाया है मनी कण्ट्रोल की एक रिपोर्ट ने, जिसने Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) की रिपोर्ट को अपना आधार बनाकर बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में थर्मल पावर प्लांट पराली जलाने की तुलना में 16 गुना अधिक वायु प्रदूषक उत्सर्जित कर रहे हैं।
CREA के अध्ययन में कहा गया है, “NCR में थर्मल पावर प्लांट 8।9 मिलियन टन धान के भूसे को जलाने से निकलने वाले 17.8 किलोटन से 16 गुना अधिक वायु प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं।”
यह निष्कर्ष ऐसे समय में आया है जब 17 नवंबर को दिल्ली की वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गई, AQI 441 पर पहुंच गया, जिससे यह देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। शहर का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), जो प्रतिदिन शाम 4 बजे दर्ज किया जाता है, 441 पर रहा, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। शनिवार को AQI 417 था।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, “गंभीर” AQI स्वस्थ व्यक्तियों के लिए जोखिम पैदा करता है और पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों पर गंभीर प्रभाव डालता है। CREA के अनुमान के अनुसार, जून 2022 और मई 2023 के बीच एनसीआर में कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट द्वारा 281 किलोटन सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) छोड़ा गया।
यहां पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में भारत विश्व में सबसे बड़े SO₂ उत्सर्जक के तौर पर जाना जाता है, और दुनिया में SO₂ उत्सर्जन के 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, जिसका मुख्य कारण इसका कोयला-आधारित ऊर्जा क्षेत्र पर निर्भरता है। 2023 में बिजली उत्पादन से भारत का SO₂ उत्सर्जन 6,807 किलोटन मापा गया, जो तुर्की (2,206 किलोटन) और इंडोनेशिया (2,017 किलोटन) जैसे अन्य प्रमुख उत्सर्जकों के उत्सर्जन से अधिक था। हाल के वर्षों में बिजली की मांग में भारी बढ़ोत्तरी को देखते हुए कोयला ब्लॉक्स के आवंटन और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में कॉर्पोरेट के लिए खनन को सुचारू बनाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई का काम चरम पर पहुंच चुका है।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए पराली से 16 गुना अधिक जिम्मेदार है थर्मल पॉवर प्लांट का उत्सर्जन
रिपोर्ट में पाया गया है कि दिल्ली-एनसीआर थर्मल पावर प्लांट उत्सर्जन और पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के बीच तुलना से SO2 प्रदूषण के पैमाने पर प्रकाश पड़ता है। एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट सालाना 281 किलोटन SO2 उत्सर्जित करते हैं, जो कि 89 लाख टन धान की पराली जलाने से होने वाले 17.8 किलोटन उत्सर्जन से 16 गुना अधिक है।
अगर यह सच है तो क्या हमें पिछले 7-8 वर्षों से सरकारें यूँ ही बेवकूफ बना रही हैं, और दिल्ली-पंजाब-हरियाणा को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है?
यहां पर CREA के विश्लेषक मनोज कुमार का कहना है कि, “एनसीआर में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से निकलने वाले 96 प्रतिशत से अधिक कण प्रदूषण द्वितीयक प्रकृति के होते हैं, जो मुख्य रूप से SO2 से उत्पन्न होते हैं। SO2 उत्सर्जन को कम करने से द्वितीयक कण पदार्थ का भार काफी कम हो सकता है, जिससे इन कणों के लंबे समय तक संपर्क से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम कम हो सकते हैं।”
वे आगे कहते हैं, “SO2 का स्तर अक्सर NAAQS को पूरा करता है, क्योंकि एक बार जारी होने के बाद, यह जल्दी से सल्फेट्स में तब्दील हो जाता है – द्वितीयक कण जो PM2.5 के प्रमुख घटक हैं। इन द्वितीयक कणों का जीवनकाल लंबा होता है, और ये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम को जन्म देते हैं। SO2 का हानिकारक कणों में यह छिपा हुआ परिवर्तन FGD स्थापना की आवश्यकता पर जोर देता है।”
यह FGD क्या है?
FGD (फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन) प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जिसका उपयोग जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों के निकास फ्लू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए किया जाता है, तथा अन्य सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जित करने वाली प्रक्रियाओं जैसे अपशिष्ट भस्मीकरण, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, सीमेंट और चूना भट्टियों से निकलने वाले उत्सर्जन को हटाने के लिए किया जाता है।
CREA की रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर, FGD सिस्टम की स्थापना से SO2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाइ जा सकती है, जो कुल 4,327 किलोटन से घटकर 1,547 किलोटन रह जाएगा। यह कुल मिलाकर लगभग 64% की कमी है, जो CFPP से वायु प्रदूषण को कम करने में FGD तकनीक के जबरदस्त संभावित प्रभाव को दर्शाता है।
इसका अर्थ हुआ कि हमारी देश की सरकार और सर्वोच्च न्यायालय यदि मर्ज का सही इलाज करना चाहे तो सिर्फ FGD प्रणाली की स्थापना से 64% SO2 या सल्फर डाईऑक्साइड में कमी लाकर हजारों लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। लेकिन वायु प्रदूषण के नाम पर विपक्षी सरकारों की आलोचना और उन्हें जनता में बदनाम कर अपनी चुनावी जीत का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।
एकबारगी देखकर तो यही समझ आता है कि हमारे देश के हुक्मरानों, न्यायविदों और नौकरशाहों तक ने सच्चाई से आँखें मूंद ली हैं, और निजी हित और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट को ही देशहित मानकर पूरे देश को एक ऐसी भट्टी में झोंक दिया है, जिससे बच निकलने की कोई सूरत निकलती नजर नहीं आती। भूले-भटके कोई समाचारपत्र यदि इस बारे में आम लोगों के ध्यानार्थ जानकारी साझा भी कर देता है तो ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ या भैंस चुरा ले जायेंगे जैसे नारों की शोरगुल में पक्ष-विपक्ष मिलकर ऐसी रिपोर्टों को कूड़े के ढेर में डालने का ही काम करती हैं।
नोट: CREA फिनलैंड में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत संस्था है, जिसके कर्मचारी एशिया और यूरोप में फैले हुए हैं। यह संस्था परोपकारी अनुदानों और कमीशन किए गए शोध से प्राप्त राजस्व के माध्यम से वित्त पोषित है।
(रविंद्र पटवाल जनचौक संपादकीय टीम के सदस्य हैं)