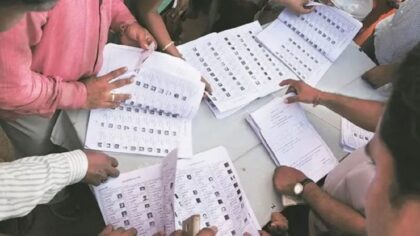भारत में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर कुछ गहरी आशंकाएं उभर रही हैं। इतिहास की गहरी घाटियों से कुछ चीखें सतह पर हैं तो भविष्य के ठहाकों की तेज ध्वनियां भी सतह पर जमा हो रही हैं। चीख और ठहाकों के एक साथ सतह पर सक्रिय हो जाने से वर्तमान परिस्थिति की रुलाइयों से गहरा संबंध है। इन रुलाइयों को ठीक-ठीक उसी संदर्भ में समझने के लिए इतिहास की गहरी घाटियों में भी झांकना जरूरी है और भविष्य की तरफ आंख गड़ाना भी जरूरी है। भारत के लोकतंत्र की अवस्था को ठीक-ठीक लोकतंत्र के संदर्भ में समझने के लिए यह जरूरी है। मुश्किल यह है कि भारत के विविध आयामों को एक साथ देखने के लिए पूर्वग्रह मुक्त मन-मस्तिष्क और खुले दिल का बहुआयामी निश्छल नजरिया और जनविवेक चाहिए।
लोकतंत्र की चिंता में भारत राष्ट्र के राजनीतिक स्वरूप और ढांचे की भी चिंता शामिल है। भारत की आजादी के समय देश-विदेश के कई राजनीतिक चिंतकों ने भारत जैसे वैविध्य-संपन्न और बहुलात्मक देश के “एक राष्ट्र” बनने और बने रहने पर संदेह व्यक्त किया था। उनके संदेह निराधार नहीं थे। हमारे राष्ट्र निर्माताओं को इस खतरे का आभास था। इस खतरे से बचाव के लिए उन्होंने पर्याप्त संवैधानिक प्रावधानों का सचेत प्रबंध किया और साफ-साफ व्यवस्था दी; India, that is Bharat, shall be a Union of States. अर्थात इंडिया, जो भारत है, राज्यों का संघ होगा। संघात्मकता ढांचा के प्रति स्वाभाविक स्थिति में पर्याप्त सम्मान के साथ-साथ अ-स्वाभाविक स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन ‘एकात्मकता’ के भी संवैधानिक प्रावधान हैं। लोकविग्रह (Balkanization) के ब्लेकहोल से बचने के लिए हमारे संविधान में पर्याप्त उपाय हैं। बात बिल्कुल साफ है कि राज्य भारत संघ के संघटक हैं, अधीनस्थ नहीं। राज्य सरकारें संघ सरकार की संप्रभुता के प्रति सम्मानशील रहते हुए स्वायत्त हैं, संघ सरकार के अधीनस्थ विभाग नहीं।
वैश्विक राजनीति और औद्योगीकरण की परिस्थिति और अन्य कारणों, जिन में भौगोलिक, सांस्कृतिक, नस्लीय आदि कारणों से युरोप-अमेरिका के राष्ट्रों में लोकविग्रह (Balkanization) की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध की ठीक समाप्ति और शीत युद्ध की शुरुआत के दौरान सब से बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत अपने सुसंगठित होने की तैयारी में लगा हुआ था। हमारे महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं और संविधान निर्माताओं को वैश्विक परिस्थिति की पूरी जानकारी थी। इसलिए संवैधानिक न्याय और भारत राष्ट्र में ढांचागत संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया।
दीर्घकालिक अ-स्वाभाविकता की स्थिति उत्पन्न हो जाने या कर देने या स्वाभाविक स्थिति को अ-स्वाभाविक बताकर आपातकालीन ‘एकात्मकता’ के उपायों पर भारत सरकार की दिलचस्पी बढ़ जाने से भारत की राष्ट्रीय एकता पर चोट होती है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से बनी लोकतांत्रिक सरकार के कई असाध्य अंतर्विरोधों में से एक अंतर्विरोध यह है कि वह संघात्मकता में राष्ट्रीय एकता के प्रति यह विश्वासी नहीं है। इसके चलते हर समय किसी-न-किसी बहाने एकात्मकता पर कुछ-न-कुछ जोर देती ही रहती है। तकनीकी रूप से यह असंवैधानिक न भी हो, व्यावहारिक रूप से भारत की राष्ट्रीय एकता पर ऐसे नजरिये से चोट ही पड़ती है। स्वाभाविक स्थिति में एकात्मकता पर जोर देते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की सोच में खोट है; संघात्मकता ही टिकाऊ राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित कर सकती है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की संप्रभुता राज्य सरकारों की संवैधानिक स्वायत्तता पर अकसर दबाव बनाती रहती है। इससे भारत राष्ट्र में ढांचागत असंतुलन का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है।
छोटे-मोटे झटकों के अलावा भारत की राष्ट्रीय एकता को कोई बहुत बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से इन झटकों का सामना करने में भारत राष्ट्र सफल रहा चाहे, मामला नगालैंड से जुड़ा हो या असम, मणिपुर, अरुणाचल आदि से जुड़ा हो। हां, एक बड़ी चुनौती पंजाब में उभरी थी। उसका भी प्रिय-अप्रिय समाधान हुआ।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल (5 जून 1975 से 21 मार्च 1977) लगाया था। जिन परिस्थितियों में आपातकाल घोषित हुआ था उनमें से एक परिस्थिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस जग मोहन लाल सिन्हा के फैसले से उत्पन्न हुई थी। असल में, 1971 में राज नारायण चुनाव में प्रधानमंत्री के निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जग मोहन लाल सिन्हा ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया। फैसले में छह वर्षों के लिए किसी निर्वाचित पद पर बने रहने से भी वंचित कर दिया गया था।
दोष? इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री सचिवालय में विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD) यशपाल कपूर की सेवाओं का इस्तेमाल करने और चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए मंच बनाने में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की मदद लेने का दोषी पाया गया था। यशपाल कपूर अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन इस्तीफे की तारीख में दो-चार दिन का अंतराल था। छह वर्षों के लिए किसी निर्वाचित पद पर बने रहने से भी वंचित कर देना एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई ऐसे राजनीतिक कदम उठाये जो लोकतांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध था। घोषित आपातकाल (5 जून 1975 से 21 मार्च 1977) में विपक्ष के राजनीतिक नेताओं और पत्रकारों पर कहर बरपा।
आपातकाल भारत के लोकतंत्र का बहुत बुरा दौर था। बहुत ज्यादतियां हुई यह सच है। लेकिन यह सब घोषित आपातकाल में हुआ था। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे अर्थात, संघात्मकता पर इस से आंच नहीं आई। हां, नागरिक अधिकार पर इसका बहुत बुरा असर जरूर पड़ा था। इस बुरे असर को इसलिए कम करके नहीं देखा जा सकता है कि आपातकाल के दौरान रेल समय पर चलने लगी थी, सरकारी दफ्तर में सभी समय पर उपस्थित होने लगे थे, सूदखोरों और महाजनों का गरीब लोगों पर दबाव काम हो गया था।
भारतीय जनता पार्टी के पिछले दस साल के शासन में कोई संवैधानिक आपातकाल तो घोषित नहीं हुई। लेकिन, ऐसे-ऐसे असंवैधानिक कारनामे, खास कर विपक्ष की राजनीति के संदर्भ में, हुए जिन्हें अंजाम देने के लिए दुनिया के किसी संविधान में कोई प्रावधान किये ही नहीं जा सकते हैं। ये कारनामे लोगों को दिखते हैं, लेकिन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण जुटाना संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी विभागों आदि का काम होता है। संस्था और विभाग में काम करनेवाले नौकरशाही की राजनीतिक सत्ता से ऐसी बेमिसाल मिलीभगत तैयार हुई कि न तो संविधान की कोई परवाह बची न लोक का कोई लाज-लिहाज बची।
राजनीतिक वैमनस्य का पहाड़ और आर्थिक विषमता की खाई ने राजनीतिक मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि जनता से जुड़े जीवनयापन के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी धर्म और आस्था से जोड़ दिया जाता है। भावनात्मक हिंसा और विपक्ष के नेताओं की सब से निकृष्ट अर्थ में खिल्ली उड़ाने की प्रवृत्ति बेलगाम ढंग से बढ़ती ही जा रही है। धर्म और आस्था के संदर्भ से जनविद्वेषी बयानों (Hate Speech) की झड़ी लग जाती है, न व्यक्ति की गरिमा बचती है और न पद की प्रतिष्ठा। मीडिया के प्रभाव में झूठ और भ्रामक वाग्मिता (Misleading Rhetoric) के प्रति ‘नागरिक स्वीकृति और सहमति’ का वातावरण बना दिया गया है।
सत्ता से असहमति के निषेध और सत्ता से अनिवार्य सहमति के मासूम स्वीकार की परिस्थिति के लिए सत्ता के शिखर से मीडिया, खासकर तरंगी और तुरंगी मीडिया को शिकारी बनाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल में ही जहर घोलने जैसा काम हुआ है। अधिक स्पष्टता से समझने के लिए कुछ और नहीं तो भ्रामक विज्ञापन पर किये गये और किये जा रहे खर्चा का ही हिसाब-किताब देख लिया जाये! मीडिया आखेटित नागरिक सहमति का सब से बड़ा, लगभग अकेला खरीदार, लोकतांत्रिक सत्ता का बन जाना संवैधानिक सावधानी और अवरोध के बावजूद संवैधानिक लोकतंत्र को अंततः लोकतांत्रिक तानाशाही की तरफ ही ले जाता है।
इस बार के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अकेले दम पर साधारण बहुमत जुटा लेने की स्थिति दिन-ब-दिन कमजोर होती दिख रही है। हालांकि, इस समय सघन भ्रमाच्छादन का वातावरण तैयार करने में बहुत सारे उद्यमी लोग लगे हुए हैं। भ्रम निवारण के उपाय बहुत कम हैं। फिर भी आम नागरिकों के मन में बात उठ रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं होता है, लेकिन सब से बड़ दल बनकर वह उभरती है तो, क्या होगा? कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर दल तो है ही! क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय दल का नेता चुनेगी? क्या विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) में शामिल दल या दलों के सदस्य नरेंद्र मोदी का समर्थन करने से परहेज करेंगे? क्या किसी विपरीत परिस्थिति में विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) के लोगों की पसंद भारतीय जनता पार्टी का कोई अन्य नेता होगा? या विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) अपनी सरकार बनायेगी? राजनीतिक साहस दिखाते हुए विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़े तो महामहिम राष्ट्रपति की भूमिका कैसी होगी? अभी कुछ दिन पहले की बात है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करते समय महामहिम के खड़े रहने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी पर बैठे रहने का जो चित्र सामने आया था वह भारत राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्रपति के पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल तो नहीं था, न उसमें लोग भविष्य के शुभ संकेत पढ़ पा रहे थे।
त्रिशंकु की स्थिति में राष्ट्रीय सरकार के गठन की सुगबुगाहट शुरू हो सकती है? नहीं, नहीं इस बात की कोई संभावना कम-से-कम अभी तो नहीं दिखती है। इस बात कि भी संभावना बहुत कम है कि सब से दल के रूप में उभरने पर भारतीय जनता पार्टी मन से नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय दल का नेता चुने। धनपतियों का दबाव जरूर नरेंद्र मोदी के पक्ष में होगा। ऐसे में विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) के दल या दल के सदस्य क्या नरेंद्र मोदी का समर्थन कर देंगे! नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही मिलीजुली सरकार बने तो क्या लोकतंत्र और संविधान पर आया हुआ खतरा कम हो जायेगा?
आम नागरिकों के मन में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को और भड़काया जायेगा। फिलहाल तो यह कि विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) की सरकार बनने के ही आसार दिख रहे हैं। सत्ता परिवर्तन की स्थिति में कांग्रेस पार्टी और खासकर न्याय योद्धा राहुल गांधी से लोगों की उम्मीद जुड़ रही है, विपरीत टीका-टिप्पणियों के बावजूद! सत्ता परिवर्तन की स्थिति में क्या विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) की सरकार पर राहुल गांधी का नैतिक प्रभाव कायम हो सकता है। एक बात साफ-साफ समझ में बिठा लेने की जरूरत है कि संविधान और लोकतंत्र की भलाई इसी में है कि सब से पहले नरेंद्र मोदी के विपक्ष मुक्त भारत के अभियान और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से देश को सोद्देश्य मतदान के माध्यम से मुक्त कराया जाये। बहुत कठिन समय है। भरोसा ‘जनता जनार्दन’ के विवेक पर है। सोच-समझकर मतदान होगा। तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद जनविवेक से स्थिति में बदलाव होगा।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)