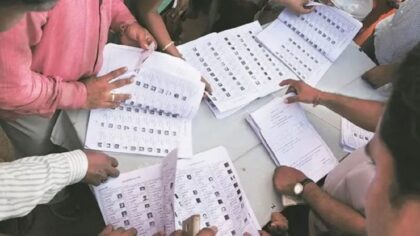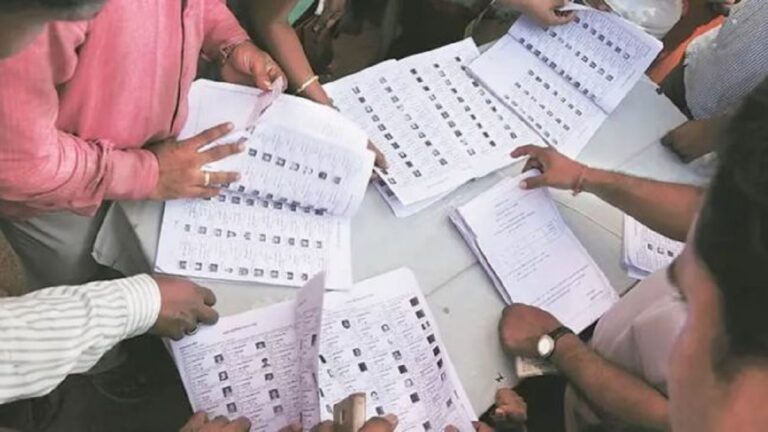“किसी लोक सेवक द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग या दुराचार, जैसे कि किसी को बयान देने के लिए धमकाना या कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश करना; आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखना; झूठे या मनगढ़ंत दस्तावेज बनाने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होना; केवल परेशान करने और धमकाने के उद्देश्य से तलाशी लेना आदि, धारा 197 दं.प्र.सं. (CrPC) के सुरक्षा कवच के तहत नहीं आ सकता।” जस्टिस पारदीवाला ने एक मामले में, जिसमें एक जांच अधिकारी के खिलाफ फैसला दिया गया, यह निर्णय सुनाया।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें एक हत्या के मामले में आरोपी को बचाने के लिए साक्ष्य में हेरफेर करने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने अपने खारिज करने के फैसले में कहा था कि पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाने से पहले धारा 197 CrPC के तहत मंजूरी लेना अनिवार्य है, जो कि नहीं ली गई थी।
हाईकोर्ट ने कानून की भाषा को शब्दशः पढ़ा, लेकिन प्रावधानों की गंभीरता और जनता के मन में कानून और व्यवस्था स्थापित करने के महत्व पर गंभीरता से विचार नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कानून की सादा भाषा से ऊपर उठकर, धारा की व्याख्या न्यायिक दृष्टिकोण से की और इसे CrPC के उद्देश्य के साथ पढ़ा। CrPC का मुख्य उद्देश्य है आपराधिक मुकदमों के संचालन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना।
इसका एक और उद्देश्य न्याय चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए पारदर्शी ढांचा सुनिश्चित करना और केवल उन्हीं आरोपियों का मुकदमा चलाना है, जो कानून की दृष्टि में दोषी सिद्ध हों।
कोर्ट ने ‘आधिकारिक कर्तव्य’ शब्द पर ध्यान केंद्रित किया और यह निर्णय लिया कि “जब कहा जाए कि किसी पुलिस अधिकारी ने झूठा मामला दर्ज किया है, तो वह यह दावा नहीं कर सकता कि धारा 197 CrPC के तहत अभियोजन की मंजूरी आवश्यक थी, क्योंकि झूठा मामला दर्ज करना और उसके लिए साक्ष्य या दस्तावेज तैयार करना किसी लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकता।”
यह पूरी घटना पुलिस या अन्य जांच अधिकारियों को कानून द्वारा प्रदान की गई छूट पर ध्यान आकर्षित करती है। पुलिस की बर्बरता और उन मामलों की संख्या में वृद्धि, जहां पुलिस ने अपने अधिकारों का उपयोग किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को दबाने के लिए किया, समाज में एक नई सामान्य स्थिति बनती जा रही है।
हमें जॉर्ज फ्लॉयड का वह अध्याय याद करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे एक अमेरिकी पुलिस अधिकारी ने ड्यूटी पर गला घोंटकर मार दिया था और जिसके कारण “ब्लैक लाइव्स मैटर” आंदोलन शुरू हुआ।
यह दिल्ली के गुरमंडी हत्याकांड का मामला था, जब एक 17 वर्षीय नाबालिग का शव उस मालिक के घर में मिला, जहां वह रोज़ काम करती थी। जब परिवार के सदस्य, कार्यकर्ता और सिविल सोसाइटी मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो पुलिस ने परिवार के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
उन्हें बेरहमी से पीटा गया और पुलिस ने उन्हें कूदने के लिए कहा। पुलिस ने उसी दिन घटना की सूचना दिए बिना शव को जला दिया। भारत ऐसी कहानियों से भरा हुआ है।
पुलिस हिरासत में शारीरिक यातना सबसे क्रूर यातनाओं में से एक है, और कानून निर्माताओं को इस वास्तविकता का गहरा अहसास था। CrPC में, पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन है। लेकिन आपराधिक प्रक्रिया में नए संशोधन ने इसे लचीला बना दिया है और अब इन 15 दिनों का उपयोग पुलिस कभी भी कर सकती है।
2019 में, पुलिस हिरासत में हुई 85 मौतों में से केवल 2.4% को पुलिस के हमले के कारण बताया गया था। हालांकि, उसी वर्ष एनजीओ प्लेटफॉर्म “नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर” द्वारा दस्तावेज़ित पुलिस हिरासत में हुई 124 मौतों में से 76% को यातना या फाउल प्ले का परिणाम बताया गया।
धारा 197 के भीतर
धारा 197(1) दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) कहती है, “जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, या ऐसा लोक सेवक है या रहा है, जिसे उसके कार्यालय से केवल सरकार की अनुमति से हटाया जा सकता है, उस पर ‘आधिकारिक कर्तव्य’ के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का दावा करते हुए किसी अपराध को करने का आरोप लगाया जाता है, तो किसी भी अदालत द्वारा उस अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लिया जा सकता, जब तक कि ‘पूर्व अनुमति’ न हो।”
यह कानून अधिकारियों को उनके विधिसम्मत कर्तव्य या आधिकारिक कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।
इसके अलावा, धारा 197(3) में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा किए गए कार्यों को भी इस अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। दिलचस्प बात यह है कि असम सरकार ने इसी धारा में एक संशोधन लाया, जिसने अन्य लोक सेवकों को भी धारा 197 के दायरे में शामिल कर दिया।
इसका मतलब है कि सरकार ने तय किया कि किसी भी प्रकार के अधिकारी, जिन्हें वे उचित समझते हैं, उन्हें धारा 197 के सुरक्षा कवच में लाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों में ‘आधिकारिक कर्तव्य’ शब्द पर गहनता से ध्यान केंद्रित किया है। हरि राम बनाम पी. बी. सूद (1956), रिज़ापलीदा बनाम असम राज्य (1992), और पृथम सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन (1987) जैसे कुछ फैसलों में अदालत ने इस कानून की संभावित परिधि को परिभाषित किया है।
शंकरराव बनाम बुर्जोर इंजीनियर (1962) के मामले में, अदालत ने आधिकारिक कर्तव्य के साथ निकटता और अविभाज्य संबंध की आवश्यकता को परिभाषित करने की कोशिश की, जो यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक तत्व हैं कि कार्रवाई आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए की गई थी या नहीं।
“धारा 197 द्वारा प्रदान की गई विशेष सुरक्षा को सख्ती से व्याख्या करनी चाहिए और जब तक अदालत के समक्ष सुरक्षा का दावा करने के लिए सामग्री प्रस्तुत न की जाए, तब तक आरोपी को सामान्य कानून द्वारा साधारण रूप से जांचा जाना चाहिए,”
बिनोद कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य के फैसले ने एफआईआर को खारिज करने का रास्ता सीमित कर दिया। लेकिन वर्तमान मामले में, जहां एमपी हाई कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया और केवल कानून की भाषा को पढ़ा।
विनोद कुमार के निर्णय में अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से सामग्री आधारों या साक्ष्य स्तर पर हेरफेर की संभावना का संकेत दिया, जिसे हाई कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया।
जब राज्य के अन्य अंग जनता के अधिकारों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका समय की आवश्यकता बन जाती है।
हाल ही में, मैं प्रोफेसर रतन लाल का एक साक्षात्कार देख रहा था, जहां उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए कहा, “अगर हम यह कल्पना करें कि वे सीधे कहेंगे कि वे संविधान में विश्वास नहीं करते, तो ऐसा नहीं होगा।
वे संविधान की बुनियादी सुरक्षा और विचार को कमजोर करेंगे और इसे अप्रासंगिक बना देंगे।” प्रोफेसर का यह कथन हर बीतते दिन के साथ सच होता जा रहा है और दुखद बात यह है कि हमारा मध्य वर्ग पुलिस राज के विचार का जश्न मना रहा है।
(निशांत आनंद कानून के छात्र हैं)