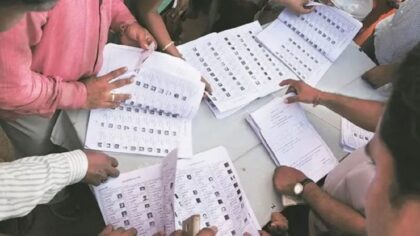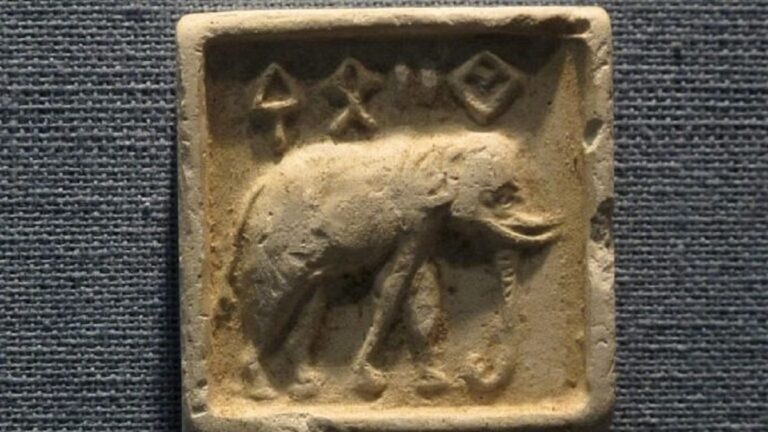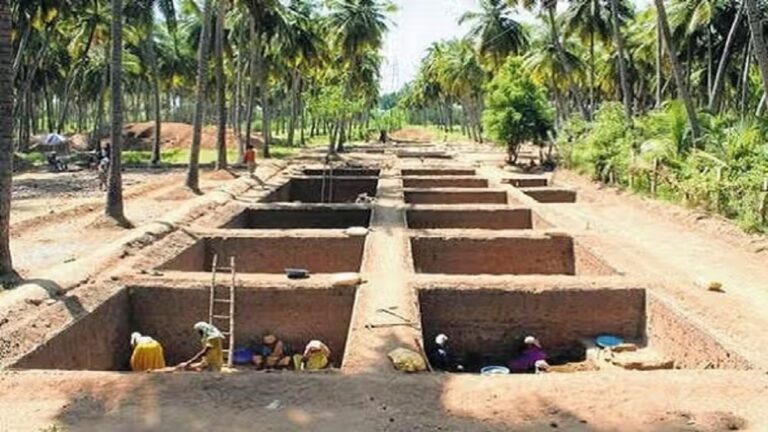अभी यह वसंत का मौसम है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए गुरुवार से लेकर शनिवार तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। इससे पहले 7-9 अप्रैल के लिए भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई थी। उस समय देश के कई अन्य हिस्सों में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की थी।
यह माना जाता है कि भारत में, खासकर उत्तर भारत में, शामें बेहद छोटी होती हैं। अब तो वसंत का मौसम भी छोटा होता जा रहा है। सर्दियों के बाद सीधे गर्मी शुरू होती दिख रही है। जब फूलों और तितलियों के मौसम में आग की चिंगारियाँ बरसने लगें, तब मौसम में आ रहे बदलाव के संकेत को जरूर समझना चाहिए।
यहाँ हीटवेव शब्द के अर्थ को देखना उपयुक्त होगा। आमतौर पर किसी क्षेत्र का ऐतिहासिक तौर पर जो सामान्य तापमान ऊपर और नीचे माना जाता है, उससे 4.5 से 6.4 डिग्री अधिक तापमान, और उसके दिनों की संख्या दो से अधिक होने पर वहाँ हीटवेव की स्थिति मानी जाती है। इससे अधिक तापमान वृद्धि को गंभीर की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन आमतौर पर सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि को हीटवेव मानने का प्रचलन अधिक है।
इस ऐतिहासिकता की माप को सामान्य तौर पर 1960-90 की अवधि के आधार पर माना गया है। हालाँकि, बहुत-सी परिभाषाएँ इससे अलग बनाई गई हैं। कुछ में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान और उसकी कुछ या कई दिनों तक बने रहने की स्थिति को हीटवेव में गिना जाता है। कुछ परिभाषाएँ इसे सामान्य से बहुत अधिक होने की स्थिति के रूप में परिभाषित करती हैं।
परिभाषाएँ जगह और क्षेत्र के हिसाब से बदलती हैं। लेकिन इस हीटवेव का जो असर इंसान पर पड़ता है, वह एक निर्णायक बात है। यह सामान्य तौर पर एक जैसा ही होता है। गर्मी होने पर पसीना निकलना एक सामान्य बात है। इससे शरीर का तंत्र खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस (टिप्पणी: मूल में 33 डिग्री गलत था, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है) होता है और इससे अधिक तापमान में शरीर खुद को उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए तरीके खोजता है।
इनमें से एक है पसीना निकलना, दूसरा है प्यास लगना, और तीसरा है क्षीण होती ऊर्जा को पाने के लिए कुछ ठंडा और तात्कालिक ऊर्जा के लिए मीठा या अन्य चीजें खाने की इच्छा होना। ये सामान्य-सी लगने वाली बातें उस समय खतरनाक स्थिति में पहुँच जाती हैं, जब तापमान असामान्य रूप से अधिक हो और शरीर की कोशिकाएँ शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए पर्याप्त पसीना न निकाल सकें।
इसका सीधा असर किडनी, श्वसन तंत्र, रक्त प्रवाह और दबाव, लीवर, और पाचन तंत्र पर पड़ता है। इस बढ़ते प्रभाव को ही हीटस्ट्रोक कहा जाता है। यह एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य पर भी इस तरह का प्रभाव डाल सकता है। लेकिन जो लोग पहले से ही बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उनके लिए यह खतरनाक साबित होता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए हीटस्ट्रोक का खतरा अधिक रहता है।
इस अप्रैल में जो हीटवेव की स्थिति बनी है, यह निश्चित रूप से प्राकृतिक विविधता में तापमान की सामान्य घटना नहीं है। पिछले साल भी भारत में असामान्य ताप की घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखी गई और यह सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया। इस वर्ष भी जो संकेत मिल रहे हैं, वे चिंताजनक हैं। पिछले साल दक्षिण और मध्य भारत के राज्य भीषण गर्मी और बाद में भारी बारिश तथा समुद्री तूफानों के शिकार बने।
इस साल हम अप्रैल के महीने में उत्तर भारत में गर्मी और पहाड़ों में होने वाली बारिश को देख रहे हैं, खासकर कश्मीर में बादल फटने की घटना सामान्य नहीं है। अप्रैल के महीने के अंतिम हफ्तों में हीटवेव की स्थिति मध्य भारत के राज्यों से लेकर ओडिशा तक बनने की संभावना अधिक है, जो बदलते मौसम के मिजाज को दर्शाता है।
कई स्रोतों और संदर्भों में मौसम विज्ञानी समुद्री हवाओं में बदलाव और धरती पर बनने वाले मौसमी चक्रों के बदलाव को चिह्नित करते दिखते हैं, लेकिन इसमें कुल कितना बदलाव आया है, इसे ठोस ढंग से पेश करना अभी भी बाकी है। हम इसके प्रभावों को देख रहे हैं और औसत के आधार पर धरती के तापमान में हुई 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को गिन रहे हैं।
पिछले साल से हुई गर्मी में अचानक वृद्धि को एल नीनो से जोड़ा गया। एल नीनो दक्षिण की ओर चलने वाली समुद्री हवाएँ हैं, जो दक्षिणी एशिया से अमेरिका, यूरोप, और अफ्रीका व एशिया के कुछ हिस्सों को प्रभावित करती हैं। ये गर्म हवाएँ हैं, जो अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक बारिश की स्थितियाँ पैदा करती हैं। ला नीना इसकी उलटी प्रक्रिया है, जिससे कम बारिश और तापमान में गिरावट देखी जाती है। अप्रैल के महीने में बनी हीटवेव की स्थिति को लेकर मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इसमें इन हवाओं की कोई भूमिका नहीं है। यह कहा जा रहा है कि इस हीटवेव के लिए मानवीय प्रभाव ही मुख्य हैं।
भारत और भारतीय उपमहाद्वीप, जिस पर प्रकृति मेहरबान रही है और जिसने सभ्यताओं को जन्म देने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जहाँ प्राकृतिक विविधताओं ने मानवीय समाज की सबसे विविध जीवन प्रणालियों को जन्म दिया, अब उन्हीं प्राकृतिक बदलावों से संकट में आ रहा है। इसमें हिमालय एक मूल जीवन प्रवाह की तरह दिखता है। इसी तरह मध्य भारत की पहाड़ी श्रृंखलाएँ धरती की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक हैं, जिनसे बने मैदानों का सिलसिला दक्षिण के समुद्री तटों से जा मिलता है।
मौसम में आ रहे बदलाव इस समूचे क्षेत्र को एक साथ प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। अब भी इन बदलावों और इससे जुड़े आँकड़ों के अध्ययन को लेकर गंभीरता का अभाव दिख रहा है। अब भी यह मान लिया जा रहा है कि यह ‘प्राकृतिक प्रकोप’ है, इसके बारे में क्या ही किया जा सकता है? जबकि सच्चाई यह है कि प्रकृति और इंसान के बीच का रिश्ता एक-दूसरे को प्रभावित करने का रहा है। निश्चित रूप से निर्णायक पक्ष प्रकृति का ही रहा है।
लेकिन जब इंसान प्रकृति पर जो प्रभाव डालता है, उसका सीधा असर उसी पर पड़ता है। यदि उसने खेती करना सीखा, तो वह एक खेतिहर समाज की ओर बढ़ा। यदि वह इसे बर्बाद करने की नीति की ओर जाएगा, तो निश्चित रूप से इसके नतीजे उससे अलग नहीं होंगे। यदि हम पिछले 20 सालों में हिमालय और मध्य भारत के हिस्सों में किए गए बदलाव और विकास के नाम पर चल रही बर्बादियों के आँकड़ों को देखें, वहाँ बसने वाले समाज की तबाही को देखें, तो हमें आज के मौसमी हालात को समझने में उतनी कठिनाई नहीं होगी, जितनी मेहनत कारणों को खोजने में की जा रही है।
कहते हैं कि मानव समाज की सबसे निर्णायक रेखा राजनीतिक रेखा होती है। यह न केवल मानवीय समाज, बल्कि धरती के अक्षांशों और देशांतरों को भी तय करती है। यही वह निर्णायक रेखा है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी और धरती पर दूरगामी प्रभावों को तय कर रही है। इस निर्णायक रेखा पर एक निर्णायक निर्णय ही प्रकृति और समाज के संबंधों तथा विकास संबंधी समस्याओं को हल करने की ओर ले जा सकता है।
हम अपने देश में एक ओर विशाल चौड़ी सड़कों को डायनासोर की तरह बढ़ते और टोल टैक्स में लोगों की आय को खाते देख रहे हैं, जबकि छोटी सड़कें दृश्य से गायब हो रही हैं। हम नदियों को जोड़ने का विशाल प्रोजेक्ट देख रहे हैं और साथ ही यह खबर भी, ठीक अप्रैल के महीने में, पढ़ रहे हैं कि जल संचयन के स्रोतों में पानी संरक्षण का प्रतिशत 45 पर आ गया है।
हम नैनीताल जैसी जगह पर, जो तालों से घिरा हुआ शहर है, पानी के आसन्न संकट की खबर पढ़ रहे हैं। हमारे शहरों की हवाओं में अब साल भर जहर घुला रहने लगा है। राजनीति में खुलेआम हिंसा और नफरत की बात होने लगी है। पूँजीपतियों के हितों के लिए पर्यावरण की बलि देना अब एक आम चलन हो गया है। ऐसे में वसंत के मौसम की उम्मीद करने का कोई अर्थ नहीं रह गया। सचमुच वसंत के वज्रनाद की आहट दिख रही है।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं)