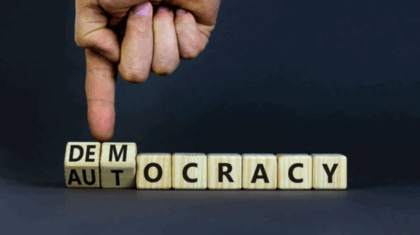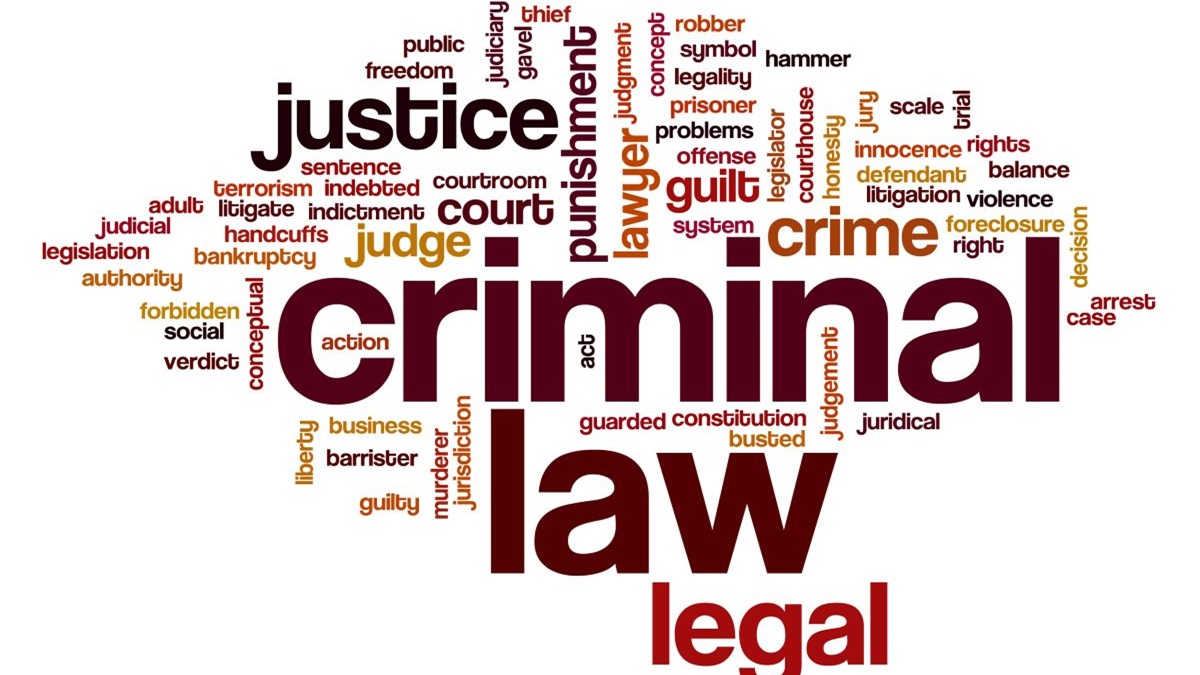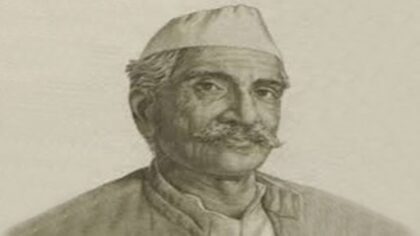दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला अपनी विशेष कानूनी प्रक्रिया और पारित आदेशों के चलते कानून जगत और आम जनता का ध्यान खींच रहा है।
आम चुनाव से एक महीने पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री की पहली बार गिरफ्तारी से लेकर, राजनीतिक प्रचार के अधिकार के अद्वितीय आधार पर उनकी रिहाई तक, इस मामले पर विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ व्यापक अकादमिक चर्चा हो रही है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के मामले को न्यायिक क्षेत्र में अलग तरीके से देखा जा रहा है जहां ED (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) द्वारा आठ सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर की गयी। इसके बाद से यह मुद्दा एक बड़े विवाद का विषय बन गया की आखिर क्या जांच एजेंसियां ट्रायल की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए लागतार नए चार्ज शीट दायर करती जा रही है।
जिसके कारण न्याय की प्रक्रिया में लगातार विलंब हो और उसका फायदा दूसरी पारी को राजनितिक रूप से मिले। धन शोधन निवारण अधिनियम (“PMLA”) की धारा 65 के तहत, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (“CrPC”) को PMLA के तहत कार्यवाही में लागू किया जाता है, जब तक कि मुकदमे के कुछ पहलुओं के लिए कोई विशेष प्रावधान न हो।
जांच चरण में, PMLA के विशेष प्रावधान मुख्य रूप से संपत्ति और व्यक्तियों की जब्ती, सर्वेक्षण, तलाशी, और गिरफ्तारी की शक्तियों को बढ़ाने पर केंद्रित हैं [धारा 16-19]।
चार्ज शीट एक प्रकार की रिपोर्ट होती है जिसे जांच एजेंसी द्वारा CrPC की धारा 173(2 ) के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। धारा 173(2) की भाषा महत्वपूर्ण है। इसमें रिपोर्ट को “जैसे ही यह पूरी हो जाती है” दाखिल करने का उल्लेख है (“यह” प्रारंभिक जांच की ओर इशारा करता है)।
धारा 173(2) और धारा 173 के शीर्षक (“जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट”) को साथ में पढ़ने से स्पष्ट होता है कि चार्जशीट केवल तभी दाखिल की जानी चाहिए जब जांच पूरी तरह समाप्त हो चुकी हो। चार्जशीट की अंतिमता पर कानून का जोर और अधिक स्पष्ट हो जाता है, जब हम धारा 167(2), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के विधायी इतिहास का विश्लेषण करते हैं।
यह धारा एक आरोपी, जिसे जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है और रिमांड पर लिया गया है, को यह अधिकार देती है कि यदि उसके रिमांड के 60 या 90 दिनों (अपराध की गंभीरता के आधार पर) के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है, तो वह डिफॉल्ट जमानत की मांग कर सकता है।
आरोपी को रिमांड पर रखने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जांच अधिकारी (IAs) अनावश्यक रूप से जांच में देरी कर आरोपी को जेल में रखने का प्रयास न करें। इसके बजाय, उन्हें एक समय सीमा दी जाएगी, जिसे पूरा न करने पर आरोपी स्वतः ही जमानत पाने का अधिकारी हो जाएगा।
41वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि 15 दिनों की “अकार्यशील” समय सीमा ने एक ऐसी प्रथा को जन्म दिया जिसकी कानूनी वैधता “संदिग्ध” थी, जहां जांच अधिकारी (IAs) नियमित रूप से प्रारंभिक या अधूरी चार्जशीट केवल आरोपी के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को बाधित करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करते थे।
इस प्रथा का समाधान करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा बढ़ाकर 60 या 90 दिन कर दी गई, ताकि “एक ऐसी प्रथा का समर्थन न किया जाए जो कानूनी सुरक्षा के उद्देश्य का उल्लंघन करती हो।” परन्तु यह प्रक्रिया हमेशा ही गंभीर अपराधों के लिए सजा के रूप में रही जहां PMLA व UAPA जैसे कानूनों में इस प्रक्रिया का प्रयोग ट्रायल की प्रक्रिया को लम्बा खींचने के लिए किया गया है।
हालिया आपराधिक प्रक्रिया संशोधन में भी यह बात निकल कर सामने आयी जहां ‘एक्सेप्शन्स’ को सामान्य रूप से लाने के प्रावधान को क़ानूनी जामा पहना दिया गया।
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की योजना के अनुसार, जांच अधिकारी (IA) को पूरी और विस्तृत जांच के बाद ही अंतिम चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। इस निर्देश की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चार्जशीट आपराधिक मामले के अगले चरणों, जैसे संज्ञान लेना और मुकदमे की प्रक्रिया में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
[सुरेश कुमार भीकमचंद जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013)]। संज्ञान लेने का चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही वह समय होता है जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेते हैं, ताकि आपराधिक प्रक्रिया शुरू की जा सके।
एक शब्द जिसे न्याय की भाषा में ‘एप्लीकेशन ऑफ़ जुडिशियल माइंड’ कहते हैं उसका प्रयोग चार्ज शीट के मामले में बेहद अहम है क्योंकि उसके बिना वाद पक्ष चार्ज शीट में जांच के नाम पर काफी विलंब कर सकता है, जिसके कारण आरोपी के मौलिक अधिकार का दमन हो सकता है।
जहां किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किये बिना ही उसे लम्बे समय तक जेल में रखा जा सकता है। उमर खालिद के मामले में या दिल्ली प्रोग्राम मामले में भी यही चीज हमें देखने को मिली जहां पर लगातार चार्ज शीट दायर करते हुए क़ानूनी प्रक्रिया को खींचने के कार्य को प्रशासनिक इकाइयों द्वारा अंजाम दिया गया।
सप्लीमेंट्री चार्ज शीट की बहस को नया तुक उस समय मिल गया जब सर्वोच्च न्यायलय ने मरियम फसीहुद्दीन मामले में कहा कि “पूरक रिपोर्ट दाखिल करने का प्रावधान इस बात का संकेत देता है कि नए मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किए जाने चाहिए, न कि जांच एजेंसी द्वारा प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट, जिसे धारा 173(2) CrPC के तहत चार्जशीट कहा जाता है, के दौरान पहले से एकत्रित और विचारित सामग्री का पुनर्मूल्यांकन या पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए।”
ऋतु छाबरिया बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज शीट दायर करने के मामले में एक अहम फैसला लिया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से जांच अधिकारियों (IAs) को अधूरी चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया था ताकि डिफॉल्ट जमानत को बाधित किया जा सके।
इस सुरक्षा प्रावधान को धारा 167 के उद्देश्य से जोड़ा गया, और इसका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि आरोपी को राज्य की असमान शक्ति के मनमाने उपयोग से बचाया जा सके। हालांकि, सरकार ने प्रक्रिया के उल्लंघन के माध्यम से इस निर्णय पर स्थगन प्राप्त कर लिया।
क्योंकि उसने IAs द्वारा सामना की गई कथित कठिनाइयों के कारण निर्णय को वापस लेने का प्रयास किया। इस निर्णय की व्यापक आलोचना की गई है, क्योंकि यह गिरफ्तार व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू को कमजोर करता है।
कई कानूनों के अंदर लगातार कानून के जानकारों ने इस बात पर जोर डाला है कि क़ानूनी प्रक्रियाओं को इस तरह से बदला जा रहा है, जिससे आपराधिक न्यायशास्त्र की मूल प्रक्रिया आम लोगों के विरुद्ध होती जा रही है।
हालांकि सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दायर करने को लेकर कोई एक समय का निर्धारण स्वयं आपराधिक प्रक्रिया कानून खुद नहीं करता पर वह अन्य प्रावधानों से उसकी सीमा और अगले स्तर के प्रक्रिया की बात स्पष्ट रूप से करता है, जिसका सीधा सम्बन्ध इससे जुड़ा हुआ है।
भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों को क़ानूनी प्रक्रिया या कानून की समझ इतनी व्यापक नहीं है वहीं लोगों के मध्य प्रशासन को लेकर एक खास प्रकार की निष्ठा उन केसेस को लेकर है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, मुस्लिम, या जाति के मुद्दे देखे जाते है।
वहां हम भी एक व्यापक मीडिया ट्रायल के शिकार हो जाते हैं और उसे ही अनुसरण करने लगते हैं। जनता की सजग भागीदारी से ही देश के अंदर एक सजग लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, जिसका एक व्यापक अभाव संविधान के बाद भी देखा जा सकता है।
(निशांत आनंद दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के छात्र हैं।)