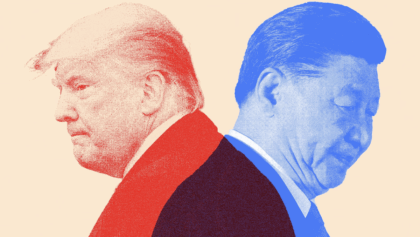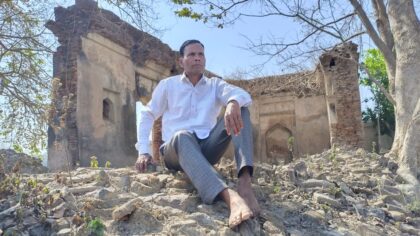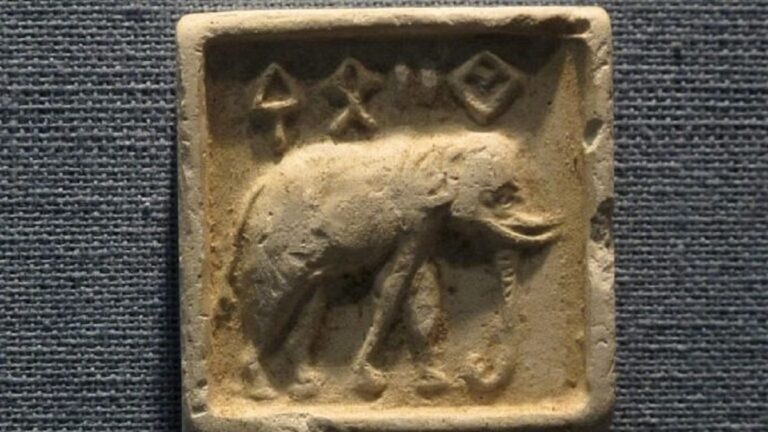नई दिल्ली। इस साल दिल्ली में जुलाई में हुई हफ्ते भर की बारिश ने सौ साल से अधिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी दिल्ली बारिश के पानी से बेहाल हो उठी। हर तरफ पानी ही पानी था। ऐतिहासिक लाल किले में बारिश का पानी भर गया। दिल्ली का केंद्र माना जाने वाला कनॉट प्लेस की दुकानों में पानी भर गया। यमुना से सटे इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। उनके घर बाढ़ में डूब रहे थे। वहीं अगस्त के महीने सामान्य से कम बारिश हुई। उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे और खुशनुमा मौसम के लिए बारिश का इंतजार करते रहे।
मानसून की दिशा पहाड़ों की तरफ ज्यादा बनी रही, जिससे हिमाचल और उत्तराखंड को भारी तबाही का सामना करना पड़ा और अभी भी पड़ रहा है। मौसम में लगातार तब्दीली और उसकी असामान्यता दिख रही है। अनुभव के आधार पर यह कहना मुश्किल होने लगा है कि इस महीने बारिश होगी और अगले महीने ज्यादा धूप रहेगी। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें, तो पिछले छह सालों में भारी बारिश के दिनों की संख्या में बढ़ोत्तरी दिख रही है। और, कुल बारिश में भी वृद्धि देखी जा रही है। आइए, इसे आंकड़ों में देखते हैं-

यहां भारी बारिश का अर्थ 64.5 मिमी से 115.5 मिमी और अत्यंत भारी बारिश का अर्थ 115.6 से 204.5 मिमी बारिश है। चरम बारिश का अर्थ 204.5 मिमी होता है, जिससे दिल्ली अभी भी बची हुई है। दिल्ली अरावली पहाड़ी पर बसा हुआ शहर है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। कभी अरावली का क्षेत्र यमुना और उसकी सहायक नदियों के बहाव से आबाद था। यमुना ने अपना रास्ता बदला और दिल्ली के पूरब उतरती चली गई। अपने पीछे इसने झीलों की एक पूरी श्रृंखला छोड़ दी, जिसकी धाराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
इस इलाके में मानसून को पहुंचने में 20 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है। साथ ही यहां पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश की भी आमद हो जाती है। इस तरह दिल्ली में औसत बारिश का फायदा मिलता है। यही कारण रहा है कि दिल्ली न बेहद सूखा इलाका है और न ही बेहद बारिश वाला। पानी के प्राकृतिक स्रोत होने की वजह से दिल्ली और आसपास का इलाका सभ्यता का केंद्र बनता गया और मध्यकाल तक आते-आते यह देश के शासन-प्रशासन की धुरी बन गया।
एक बार फिर मौसम करवट बदलते हुए दिख रहा है। ऊपर के आंकड़ों में देख सकते हैं कि पिछले तीन सालों में भारी बारिश की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिख रही है। यही स्थिति दिल्ली में बढ़ते औसत तापमान का भी है। दिल्ली में अमूमन बेहद ताप वाली गर्मी और जाड़ों में एकदम हड्डी गला देने वाली ठंड पड़ती है। दिल्ली में साल भर में औसत तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन मौसम विभाग के आंकड़े दिखा रहे हैं कि पिछले चालीस सालों में औसत तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है।
दिल्ली में सफदरजंग स्थित मौसम विभाग के आंकड़े दिखा रहे हैं इसके पूर्ववर्ती समय में औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। केवल 1997 ही ऐसा साल था जब औसत तापमान 29.66 डिग्री सेल्सियस था। 1980 से 1992 के बीच औसत तापमान 31.59 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद 2020 तक यह 32.01 हो गया। 1989 औसतन सबसे अधिक गर्म साल रहा, लेकिन आने वाले तीन सालों में तामपान में जबरदस्त गिरावट आई और यह गिरते हुए 1997 में औसतन 29.66 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था। इसके बाद की वृद्धि मध्यम स्तर पर रही लेकिन लगातर बढ़त के साथ बनी रही।
यहां एक बात ध्यान में रखी जाए कि 1990 के बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों को बंद किया गया और पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियों की जगह सीएनजी वाली गाड़ियों को लाया गया। इसी समय दिल्ली-एनसीआर में नये मेगा शहर बने और तेजी के साथ शहरी इलाकों में वृद्धि देखी गई। यदि हम केवल दिल्ली को ध्यान में रखें तो प्रदूषण से होने वाली समस्याओं में कोई खास बदलाव नहीं दिखता है। हम यहां मौसम के असामान्य होने की प्रवृत्तियों को जरूर देख सकते हैं।
दरअसल, इन्हीं वर्षों में दिल्ली एक उत्पादक शहर के बजाए एक ऐसे आरामगाह में बदलने की मशक्कत में लग गया, जो दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन जाए। वस्तुतः दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसे बेहद आकर्षक बनाया जा सकता है। यहां यमुना से छूट गई एक और नदी है, जिसने आज तक यमुना का साथ नहीं छोड़ा। यह नदी है साहबी या साबी नदी। इस शहर ने उसे बड़े नाले में बदल दिया है। यहां यमुना का विशाल पाट है, जिसके किनारे जैव विविधता से भरे हुए थे। अरावली की पहाड़ियां उसके तट को छूती थीं।
उत्तरी दिल्ली का रिज न सिर्फ यमुना का तट छूता था, वह झीलों से भरा हुआ था। एक खूबसूरत लैंडस्केप जो मजनू का टीला से शुरू होता है तो वह बढ़ते हुए करोलबाग, धौला कुंआ, मानेसर से चलते हुए जींद और अलवर से होते हुए जयपुर तक चला जाता है। दूसरी ओर यह ओखला, तुगलकाबाद से होते हुए फरीदाबाद और आगे की पहाड़ियों की ओर बढ़ता है। ये सारे ही इलाके, जो दिल्ली में पड़ते हैं- जंगल, किले, ध्वस्त ऐतिहासिक इमारतों और प्रागैतिहासिक टीलों से भरे हुए हैं।
1990 के बाद, विकास की जो हमने सरपट दौड़ देखी है, उसमें सिर्फ दिल्ली ही नहीं दिल्ली के आसपास उभरते मेगा शहरों ने अरावली की पहाड़ियों, ऐतिहासिक इमारतों और प्रागैतिहासिक मानवीय चिन्हों को रौंद डाला है। कई छोटी नदियों को इसने नष्ट कर डाला है। खुद दिल्ली में पिछले 15 सालों में 3.84 वर्ग किमी का जंगल खत्म हो गया है। दिल्ली के पास कुल 195 वर्ग किमी जंगल है जो यहां के कुल क्षेत्रफल का 13.15 प्रतिशत है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किमी है जिसका 103 वर्ग किमी नोटिफाईड जंगल के तौर पर दर्ज है।
ऊपर का आंकड़ा जंगल का क्षेत्र खत्म होने के बारे में है। पेड़ों की कटाई एक अलग मसला है। विकास कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई अलग से चलती है। मई, 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय को यहां की सरकार ने बताया कि विकास कार्यों के मद्देनजर पिछले तीन सालों में 77,000 हजार पेड़ों की कटाई हुई है। सरकार पेड़ों को बचाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कहीं और रोपने के लिए ले जाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसे पेड़ों में से तीन में से एक पेड़ ही जीवित रह पाते हैं।
पर्यावरण और पारिस्थितिकी एक स्थानीय मसला नहीं होता। लेकिन, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि स्थानीय मसलों का स्थानीय पर्यावरण और परिस्थितिकी पर असर नहीं पड़ता। दिल्ली में एक विशाल वातानुकूलित मेट्रो की व्यवस्था का दूरगामी तौर यहां के पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इसे अभी देखा जाना है लेकिन इसके लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति चाहे वह ताप घरों से संचालित संयंत्रों से हो या हाईड्रो प्रोजेक्ट से, दोनों ही अपने उत्पादक स्थल पर गहरा असर जरूर डालते हैं।
इसे हम उत्तराखंड और हिमाचल में हो रही तबाहियों में देख सकते हैं। इसे झारखंड के कोयला खदानों और नदियों पर बने बांधों से होने वाले नुकसानों में भी देख सकते हैं। एक आलीशान, आरामदायक, अनुत्पादक शहर बनाने के लिए पर्यावरण और परिस्थितिकी का नुकसान भयावह है। यहां तक कि जिस शहर को ऐसा बनाया जा रहा है, वह भी इसके भयावह नुकसान से बाहर नहीं है। दिल्ली के मौसमी आंकड़े बता रहे हैं कि यह शहर भी बढ़ते तापमान, बारिश और घटते जंगल से त्रस्त है।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं।)