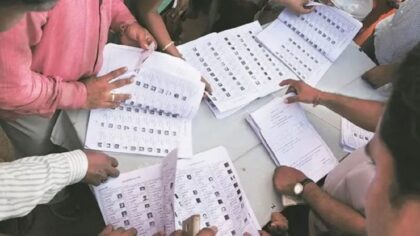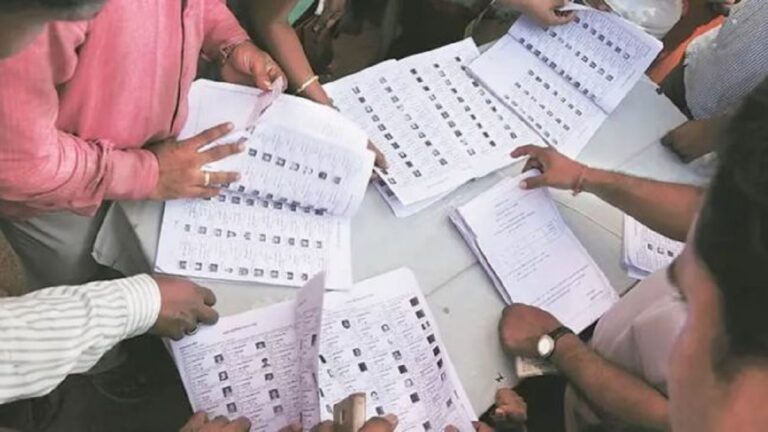आम चुनाव 2024 में सत्ता परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। यदि सचमुच सत्ता परिवर्तन होता है, तो भारत के लिए यह नवजीवन से कम नहीं होगा। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र हमें उत्तरजीविता में मिली है। इस नवजीवन को समझने के लिए पुरखों के ‘पुरुषार्थ और पराक्रम’ के प्रसंगों को याद कर लेना रीतिबद्धता की दृष्टि से नहीं लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की दृष्टि से संगत विचार है।
भारत पुराना देश और नया राष्ट्र है। इसके मूल्य-बोध में पुराचार और नवाचार की रस्साकशी चलती रहती है। इस रस्साकशी में दुराचार अपनी जगह बना लिया करता है। ध्यान देने की बात है कि सारे पुराचार आरंभ में नवाचार ही होते हैं। महत्वपूर्ण नवाचार भी कभी-न-कभी पुराचार में बदल जाता है। विडंबना है कि दुराचार का अपना घर आचार की जमीन पर बना होता है। पुराचार हो या नवाचार ये आचार की जमीन के किरायेदार ही होते हैं। किरायेदार तो आते-जाते रहते हैं। मकानदार टिका रहता है। जीवन की जमीन पर आचार-विचार की मिल्कियत के साथ-साथ पुराचार, नवाचार और दुराचार की हैसियत, रिहाइश और रिश्तेदारी को इस रूपक के माध्यम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है।
कहना न होगा कि भारत बहुत मुश्किल से नव-फासीवाद की पकड़ से निकलने की कोशिश कर रहा है। इस समय, इस कोशिश की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्ववाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सर्वसत्तावादी नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) के जनादेश प्राप्त कर लेने से मानी जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संगठन-शक्ति और वैचारिकी से समर्थित भारतीय जनता पार्टी कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं है।
राजनीतिक दल के रूप धरकर यह प्रतिक्रियावादी और हिंदू धर्म की एकल धारा को राजनीति से जोड़कर भारत के जिस राज-सत्ता का नियंत्रण करना चाहती है, उस भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर न विश्वास है, न आस्था। इस अर्थ में सत्ता की राजनीति के लिए विश्वसनीय नहीं होने के कारण साधारण और सामान्य राजनीतिक दल नहीं है।
‘अति-दक्षिणपंथ’ का मिजाज पूंजीवाद को नहीं, सामंतवाद को पसंद करता है। फासीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसकी राजनीति समाज में समानता, लोकतंत्र या सार्वभौम मानव मूल्यों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं रखती है। बल्कि कहना चाहिए कि उनके प्रति हमेशा शत्रुता, युद्ध और संघर्ष का भाव रखती है। फासीवाद इसके लिए पूंजीवाद के ही किसी-न-किसी तरह की शुद्धतावादी (Puritanism) संस्करण को साधता है। नस्लीय शुद्धता इसे सबसे उपयुक्त लगती है। भारत में नस्लीय शुद्धता इसलिए उपयुक्त नहीं ठहरती है कि इसकी वर्ण-विभक्ति नस्लीय भेद और आधारित न होकर सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पर आबादी के शोषक विभाजन और भेद-भाव को बढ़ावा दिया जाता है। भारत के ‘अति-दक्षिणपंथ’ के मिजाज को सामंतवाद और धार्मिक प्रसंग का नव-फासीवाद में अंधश्रद्धा और सनातन के नाम पर अपना आडंबर फैलाता है।
साधन और साध्य की शुचिता, संवैधानिकता, नैतिकता, तार्किक संगति, सच-झूठ से जुड़े किसी सवाल को ये अपने आस-पास भी नहीं फटकने देते हैं, इनकी सफलता का सूत्र है, ‘येन केन प्रकारेण’ यानी जैसे भी हो। कहा जा रहा है कि यह दो विचारधाराओं का संघर्ष है। संवैधानिक लोकतंत्र की किसी भी राजनीतिक विचारधारा को संविधान की परिधि के अंदर ही हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा संवैधानिक परिधि के बाहर ही अधिक सक्रिय रहती है।
भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक राष्ट्रवाद में नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में यकीन है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत प्रभावशाली और चमकीला पदबंध ही नहीं, चमत्कारी पदबंध भी है। संवैधानिक राष्ट्रवाद बहुत समझदारी भरा, समावेशी और संविधान-सम्मत बहु-सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान का महत्व समझानेवाला पदबंध है। आज की राजनीति के संदर्भ में इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को फिर से समझने की कोशिश करनी होगी।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के पीछे एलेन ओक्टेवियन ह्यूम (4 जून 1829 – 31 जुलाई 1912) की बहुत बड़ी भूमिका थी। इटावा के कलेक्टर के रूप में 1857 की ‘क्रांति’ के ताप का ए ओ ह्यूम को अनुभव था। 1587 की ‘क्रांति’ के पीछे भारतीयों की एकता की ताकत थी। अंग्रेजी राज के ‘हितैषियों’ ने भारतीयों की एकता को तोड़ने की परियोजना पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजी राज के ‘हितैषियों’ के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिंदू-मुस्लिम एकता थी। उन्होंने हिंदू-मुसलमान के बीच विभाजन की खाई बनानी शुरू कर दी।
भारत के सामने न सिर्फ हिंदू-मुसलमान की पारस्परिक एकता और जनता की गंगा-जमुनी संस्कृति को बचाने की जरूरत थी, बल्कि भारतीयों की एकता को बनाये रखने के लिए वर्ण-विभक्त हिंदूओं के बीच एकता बनाने के लिए व्यापक समाज-सुधार की भी चुनौती थी। इस चुनौती के ऐतिहासिक संदर्भ की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए महादेव गोविंद रानाडे (1842-1901) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दो साल बाद वर्ण-विभक्त हिंदुओं में समाज-सुधार के लिए (भारतीय राष्ट्रीय) सोशल कांफ्रेंस की स्थापना की। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दो वर्ष बाद हुई थी। इस सोशल कांफ्रेंस का लक्ष्य कांग्रेस के वर्ण-विभक्त हिंदुओं के सामाजिक पहलू को आगे बढ़ाना था। वर्ण-विभाजन हिंदुओं के बीच व्यापक साझापन का सबसे बड़ा रोड़ा था। ध्यान देने की बात यह भी है कि सही मायने में स्त्री-पुरुष के बीच भी व्यापक साझापन के अभाव को भी सोशल कांफ्रेंस ने गहराई से समझा। कहना न होगा कि साझापन समाज का प्राप्त और व्यक्ति के सामाजिक होने का आधार होता है।
सोशल कांफ्रेंस ने मुख्य रूप से महिलाओं के सामाजिक उत्थान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ऐतिहासिक जरूरत को पूरा करने में लगी थी। सोशल कांफ्रेंस हिंदुओं में व्यापक साझापन विकसित करने पर केंद्रित थी। कुछ समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सोशल कांफ्रेंस का सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन एक ही पंडाल में होता था। दोनों के कार्यक्रम में न सिर्फ प्रति-पूरकता थी बल्कि व्यापक साझापन भी था। यह इतना प्राकृतिक था कि इसे भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा के आकाश में उड़ान पर निकले ‘राष्ट्रीय पंछी’ के दो डैनों के रूप में समझा गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सोशल कांफ्रेंस की प्रति-पूरकता और साझापन के ‘राष्ट्रीय पंछी’ डैनों को घायल कर दिया गया। किसने घायल किया? अंग्रेजों ने? नहीं अंग्रेजों ने नहीं। फिर यह कैसे हुआ! बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी नेताओं ने सोशल कांफ्रेंस के अनुयायियों के साधारण सुधारों के प्रस्ताव का भी सख्त विरोध किया।
असल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता थे बाल गंगाधर ‘लोकमान्य’ तिलक (1865-1920)। ‘लोकमान्य’ तिलक (1865-1920) रूढ़िवादी चितपावन ब्राह्मण थे। ‘लोकमान्य’ तिलक की रूढ़िवादिता सोशल कांफ्रेंस के साझापन को न सिर्फ बिल्कुल नापसंद करते थे, बल्कि स्त्रियों और गैर-ब्राह्मणों की शिक्षा को ‘राष्ट्रीयता के लिए क्षतिकारक’ मानते थे। उनका इरादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रवाद को अति-दक्षिणपंथी विचारधारा से ‘येन केन प्रकारेण’ जोड़ना था।
‘लोकमान्य’ तिलक उस समय भी विरोध कर रहे थे जब लड़कियों, शूद्रों तथा अतिशूद्रों की शिक्षा के लिए जोतीराव गोविंदराव फुले (11अप्रैल 1827 – 28 नवंबर 1890) स्कूल स्थापित करने के काम में लगे थे। यह भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है कि महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले (3 जनवरी 1831 – 10 मार्च 1897) को शिक्षित किया और उन्हें अपने आंदोलन से जोड़ा। स्कूलों का लगातार विरोध करते रहे। महादेव गोविंद रानाडे (1842-1901) के बाद ‘लोकमान्य’ तिलक और उनके अनुयायियों का विरोध महादेव गोविंद रानाडे के सोशल कांफ्रेंस और उनके अनुयायियों पर भारी पड़ गये।
इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सोशल कांफ्रेंस का साझापन घायल हो गया। मोहनदास करमचन्द गांधी (2 अक्तूबर 1869 – 30 जनवरी 1948) ने चंपारण सत्याग्रह (1918) के अनुभवों के आलोक में इस ‘घायल साझापन’ के इलाज की जरूरत के ‘सत्य’ को तो समझा लेकिन ‘अहिंसा’ ने जरूरी ‘शल्य चिकित्सा’ की इजाजत नहीं दी और उन्होंने ‘मरहमपट्टी’ तक अपने को रोक लिया। ध्यान देने की बात है कि तब तक महात्मा फुले विदा हो चुके थे और ‘लोकमान्य’ तिलक (1865-1920) जीवित थे और उनके अनुयायियों की सक्रियता बनी हुई थी। याद किया जा सकता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने वाले डॉ केशव राव बलीराम हेडगेवार (1 अप्रैल 1889 – 21 जून 1940) का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और 27 सितम्बर 1925 को नागपुर में आज के सत्ताधारी दल, भारतीय जनता पार्टी के पितृ-संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठन किया।
भारत की चिकित्सा पद्धति में ‘शल्य चिकित्सा’ से थोड़ा दुराव का ही भाव रहा करता है। भीमराव रामजी आंबेडकर (14 अप्रैल 1891 – 6 दिसंबर 1956) की उम्र दस साल की रही होगी जब महात्मा फुले विदा हो गये। उधर दक्षिण भारत में इरोड वेंकट रामासामी पेरियार (17 सितम्बर 1879 – 24 दिसम्बर 1973) सामाजिक रूप से सक्रिय थे। पेरियार की सक्रियता का सामाजिक परिणाम प्रभावी ढंग से दक्षिण भारत में वहां के समाज में स्थापित हुआ। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सहमति-असहमति का एक पक्ष वर्ण-विभक्त हिंदू परिधि में ‘इलाज’ की मरहमपट्टी और ‘शल्य चिकित्सा’ से भी जुड़ा था। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने बहुत धैर्य से काम लिया।
इतिहास की विडंबना है कि जिस महात्मा गांधी का विश्वास मरहमपट्टी पर था, उन्हें गोली मार दी गई! जिस ‘अति-दक्षिणपंथी’ को कांग्रेस के राष्ट्रवाद की विचारधारा बाल गंगाधर ‘लोकमान्य’ तिलक बनाना चाहते थे उस ‘अति-दक्षिणपंथ’ को तो महात्मा गांधी की मरहमपट्टी भी बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम विनायक गोडसे (19 मई 1910 – 15 नवंबर 1949) ‘अति-दक्षिणपंथ’ की विचारधारा नायक रूप में प्रतिष्ठित हैं! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने भारत के संविधान बनाने की तैयारी में अपने बहुआयामी ज्ञान, अनुभव, अद्भुत तर्क-शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ‘अति-दक्षिणपंथ’ की ‘शल्य चिकित्सा’ कर दी। संविधान के संविधान सभा के द्वारा अनुमोदन और ‘हम भारत के लोगों’ के द्वारा आत्मार्पण ने ‘अति-दक्षिणपंथ’ को तिलमिलाकर रख दिया। उस समय कई लेख लिखे गये। कहा गया कि भारत के संविधान में कुछ भी ‘भारतीय’ नहीं है।
‘अति-दक्षिणपंथ’ की नजर में ‘भारतीय होने’ का अर्थ समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पिछले दस साल के स्वेच्छाचारी और सर्वसत्तावादी शासन काल में ‘अति-दक्षिणपंथ’ भारत के संविधान से ‘अ-भारतीय’ के निकास और ‘प्रबुद्ध शुद्ध भिन्न भारतीय’ के प्रावधानों के प्रवेश की कोशिश में लगा रहा है। शीघ्र ही समझ में गया कि यह सब बहुत आसानी से होनेवाला नहीं है। इसके लिए संविधान को पहले व्यवहार में नकारकर माहौल बनाना और बाद में पूरे संविधान को बदलना ही एक मात्र उपाय समझ में आया। इस सारे उथल-पुथल के मूल रहस्य को इस तरह से भी समझा जा सकता है।
आजादी के आंदोलन के दौरान रामराज की बहुत चर्चा होती रही है। रामराज के प्रति लोगों में बहुत आकर्षण रहा है। भगवान राम के कई रूप रहे हैं, जिसकी जैसी भावना। सत्ताधारी दल जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संदर्भ लेते हैं, वह गोस्वामी तुसलीदास के रामचरितमानस के राम हैं। रामचरितमानस में तुसलीदास ने रामराज का वर्णन किया है, “दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहिं काहुहि ब्यापा।।” इस रामराज का एक लक्षण है, “बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप बिषमता खोई।।” एक अन्य लक्षण है, “बरनाश्रम निज निज धरम बनिरत बेद पथ लोग। चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग।।” लक्षण और भी हैं।
जो लोग राम राज की बात करते हैं, वे विषमता पर मुंह चांपे रखते हैं! वोट की राजनीति में मानें या न मानें, लेकिन समाज में सनातन धर्म का हवाला देकर सारा जोर “बरनाश्रम” के पालन पर होता है। काम की बात यह है कि जीवन में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप (यहां ‘ताप’ का अर्थ ‘दुख’ है) अलग-अलग होते हैं। ये दुख अलग-अलग हैं, तो इनके कारण भी अलग-अलग होंगे और समाधान भी अलग-अलग होगा। इन्हें मिलाना नहीं चाहिए। धार्मिक, दैविक या आध्यात्मिक मामलों में साधना को, जीवन की भौतिक मामलों की जरूरतों को पूरा करने को अलग रखा जाना चाहिए।
लेकिन सनातन के आधार पर राज व्यवस्था चलाने की कोशिश करने वाले धार्मिक, दैविक या आध्यात्मिक का शोर मचाकर भौतिक जरूरतों को पूरा करने के अपने संवैधानिक दायित्व से हाथ झाड़ लेता है। हालांकि अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धुरफंदिया राजनीति करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते। भारत के लोगों को सनातन-सम्मत त्रेता का रामराज नहीं, संविधान-सम्मत आज की लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था चाहिए।
अभी आम चुनाव 2024 के तीन चरण अभी बाकी हैं। इस बात के संकेत हैं कि जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। चुनाव परिणाम के साथ यदि सत्ता परिवर्तन होता है, तो भी ‘अति-दक्षिणपंथ’ शांत बैठने वाला नहीं है! क्या-क्या कर सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। जिन लक्ष्यों के लिए तब महादेव गोविंद रानाडे के सोशल कांफ्रेंस, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार, डॉ राम मनोहर लोहिया और एक अर्थ में गोली-बिद्ध महात्मा गांधी की भी राजनीतिक लाइन को फिर से समझना है।
इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को ऐतिहासिक मौका मिलता है तो उन्हें गंभीरता से अपनी राजनीतिक उत्तरजीविता की ऐतिहासिकता का संदर्भ समझते हुए आत्मावलोकन और राजनीतिक साहस को अधिक सुसंगत बनाये रखने के लिए तत्पर रहना होगा। सत्ता परिवर्तन होने की स्थिति में भी ‘अति-दक्षिणपंथ’ कुर्सी के ‘ऊपर’ से भले उतर जाये कुर्सी के ‘नीचे’ अपनी कोई-न-कोई रहस्यमय जगह सुरक्षित कर ले सकता है।
सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, संवैधानिक अन्याय, युवा अन्याय, नारी अन्याय को दूर करने की कोशिश में कोताही हुई तो उसकी तार्किक परिणति की राजनीति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसलिए भारत के इस नवजीवन में सत्य, शंका, संभावना, समस्या और समाधान के संदर्भ में मजबूती, कमजोरी, अवसर और आशंका (SWOT : Strength, Weakness, Opportunity and Threat) पर चौकस सत्ता परिवर्तन होने की स्थिति में भारत के शासक वर्ग की पीढ़ी बदल जायेगी। फिलहाल बहुत उम्मीद से नई पीढ़ी का इंतजार देश को है।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)