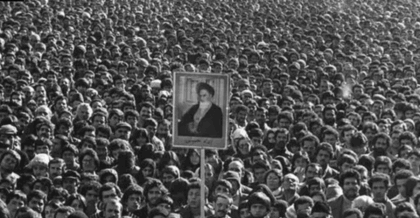“प्रजातियों का विलुप्त होना, अधिक व्यापक बीमारियां, असहनीय गर्मी, पारिस्थितिकी तंत्र का पतन, और बढ़ते समुद्रों से खतरे में शहर-ये और अन्य विनाशकारी जलवायु प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आज जन्मे बच्चे के 30 साल का होने से पहले ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे।“ जी हाँ यह मानना है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के उस रिपोर्ट का जिसे फ्रांस की एक न्यूज़ एजेंसी ने लीक करते हुए प्रकाशित किया। रिपोर्ट की मानें तो 21 वीं सदी का सही से निकल जाना भी पृथ्वीवासियों के लिए एक गहरी चुनौती बन सकती है। जहाँ पर बढ़ते तापमान और कार्बन के उत्सर्जन की बढ़ती दर ने पूरे तरीके से मानव संस्कृति को ऐसे स्थिति में ला खड़ा किया है जहाँ से वापस होना लगभग असंभव दिख रहा है।
आईपीसीसी (इंटरनेशनल पैनल ऑफ़ क्लाइमेट चेंज) ने 4000 पन्नों के अपने रिपोर्ट, जो आरोप-पत्र जैसा प्रतीत होता है जहाँ मानव के कर्त्तव्यबोध की अनदेखी का एहसास दिलाता है। हालांकि आईपीसीसी की भाषा को अगर ध्यान से देखें तो यह वही 50 साल पुराना राग अलापते नजर आया जहां उसने ‘राज्य-प्रेरित’ जलवायु परिवर्तन को ‘मानव-केंद्रित’ बता दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, जंगल और समुद्र जो हमारे लिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे बड़े हथियार हो सकते थे सब मानव संस्कृति के खिलाफ खड़े हैं। 2010-2020 में जंगल कटाई के आंकड़े बताते है कि हर साल लगभग 4.7 मिलियन हेक्टेयर जंगल की कटाई पूरे विश्व में हो रही है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वनों की कटाई जो 1990 में 384000 हेक्टेयर थी वह बढ़कर 2020 में 668400 हेक्टेयर हो गयी।
यूके स्थित यूटिलिटी बिडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले 30 वर्षों में 6,68,400 हेक्टेयर जंगल खोने के बाद वनों की कटाई की दर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ब्राज़ील और इंडोनेशिया क्रमशः पहले और तीसरे स्थान पर रहे, जिसमें ब्राज़ील ने 16,95,700 हेक्टेयर और इंडोनेशिया ने 6,50,000 हेक्टेयर वनों की कटाई दर्ज की। भारत ने 1990 से 2020 के बीच वनों की कटाई में सबसे अधिक वृद्धि के लिए भी सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसमें वनों के नुकसान में 2,84,400 हेक्टेयर का अंतर दर्ज किया गया। अर्थात यह आंकड़े लगभग दोगुने से ज्यादा हो गए है।
2021 में धरती विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने संसद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि हिन्द महासागर क्षेत्रों में तटीय इलाकों में समुद्र का स्तर प्रत्येक वर्ष 1.7 mm की दर से बढ़ रहा है। वहीं वैश्विक स्तर पर यह आंकड़े और भी डराने वाले हैं जहाँ 1901 से 2018 के मध्य समुद्र का जलस्तर 0.20 मीटर के स्टार तक बढ़ चुका है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) का कहना है कि यदि वैश्विक तापमान को किसी तरह 1.5 डिग्री सेल्सियस (औद्योगिक युग से पहले के स्तरों की तुलना में) पर सीमित कर भी दिया जाए, तब भी समुद्र का स्तर उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा। हालांकि, हर डिग्री का मामूली हिस्सा भी महत्वपूर्ण है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने वक्तव्य में बताया कि “यदि तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो समुद्र स्तर में यह वृद्धि दोगुनी हो सकती है, और तापमान में और वृद्धि के साथ समुद्र स्तर तेजी से बढ़ सकता है। किसी भी स्थिति में, बांग्लादेश, चीन, भारत और नीदरलैंड जैसे देश बड़े खतरे का सामना करेंगे।”
इन आंकड़ों के तकनीकी अन्वेषण से यह पता चलता है कि समुद्र के स्तर में उभार का सबसे बड़ा कारण थर्मल एक्सपेंसन है।थर्मल एक्सपेंशन के ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमे ग्रीन हाउस गैस को समुद्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वैज्ञानिक आंकड़ों की मानें तो पूरे ग्रीन हाउस गैस के अवशोषण का 90 प्रतिशत समुद्र में जाता है जिससे उसके हीट सेक्वेस्ट्रेशन की क्षमता में और इजाफा होता है। वही अन्य कारणों में ग्लेशियर के लगभग 40 % तक का इजाफा दर्ज किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस से यह दोनों ही प्रक्रियाओं में तेजी से इजाफा हुआ है।
असमान आर्थिक दशा जिस पर सबसे कम चर्चा है
दिलचस्प बात यह है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भी वैश्विक स्तर पर उच्च उत्सर्जक हैं, और समृद्ध देशों में वैश्विक स्तर पर निम्न उत्सर्जक पाए जाते हैं। अनुमानित रूप से, उत्तर अमेरिका में सबसे अमीर दस प्रतिशत लोग दुनिया के सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जक हैं, जो प्रति व्यक्ति औसतन 73 टन कार्बन उत्सर्जन करते हैं। यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की गरीब आधी आबादी के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से 73 गुना अधिक है।
पूर्वी एशिया के धनी लोग भी बहुत अधिक उत्सर्जन करते हैं, हालांकि यह उत्तर अमेरिका की तुलना में काफी कम है। परन्तु इसपर किसी भी पर्यावरण सम्मेलन में सबसे काम चर्चा हो रही है, जिसका एक सीधा आंकड़ा इस बात से निकला जा सकता है जहां वैश्विक स्तर पर फासीवादी ताकतों का उभर हुआ है, जो खुले तौर पर पूंजीपतियों की इच्छा के अनुसार अपने नियमों और कानूनों को ढलते हैं।
वैश्विक जगत में साम्राज्यवाद के एकाधिकारी प्रवृत्ति से गुजरने के कारण पैसे कुछ हाथों में सिमट रहे हैं। 1970 के बाद से जो इस प्रक्रिया में तेजी वैश्विक स्तर पर देखी गयी उसे भारतीय उपमहादेश में 1980 के दशक के आखिरी से महसूस किया जाने लगा। जिसके बाद इस प्रक्रिया में लगातार वृद्धि ही देखी गयी है। इसीलिए तमाम पर्यावरण सम्मेलनों में उछाले जा रहे ‘समावेशी विकास’ के जुमले के निहितार्थ की भी पर्दाफाश करने की जरूरत है। जहां आदिवासी जनता के ‘मेन स्ट्रीमिंग’ के चक्कर में उनके संसाधनों से न केवल दूर किया जा रहा है अपितु समावेशन के नाम पर उनकी संस्कृतियों को भी खुद के अंदर शामिल किया जा रहा है।
न्यायिक क्षेत्र को बिल्कुल भी इस साम्राज्यवादी अभियान से दूर रखने की आवश्यकता नहीं है। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनते हुए यह घोषणा की कि समाज के सभी निजी संपत्ति को सरकार सार्वजनिक महत्व की संपत्ति नहीं बना सकती है। जिससे एक बात स्पष्ट है कि सरकार सभी संपत्ति को अपने अधीनस्थ नहीं कर सकती है।परन्तु सम्पत्तियों के अधिग्रहण के इतिहास को अगर देखें तो यह हमेशा ही गरीब और माध्यम किसान के हित में न होकर बड़े पूंजीपतियों के हित में रही है। जैसे कभी भी भूमि सुधार को लागू नहीं किया गया पर अभी अधिग्रहण देश में लैंड-बैंक बनाने की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है।
परन्तु न्यायालय ने इस फैसले में एक महत्वपूर्ण बात कही जिस पर मैं अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जहां माननीय न्यायालय ने बताया कि भारत का संविधान किसी आर्थिक नीति को अंतिम लक्ष्य मानके नहीं चलता है। अगर भारत की आर्थिक नीति में बदलाव है तो विधि निर्माण और न्यायिक संकल्पना भी उसी तरह से होनी चाहिए। परन्तु क्या न्यायालय के संज्ञान में यह बात नहीं है कि नयी आर्थिक नीति के कारण देश में लगातार विषमताएं बढ़ी है। अगर न्यायालय खुद को कंपन्सेशन दिलाने तक ही सीमित कर देगा तो यह सच है कि देश के नागरिकों के मूल अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार महज कागजों में सिमट के रह जाएंगे।
परन्तु न्यायालय के इस निर्णय ने मार्क्स के एक बात को बिलकुल सार्थक साबित कर दिया जहां कार्ल मार्क्स यह कहता है कि किसी भी उत्पादन सम्बन्ध में समस्त सुपर स्ट्रक्चर (ऊपरी ढांचा) आधार को संरक्षण प्रदान करता है। पर्यावरण और मानवाधिकार के मुद्दों पर न्यायालयों को खुद को आवश्यक रुप से जुडिशल एक्टिविज्म दिखाना चाहिए क्योंकि यहां पर ‘सक्रिय न्यायपालिका’ ही एक बेहतर नागरिक केंद्रित और भविष्य को संरक्षित करने वाले युक्तियुक्त लेने सक्षम जान पद सकता है।
(निशांत आनंद दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के छात्र हैं)