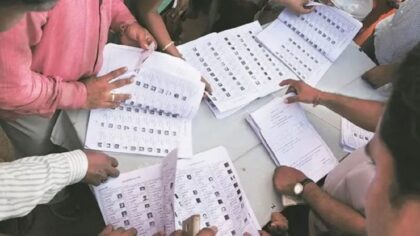जाने-अनजाने नरेंद्र मोदी के दस साल के शासन काल को भारत की राजनीति में नकारात्मक प्रभाव के लिए बहुत याद किया जायेगा। कहा जाता है कि नकार और सकार एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। एक को नियंत्रित करके दूसरे को आगे बढ़ाने की सचेत प्रक्रिया अपनाई जाती है।
आगे बढ़ने में किसे नियंत्रित किया जाता है और किसे खुली छूट दी जाती है, इससे नकारात्मकता या सकारात्मकता की गतिमयता बनती है। कहना न होगा कि नरेंद्र मोदी के दस साल के शासन काल में नकारात्मकता के कई उदाहरण, बिना खोजे ही मिल जायेंगे।
नरेंद्र मोदी के शासन काल को तकनीकी एवं अन्य कारणों से भले ही भारतीय जनता पार्टी का शासन काल कहा जाये, लेकिन व्यावहारिक अर्थ में इसे नरेंद्र मोदी का शासन काल ही कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए। कहने में कुछ जोड़ना ही हो तो इसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में कॉरपोरेट का शासन काल कहा जा सकता है।
फिर भी किसी गंभीर विश्लेषण में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के रूप में ही इस विलक्षण दौर को चिह्नित किया जाना चाहिए। मुश्किल यह है कि न राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ चुनाव लड़कर जनता के प्रति उत्तर-दायी होता है और न कॉरपोरेट ही उस अर्थ में जनता के प्रति उत्तरदायी ठहरता है।
बची भारतीय जनता पार्टी, तो उसने अपने भाग-सोहाग को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के कर-कमलों में ही सौंप दिया था। भारतीय जनता पार्टी तो ‘मोदीमय’ हो गई और मीडिया-जनित आत्म-मुग्धता में निश्चिंत हो गई कि पूरा भारत भी उसी की तरह से ‘मोदीमय’ हो चुका है! 2024 ने बहुमत-विहीन करते हुए इस भ्रम को बुरी तरह से तोड़ दिया।
लोकतांत्रिक भारत के दस साल के इस शासन काल में चुनावी तानाशाही भारत को थोड़ा हिला-डुलाकर देख गई है। कहा जाता है कि हृदय रोगियों को लगनेवाले आघात को लोग गिनते रहते हैं। दो बार के ऐसे आघात के बाद हितैषियों की जमात को बड़ा संकेत मिल जाता है।
भारत के लोकतंत्र को दो-दो बार ‘चुनावी तानाशाही’ का आघात लग चुका है। इसके पहले इंदिरा गांधी के शासन काल में घोषित 1975-77 के आंतरिक इमरजेंसी की ‘चुनावी तानाशाही’ के दौर को याद किया जा सकता है।
इंदिरा गांधी के शासन काल में घोषित इमरजेंसी की ‘चुनावी तानाशाही’ की अवधि दो साल से भी कम की थी। 2014 से शुरू हुए नरेंद्र मोदी के शासन काल में अघोषित होने पर भी ‘चुनावी तानाशाही’ का रंग-रूप घोषित इमरजेंसी से कम खतरनाक नहीं रहा, बल्कि कहा जा सकता है कि कुछ अधिक ही भयावह रहा।
पचास साल से कम की अवधि में दो-दो ‘चुनावी तानाशाही’ का भारत में दस्तक देना कोई साधारण बात नहीं है। नरेंद्र मोदी के शासन काल का एक ‘निकृष्ट किंतु सकारात्मक’ पहलू यह है कि इसने भारत के लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति का एहसास करा दिया है।
अब यह नागरिक समाज का दायित्व है कि वह इस ‘नायाब एहसास’ को समय रहते सावधानी से समझने की कोशिश करे।
इंदिरा गांधी की सत्ता को संसद के अंदर विपक्षी राजनीतिक दलों से कोई खतरा नहीं था। बल्कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा अयोग्य ठहरा दिये जाने के फैसले के बाद, सड़क पर तेज हो गई राजनीतिक गतिविधियों के बीच असली खतरा कुछ देर के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं से पैदा हो गया था।
तमाम तरह की आशंकाओं से घिरी इंदिरा गांधी, उन खतरों से मुकाबला के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं से अधिक न्यायिक प्रक्रिया पर ही भरोसा कर पा रही थी।
उच्चतम न्यायालय ने 24 जून 1975 को उच्च-न्यायालय के अयोग्यता संबंधी फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन एक दिन बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी।
‘आंतरिक गड़बड़ियों’ के चलते देश की सुरक्षा के खतरा को आपातकाल की घोषणा का आधार बनाया गया। कुल जमा यह कि अंततः विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने देश पर आंतरिक आपातकाल थोप दिया।
इस ‘विपरीत राजनीतिक परिस्थिति’ और ‘राजनीतिक प्रबंधन’ की विफलता पर पक्ष-विपक्ष में ढेर सारे तर्क-वितर्क किये जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद हर किसी को यह तो मानना ही होगा कि भारत के लोकतंत्र के मुख्य द्वार तक ‘चुनावी तानाशाही’ का खतरा तो पहुंच ही गया था!
ऊपर से ‘शांत’ दिख रहे राजनीतिक परिवेश और अन्य कारणों से इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव का ऐलान कर दिया। अवसर मिलते ही भारत के मतदाता समाज ने ‘चुनावी तानाशाही’ के खतरे को चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त कर दिया।
‘चुनावी तानाशाही’ के खतरे का ‘चुनावी प्रक्रिया’ से समाप्त होना दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में विरल घटना है। हालांकि यह तभी संभव हो सका था, जब ‘चुनावी प्रक्रिया’ संस्थागत दूषण से मुक्त थी।
1977 की चुनावी हार के बाद इंदिरा गांधी संजय गांधी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी।
संजय गांधी को विपक्षी शासन से तो उस तरह का कोई ‘खतरा’ नहीं हुआ जिसको लेकर इंदिरा गांधी चिंतित थी। बल्कि तत्कालीन सत्तारूढ़ दल की सत्ता-राजनीति के आंतरिक कलह के कारण बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में संजय गांधी राजनीतिक तौर पर इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के लिए बेहतर उपकरण साबित हुए।
एक हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु ने देश की राजनीति का पूरा परिदृश्य ही बदलकर रख दिया।
1977 में चुनावी हार के बाद ऐसी काना-फूसी भी सुनी गई थी कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी अपने बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ भारत छोड़कर इटली जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राजीव गांधी अपने परिवार के साथ भारत में ही बने रहे।
न सिर्फ बने रहे बल्कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद हुए आम चुनाव में भारत के संसद के अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सांसदों के समर्थन से चलनेवाली सरकार के मुखिया बने।
विपरीत राजनीतिक परिस्थिति में बहुमत हासिल न कर पाये और विपक्ष में बैठने का फैसला किया। यहां से भारत की राजनीति में भारी उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया। फिर आम चुनाव के दौरान ही 21 मई 1991 को राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। यह ‘गांधी परिवार’ में लगातार दूसरी पीढ़ी की शहादत थी।
राजीव गांधी के परिवार सहित भारत छोड़कर इटली जाने की काना-फूसी के 16 साल के अंदर राजीव गांधी की हत्या हो जाना श्रीमती सोनिया गांधी के लिए कितना बड़ा हादसा रहा होगा इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। इस बीच ‘गांधी परिवार’ सत्ता से दूर, बिल्कुल दूर-दूर रहा।
‘गांधी परिवार’ भी क्या कहा जाये! पूर्ण रूप से भारतीय हो चुकी विदेशी मूल की श्रीमती सोनिया गांधी ने सास और पति की हत्या के बाद किस तरह से अपने बच्चों को संभाला होगा, ये वही जानती हैं। राजीव गांधी की हत्या के तेरह साल बाद 2004 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी को चुनाव में पराजित कर सोनिया गांधी सत्ता के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई!
विपक्ष के नेताओं के प्रत्यक्ष विरोध असहमत नेताओं के तमाम हो-हल्ला के बाद भी सोनिया गांधी के पास खुद भारत के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ दिख रहा था। रास्ता साफ दिख रहा था, मगर साफ था नहीं। प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह बने।
सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनीं! इसलिए नहीं बनी कि दादी और पिता की हत्या के दर्द के तूफान से रूबरू राहुल गांधी अपनी मां की जान को खतरे में डालने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं हुए। बच्चों के हित और जिद में मां के त्याग और बलिदान की कहानियां दुनिया में कई होंगी।
लेकिन दुनिया के सब से बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने के अवसर के त्याग का ऐसा उदाहरण शायद ही कोई दूसरा हो! आज घोषित इमरजेंसी के जून 2025 में पचास पूरा होने पर ‘संविधान हत्या दिवस’ मनाने की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी को यह ध्यान होना चाहिए कि जिस राहुल गांधी ने 2004 में अपनी मां को भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोक लिया था, उसी राहुल गांधी को आज भारत के अवश्यंभावी प्रधानमंत्री के रूप में देखनेवालों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है।
आम चुनाव 2024 के नतीजों के विचारधारात्मक आघात से राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और बहुमत से वंचित भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमात की समझ में नहीं आ रहा कि इस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का करें तो, क्या करें।
इतिहास का अनुभव बताता है कि शक्ति के नाश का विष शक्ति की नाभि में ही रहता है, भले ही घमंड में चूर शक्तिवान उस विष को अपने अंत समय तक अमृत ही समझता रह जाये! ‘अमृत महोत्सव’ में उलझा रह जाये! भारत की संस्कृति में नाभि में अमृत बसाये रावण से बड़ा कोई अन्य उदाहरण नहीं है।
राम स्वर्ण-सत्ता के घमंड को चूर करने में कामयाब होने के कारण निर्बल के बल हो गये। विडंबना यह कि ‘इधर के राम भक्त’ सत्ता के घमंड में दिन को दिन और रात को रात समझने का विवेक ही गंवा बैठे। ‘घमंड में चूर’ का घमंड अंततः चूर-चूर हो ही जाता है।
सावधानी के अंतर्गत सब से पहले 1975-77 के दौर की राजनीतिक पृष्ठ-भूमि और शासकीय अनुभवों को भी याद कर लेना चाहिए।
आजादी के आंदोलन के दौर में भी दक्षिण-पंथी राजनीति कोई कम सक्रिय नहीं थी। भले ही उस की सक्रियता आंदोलन की मूल आकांक्षा की विपरीत दिशा में थी, मगर थी। संविधान बनने के समय भी वह व्यापक भारत बोध के खिलाफ सक्रिय थी।
उनका विचार और बोध आत्मसातीकरण की दीर्घकालिक प्रक्रिया में बनते चले गये मिलनसार गंगा-जमुनी भारत-बोध के विरुद्ध और भेद-भावमूलक तथा उच्च-कुल-शील अनुकूल था। अपनी तमाम सक्रियता के बावजूद दक्षिण-पंथ भारत-बोध के आधुनिक और समतामूलक संवैधानिक प्रसंग की राह में रोड़ा न अटका सका।
उस समय कांग्रेस और ‘देश बनानेवाले’ नेताओं ने दक्षिण-पंथ विचार से टकराव में गये बिना आगे बढ़ने का फैसला किया था। उन्हें उम्मीद थी कि धीरे-धीरे दक्षिण-पंथ संविधान की अनुकूलता में अपना परिप्रेक्ष्य सही कर लेगा। मगर इतिहास ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ।
भारत में दक्षिण-पंथ का शिरोमणि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ से निर्णायक विचारधारात्मक संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी से निर्णायक चुनावी संघर्ष की घड़ी आ गई है।
पुराने राजघरानों के वंशधर और नये कॉरपोरेट घराने के सूत्रधार स्पष्ट कारणों से इस संघर्ष में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही अनुकूल रहते हैं। लेकिन यह अनुकूलता तभी तक रहती है, जब तक मतदाता समाज अपने ही विरुद्ध अपने को इस्तेमाल किये जाने की निकृष्ट राजनीति की रणनीति के विरोध में सक्रिय नहीं होता है।
इस समय दक्षिण-पंथ यानी राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने-अपने अहं और अस्तित्व की रक्षा के लिए आंतरिक संघर्ष और घात-प्रतिघात में लगे हुए हैं। माना जा सकता है कि 2024 के आम चुनाव के नतीजे ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए दक्षिण-पंथ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का अवसर समतामूलक राजनीतिक दलों को दिया है।
यहां से भारत की राजनीति निर्णायक लोकतंत्र की नई यात्रा पर निकल पड़ी है। निर्णायक लोकतंत्र की राजनीति का रास्ता जनांदोलन और जनसंघर्ष से तय होता है, महज चुनाव से नहीं! निर्णायक लोकतंत्र की राह में कांटे ही नहीं माया के मोहक वन भी हैं। वन को उपवन समझने की भूल घातक हो सकती है।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)