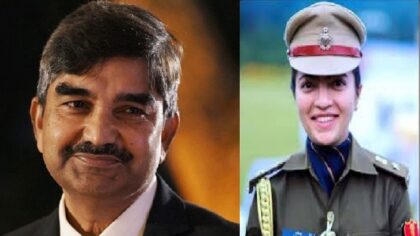मुस्लिम महिलाएं लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानूनों के पक्ष में हैं, पर मुस्लिम महिला समूह जानते हैं कि महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ और हर उस शै, जो मुस्लिम है, का खलनायकीकरण करने वाली राजनीति से भी भिड़ना होगा।
आगामी एक साल में होने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक आज़माए नुस्खे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मुद्दा उछाला है। लगे हाथ 22वें न्यायिक आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर धार्मिक और अन्य संस्थाओं से यूसीसी पर विचार आमंत्रित किए हैं। टिप्पणियां या सुझाव देने के लिए कोई मसौदा साझा नहीं किया गया है, इससे समझा जा सकता है कि यह अधिसूचना केवल लोगों को यह याद दिलाने के लिए है कि केवल भाजपा ही है जो भारतीय मुस्लिमों को “धर्मनिरपेक्ष कानून को मानने वाले नागरिक” बना सकती है।
21वें न्यायिक आयोग ने 2018 में पारिवारिक कानून के सुधारों पर 185 पृष्ठों के अपने परामर्श पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि “आज की तारीख में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है।” इसके बावजूद, पांच वर्ष बाद, यह अधिसूचना हमारे सामने आई है। इस कदम के पीछे अवसरवादी राजनीति को पहचानने के बावजूद मेरा कहना है कि प्रगतिशील समूहों, मुस्लिम और नारीवादी, जो लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानूनों की वकालत करते रहे हैं, को इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
पारिवारिक कानून में सुधार
भारत में हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन हिन्दू कानून से शासित हैं जबकि पारसी, ईसाई और मुस्लिमों के अपने निजी कानून हैं जो उनके धार्मिक कथनों पर या उन कथनों की समझ पर आधारित हैं। पारिवारिक कानून के रूप में जाने जाने वाले इन कानूनों में शादी, तलाक, बच्चों की कस्टडी और उत्तराधिकार के मुद्दे शामिल हैं। जिन्हें आज हम पर्सनल लॉ कहते हैं, अंग्रेजी शासन में बने थे।
मुस्लिम, हिन्दू, ईसाई, पारसी या आदिवासी, हर समुदाय से महिलाओं ने कभी न कभी अपने समुदाय में भेदभावकारी निजी कानूनों को चुनौती दी है या समाधान के लिए अदालतों की राह पकड़ी है।
संविधान सभा ने देश के शासन के लिए आवश्यक कई कानूनों पर चर्चा की। इनमें शादी और उत्तराधिकार से संबंधित पारिवारिक कानून भी शामिल थे। माना जाता है कि ऐसे समय में जब विभाजन की यादें ताजा थीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव एक मुश्किल कार्य रहा होगा। संविधान में स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में यूसीसी जो जोड़ा गया इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में यह बनाया जाएगा जबकि हिंदुओं, जो बहुसंख्या में थे, के लिए सुधार हिन्दू कोड बिल के जरिए बनाए गए।
मुस्लिम, हिन्दू, ईसाई, पारसी या आदिवासी, हर समुदाय से महिलाओं ने कभी न कभी अपने समुदाय में भेदभावकारी निजी कानूनों को चुनौती दी है या समाधान के लिए अदालतों की राह पकड़ी है। इन संघर्षों के साथ महिलाओं को पारिवारिक संस्था को भी चुनौती देनी पड़ी है जबकि अक्सर हमारे देश की महिलाओं का यह एकमात्र सहारा होता है। कानून और रीति-रिवाजों में समान अधिकार प्राप्त करने की औरतों की लड़ाई लंबी और कठिन रही है।
जब बालिका वधू रुखमाबाई, ने 1885 में बाल विवाह को चुनौती दी, बाल विवाह अधिनियम में सुधार के विरोधियों में एक राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक भी थे। मैरी रॉय को केरल के सीरियन ईसाई समुदाय में उत्तराधिकार कानूनों में अपने भाइयों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ लड़ना पड़ा था। शाह बानो को अपने पूर्व शौहर और पांच बच्चों के पिता को अदालत में खींचना पड़ा जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर विवादास्पद (लेकिन आवश्यक) चर्चा और बहस शुरू हुई।
गूलरुख गुप्ता ने वलसाड पारसी पंचायत को उसके उस फैसले के खिलाफ अदालत में खींचा जिसके तहत गैर पारसी पुरुषों से विवाह करने वाली महिलाओं को अपने अभिभावकों की अन्त्येष्टि में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। बिहार में हो महिलाओं और महाराष्ट्र में आदिवासी महिलाओं ने अपनी सामुदायिक पंचायतों के खिलाफ क्रमश: संपत्ति और यौनिकता के अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ी है।
बहुसंख्यक होने के बावजूद हिन्दू कोड बिल के जरिए सुधारों को हिन्दू परंपरावादियों ने चुनौती दी थी उनका बिल में कई प्रावधानों से विरोध था। बीआर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित प्रस्तावित बिल पहले आम चुनावों से एन पहले छोड़ दिया गया।
कई वर्षों के विचार-विमर्श के बाद जवाहरलाल नेहरू, हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू नाबालिक और सरंक्षण अधिनियम और हिन्दू दत्तक एवं गुज़ारा भत्ता अधिनियम, 1955-56 में टुकड़ों में पारित कराने में सफल हुए। 2005 में जाकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद हिन्दू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला।
यह लगना स्वाभाविक है कि लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले समान कानून सभी के लिए बेहतर हैं। लेकिन 1985 में शाह बानो निर्णय के बाद बिगड़े माहौल में, पर्सनल लॉ में किसी भी सुधार की मांग को अल्पसंख्यक विरोधी माना जाने लगा है।
एक तरफ, अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक नेताओं ने निजी कानून बनाए रखने के अपने “अधिकार” पर जोर देना शुरू किया और दूसरी तरफ संघ परिवार जैसे हिन्दू दक्षिणपंथी समूहों ने “यूसीसी” का इस्तेमाल अपने अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे को बढ़ाने के लिए करना शुरू किया।
यह भी चिंता थी ही कि समान कानून जरूरी नहीं कि लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाला हो। इसलिए, कुछ महिला समूहों ने हिन्दू दक्षिणपंथियों की अवस्थिति से खुद को अलग करने के लिए “यूसीसी” शब्द को त्यागकर समानधिकारवादी नागरिक संहिता या लैंगिक आधार पर भेदभाव रहित न्यायपूर्ण कानूनों के पक्ष में कानून में लैंगिक न्याय और सुधारों की मांग जारी रखी। (गांधी, गंगोली और शाह 1996)
लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानूनों के लिए संघर्ष
मुस्लिम यूसीसी के खिलाफ हैं, यह मिथक मुस्लिम और हिन्दू, दोनों समुदायों के दक्षिणपंथी तत्वों के राजनीतिक हितों के अनुकूल है। मुस्लिम लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानूनों के पक्ष में हैं और मानते हैं कि कोई एक धर्म सभी महिलाओं को न्याय नहीं दे सकता। मुस्लिम महिलाओं की तरफ से लगातार निजी कानूनों को चुनौती देने का प्रयास करना इसका प्रमाण है। साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि मुस्लिम महिलायें भी मुस्लिम समुदाय की ही सदस्य हैं।
1978 में शाह बानो ने अपने वकील पति से गुज़ारा भत्ता मांगते हुए याचिका दाखिल की। पति, जो निजी कानूनों की अच्छी जानकारी रखता था, ने उसे तलाक देने का फैसला किया और इद्दत की अवधि के बाद गुज़ारा भत्ता देने से मना कर दिया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उन्हें राहत दी लेकिन इसका परंपरावादी मुस्लिमों ने विरोध किया जो मानते थे कि अदालत ने शरीयत कानून में हस्तक्षेप किया है।
1983 में, शहनाज़ शेख, जिन्होंने बाद में महिलाओं की संस्था आवाज़-ए-निसवां शुरू की, ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के कई प्रावधानों के खिलाफ याचिका दाखिल की। 1999 में देश भर में मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्य करने वाले महिला समूहों ने मुस्लिम वुमन’स राइट्स नेटवर्क की स्थापना की। मुस्लिम पर्सनल लॉ के सुधारों के लिए इसका निम्नलिखित चार सूत्रीय एजेंडा था:
• तीन तलाक पर प्रतिबंध
• बहुविवाह पर प्रतिबंध
• मुस्लिम महिलाओं के लिए समान संरक्षण और कस्टडी अधिकार
• मुस्लिम महिलाओं के गुज़ारा भत्ता अधिकार
बाद में नेटवर्क की चर्चाओं में उनके एजेंडा में समान उत्तराधिकार अधिकार भी जोड़े गए।
धार्मिक ढांचे में रहकर कानून में असमानता को सुलझाने के कार्य के प्रयास के अलावा मुस्लिम वुमन’स राइट्स नेटवर्क ने नारीवादी समूहों के साथ मिलकर अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ को चुनौती देने के बारे में कानूनी सलाह भी ली।
2004 में नेटवर्क के कुछ सदस्यों ने लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाला एक निकाहनामा बनाने की दिशा में प्रयास किए थे, जिसमें विवाह की शर्तें, मेहर (विवाह के समय पत्नी को पति की तरफ से दी जाने वाली चीजें या रकम), तलाक और तलाक के बाद अधिकार शामिल थे। इस निकाहनामे ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी, जो है तो एक गैर सरकारी संस्था पर अक्सर मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारी संस्था मानी जाती है) को अपना निकाहनामा बनाने पर मजबूर किया, जिसमें तलाक के लिए भी शर्तें स्पष्ट की गई थीं।
एआईएमपीएलबी के इस महिला विरोधी निकाहनामे के मसौदे की मुस्लिम महिलाओं ने आलोचना की थी, 2005 में एक संवाददाता सम्मेलन में एआईएमपीएलबी को स्त्रीद्वेषी संस्था, जो मुस्लिमों की प्रतिनिधि नहीं थी, करार देते हुए इसकी प्रति फाड़ी थी।
2007 में कुछ मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों को लेकर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) बनाया। इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोडीफिकेशन था, इस्लाम के नाम पर अनुचित रीतियों को त्यागना था। जब शायरा बानो ने अदालत में अपने तीन तलाक को चुनौती दी, बीएमएमए, बेबाक कलेक्टिव (मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करने हेतु 2013 में गठित) और अन्य संस्थाएं याचिका में शामिल हो गईं, जिसकी परिणिती 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 में हुई। बीएमएमए ने कई बार कोडीफाइड मुस्लिम फैमिली लॉ का मसौदा सरकार को दिया है पर कोई प्रतिसाद नहीं मिला।
मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी, जो 2003 में बना था, 2016 में इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी बना। वह भी मुस्लिम रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है और कर्नाटक में पिछले साल हिजाब विवाद समेत कई विवादग्रस्त मुद्दों पर सार्वजनिक रुख अपनाया है।
देश भर में नारीवादी नजरिए से मुस्लिम महिलाओं के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्य करने वाले कई संगठन हैं। यह समूह नारीवादी संगठनों के साथ मिलकर अनुचित कानूनों को चुनौती देते रहे हैं और लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानून प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते रहे हैं।
मुंबई के फोरम अगेन्स्ट अप्रेशन ऑफ वुमन (एफएओडब्ल्यू) विवाह, तलाक और उत्तराधिकार समेत कई मुद्दों पर 1995 में लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले विधेयकों का प्रस्ताव दिया। एफएओडब्ल्यू ने सामाजिक सुरक्षा और असमलैंगिक तथा समलैंगिक रिश्तों में महिलाओं के अधिकार बढ़ाने के लिए कानूनों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
महिला समूहों ने ‘धर्मनिरपेक्ष’ विशेष विवाह अधिनियम में भी आवश्यक बदलाव सुझाए हैं। उन्होंने लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानूनों के कई मसौदे बनाए हैं और जब भी यूसीसी का मामला उठाया जाता रहा है, न्यायिक आयोग को सुझाव दिए हैं।
लैंगिक न्याय चाहने वाले मुस्लिम महिलाओं के समूहों में आगे के रास्ते को लेकर विचारों में विभिन्नता है- बीएमएमए ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के कोडीफिकेशन का प्रस्ताव दिया है और मुस्लिम वुमन’स राइट्स नेटवर्क ने धर्मनिरपेक्ष लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानूनों का प्रस्ताव दिया है। धर्मनिरपेक्ष लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानूनों की मांग करने वाले महिला समूह जानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ और हर उस शै, जो मुस्लिम है, खलनायकीकरण करने वाली राजनीति से भी भिड़ना होगा।
मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या दे सकता है?
मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी भी और निजी कानून की तरह न तो पूरी तरह अच्छा है और न पूरी तरह बुरा। एक धर्मनिरपेक्ष देश में यूसीसी का मतलब बाकी आबादी पर मौजूदा हिन्दू कानून लादना नहीं हो सकता। जैसे भारतीय संविधान ने दुनिया भर के संविधानों से अच्छी बातें लीं उसी तरह दूसरे देशों या धार्मिक समुदायों के कानूनों या अच्छी बातों से मदद लेने की आवश्यकता है। यदि हम लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानून चाहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी बहुत कुछ है।
तलाक: मनमाने तीन तलाक का एक औजार के रूप में दक्षिणपंथियों द्वारा मुस्लिम समुदाय का खलनायकीकरण करने के लिए किया जाता है। लेकिन, मुस्लिमों के पास तलाक के लिए और भी कई विकल्प हैं और धर्म यह मानता है कि शादियां सुसंगति के अभाव में टूटती हैं और बिना किसी एक साथी की गलती के भी। यह बिना किसी एक साथी की गलती के तलाक और शादी के सुसंगति टूटने की बात हमारे धर्मनिरपेक्ष कानूनों में नहीं है। कुरान की प्रक्रिया के अनुसार सुलह मध्यस्थता का प्रयास सभी तरह के इस्लामिक तलाकों के लिए जरूरी है।
यूसीसी तलाक-ए-हसन की भावना शामिल कर सकता है, जो तलाक के प्रभावी होने से पहले तीन महीने की अवधि विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता के लिए देता है। फ़सख-ए-निकाह पत्नी की तरफ से शुरू की गई तलाक प्रक्रिया है जब पति उसे तलाक देने से मना कर देता है। यदि पति सुलह करने या तलाक देने से मना करे तो काज़ी फ़सख-ए-निकाह की घोषणा कर शादी को निरस्त कर सकता है। यह विकल्प वह मुस्लिम महिलाएं अपनाती हैं जिनके पति तलाक देने से मना कर दें, वैसे ही जैसे अदालतों में लोग अनुपस्थित रहकर वर्षों तक तलाक की प्रक्रिया को लंबा खींचते रहते हैं।
देश भर में पारिवारिक अदालतें बोझ से दबी हैं, एक तलाक की लड़ाई में औसत समय तीन से पांच साल और उससे भी अधिक लग रहा है। गलती बिना तलाक के न होने का मतलब है कि एक पक्ष के पास किसी प्रकार की क्रूरता का प्रमाण तलाक के लिए होना चाहिए।
आज की तारीख में हमें यह समझने की जरूरत है कि रिश्ते में दंपति एक दूसरे के प्रति अपेक्षाएं जानते हैं और मानते हैं कि सुसंगति का अभाव अलग होने के लिए पर्याप्त कारण है। तलाक की प्रक्रिया में किसी एक साथी को खलनायक बनाना जरूरी नहीं है या सालों मामले को खीचकर लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने से रोकना सही नहीं है।
बहु-विवाह/द्वि-विवाह: मुस्लिम पर्सनल लॉ का दूसरा पहलू जिसका इस्तेमाल समुदाय का खलनायिकीकरण करने के लिए किया जाता है वह है पुरुषों को चार पत्नियों की इजाजत। 1974 के एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार 5.6 फीसदी मुस्लिम पुरुष और 5.8 फीसदी उच्च जातियों के हिन्दू बहु-विवाह और द्वि-विवाह रिश्तों में थे। 2001 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण (एएचएफएस) आंकड़ों के अनुसार यह संख्या गिरकर मुस्लिमों में 1.9 फीसदी और हिंदुओं में 1.3 फीसदी हो चुकी है। बहु-विवाह सबसे अधिक आदिवासी समुदायों में होते हैं।
एक हिन्दू पुरुष की दूसरी पत्नी, को द्वि-विवाह शादी, जिसे कि कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, में होने के लिए दंडित किया जाता है। यूसीसी यदि बहु-विवाह को गैरकानूनी करार देता है, द्वि-विवाह शादियों में महिलाओं को अधिकार रहित छोड़ देगा।
यदि यूसीसी सभी पुरुषों के लिए बहु-विवाह गैरकानूनी करार देता है, तो इसे दूसरी पत्नी (हिन्दू या मुस्लिम या किसी भी धर्म से) के अधिकारों के बारे में सोचना होगा, जो इस समय मुस्लिम कानून में उपलब्ध हैं। यदि द्वि-विवाह विवाहों में महिलाओं के अधिकार छीन लिए जाते हैं तो यूसीसी को द्वि-विवाह विवाहों में महिलाओं के अधिकारों के बारे में सोचना ही होगा। महिलाओं को पुरुषों के कृत्यों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
संपत्ति का अधिकार: हिन्दू कोड बिल में हिन्दू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने से बहुत पहले, इस्लाम ने महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा दिलवाया। आज के कानून के अनुसार, महिलाओं को विरासत में असमान हिस्सा मिलता है। हिन्दू अपनी बहनों को संपत्ति में समान हिस्सा कानून के बावजूद देना नहीं चाहते जैसा कि अदालतों में कई संपत्ति विवादों में देखा जा सकता है।
कानून द्वारा संपत्ति में समान हिस्सा निर्दिष्ट किया गया तो सभी मुस्लिम महिलाओं को लाभ होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ समूची संपत्ति किसी को दे देने, जिससे कि महिलाओं को विरासत से बाहर रख सकता हो, की अनुमति नहीं देता। यूसीसी इस प्रावधान को अपनाने से लाभान्वित हो सकता है।
मुस्लिम महिलाएं कस्टडी और संरक्षण के समान अधिकार चाहती हैं और गोद लेने का अधिकार भी (अपने लिए ही नहीं पर देश की सभी महिलाओं के लिए) वह यह भी मांग करती हैं कि महिलाओं और बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
परिवार से संबंधित कानून में समानता के अलावा महिला समूहों ने बार-बार मैरिटल रैप (विवाह में बलात्कार) का मुद्दा भी उठाया है। दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का प्रावधान शादियों में बलात्कार का वैधकीकरण है और इसे तुरंत निरस्त करना चाहिए।
विशेष विवाह अधिनियम में आवश्यक बदलावों में नोटिस अवधि की आवश्यकता को समाप्त करना है जो अंतर-धार्मिक विवाहों में दम्पत्ति जान जोखिम में पड़ने का कारण बनने लगा है, खासकर हाल के समय में।
निष्कर्ष
विभिन्न धर्मों में पितृसत्ता मानने वालों ने धर्म का इस्तेमाल महिलाओं को उनके अधिकार न देने के लिए किया है। मुस्लिम परंपरावादी मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का कड़ा विरोध करेंगे ही, ठीक उसी तरह जैसे हिन्दू महासभा के सदस्यों ने हिन्दू कोड बिल का विरोध किया था, जिससे अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था।
रूढ़िवादियों के विचारों को समूचे समुदाय के विचार मान लेना विभाजन ही पैदा करेगा और समाज में महिलाओं के अपने अधिकारों के लिए किए संघर्षों को मिटा देगा। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि महिलाओं की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी समुदाय में अन्य आवाज़ें।
यूसीसी प्रस्तावित करने में इस सरकार का इरादा समझते हुए, मैं दोहराना चाहूंगी कि मुस्लिम लैंगिक आधार पर भेदभाव रहित कानूनों के पक्ष में हैं और मानते हैं कि कोई एक धर्म सभी महिलाओं को न्याय नहीं दे सकता। हमें शासन की तरफ से दिए इस मौके का इस्तेमाल सभी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि यूसीसी की दिशा में उठाए जाने वाले किसी भी कदम की आवश्यकता देश भर में महिला समूहों और अन्य हितधारकों से मशविरा करना है।
[मैं अपने नारीवादी साथियों, खासकर फोरम अगेन्स्ट अप्रेशन ऑफ वुमन की महिलाओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिनके साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव रहित कानूनों के बारे में कई चर्चाओं और कार्यों में शामिल रही और जिन्होंने मेरी राजनीति को आकार दिया और इस लेख को भी समृद्ध किया। चयनिका शाह और सुजाता गोथसकर का उनकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद और मेरा साउन्डिंग बोर्ड बनने और यह लेख संपादित करने के लिए साना कान्ट्रैक्टर का बहुत-बहुत शुक्रिया]
(साबाह खान का यह लेख इंडिया फोरम की वेबसाइट से साभार लिया गया है। मूल अंग्रेज़ी लेख का हिन्दी अनुवाद महेश राजपूत ने किया है। साबाह खान मुस्लिम वुमन’स राइट्स नेटवर्क की 1999 में शुरुआत से सदस्य हैं। वह परचम की सह संस्थापक हैं जो समाज के युवाओं के साथ ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करता है जिसमें बहुलता, भिन्नता और परस्पर निर्भरता के प्रति सम्मान हो।)