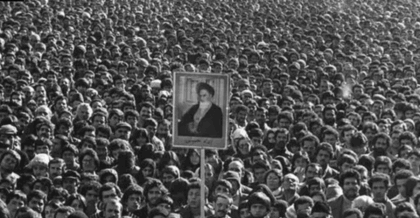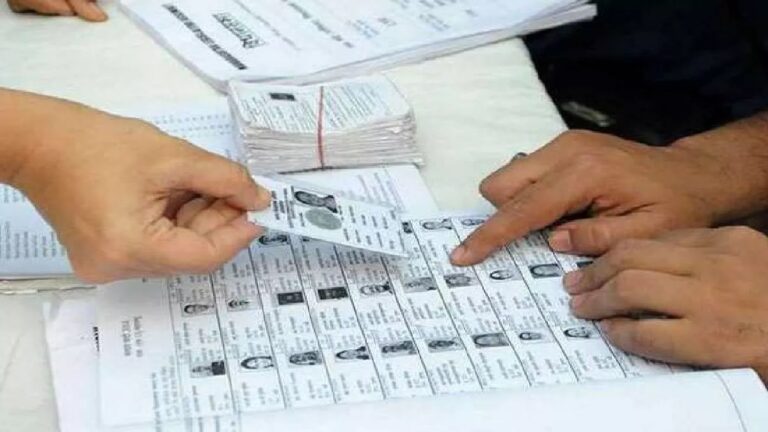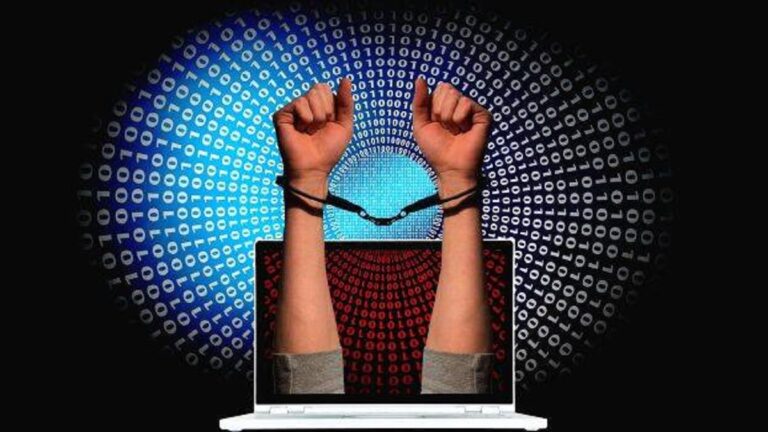चंद्रयान-3 अपनी मंजिल के बहुत करीब है। फिलहाल यह अपने दो अवतारों में चंद्रमा के इर्दगिर्द घूम रहा है। एक इसका प्रॉपल्शन मॉड्यूल, जो चंद्रमा से 153 किलोमीटर की न्यूनतम और 163 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई वाली लगभग गोलाकार कक्षा में रहकर चंद्रमा के प्रेक्षण ले रहा है। उसकी कक्षा स्थायी है और एक चंद्र-उपग्रह के रूप में यह लंबे समय तक यहां बना रह सकता है। दूसरा लैंडिंग मॉड्यूल, जो चंद्रयान से अलग से होने के बाद चंद्र सतह से 30 किलोमीटर की न्यूनतम और 100 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई वाली अस्थायी कक्षा में घूम रहा है, जहां से उसकी दिशा बदलते हुए और रफ्तार घटाते हुए चंद्रमा पर उतारने की जटिल प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
ध्यान रहे, चंद्रयान-3 ज्यादातर मामलों में हूबहू चंद्रयान-2 का ही दोहराव है। अभी तक संपन्न हुई प्रक्रिया में दोनों के बीच एक ही फर्क रेखांकित करने लायक है कि चंद्रयान-2 का एक काम चंद्रमा की कक्षा में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में ऑर्बिटर की स्थापना करने का था, जो इस बार उसके कार्यभार में नहीं शामिल है। इस सोच के ही मुताबिक इस बार प्रॉपल्शन मॉड्यूल में ईंधन कम और लैंडर मॉड्यूल में ज्यादा रखा गया है। वैसे भी 2019 में स्थापित ऑर्बिटर अभी बिल्कुल चाक-चौबंद है और चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए बारीक नक्शे उसके ही बनाए हुए हैं।
जितनी उत्सुकता चंद्रयान-3 को लेकर अभी भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में देखी जा रही है, वह अबतक गिने-चुने अंतरिक्ष अभियानों के ही हिस्से आई है। चंद्रयान-2 से निकला विक्रम लैंडर उतराई के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान को अपने करतब दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाया था। सबके मन में यह सवाल है कि अपनी उस नाकामी से इसरो क्या इतनी सीख ले पाया है कि ढाई लाख मील दूर मौजूद सुई में धागा पिरोने का काम इस बार बेखटके कर डाले। इसका रोमांच बिल्कुल तड़ातड़ी में नजर आए रूस के लूना-25 अभियान से थोड़ा और बढ़ गया है, जिसकी लांचिंग चंद्रयान-3 के महीने भर बाद हुई जबकि लैंडिंग का लक्ष्य इससे दो दिन पहले रखा गया है।
आर्टेमिस का चक्कर
रूसी वैज्ञानिकों और राजनयिकों के ऐसे बयान आ रहे हैं चंद्रयान-3 और लूना-25 के बीच कोई होड़ नहीं है। यह भी कि लूना-25 की लांचिंग 2021 में की जानी थी, कुछ-कुछ वजहों से टलती हुई यह अब हो पाई है। बहरहाल, वे कुछ भी कहें लेकिन हैट में से खरगोश निकालने की तरह सामने आए लूना-25 अभियान का एक मकसद साफ है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में पहली बार अपना यान उतारने का सेहरा रूस के ही सिर बंधना चाहिए, भारत के नहीं, जिसकी रॉकेट साइंस में थोड़ी मददगार भूमिका रूस की भी रही है। इसका दूसरा पहलू यह है कि भारत अभी चंद्रमा की खोजबीन और उसके दोहन के लिए बनाई गई अमेरिका की आर्टेमिस परियोजना का हिस्सा बन गया है।
रही बात चंद्रयान-3 की लांचिंग से लैंडिंग तक का समय लगभग 40 दिन और लूना-25 के लिए यह महज 10 दिन होने का तो इसका मुख्य कारण दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाली लांचिंग वेहिकल्स की ताकत में फर्क होना है। रूसी सोयुज यान बहुत ताकतवर है और धरती से चांद तक का रास्ता वह कम समय में तय कर लेता है। भारत के पास भी मजबूत रॉकेट मौजूद हैं लेकिन अपने चंद्र अभियान को तुरत-फुरत निपटा देने की बात उसके अजेंडा पर नहीं थी। ऐसे में चंद्रयान-3 की लांचिंग में पृथ्वी के गुरुत्व का इस्तेमाल उसने गुलेल की तरह किया और सौर ऊर्जा का भी पूरा फायदा उठाया। बात चंद्रमा पर इंसान उतारने की होगी तो रूस को भी दोगुनी ताकत वाला रॉकेट आजमाना होगा।
चंद्रयान-3 और लूना-25 के मकसद पर बात करनी हो तो इनमें दो बड़े फर्क हैं। चंद्रयान-3 का अभियान कुल 14 दिनों के लिए है, यानी चंद्रमा के एक दिन के बराबर। उसे लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारना है और अगले चौदह दिनों में एक छोटी ऑटोमेटिक गाड़ी, रोवर को वहां 500 मीटर चलाना है। इसके उलट रूस को अपना लैंडर एक साल या उससे ज्यादा समय तक चंद्रमा पर ही रखकर उसकी सतह और वायुमंडल से जुड़े ब्यौरे जुटाने हैं।
ज्यादा बारीकी में जाएं तो चंद्रयान-3 की कोशिश चंद्रधूल का तात्विक अध्ययन करने के अलावा वहां मौजूद पत्थरों की क्रिस्टलीय संरचना समझने की रहेगी। सूरज की भीषण गर्मी चंद्रमा की सतह के पास वायुमंडल या धूल-भाप और आवेशित कणों के घोल जैसा कुछ बनाती है या नहीं, यह जानने का प्रयास भी वह करेगा। इसके लिए जरूरी यंत्र लैंडर और रोवर में लगे हैं। इसके अलावा सूक्ष्म भूकंपीय तरंगों का प्रेक्षण लेना भी इस मिशन का एक मकसद है, जिनके अध्ययन से चंद्रमा की भीतरी सतहों और उसके केंद्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं।
चंद्रयान-3 अभियान में एक जरूरी प्रेक्षण चंद्रमा की ताप चालकता को लेकर लिया जाना है। यानी सूरज की गर्मी वहां कितने समय में कितनी गहराई तक पहुंच पाती है। चंद्रमा पर भविष्य में बनने वाली वैज्ञानिक बस्तियों का स्वरूप काफी कुछ इसी पर निर्भर करेगा। इस प्रेक्षण के लिए एक कील को चंद्रमा की सतह पर दस सेंटीमीटर गाड़ दिया जाएगा और सवा सौ डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा तापमान वाले, कुल चौदह दिन लंबे तीखे चंद्र-दिन में कील के हर हिस्से के तापमान का प्रेक्षण लेते हुए चंद्रमा की ताप चालकता को लेकर पहली बार कुछ नतीजे निकाले जाएंगे।
नरक जैसे दिन-रात
यहां चंद्रमा के दिन-रात को लेकर कुछ जरूरी बातों का जिक्र भी जरूरी है। यह आकाशीय पिंड अपनी धुरी पर नहीं घूमता। स्पेस साइंस में इसे टाइडली लॉक्ड कंडीशन बोलते हैं। इसके चलते चंद्रमा का एक हिस्सा ही हमें हमेशा दिखाई पड़ता है, दूसरा यानी पीछे वाला हिस्सा हमारे लिए हमेशा अदृश्य ही बना रहता है। जाहिर है, जैसे धरती के दिन-रात इसके अपनी धुरी पर घूमने पर निर्भर करते हैं, वैसा कुछ चंद्रमा के साथ नहीं है। पृथ्वी का चक्कर काटते हुए जो हिस्सा सूरज के सामने पड़ जाए वहां दिन और जो पीछे पड़े वहां रात। दिन और रात को बांटने वाली तीखी टर्मिनेटर रेखा का चमत्कार रोज-रोज बदलने वाली चंद्रमा की शक्लों के रूप में हम यहीं से देख सकते हैं।
चंद्रमा की भूमध्य रेखा पर रात के समय थर्मामीटर में पारा जीरो से बहुत नीचे, माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड- कभी इससे थोड़ा कम, कभी ज्यादा- तापमान दिखाता है। फिर रात बीतने पर धरती के चौदह दिनों जितना ही लंबा, अपनी गर्मी की वजह से बेहद खतरनाक दिन वहां उगता है तो पारा धीरे-धीरे नहीं, बल्कि अचानक ही चढ़कर 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सीधे 300 डिग्री सेंटीग्रेड की उछाल।
टेंपरेचर की यह रेंज इतनी बड़ी है कि कामकाजी दायरे में आने वाली धरती की ज्यादातर चीजें सिर्फ इसके सर्द-गर्म के असर में आकर बिल्कुल नाकारा और जब-तब भुरभुरी होकर रह जाती हैं। इससे भी बड़ी समस्या रेडिएशन की है। सौर ज्वालाओं के साथ आने वाले जानलेवा रेडिएशन से बचाने के लिए ओजोन लेयर या चुंबकीय आवरण जैसी कोई चीज तो वहां है ही नहीं, साथ में ऐसी कोई आड़ भी खोजना मुश्किल है, जहां छिपाकर मशीनों के सर्किट बचाए जा सकें। अभी जब 2030 के दशक में प्रायोगिक तौर पर थोड़े-थोड़े समय के लिए वैज्ञानिकों को चांद पर रखने की बात अमेरिका और चीन में चल रही है, तब पहला सवाल सबके सामने यही है कि वहां ये रहेंगे कहां और उनके उपकरण कैसे काम कर पाएंगे?
ध्यान रहे, चंद्रमा से जुड़े चंद्रयान-1 के जिस सबसे महत्वपूर्ण प्रेक्षण को लेकर दुनिया के वैज्ञानिक हलकों में विवाद आज तक हल नहीं हो पाया है, उसका संबंध वहां पानी की मौजूदगी से है। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल को धरती की सबसे सूखी जगह माना जाता रहा है, लेकिन अपोलो अभियान के दौरान चंद्रधूल और पत्थरों के जो नमूने वहां से लाए गए, उनके अध्ययनों से पता चला कि वे सहारा की रेत से भी सौ गुना, बल्कि उससे भी ज्यादा सूखे हैं। इतने सूखे कि चीजों को ‘बोन ड्राई’ यानी हड्डी की तरह सूखा बताने का मुहावरा भी उनके लिए बेकार है।
सन 2008 में चंद्रयान-1 से जो मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद शैकल्टन क्रेटर में गिराया गया, उससे उड़े मलबे के स्पेक्ट्रम में पहली बार हाइड्रॉक्सिल आयनों की शिनाख्त चांद पर की गई। हाइड्रॉक्सिल आयन पानी के अणु का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद अमेरिकियों ने शैकल्टन के पास में ही मौजूद एक और क्रेटर के साथ यह क्रिया दोहराई तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। कुल मिलाकर चंद्रमा पर पानी का मामला आज भी अटकलों से ही घिरा है।
सिर्फ एक दावे पर नासा का सबसे ज्यादा जोर रहा है कि चंद्रमा पर पानी अगर किसी जगह जरा भी मात्रा में और किसी भी अवस्था में मिल सकता है तो वह जगह दक्षिणी ध्रुव के आसपास, ऊंचे पहाड़ों से घिरे किसी गड्ढे में ही होनी चाहिए। इसी उम्मीद में लूना-25 और चंद्रयान-3, दोनों को चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में 70 डिग्री अक्षांश रेखा के करीब एक-दूसरे से थोड़ा पूरब-पश्चिम में उतारा जाना है, हालांकि इन जगहों पर पानी तक कोई संयोग ही इन्हें पहुंचा सकेगा। पृथ्वी के भूगोल से चंद्रमा की कोई सीधी तुलना अटपटी ही हो सकती है, लेकिन इन यानों को उतारने की जगहें अगर हमारे ग्रह पर होतीं तो इन्हें अंटार्कटिका महाद्वीप के किसी समुद्रतटीय इलाके में दर्ज किया जाता।
आधी सदी बाद सोकर जागे
बहरहाल, इन दोनों अभियानों से जुड़ी बातें लंबे समय तक चर्चा में रहने वाली हैं। अभी तो सफलता-विफलता से परे इनके महत्व को लेकर ही बात की जानी चाहिए। इसकी शुरुआत इस दिलचस्प तथ्य से करते हैं कि लूना-25 से ठीक पहले संपन्न हुआ लूना-24 अभियान सन 1976 की, यानी अब से 47 साल पहले की बात है। रूस के साइंटिफिक टेंपर को लेकर बड़ी चर्चा होती रही है, लेकिन यह कैसी वैज्ञानिकता है, जिसके नींद से जागने में आधी सदी गुजर जाती है? रही बात उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी अमेरिका की, तो उसकी दो मून लैंडिंग में रूस से भी कहीं ज्यादा बड़ा फासला दर्ज किया जाएगा। चंद्रमा पर सुरक्षित तरीके से अपना अंतिम यान अमेरिका ने सन 1972 में उतारा था और आगे यह बारी शायद 2024 में ही आ सके।
चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, यानी सुरक्षित रूप में यान उतारने की उपलब्धि अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने हासिल की है, चंद्रयान-3 की सॉफ्टलैंडिंग कराकर भारत इस सूची में चौथा देश बन सकता है। लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि कम से कम तीन देशों के लिए तो चंद्रमा पर यान उतारना अब एक सामान्य बात हो गई होगी। सचाई यह है कि मानवजाति चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक एक बार ईजाद करके जैसे भूल ही गई है। रूस और अमेरिका, दोनों को चंद्रमा पर अपना यान उतारे हुए आधी सदी या इसके आसपास का समय हो गया है। इसी के चलते यह षड्यंत्र सिद्धांत चल निकला कि चंद्रमा पर इंसानी कदम कभी पड़े ही नहीं, अपोलो-11 की तस्वीरें एरिजोना के रेगिस्तान में उतार ली गईं।
पृथ्वी के इस अकेले उपग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग में अकेली महारत फिलहाल चीन को हासिल है, जिसने 2013 से 2020 के बीच यह काम तीन बार फूलप्रूफ ढंग से किया है। उसका यान वहां से सैंपल लेकर आया है और उसका एक रोवर यूटू-2 पिछले चार वर्षों से चंद्रमा की पीछे वाली, यानी पृथ्वी के लिए अदृश्य सतह पर सक्रिय है। वहां यान उतारने की एक कोशिश इजराइल ने भी की है, लेकिन 2019 में उसके यान बेरेशीट के लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे। सतह पर पहुंचने से दो किलोमीटर पहले कमांड सेंटर से उसका संवाद टूट गया और लैंडर का कुछ पता नहीं चला।
दुनिया के लिए यह पहला मौका है जब दो देशों के अंतरिक्षयान सिर्फ एक-दो दिन और सौ-दो सौ किलोमीटर के फासले पर चांद को आराम से छूने का प्रयास कर रहे हैं। और देश भी ऐसे जिनमें कभी कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं रही। भारत अभी अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई आर्टेमिस परियोजना का हिस्सा जरूर बन गया है, लेकिन हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि अपने वैज्ञानिक प्रयासों को किसी भू-राजनीतिक योजना का हिस्सा न बनने दें। आर्टेमिस में शामिल 27 मुल्कों की मजबूरी भले ही अमेरिकी जुबान में बात करने की हो, लेकिन उनमें से किसी के भी पास इसरो जैसी कोई संस्था नहीं है, जो बिना किसी महाशक्ति के संरक्षण के अपनी रॉकेट साइंस को इस मुकाम तक लेती आई है। हमारी उपलब्धियों को अमेरिका से जोड़कर देखा जाए, इसमें हमारा क्या फायदा है?
खैर, अभी यह किस्सा यहीं खत्म करते हैं। आगे बात करेंगे चंद्रमा को लेकर अचानक शुरू हुई इस नई भागम-भाग की वजहों पर, और फिर इस कयास को लेकर कि धरती की लड़ाइयां क्या चंद्रमा को भी गिरफ्त में लेने जा रही हैं।
(चंद्रभूषण वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं।)