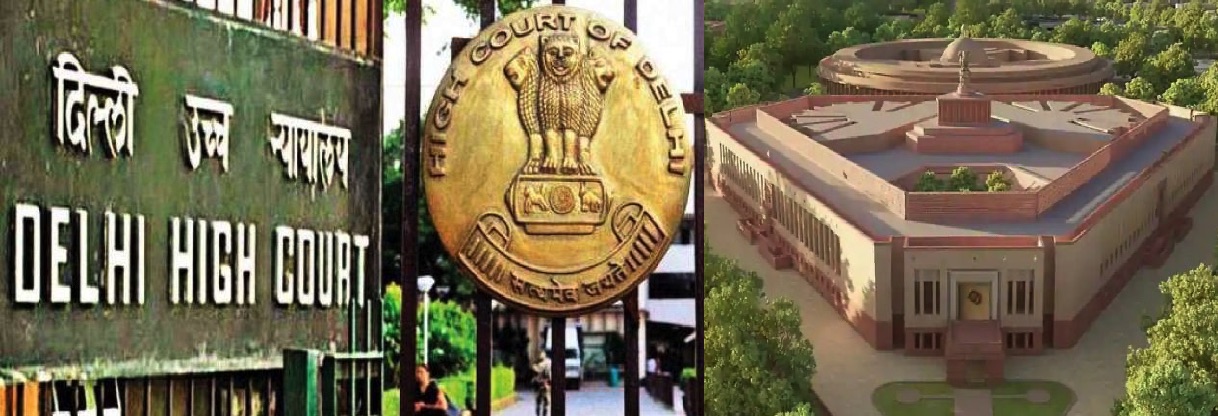दिल्ली हाईकोर्ट को लगा कि ‘राष्ट्रीय महत्व’ वाले ‘सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ को रोकना सही नहीं है और इसे अदालती दख़लन्दाज़ी के ज़रिये रोकने की माँग न सिर्फ़ अनुचित है, बल्कि ‘जनहित की दुहाई’ देने वाली धारणा का भी ‘बेज़ा इस्तेमाल’ है। लिहाज़ा, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का ज़ुर्माना ठोंक दिया। हमारी अदालतें सरकार के हरेक नाकामी की अनेदखी भले ही करें, लेकिन उन्हें जनहित याचिका का बेज़ा इस्तेमाल, न तो बर्दाश्त के क़ाबिल लगा और ना ही माफ़ी के लायक। इसीलिए हाईकोर्ट ने सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ‘अड़ंगा लगाने वालों’ को सबक सिखाने के लिए एक लाख रुपये की Cost लगा दी। अदालती भाषा में ऐसे ज़ुर्माने को Cost भी कहते हैं।
कहाँ एक रुपये की मानहानि, कहाँ एक लाख की कॉस्ट?
जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मानहानि के लिए प्रशान्त भूषण पर एक रुपये का सांकेतिक ज़ुर्माना लगाया था, वहीं हाईकोर्ट ने इसका लाख गुना ज़्यादा कॉस्ट लगाकर आख़िर क्या नज़ीर पेश की? कहीं ये पूरी क़वायद ‘चींटी मारने के लिए तोप चलाने’ जैसी तो नहीं? कहीं हाईकोर्ट का मकसद उन लोगों को कॉस्ट रूपी तोप के गोलों से डराने का तो नहीं जो किसी भी सरकारी नीति या रवैये के आलोचक हैं और अहंकारी बहुमत वाली सरकार को आड़े हाथों लेने के लिए अदालत को अपना हथकंडा बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र और संविधान की भावना के लिहाज़ से देखें तो ये सभी सवाल सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
मामला बहुत संगीन ना होता तो क्या हाईकोर्ट को बहस सुनने के बाद फ़ैसला सुनाने में दो हफ़्ते लग जाते? 19 मई को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फ़ैसला रिज़र्व (लम्बित) रख लिया था। ज़ाहिर है, 31 मई तक चीफ़ जस्टिस की बेंच ने ऐतिहासिक फ़ैसले के एक-एक शब्द पर माथापच्ची की होगी। हालाँकि, सबको मालूम था कि हाईकोर्ट का फ़ैसला क्या होने वाला है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में दख़ल देने से कन्नी काट ली तो फिर हाईकोर्ट की क्या बिसात कि वो मोदी सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं में टाँग फँसाये!
अदालती बहस की ज़रूरत ही नहीं थी
हाईकोर्ट ने जिन तथ्यों और तर्कों के आधार पर सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को निलम्बित करने की माँग को ख़ारिज़ किया, उसके अनुसार तो जनहित याचिका को पहली सुनवाई यानी एडमिशन के वक़्त ही ख़ारिज़ हो जाना चाहिए था। यदि अदालत को केन्द्र सरकार की दलीलों के पीछे मौजूद ‘सच और झूठ’ की पड़ताल किये बग़ैर ही फ़ैसला सुनाना था तो फिर अदालती बहस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी! अरे माई लॉर्ड, याचिका में सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने की गुहार नहीं लगायी थी। उसमें तो सिर्फ़ इतना कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए यदि पूरी दिल्ली में लॉकडाउन है तो मेहरबानी करके उन मज़दूरों की ज़िन्दगी को जोख़िम में नहीं डाला जाए जो सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं।
अदालत सिर्फ़ क़ानूनी झगड़ा सुनें
यदि ये सही है कि सरकार को निरंकुश होकर नीतिगत फैसले लेने और अपनी प्राथमिकताएँ तय करने का पूरा अधिकार है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और देश की कई हाईकोर्ट्स में ऐसी अनेक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई क्यों हो रही है, जहाँ कोई क़ानूनी झगड़ा नहीं है? दरअसल, संविधान में मौजूद नागरिकों के मूल अधिकारों यानी Fundamental Rights का संरक्षक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। इसीलिए लोगों को वहाँ गुहार लगानी पड़ती है। अब यदि कोर्ट में इस बात की भी सज़ा मिलने लगे कि कोई वहाँ गया ही क्यों तो समझ लीजिए कि हम कितने भयानक दौर में पहुँच चुके हैं!
कॉस्ट का असली मतलब क्या?
सज़ा के दो मक़सद होते हैं। पहला, जैसी करनी वैसी भरनी। और दूसरा, लोगों को सन्देश देना कि ख़बरदार, लक्ष्मण रेखा लाँघने की कोशिश मत करना वर्ना दंडित किये जाओगे। एक लाख रुपये की कॉस्ट तो उसे भरनी पड़ेगी जिसने अदालत के ज़रिये उस सरकार से संवेदनशील होने की अपेक्षा की थी जो कम से कम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नज़र में पहले से ही परम-संवेदनशील है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले में उन लोगों के लिए बेहद कड़ा सन्देश छिपा हुआ है जो इस मामले से सबक नहीं लेकर मुँह उठाये हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाने की मंशा रख सकते हैं।
न राम-भरोसे, ना अदालतों के!
पूरे प्रसंग को आप आप चाहें तो ‘बचाव का अचूक नुस्ख़ा’ या ‘अदालत निर्मित सरकारी कवच-कुंडल’ की तरह देख सकते हैं। ये फासीवाद का ऐसा चेहरा है, जो इंसाफ़ की अदालत से बाहर आया है। हमारे पास अनेक मिसाल है कि जनता यदि सरकार के ‘विकास रथ’ के रास्ते में रोड़े अटकायेगी तो उसे NSA, UAPA और देशद्रोह के क़ानूनों से ठोंका जाएगा। और, यदि कोई औरों की तकलीफ़ें देख अदालतों से फ़रियाद करेगा तो उसे ‘कॉस्ट’ से निपटाया जाएगा। कोई हालात को ‘राम भरोसे’ भी नहीं कह सकता। राम वादियों को ये बर्दाश्त नहीं कि उनकी उपलब्धियों या नाकामियों का श्रेय भगवान राम को मिल जाए। यानी, भगवान पत्थर की मूर्ति बनकर सिर्फ़ मन्दिरों में पड़े रहें। करें-धरें कुछ नहीं। और यदि वही सब करने वाले हैं तो भी कोई, किसी को भी, उनके यानी राम के ‘भरोसे’ का वास्ता नहीं दे। वर्ना, हुक़्मरान और उनकी अदालतें आग-बबूला हो जाएँगी।
विकास में रोड़ा बर्दाश्त नहीं
अरे माई लॉर्ड, याचिकाकर्ताओं की यही तो दलील थी कि आपदा के दौर में जो संसाधन इस प्रोजेक्ट में झोंके जा रहे हैं, उनका प्राथमिकता से इस्तेमाल अस्पताल, बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाई, टीका और अन्त्येष्टि वग़ैरह के संसाधनों को विकसित करने पर किया जाए। जवाब में ज़ाहिर है, सरकार यही तो कहेगी कि महामारी से जूझने के लिए उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। साफ़ है कि यदि संसाधन की कमी नहीं है, नीतियों में खोट नहीं है, क्रियान्वयन में दिक्कतें नहीं हैं तो फिर तेज़ी से कड़े फ़ैसले लेने वाली अद्भुत सरकार के लिए राष्ट्रीय महत्व वाले सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को निलम्बित करने की माँग का कोई तुक़ नहीं हो सकता।
अलबत्ता, ये किससे छिपा है कि संसाधनों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें किस कदर तरस रही हैं? पेट्रोल-डीज़ल की आसमान छूती क़ीमतों से बढ़कर और क्या गवाही हो सकती है! ग़रीब से ग़रीबतर होते जा रहे देश में पेट्रोल-डीज़ल का दाम सारी दुनिया से ज़्यादा है, क्योंकि हमारी सरकारों के लिए यही कामधेनु है। इन पर लागू भारी-भरकम टैक्स ही तो हमारी डबल और सिंगल इंजन वाली सरकारों के लिए विकास का पहिया है।
नारा नहीं, नीति है ‘सब चंगा सी’
देश की 90 फ़ीसदी आबादी बीते सात साल से लगातार मन्दी, बेरोज़गारी, छँटनी, गिरती आमदनी और बेतहाशा भाग रही महँगाई के दलदल में धँसती ही जा रही है, लेकिन सरकार का नारा ही नहीं, नीति भी है ‘सब चंगा सी’। कोरोना ने जिनकी जान ले ली, वो अभागे तो चले गये। जीते जी उनकी किस्मत जैसी भी रही हो, उनके शवों की किस्मत भी ऐसी नहीं थी कि उसकी गरिमामय अन्त्येष्टि हो सके। कोरोना की भेंट चढ़ गये लाखों भारतवासियों के करोड़ों करीबी रिश्तेदारों ने भी मौत को बेहद क़रीब से देखा है। कई किस्मत वाले ऐसे ज़रूर हैं जो निकम्मे एलोपैथी की वजह से मौत का पाला छूकर वापस भी लौट आये। कोई ऐसे सभी लोगों से पूछे कि उन्होंने निजी और सार्वजनिक संसाधनों की कैसी तंगी झेली है!
सविनय अवज्ञा है अगला रास्ता
साफ़ दिख रहा है कि सेन्ट्रल विस्टा फ़ैसले के ज़रिये दिल्ली हाईकोर्ट ने ना सिर्फ़ सरकार की निरंकुशता पर अपनी मोहर लगा दी, बल्कि निरंकुशता के ख़िलाफ़ मिमियाने वाली आवाज़ों का भी गला घोंट दिया है। क़ानूनी तौर पर याचिकाकर्ताओं के पास ‘कॉस्ट’ के ख़िलाफ़ अपील करने का रास्ता मौजूद है। लेकिन बेहतर होगा यदि वो एक लाख रुपये का ज़ुर्माना भरने के बजाय वैसे ही ‘जेल जाने’ की बात करें जैसा प्रशान्त भूषण ने किया था। एक बार फिर से भारत को गाँधी जी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन यानी Civil disobedience movement की ज़रूरत है। वर्ना, ये कल्पनातीत है कि सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति अदालतों का भक्तिभाव देश को रसातल की किस गहराई में पहुँचा देगा!
(मुकेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)