किसी समुदाय के व्यक्ति, विचार, भाषा व नायक पर हमला निंदनीय होते हुए भी इस मायने में अपनी सार्थकता छोड़ जाता है कि वो एक कारण प्रदान करता है सुप्त सामूहिक चेतना व प्रतिरोध को जगाने का, अपने वर्ग समुदाय के ऐतिहासिक नायकों उनके विचारों और संघर्षों से खुद को जोड़कर देखने, सोचने और मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। तुग़लकाबाद दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहले संत रविदास के मंदिर तोड़े जाने और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही मंदिर के पुर्ननिर्माण के आदेश के संदर्भ में संत रैदास के साहित्य और विचार पर एक फौरी नज़र।
पंद्रहवीं सदी को रैदास का काल नियत किया जाता है। उस समय काल में सत्ता द्विकेंद्रित था- राजसत्ता और धर्मसत्ता। मुस्लिम शासकों के राजसत्ता में आसीन होने के बाद धर्मसत्ता भी द्विकेंद्रीय होकर हिंदू धर्मसत्ता और इस्लाम धर्मसत्ता हो गया। हिंदू धर्मसत्ता की कमान ब्राह्मणों तो इस्लाम धर्मसत्ता की कमान काजी-मुल्लों के हाथ में थी। धर्मसत्ता का राजसत्ता में सीधा दख़ल था, जबकि राजसत्ता, धर्मसत्ता के मुआमले में टांग नहीं अड़ा सकता था।
हिंदू और इस्लाम दोनों ही मज़हब समाजिक परिस्थिति और संसाधनों के असमान वितरण पर आधारित वर्ग एवं वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था मानते थे और वंचित निम्न तबके के शोषण, उत्पीड़न को अपना धार्मिक जन्माधिकार। हिंदू धर्म जहां वर्ण व्यवस्था को पूर्व जन्म का कर्मफल बताकर न्यायसंगत ठहराता, तो इस्लाम भी वर्ग व्यवस्था को अल्लाह का न्याय तथा वर्तमान दुखों और अभावों के विरुद्ध संघर्ष को ‘बिगाड़’ बताता। दलित, शूद्र, वंचित जन तीनों ओर से मार खाने को अभिशप्त थे। अपने समय को दर्ज करते हुए रैदास लिखते हैं, ‘दास रैदास यह काल व्याकुल, त्राहि त्राहि अवर अवलंबन नहीं मेरैं।’
‘श्रम’ की जीवन मूल्यों के तौर पर स्थापना
हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में जीवन का अस्वीकार है और दोनों ही धर्मों के धर्माधिकारी अपने धर्मावलंबियों से इस जीवन में रमने, भोगने के बजाय स्वर्ग और जन्नत की चिंता करें। रैदास अपने समय में हिंदू और इस्लाम के इस जीवन के अस्वीकार के दर्शन के खिलाफ़ खड़े होते हैं। जीवन की स्वीकृति के पक्ष में दलीलें पेश करते हैं।
रैदास का साहित्य दरअसल जीवन के स्वीकार का साहित्य है। इसमें एक स्वर शोषक वर्ग के प्रपंचों के प्रतिरोध और आक्रोश का है तो वहीं दूसरा स्वर सुखी समाज की आकांक्षा और समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति का है। रैदास एक ओर जहाँ बनी-बनाई धार्मिक-सामाजिक मान्यताओं और इन्हें स्थापत्य व स्थायित्व देने वाले धर्मग्रंथों का विखंडन करते हैं वहीं दूसरी ओर नए जीवन मूल्यों की संरचना भी करते हैं।
रैदास के समय काल में श्रम और सृजन करने वाला वर्ग बहुत ही अवमूल्यित, अपमानित और तिरस्कृत था। श्रम व सृजन करने वाला वर्ग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से पिछड़ा व अछूत माना जाता था। धार्मिक व्याख्याओं में दासों, और श्रम-गुलामों को पिछले जन्म का कर्ज़ बताकर जायज ठहराया जाता था। रैदास सभी धार्मिक व्याख्याओं को नकारते हुए श्रम मूल्य को जीवन का सबसे बड़ा मूल्य बताते हैं और श्रम संस्कृति के महत्व को रेखांकित करके लिखते हैं-
रैदास श्रम करि खाइहि, जौं लौं पार बसाय
नेक कमाई जउ करइ कबहुँ न निहफल जाय
जबकि उस काल में श्रमहीन वर्ग धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से श्रेष्ठ, मान्यता-प्राप्त व अधिकार-संपन्न था। उसे शूद्रों, दासों और श्रम गुलामों के उत्पीड़न का धार्मिक-सामाजिक मान्यता प्राप्त था। हर तरह की सुख-सुविधा पर उनका ही एकाधिकार था। रैदास उच्चता और श्रेष्ठता के नाम पर होने वाली बिना श्रम की इस हरामखोरी व परजीविता को हतोत्साहित करते हैं-
धरम करम जाने नहीं, मन मह जाति अभिमान
ऐ सोउ ब्राह्मण सो भलो रविदास श्रमिकहु जान
ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूती देने वाले धर्मग्रंथों का विखंडन
प्रतिरोध के दो स्तर होते हैं। पहले स्तर के तहत पहले से मौजूद वर्चस्ववादी ढांचे को विखंडित (डिकंस्ट्रक्ट) करना और दूसरे स्तर के तहत एक प्रतिरोधी ढांचे का निर्माण (कंस्ट्रक्शन) करना। रैदास ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्राह्णवाद के आधारभूत धर्मग्रंथों के विखंडन की ज़रूरत को न सिर्फ़ बड़ी शिद्दत से महसूस किया बल्कि ख़ुद भी खंडन किया। उनके इस तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिबोध के अभियान को आगे चलकर ज्योतिबा फुले, डॉ. भीमराव अम्बेडकर और ललई यादव ने और मजबूती से आगे बढ़ाया। रैदास लिखते हैं-
चारिव वेद किया खंडौती, जन रैदास करे दंडौती
या फिर
वर्णाश्रम अभिमान तजि, पद रज बंदहिजासु की
सन्देह-ग्रंथि खण्डन-निपन, बानि विमुल रैदास की
भाग्यवाद के बरअक्स कर्म के प्रधानता की स्थापना
रैदास अपनी रचनाओं में ब्राह्मणी व्यवस्था, पाखंडवाद, आडंबरवाद, अंधविश्वास के खिलाफ़ बहुत ही उग्र व तीव्र प्रतिरोध दर्ज करते हैं। अपने समय समाज के वर्चस्ववादी सत्तासीन वर्ग की धर्मसत्ता-व्यवस्था की राजनीति को वो जबर्दस्त चुनौती देते हैं। वेदान्त के प्रस्थानत्रयी के स्मृति प्रस्थान यानि गीता में कर्मयोग के नाम पर दासत्व, गुलामी व बेगारी को भाववाद की चाशनी में लपेटकर यूं कहा गया है-
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि
कर्मयोग के नाम पर भाग्यवाद को अधिक मजबूती से स्थापित करने वाले भगवद् गीता के उक्त दर्शन को उलटते हुए रैदास कहते हैं-
करम बंधन में बन्ध रहियो, फल की ना तज्जियो आस
कर्म मानुष का धर्म है, सत् भाखै रैदास
रैदास ने अपने समय का साहित्य रचते हुए ब्राह्मणवाद को ठोस चुनौती दी। अपनी लेखनी से उन्होंने ये विचार समाज को दिया कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं होता है। ‘जन्मना ब्राह्मण पूज्यनीय’ के ब्राह्मणवादी दर्शन को उलटते हुए वो समाज से ‘कर्मणा पूज्यनीय’ की बात कहते हुए समतामूलक कर्म सिद्धांत स्थापित करने वाले दोहे लिखते हैं-
ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन,
पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीन
उपरोक्त दोहे में व्यक्त रैदास के विचार का असर उस समय-काल के समाज पर कितना व्यापक और प्रभावशाली रहा होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रैदास के डेढ़ सदी बाद तुलसीदास को रैदास के उक्त दोहे के विरोध में राम के हवाले से लिखना ही पड़ा- पूजहि विप्र सकल गुण हीना। शुद्र न पूजहु वेद प्रवीणा।
समतामूलक समाज के जिस सिद्धांत को उन्होंने उस जमाने में बताने की कोशिश की, देखा जाए तो आज भी उतना ही प्रासंगिक और असरदार है तभी उनकी इस अवधारणा पर आवाज़ उठ रही है। रैदास ने सीधे-सीधे लिखा कि–
रैदास जन्म के कारने होत न कोई नीच, नर कूं नीच कर डारि है, ओछे करम की नीच
दया धर्म जिन्ह में नहीं, हद्य पाप को कीच,
रविदास जिन्हहि जानि हो महा पातकी नीच
कर्मकांड की आर्थिकी पर चोट
कोई भी धार्मिक-व्यवस्था समाजिक-आर्थिकी पर अपना नियंत्रण स्थापित किए बिना ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। अकूत धन-संपदा संपन्न मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्ज़ा और धनार्जन करने वाले कर्मकांडों पर ब्राह्मणों का एकाधिपत्य सदियों से रहा है। रैदास इस ब्राह्मणवादी धर्म की अर्थनीति को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं, पाखंडों की पहचान करते हैं जो कर्मकांडों के जरिए आर्थिक शोषण करने वाली उनकी युक्तियों का अपने पदों में वैचारिक तर्कों द्वारा भंडाश्राद्ध करते हैं-
जीवन चारि दिवस का मेला रे
बांभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे
मंदिर भीतर मूरति बैठी, पूजति बाहर चेला रे
लड्डू भोग चढावति जनता, मूरति के ढिंग केला रे
पत्थर मूरति कछु न खाती, खाते बांभन चेला रे
जनता लूटति बांभन सारे, प्रभु जी देति न धेला रे
पुन्य पाप या पुनर्जन्म का, बांभन दीन्हा खेला रे
स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे
जितना दान देव गे जैसा, वैसा निकरै तेला रे
बांभन जाति सभी बहकावे, जन्ह तंह मचै बबेला रे
छोड़ि के बांभन आ संग मेरे, कह विद्रोहि अकेला रे
मंदिर के बरअक्स मन की प्रतिस्थापना रैदास के समय-काल में वर्चस्ववादी ब्राह्मण समाज ने छुआछूत का जबर्दस्त आतंक मचा रखा था। एक तरफ मंदिरों व नदी, तालाब जैसे दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर दलितों, शूद्रों, दासों के लिए प्रवेश वर्जित किया हुआ था वहीं दूसरी ओर उन्हें धार्मिक सामाजिक संस्कारविहीन बताकर उन्हें पशु तुल्य समझा बताया जाता था। एक ओर ये प्रचार-प्रसार किया जा रहा था कि ईश्वर की शरण में आए बिना मुक्ति नहीं है वहीं दूसरी ओर उन्हें ईश्वर से मिलने के रास्ते भी सख्ती से बंद करके रखे गए थे। रैदास दलित समुदाय के लोगों की पीड़ा को समझते थे अतः उन्होंने मंदिर के बरअक्स मन की परिकल्पना की। मन की शुद्धता और सादगी को तरजीह देते हुए रैदास लिखते हैं-
मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप
इसी तरह वो पाखंडवादी खर्चीले तीर्थयात्रा जैसे दिखावों के खिलाफ़ भी लिखते हैं और हर तीर्थ को अपने मन में खोजने का आग्रह करते हैं-
का मथुरा, का द्वारका, का काशी, हरिद्वार?
रैदास जो खोजा दिल आपना तो मिलिया दिलदार
ऐसे ही
मन चंगा तो कठौती में गंगा
कुछ धार्मिक, समाजिक राजनीतिक यातना और कुछ जोगियों, वैरागियों की तरह की तरह घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी से भाग कर जोगिया रमाने लगे। रैदास को दलित समाज के पुरुषों में लगी इस नई बीमारी से दुखी हुए। दलित परंपरा श्रम संस्कृति की वाहक रही है। रैदास खुद चर्मकार थे और चमड़े का काम करके जीवन-यापन करते थे। वे मेहनत करके जीने को सबसे बड़ा जीवन मूल्य मानते हैं और घर-बार छोड़कर वन जाने या संन्यास लेने को ढोंग-पाखण्ड बताते हैं और दलित जनों को पाखंडवादी कर्मकांडों में न उलझने की नसीहत देते हुए लिखते हैं-
नेक कमाई जउ करइ, गृह तजि वन नहिं जाय
रैदास हमारो राम राय, ग्रह महिं मिलहिं आय
वन खोजो पी न मिलै, वन मैं प्रीतम नांहि
रैदास पी हम बसै, रहियो मानव प्रेमी मांहि
रैदास व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते हैं अपने पदों में आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति भावना की रचना करते हुए भक्ति के नए आयाम खोलते हैं-
राम हमउ मँहि रमि रह्यो, विसव कुटुंबह मांहि
पंथनिरपेक्षता की अवधारणा और सांप्रदायिक समन्वय का प्रयास
चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों के सत्ता में काबिज होने के बाद सत्ता संघर्ष के लिए युद्ध और षडयंत्र बढ़ा। इसके प्रभाव में समाज में हिंसा, अशांति और अस्थायित्व बढ़ा। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बाद समाजिक सत्ता संरचना में बड़ा फेरबदल हुआ, सत्ता के करीब दूसरे धर्म-वर्ग के लोग आ गए, टैक्स की मार से बचने के लिए बड़ी तादाद में वंचित दलित समुदाय के लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। इससे सामाजिक संरचना में भारी फेरबदल हुआ। हिंदु-मुस्लिम समाज में विद्वेष, नफ़रत, घृणा और वैमनस्य बढ़ा इसका ख़ामियाजा दोनों संप्रदायों के वंचित तबके को उठाना पड़ता। रैदास सत्ता राजनीति के विद्वेष के समाज पर पड़े कुप्रभावों को देखते समझते हैं और उसके खिलाफ़ बहुत सशक्त आवाज़ उठाते हैं।
रैदास इस बात को भलीभाँति समझते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद और अंध विद्वेष समाज और मनुष्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं और इनसे वैचारिक तार्किकी खड़ा करके निपटा जा सकता है। कोई ताज़्जुब नहीं कि सांप्रदायिक सद्भाव के उनके हर दोहे में एक से बढ़कर एक व्यवहारिक जीवन दर्शन के तर्क होते हैं जिनका निहितार्थ ही व्यक्ति के भीतर की धार्मिक जड़ता और अंधास्था को तोड़कर उनमें मानवीय वैचारिकी और प्रेम व सद्भावना का विकास करना है-
हिन्दू तुरूक महि नाहि कछु भेदा दुई आयो इक द्वार,
प्राण पिण्ड लौह मास एकहि रैदास विचार
आज देश समाज में धर्म-परिवर्तन को बेहद डरावने और ख़तरनाक रूप में पेश किया जा रहा है। निजी आस्था को सामुदायिक अस्मिता का सवाल बनाकर लोगों को डराया जा रहा है और जोर-जबर्दस्ती के धर्मांतरण को घरवापसी के नाम से जस्टिफाई किया जा रहा है। रैदास अपने समय में हुए स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए बहुत सुंदर रूपक गढ़ते हैं और बताते हैं कि धर्मांतरण से व्यक्ति का धार्मिक पहचान भले बदल जाए, उसके मानवीय गुणधर्म नहीं बदलते-
रैदास कनक और कंगन माहि जिमि अंतर कछु नाहिं
तैसे ही अंतर नहीं हिन्दुअन तुरकन माहि
रैदास सांप्रदायिक विद्वेष के विकास की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं इसीलिए वो उसके खिलाफ़ रणनीतिक तौर पर कई स्तरों पर अलगाते हैं और बारी-बारी से उन पर आक्रमण करते हैं। पहले वो हिंदू-मुस्लिम का विभेद खत्म करते हैं फिर उन्हें एक-दूसरे से जोड़ने का यत्न रचते हैं। अपने विवेकशील तर्कों द्वारा दो सांप्रदायों के बीच एक सद्भावना-सेतु निर्मित करने की कोशिश करते हैं और पंथनिरपेक्षता की संकल्पना विकसित करते हुए लिखते हैं-
मसजिद सो कछु घिन नहीं मन्दिर सों नहीं पिआर,
दोउ मँह अल्लह राम नहिं, कह रैदास चमार
मुसलमान से दोस्ती, हिन्दुवन से कर प्रीत,
रैदास ज्योति सभ हरि की, सभ हैं अपने मीत
मंदिर-मस्जिद एक है, इन मँह अनतर नाहिं
रैदास राम रहमान का, झगड़ऊ कोउ नाहिं।
रैदास हमारा राम जोई, सोई है रहमा
काबा कासी जानि यहि, दोउ एक समान
जाति व्यवस्था पर चोट
मध्यकालीन हिंदू समाज की ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शूद्रों और दलितों का मजाक उड़ाया जाता है। रैदास भी अपने समय में इन अपमानजनक अनुभूतियों से गुज़रते हैं और अपने दोहों में दर्ज करते हैं-
हम अपराधी नीच घर जन्में, कुटंब लोग हाँसी रे
चमार जाति संपूर्ण भारत में अछूत समझी जाती थी, जिसमें उत्पन्न व्यक्ति को दूसरी उच्च जातियों में उत्पन्न व्यक्ति, छूना तक पाप समझते थे। रैदास के समय काल में अमानुषिक अस्पृश्यता की यातना किस हद तक व्याप्त थी उसकी वेदना रैदास के निम्न पंक्ति में महसूस की जा सकती है–
रैदास तूँ कॉवचि फली, तूझे न छिवै कोय
रैदास जाति-पाँति और छुआ-छूत की यातना से गुज़रकर संघर्ष करते हैं और इस अमानुषिक बुराई के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करते हैं और ब्राह्मणी व्यवस्था से उसके ही भाषा में सवाल पूछते हैं-
रैदास एक ही नूर ते जिमि उपज्यों संसार
ऊँच-नीच किहि विध भये, ब्राह्मन और चमार
रैदास अपने प्रतिरोध का मानवीय प्रेम और समन्वय के पक्ष में विस्तार करते हुए स्पष्ट लिखते हैं कि जाति एक ऐसी बाधा है, जो आदमी को आदमी से जुड़ने नहीं देती है। वे कहते हैं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तब तक नहीं जुड़ सकता, जब तक जाति का खात्मा नहीं हो जाता। उनकी इन जाति संबंधी चिंताओं से अपने समय में गांधी और अंबेडकर भी जूझते हैं-
जात-पात के फेर महिं उरझि रहे सब लोग
मानुषता को खात है, रैदास जात का रोग
जाति-जाति में जाति हैं, जो केतन के पात,
रैदास मनुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात
रैदास ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को उलट देते हैं और वर्ण व्यवस्था को पुनर्परिभाषित करते हैं-
रैदास की दृष्टि में ब्राह्मण वो हैं-
ऊँचे कुल के कारणै ब्राह्मन कोय न होय, जउ जानहि ब्रह्म आत्मा, रैदास कहि ब्राह्मण सोय
रैदास की दृष्टि में क्षत्रिय वो हैं-
दीन-दुखी के हेत जउ वारै अपने प्रान, ‘रैदास’ उह नर सूर कौ, साँचा छत्री जान
रैदास की दृष्टि में वैश्य वो हैं-
रैदास वैस सोई जानिये, जउ सतकार कमाय,
पून कमाई सदा लहै, लौटे सर्वत सुखाय
साँची हाटी बैठि करि, सौदा साँचा देई,
तकड़ी तौले साँच की, रैदास वैस है सोई
रैदास की दृष्टि में शूद्र वो हैं-
रैदास जउ अति अपवित, सोई सूदर जान, जउ कुकरमी असुधजन, तिन्ह ही सूदर मान।
दलित अस्मिता विमर्शकार
मध्यकालीन काल खंड में जहाँ शूद्रों और दलितों को पाप योनि कहकर हीनता बोध से भर दिया जाता था। दलित, शूद्र जातियों को गालियों के बतौर इस्तेमाल किया जाता है। सवर्ण भाषा में कथित निम्न जातियों के लिए अपमान सूचक मुहावरे गढ़े गए। रैदास न सिर्फ़ उस ब्राह्मणवादी भाषिक संस्कृति के खिलाफ़ संघर्ष करते हैं बल्कि उसके विरुद्ध एक अवर्ण भाषिक संस्कृति निर्मित करते हैं जिसमें वो लगातार अपनी जाति को डंके की चोट पर पूरे आत्म सम्मान के साथ गाते बजाते थे। रैदास जाति से चर्मकार थे और और अपने काम व जाति को लेकर उनके मन में कोई कुंठा या ग्लानि नहीं थी तभी तो उन्होंने अपनी वाणी में भी बार-बार स्वयं को चमार उद्घोषित करते हुए लिखा है-
नागर जनाँ मेरी जाति विखियात चमार
रिदै राम गोविंद गुन सार
कह रैदास खलास चमारा
जो सहरू सो मीतु हमारा
मेरी जाति कमीनी पॉति कमीनी ओच्छा जनमु हमारा
तुम सरना गति राजा रामचंद्र कहि रैदास चमार
जबकि सवर्ण समाज चमारों से अछूत मानता और घृणा करता था, क्योंकि इस जाति के लोग मृत पशुओं को ढोने, उनकी खाल निकालकर जूता बनाने जैसा सृजन का काम करते थे, और उन मृत पशुओं का मांस भी खाते थे। अपनी वाणी में रैदास ने अपने परिवार के लोगों का बनारस के आसपास मृत पशुओं को ढोने का उल्लेख कुछ इस तरह किया है-
मेरी जाति कुटवांढला ढोर ढोवन्ता
नितहि बनारसी आस-पासा
जाके कुटुंब के ढेढ सभ ढोर ढोढ़त
फिरहि बनारसी आस-पासा
आचार सहित विप्र कराहिं डंडउति
तिन तैन रविदास दासान दासा
समाजवादी सोच और एक समतामूलक नगर की परिकल्पना
ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिलै सबन को अन्न
छोट बड़ो सब सम बसै, रैदास रहै प्रसन्न
ऐसे मानवीय, संवेदनीय और समतामूलक राज व शहर की आकांक्षा वही कर सकता है जिसे जीवन मूल्यों की अनुभूतिपरक गहरी समझ हो। हर विचार, व्यवहार और दर्शन के ऊपर जीवन को स्वीकृति देने वाला ही भूख की पीड़ा को समझ सकता है और वहीं सभी व्यक्तियों के लिए अन्न की उपलब्धता की बात कर सकता है।
रैदास के समकालीन कबीर भी अपने समय की समाजिक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था का विरोध करते करते एक नए देश की कल्पना करते हैं। लेकिन चूंकि कबीर के यहां जीवन का स्वीकार नहीं है इसलिए उनकी कल्पना के नगर में सबके लिए अन्न की उपलब्धता की बात भी नहीं है। कबीर वर्ण, धर्म, त्रिदेवविहीन समतामूल्क देश की कल्पना तो करते हैं साथ ही वो जीवन से भी मुक्ति की बात करते हैं। वो वर्णवादी समाजिक व्यवस्था के उलट समतामूलक होने के साथ साथ भाववादी भी है-
जहवां से आयो अमर वह देसवा
पानी न पान धरती अकसवा, चाँद न सूर न रैन दिवसवा।
बाम्हन छत्री न सूद्र बैसवा, मुगल पठान न सैयद सेखवा
आदि जोत, नहिं गौर गनेसवा,ब्रह्म बिसनु महेस न सेसवा
जोगी न जंगम मुनि दुरबेसवा आदि न अंन न काल कलेसवा
दास कबीर के आए संदेसवा, सार सबद गहि चलौ वहि देसवा
जबकि रैदास अपने समय की यातनादायी व्यवस्था से मुक्ति की तलाश करते हुए एक दुःखविहीन नगर समाज की कल्पना करते है, उनके इस काल्पनिक नगर का नाम बेग़मपुरा है। बेग़मपुरा में ऊंच-नीच, अमीर-गरीब और छूतछात का भेद नहीं है। कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, यहां कोई संपत्ति का मालिक नहीं है। कोई अन्याय, कोई चिंता, कोई आतंक और कोई धार्मिक, राजनीतिक समाजिक यातना नहीं है। रैदास एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, जहां संपत्ति पर निजी मालिकाना नहीं होगा, समाज अमीर और गरीब में बंटा नहीं होगा, कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं होगा और न ही वहां कोई छूत-अछूत होगा। अपने इस देश समाज का नाम बेग़मपुरा उन्होंने किसी स्त्री के नाम पर दिया है, या इसका अर्थ बिना ग़म यानी बिना दुख के अधार पर दिया गया है, कुछ कह नहीं सकते पर दोनों ही स्थितियों में ये सार्थक नाम है। रैदास अपने बेग़मपुरा शहर के बाबत लिखते हैं-
बेगमपुरा सहर को नाउ, दुखु-अंदोहु नहीं तिहि ठाउ
ना तसवीस खिराजु न मालु, खउफु न खता न तरसु जुवालु
अब मोहि खूब बतन गह पाई, ऊहां खैरि सदा मेरे भाई
काइमु-दाइमु सदा पातिसाही, दोम न सोम एक सो आही
आबादानु सदा मसहूर, ऊहाँ गनी बसहि मामूर
तिउ तिउ सैल करहि जिउ भावै, महरम महल न को अटकावै
कह ‘रविदास’ खालस चमारा, जो हम सहरी सु मीतु हमारा
समकालीन होकर भी कबीर से अलग भाषा, स्वर
रैदास और कबीर न सिर्फ़ समकालीन और गुरुभाई थे वरन् अपने समय की सामाजिक-राजनीति और धार्मिक अर्थनीति में निहित पक्षपाती दमनकारी व्यवस्था का भंडाफोड़ कर अपने समय के समाज को ज्ञान, तर्क विवेक और प्रतिरोध की मशाल दिखाने वाले युग-प्रवर्तक थे। कबीर की ही तरह रैदास ने भी लोक-बोलियों को अपनी अभिव्यक्ति की भाषा बनाई। रैदास की काव्यभाषा बोल-चाल की ब्रजभाषा है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू-फ़ारसी के शब्दों का भी समावेश है।
कबीर जहाँ धार्मिक विसंगतियों पर बोलते हुए बहुत आक्रामक होकर भाषा में हमलावर रुख़ इख़्तियार कर लेते हैं-
चली कुल बोरनी गंगा नहाय
तो वहीं रैदास इसी बात को आग्रहपूर्वक सौम्य सहज भाषा में कहते हुए मन को ही गंगा तीरथ बना देते हैं कि-
मन चंगा तो कठौती में गंगा
स्त्री के लिए समकालीनों से अलग जीवन दृष्टि
रैदास के समकालीन जहां स्त्री को सती माता कहकर गुणगान या माया महाठगिनी कहकर स्त्री की छाया तक से पीछा छुड़ाने की बात कह रहे थे, रैदास झाली रानी और मीराबाई को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करते हैं और स्त्री को अधिकार और सम्मान देने की बात कहते हैं। उनके समकालीनों में किसी भी कवि की दृष्टि स्त्री के प्रति उतनी उदार और मानवीय नहीं है जितनी की रैदास की है। तभी तो अपने समय के समाज के तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए मीरा और झाली रानी रैदास का शिशत्व ग्रहण करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार करती हैं।
ख़ुद मीराबाई कई दोहों में रैदास का गुणगान लिखती हैं-
खोज फिरूं खोज वा घर को, कोई न करत बखानी
सतगुरु संत मिले रैदासा, दीन्ही सुरत सहदानी
वन पर्वत तीरथ देवालय, ढूंढा चहूँ दिशि दौर
मीरा श्री रैदास शरण बिन, भगवान और न ठौर
मीरा म्हाने संत है, मैं सन्ता री दास
चेतन सता सेन ये, दासत गुरु रैदास
मीरा सतगुरु देव की, कर बंदना आस
जिन चेतन आतम कह्या, धन भगवान रैदास
गुरु रैदास मिले मोहि पूरे, धुर से कलम भिड़ी
सतगुरु सैन दई जब आके, ज्याति से ज्योत मिलि
मेरे तो गिरीधर गोपाल दूसरा न कोय
गुरु हमारे रैदास जी सरनन चित सोय
कबीर जीवन के अस्वीकार के कवि हैं इसीलिए स्त्री-पुरुष संबंध पर लिखते हुए कबीर घोर स्त्री विरोधी स्वर में लिखते बोलते हैं कि स्त्री बुद्धि-विवेक हर लेती है-
नारी सेती नेह, बुधि विवेक सभी हरै
बृथा गबावै देह, कारज कोई ना सरै
वहीं रैदास पांचों इंद्रियों को अपनी सखी-सहेली बताते हुए लिखते हैं कि इंद्रियां मेरी सखी सहेली बन गई हैं और उन्होंने मुझे असली निधि को बता दिया है। अब मैं इस संसार में रहकर ही प्रसन्न रहता हूँ, और वह भी मेरे भीतर समा गया है। अब वह मुझे सहज रूप में सम्मुख दिखता है।
पंचू मेरी सखी सहेली, तिनि निधि दई दिखाई
अब मन फूलि भयौ जग महियां, उलटि आप मैं समाई
कबीर समेत दूसरे समकालीनों के यहाँ, जहाँ स्त्री और स्त्री की यौनिकता को ईश्वर प्राप्ति में बाधा बताया गया है ये कहकर कि कामिनी का प्रेम नर्क मिलता है-
कबीर नारी की प्रीति से, केते गये गरंत
केटे और जाहिंगे, नरक हसंत हसंत
वहीं रैदास स्त्री की सेक्सुअलिटी को भक्ति के रूपक के तौर पर गढ़ते हुए भक्ति को जीवनधर्मी बनाने की वकालत करते हैं-
सह की सार सुहागनी जानै, तजि अभिमानु सुख रलीआ मानै
तनु मनु देइ न अंतरु राखै, अवरा देखि न सुनै अभाखै
(जनचौक के विशेष संवाददाता सुशील मानव का लेख।)







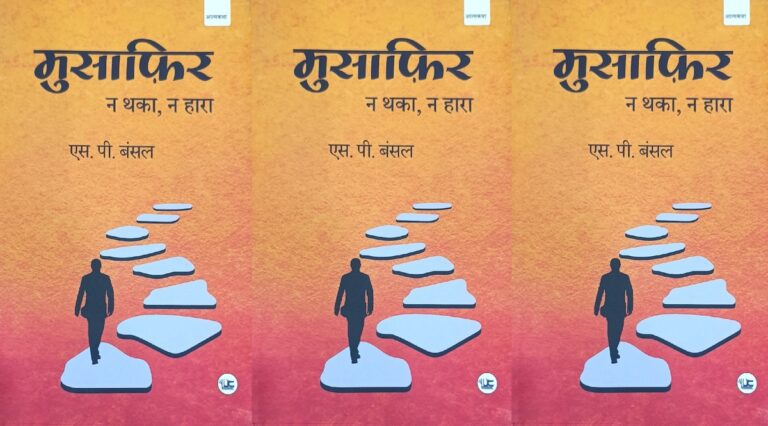


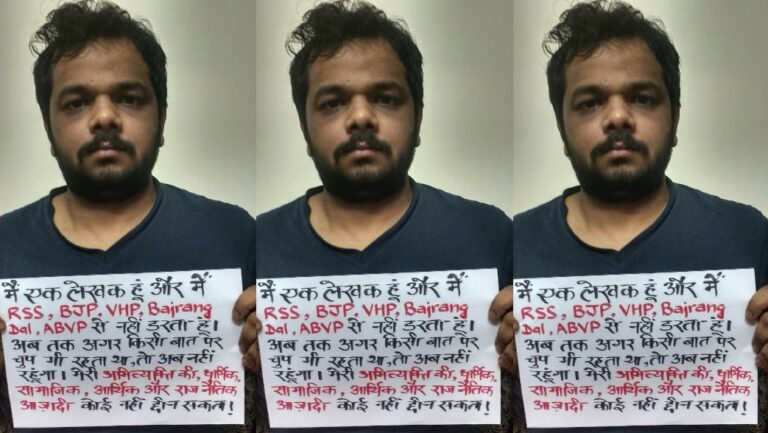



जीवन चारि दिवस का मेला रे
बांभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे
मंदिर भीतर मूरति बैठी, पूजति बाहर चेला रे
लड्डू भोग चढावति जनता, मूरति के ढिंग केला रे
पत्थर मूरति कछु न खाती, खाते बांभन चेला रे
जनता लूटति बांभन सारे, प्रभु जी देति न धेला रे
पुन्य पाप या पुनर्जन्म का, बांभन दीन्हा खेला रे
स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे
जितना दान देव गे जैसा, वैसा निकरै तेला रे
बांभन जाति सभी बहकावे, जन्ह तंह मचै बबेला रे
छोड़ि के बांभन आ संग मेरे, कह विद्रोहि अकेला रे
कृपा इन पंक्तियों का अर्थ समझाये ।
जीवन चारि दिवस का मेला रे
बांभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे
मंदिर भीतर मूरति बैठी, पूजति बाहर चेला रे
लड्डू भोग चढावति जनता, मूरति के ढिंग केला रे
पत्थर मूरति कछु न खाती, खाते बांभन चेला रे
जनता लूटति बांभन सारे, प्रभु जी देति न धेला रे
पुन्य पाप या पुनर्जन्म का, बांभन दीन्हा खेला रे
स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे
जितना दान देव गे जैसा, वैसा निकरै तेला रे
बांभन जाति सभी बहकावे, जन्ह तंह मचै बबेला रे
छोड़ि के बांभन आ संग मेरे, कह विद्रोहि अकेला रे
कृपा इन पंक्तियों का अर्थ समझाये ।