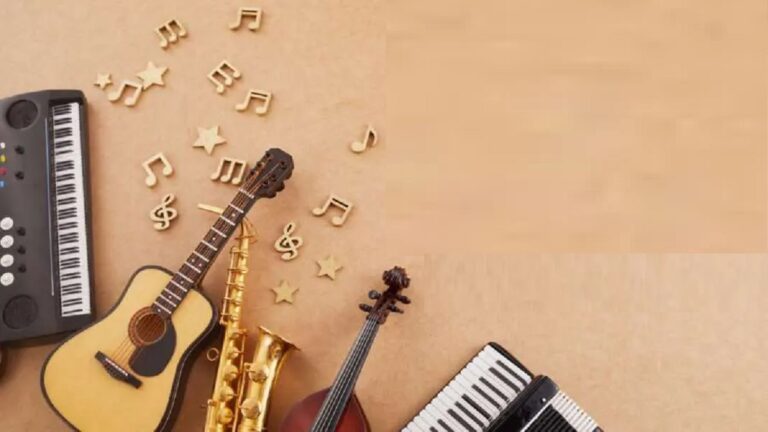उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में जेल कार्य आवंटन में जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह फैसला द वायर की पत्रकार सुकन्या शांथा द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय को पलट दिया गया, जिसमें जेल के कैदियों को जाति के आधार पर अलग करने की बात कही गई थी।
यह मामला सी. अरुल बनाम सरकार के सचिव (2014) से जुड़ा हुआ है, जिसमें याचिका में यह प्रार्थना की गई थी कि कैदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाए और जेल प्रशासन को पालयमकोट्टई जेल के कैदियों को जाति के आधार पर विभाजित करने से रोका जाए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
सी. अरुल मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने राज्य के उस विश्लेषण पर विचार किया था, जिसमें कहा गया था कि “कैदियों को विभिन्न जातियों के आधार पर अलग-अलग ब्लॉकों में रखा जाता है, ताकि तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन जिलों में आम तौर पर होने वाली सामुदायिक झड़पों से बचा जा सके।”
भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने उच्च न्यायालय द्वारा समर्थित इस तर्क का संज्ञान लिया और कहा कि “यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह जेल परिसर के भीतर अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखे, ताकि बिना जाति-आधारित अलगाव जैसे चरम उपायों का सहारा लिए कोई अप्रिय घटना न हो।”
‘अलग लेकिन समान’ (separate but equal) का सिद्धांत
उच्चतम न्यायालय ने जाति के मामले में ‘अलग लेकिन समान’ के तर्क की निंदा की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव का औचित्य था।
यह सिद्धांत यह तर्क देता था कि जब तक अलगाव कानून गोरे और अश्वेत लोगों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, तब तक ये कानून अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन नहीं करते, जो राज्यों को “अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करने” से रोकता है।
व्यवहार में, “अलग लेकिन समान” एक छलावा था; अश्वेत नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की थी। इस सिद्धांत को अंततः अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 1954 में ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ टोपीका मामले में पलट दिया।
‘अलग लेकिन समान’ वाक्यांश का मूल लुइसियाना के ‘सेपरेट कार एक्ट 1890’ से है। यह कानून राज्य में संचालित सभी रेलगाड़ियों को अश्वेत और श्वेत यात्रियों के लिए अलग-अलग डिब्बे प्रदान करने की आवश्यकता थी।
मिश्रित नस्ल के होमर प्लेसी ने इस कानून को चुनौती दी और श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका मानना था कि मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचेगा और वे इस भेदभावपूर्ण कानून को निरस्त करवा पाएंगे।
लेकिन उनका यह प्रयास विफल हो गया और अदालत ने कानून की वैधता को बरकरार रखते हुए उनकी गिरफ्तारी को कानूनी ठहराया।
विभिन्न जेल मैनुअल का अध्ययन
न्यायालय ने राजस्थान जेल मैनुअल के दो प्रमुख नियमों, नियम 37 और नियम 67 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है, “सभी शौचालयों में ठोस और तरल मल-मूत्र के लिए अलग-अलग पात्र प्रदान किए जाएंगे, और उनका उपयोग सभी कैदियों को अच्छी तरह से समझाया जाएगा।
मेहतर ठोस मल के लिए प्रत्येक पात्र में कम से कम 1 इंच मोटी सूखी मिट्टी की परत डालेंगे, और प्रत्येक कैदी पात्र का उपयोग करने के बाद अपने मल को एक स्कूप सूखी मिट्टी से ढक देगा। मूत्र पात्रों को एक तिहाई पानी से भरा जाएगा।”
नियम 67 में कहा गया है, “रसोइये गैर-आदतन वर्ग के होंगे। इस वर्ग के किसी भी ब्राह्मण या पर्याप्त उच्च जाति के हिंदू कैदी को रसोइया नियुक्त करने के लिए पात्र माना जाएगा।”
ये दोनों नियम भारतीय समाज में व्याप्त वास्तविक जाति आधारित विभाजन को दर्शाते हैं, जहां समाज जातिगत भेदभाव की मोटी रेखा से चलता है।
बौद्धिक भेदभाव
न्यायालय ने यह भी देखा कि जेल कार्य में जाति आधारित भेदभाव को ‘बौद्धिक भेदभाव’ या ‘उचित वर्गीकरण’ नहीं माना जा सकता है।
यह अधिनियम अनुच्छेद 15 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है, जो कहता है, “राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।” यह अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का भी उल्लंघन है।
बौद्धिक भेदभाव के मामले में, यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि समान लक्षणों वाले व्यक्तियों के एक विशेष समूह का निर्माण किया जाता है। इस वर्गीकरण का एक तार्किक संबंध होना चाहिए जो उसके निर्माण के आधार को स्पष्ट करे, जिसे देश ढूंढना चाहता है।
जैसे कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, केवल कामकाजी महिलाओं के लिए उपलब्ध है लेकिन सभी महिलाओं के लिए नहीं। यह लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए आवश्यक है ताकि वे अपेक्षित बच्चे की उचित देखभाल कर सकें, जो आवश्यक भी है।
भारत जैसे देश में इस नियम का महत्व बहुत स्पष्ट है, जहां लोग एक-दूसरे से बहुत भिन्न तरीकों से रहते हैं। उचित भेदभाव की अनुमति है। यदि भेदभाव का आधार न्यायसंगत, तार्किक और उचित है, तो ऐसे भेदभाव को समाज के लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है।
वर्गीकरण का सिद्धांत विधायिका को कानून बनाने की अनुमति देता है। विधायिका कानून बनाते समय सामाजिक असमानताओं और विभिन्न समुदायों के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली अन्य चुनौतियों को ध्यान में रखती है।
यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि उन समुदायों को अवसर दिया जाए जो पीड़ित हैं और जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है, न कि समाज के भीतर की खाई को भरने के लिए।
निष्कर्ष
यह ध्यान में रखते हुए कि जेल वर्तमान में प्रचलित उत्पादन के तरीके के एक प्रतिबिंब और सुपर-स्ट्रक्चरल पहलू का प्रतिनिधित्व करती है।
अपराधी मैनुअल में प्रगतिशील रूप से बदलाव करना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह जेलों में या कानूनी व्यवस्था में जातिगत भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि सामंती व्यवस्था की जड़ें पूरी तरह समाप्त नहीं हो जातीं।
इसके लिए राज्य की इच्छा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि न्यायालय के प्रयास। यह उस कल्पनाशील वास्तविकता को स्वीकार करना कठिन है, जहां अधिकांश राजनीतिक आर्थिक निर्णय जाति के आधार पर लिए जाते हैं, और यह उम्मीद करना मुश्किल है कि वे समाज के ‘कार्य करने वाले मैनुअल’ को बदलने की कोई इच्छा दिखाएंगे।
(निशांत आनंद दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के छात्र हैं)