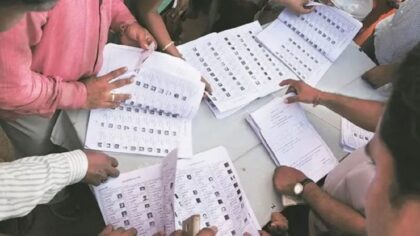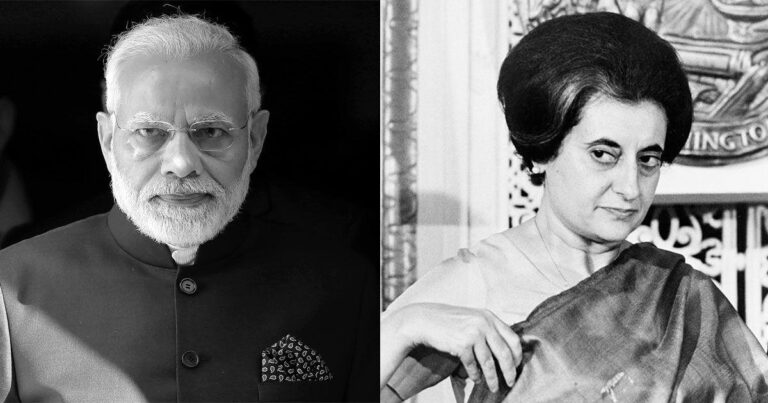तय कार्यक्रम के अनुसार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस लिहाज से 22 जनवरी 2024 का दिन भारत में कई दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्त्व का होने जा रहा है। एक लंबे विवाद, उफान और आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो रहा है। विवाद और असंतोष को दरकिनार करते हुए सभी पक्षों ने अदालत के फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया।
विवाद और असंतोष राजनीति के दो पांव हैं। राजनीति इन्हीं दो पांवों के सहारे अपना सफर तय करती है। यह मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल विवाद और असंतोष को हवा देने से बाज नहीं आ रहा है। यह हवा लपक कर संसदीय लोकतंत्र की मान्य पद्धतियों पर और बिल्कुल सामने उपस्थित आम चुनाव पर भी असर डाल रही है।
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भारत के राजनीतिक दलों को रामभक्त और रामद्रोही के दो खांचों में रखकर देखने-दिखाने में लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व अपने हर राजनीतिक विरोधी को रामद्रोही के खांचे में डालकर आम नागरिकों के सामने पेश कर देती है। इतना ही नहीं, इसी रौ में सभी विरोधी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रामद्रोही, देश विरोधी, भ्रष्टाचारी और न जाने क्या-क्या होने का हल्ला, हंगामा खड़ी करती रहती है।
वहीं अपने साथ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नेताओं को उनके कुकृत्यों और अपराधों को कानूनी प्रावधानों की दंडात्मक कार्रवाइयों से बिना किसी लोक-लाज और संकोच के बचाती रहती है।
भगवान क्षमाशील होते हैं। शरणागत के पाप दूर करते हैं। दंड से बचाते हैं। यह सहज भक्ति का गुण और उसका सांस्कृतिक प्रभाव है। इसका राजनीतिक गुण और प्रभाव का फलितार्थ यह है कि जो शरणागत का पाप धो डाले और दंड से बचा ले वही भगवान है।
कहां संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के प्रधानमंत्री, डॉ मनमोहन सिंह का वह दौर, जब उन आरोपों पर मंत्री भी जेल चले गये जिन आरोपों पर आज तक अदालतों में कुछ नहीं निकला! कहां प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी का ‘बंद लिफाफों’ और ‘खुले आम सब कुछ’ का यह दौर! दोनों में अंतर तो है न! साधारण मनुष्य और अवतारी पुरुष होने का अंतर।
लोग लोकतंत्र के कारोबार के लिए 2024 के आम चुनाव में क्या करते हैं, फिर ‘भगवान’ को ही चुनते हैं या साधारण मनुष्य को, देखना दिलचस्प होगा। जहां तक, राम की बात है तो विरोध भगवान राम का नहीं, भगवान राम को कब्जे में लेने के कुप्रयास का विरोध तो सदा रहा है। इस देश में ‘हिंदू तुरक’ हर किसी के हैं राम। शासक मुसलमान, साधक जुलाहा। किसका दबाव जो, ‘कहै कबीर एक राम जपहु रे, हिंदू तुरक न कोई’।
कबीर सावधान भी करते हैं कि सिर्फ राम का नाम जपना पर्याप्त नहीं है, वे कहते हैं, ‘पंडित बाद बदैं ते झूठा। रांम कह्यां दुनियां गति पावै, खांड कह्यां मुख मीठा॥’ भक्ति, धर्म, प्रथा, पुरोहित, झूठ-सच आदि को अपनी जगह ससम्मान रहने दें, ताकि राजनीति, कानून, संविधान, लोकतंत्र, आदि अपनी जगह विधिवत काम करते रह सकें।
एक बात तय है कि 2024 का आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्त्व का है। संकेत सकारात्मक नहीं हैं। असल में लोकतंत्र की प्राण-शिराएं इसकी संस्थाओं की लोकतांत्रिक सक्रियताओं में रहती हैं। इस समय संस्थाओं की लोकतांत्रिक सक्रियताएं अपनी विश्वसनीयता के न्यूनतम स्तर पर है।
अन्य संस्थाओं की बात रहने भी दें तो केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका पर तो बात करनी ही होगी, क्योंकि भय मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव संपन्न होना बहुत जरूरी है। यह साफ दिखता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता भय मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी वातावरण बनाने में नहीं है।
इधर, इवीएम को लेकर भी तरह-तरह की शंकाएं खड़ी हो गई हैं। ये शंकाएं कितनी वास्तविक हैं, कितनी कल्पित या दुर्भावना प्रेरित यह साबित करना केंद्रीय चुनाव आयोग का प्राथमिक दायित्व है। इवीएम का थोड़ा-सा भी संदेहास्पद बना रहना भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता को पूरी तरह ध्वस्त कर दे सकता है। इस तरह की शंकाओं के सिर्फ घोषणाओं और अधिसूचनाओं आदि से दूर नहीं किया जा सकता है।
शंका करने वाले नागरिकों की आवाज को किसी भी तरह से दबा देना या दबाव में लाकर खामोश कर देने से मतदाताओं का विश्वास नहीं जीता जा सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग क्या करता है, देखना और इंतजार करना जरूरी है। चुनाव में धांधली तो धांधली, धांधली की जरा-सी आशंका भी लोकतंत्र के प्रति आस्था को तोड़कर रख देगी।
किसी भी हाल में इन आशंकाओं को पूरी तरह से निर्मूल किये बिना चुनावों में इवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो, पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख पर बट्टा लग जाने का खतरा है, यह किसी के लिए शुभ नहीं हो सकता है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, अटल विहारी बाजपेयी के इस कथन की याद आ रही है कि सत्ता आयेगी, जायेगी, देश बना रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए, लोकतंत्र बना रहेगा।
समस्याएं और भी हैं। लोकतंत्र पर ठहर कर विचार किये जाने की जरूरत है, उत्तेजना और उन्माद के इस्तेमाल के प्रभाव से बने आक्रामक वातावरण में निष्पक्ष चुनाव की आशा नहीं की जा सकती है। विचार के लिए उत्तेजना और उन्माद से अधिक खतरनाक और कुछ हो नहीं सकता है। लोकतंत्र विचारों से चलता है। विचार संवाद से बनते हैं। जितने तरह के संवाद उतने तरह के विचार बनते चलते हैं। जितने तरह के विचार उतने तरह के लोकतंत्र।
दुनिया में तरह-तरह के विचार हैं, इसलिए तरह-तरह के लोकतंत्र हैं। विचार नित्य होते हैं, विचारधाराएं समय-समय पर रणनीतिक एवं अन्य कारणों से भी बदलती रहती हैं। विचारधाराओं के साथ लोकतंत्र का स्वरूप भी बदलता रहता है। जब लोकतंत्र पर किसी एक विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल की कट्टरताओं का कब्जा होता है तो वह किसी भी तरह से लोकतंत्र पर अपने कब्जा को बनाये रखने के लिए हर स्तर पर अन्य और इतर विचारधाराओं का विरोध करता है।
यहीं से लोकतंत्र में विवेकहीन सर्वाधिकारवादी तानाशाही शासन का आरंभ होता है; यहीं से अन्य एवं इतर विचारधाराओं के विरोध के लिए, संवाद और विचार की स्वायत्त प्रक्रिया के बाधित होने की भी शुरुआत होती है। निःशर्त संवाद के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने-आप में शर्त होती है। संवाद और विचार की स्वतःस्फूर्त्त एवं स्वायत्त प्रक्रिया को रोकने के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डर का माहौल बनाया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त होने की हद तक सीमित कर दिया जाता है।
अभिव्यक्ति मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति है, जैसे भूख, नींद आदि। अभिव्यक्ति की आकांक्षा और अकुलाहट को समाप्त नहीं किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है यहां तक कि भटकाव के अन्य तरीके से इसे संतुष्ट भी किया जा सकता है। संवाद को भटकावों और निरर्थकताओं के इतर प्रसंगों से जोड़ दिया जाना और निरंतर जोड़े रहना, अभिव्यक्ति की आकांक्षा और अकुलाहट को संतुष्ट करने का ही एक तरीका है।
आज की राजनीति में दलीय कोलाहलों के बीच विचारधारा का संघर्ष जोरों से जारी दिखता है। जो दिखता है, और जैसा दिखता है, अक्सर वह वैसा ही और वही होता नहीं है। यह विचारधाराओं के बीच का संघर्ष होता तो इसका रूप दूसरा होता; असल में यह भावधाराओं के बीच का झकमझोल है, जिसमें लोकतंत्र उलझ-पुलझकर छटपटा रहा है।
इंडिया (I.N.D.A – इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इनक्लुसिव अलायंस) और खासकर राहुल गांधी बार-बार विचारधाराओं के बीच संघर्ष की बात कह रहे हैं। भावधारा नैसर्गिक और सांस्कृतिक होती हैं, विचारधारा अर्जित और वैचारिक होती हैं। विचारधाराएं भावधाराओं से नहीं निपट सकती हैं। विचारधारा की उपयुक्तता का मूल्यांकन मतदान से संभव नहीं हो सकता है।
मतदान एकाधिक विकल्प में से किसी एक के चयन का जरिया होता है, इसे मूल्यांकन का जरिया नहीं माना जा सकता है। प्रसंगवश, माता-पिता, भाई-बहन, जाति-धर्म, पूण्य-भूमि आदि बहुतेरे ऐसे प्रसंग हैं, जिनके लिए लोग जीते-मरते रहते हैं, उनके चयन में उन लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। समुदाय और समूह में विचारधारा नहीं भावधारा अधिक सक्रिय रहती है।
जीवन को बचाने का प्रयास हर किसी को करना चाहिए। विचारधारा जो भी हो, भावधारा जैसी भी हो, जैसा भी हो मत, जो भी फैसला करें आप, देर बहुत हो गई है, और देर न हो! ‘बंद लिफाफों’ और ‘खुले आम सब कुछ’ के अमृत-काल में एक बार फिर निराला की यह कविता पढ़ लें-
‘जल्द-जल्द पैर बढ़ाओ,
आओ, आओ।
आज अमीरों की हवेली
किसानों की होगी पाठशाला,
धोबी, पासी, चमार, तेली
खोलेंगे अंधेरे का ताला,
एक पाठ पढ़ेंगे, टाट बिछाओ।
यहां जहां सेठ जी बैठे थे
बनिए की आंख दिखाते हुए,
उनके ऐंठाए ऐंठे थे
धोखे पर धोखा खाते हुए,
बैंक किसानों का खुलाओ।
सारी संपत्ति देश की हो,
सारी आपत्ति देश की बने,
जनता जातीय वेश की हो,
वाद से विवाद यह ठने,
कांटा कांटे से कढ़ाओ।’
(प्रफुल्ल कोलख्यान लेखक और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)