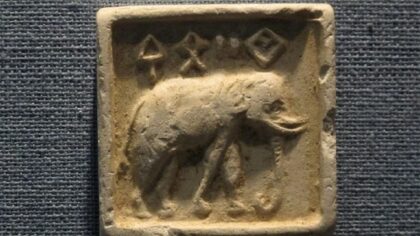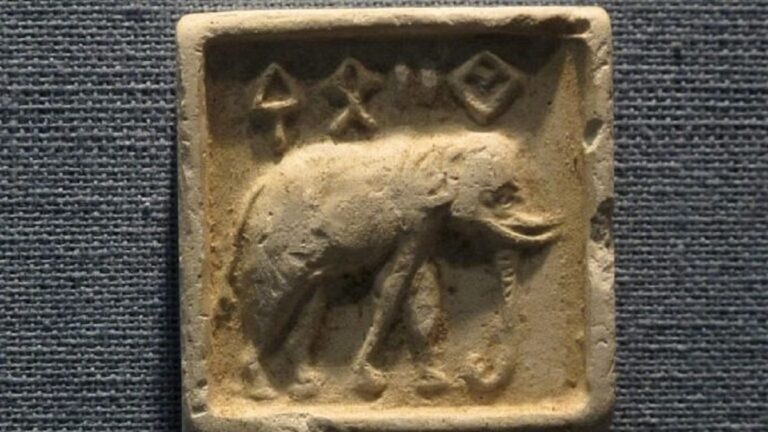लोकतंत्र चुनाव-दर-चुनाव भटकने वाली व्यवस्था नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति का चुनावी राजनीति में सिमटकर रह जाना लोकतंत्र को चुनाव-दर-चुनाव भटकने वाला बना देता है।
यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि राजनीतिक दलों के लिए लोकतंत्र का मूल मतलब चुनाव और सत्ता है, जनता के लिए चुनाव का मूल मतलब हर प्रकार के अन्याय से बचाव के साथ सभ्य और बेहतर सामाजिक और नागरिक जीवन।
चुनावी राजनीति से नेताओं को सत्ता मिल जाती है, जनता को वह नहीं मिलता है जिसकी उम्मीद में वह टकटकी लगाये रहती है। जनता के लिए लोकतंत्र का मतलब जीत के जश्न में झूमते नेताओं को वह मुंह बाए सुनना भर रह जाता है।
चुनावी राजनीति में फंसा भारत राजनीतिक के साथ-साथ भारी नैतिक-संकट से गुजर रहा है। राजनीतिक-संकट और नैतिक-संकट में अंतरावलंबी संबंध है। इस अंतरावलंबन की गुत्थियों को सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती है।
संकट की घड़ी में पुरखों की याद आती है। समस्याओं को सुलझाने के लिए पुरखे खुद नहीं आते हैं, पुरखे अपने सुझाव अपनी स्मृतियों के धागों में गांठ डालकर सुमति संपन्न संतति के पास छोड़ जाते हैं।
पुरखों की एक मात्र चाह होती है कि उनकी संतति का मन अटूट और एक रहे। मन का एक होना या रहना बहुत टेढ़ा मामला होता है। कबीर को एक रहने की बाधाओं का भरपूर एहसास था। समाज में सुलझाव-उलझाव की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है।
कह देना या अच्छी-अच्छी बात करना ही काफी होता तो ‘खांड कहने से ही मुंह मीठा हो जाता’! किसी-न-किसी हद तक भारत आब तक बड़ा नहीं भी तो छोटा ही सही, किसी-न-किसी कैटैगरी का ‘विश्व-गुरु’ जरूर बन गया होता!
महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन को नैतिक आनंद से जोड़कर आंदोलन को उत्सव में बदलने की कोशिश की, कहा जा सकता है कि कुछ हद तक सफल कोशिश की थी। आंदोलन को उत्सव में बदलना कभी-कभी जरूरी हो जाता है।
आंदोलन को उत्सव में बदलना बहुत आसान नहीं तो उतना मुश्किल भी नहीं होता है। लेकिन उत्सव को आंदोलन में बदलना! बहुत मुश्किल, लगभग अ-संभव ही होता है।
आंदोलन किसी-न-किसी दुख से उत्पन्न होता है। आंदोलन दुख को आनंद में बदलते हुए अंततः आंदोलन को उत्सव में बदल देता है। बाद में लोग उत्सव से आनंद तत्व के चुक जाने के बावजूद उत्सव की परंपरा में बहते रहते हैं। या फिर परंपरा को ढोते रहते हैं।
उत्सव तत्काल मजा से जुड़कर लोगों को संतुष्ट करता रहता है। लगता है यही संतोष उत्सव को आंदोलन में बदलने से रोक लेता है।
वाम-पंथ से जुड़े नेताओं ने आजादी के आंदोलन के नैतिक आक्रोश को क्रांति से जोड़ने की जबरदस्त कोशिश की। एक हद तक कोशिश सफल भी हुई, लेकिन एक ही हद तक। बाबासाहेब ने आजादी के आंदोलन को ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद की अनैतिकता के विरुद्ध समाज-आर्थिक नैतिकता से जोड़ने की कोशिश की।
आंदोलन और उत्सव की अदल-बदल की प्रक्रिया पर अलग से बात की जा सकती है। आज की समस्याओं से परेशान लोगों को आजादी के आंदोलन के दौरान हुए पुरखों के इन अनुभवों को जरूर याद करना चाहिए।
जो भी हो, एक बात तय है कि आजादी के आंदोलन के दौर में विचारधारा और वक्तव्य, जो भी उभरकर आया उन सभी में उन्नत सामाजिक स्वप्न की प्रेरणा जरूर थी। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि अपने ढंग का उन्नत सामाजिक स्वप्न तो विचारधारा-हीन बकवास में भी था। लेकिन इतना कहना काफी नहीं है।
महात्मा गांधी भारत की राजनीति में प्रवेश के पहले 1894 में स्थापित नेटाल इंडियन कांग्रेस के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय को राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया।
जनवरी 1897 में भारत से वापसी पर अपने ऊपर हुए हमले में किसी को भी आरोपी बनाने से इनकार कर महात्मा गांधी ने राजनीतिक आंदोलन में नैतिक तत्व को समाविष्ट कर एक नये राजनीतिक औजार की खोज कर ली।
अपनी गलत नीतियों का औचित्य प्रमाणित करने के लिए शासकों के द्वारा अदालत के इस्तेमाल की चालाकी की अनैतिकता को गांधी ने ठीक-ठीक चिह्नित कर लिया था।
‘आंदोलन के खिलाफ अदालत’ के इस्तेमाल को विधिवेत्ता के रूप में महात्मा गांधी ने सविनय समझ लिया था। महात्मा गांधी ने नैतिकता, जिसकी अभिव्यक्ति वे मुख्य रूप से सत्य और अहिंसा के रूप में करते थे, को अपना सब से बड़ा राजनीतिक औजार बना लिया।
गांधी-विचार, बाबासाहेब के विचार, वाम-विचार, समाजवादी-विचार आदि में नैतिकता की समझ भिन्न-भिन्न पृष्ठ-भूमि से बनी थी। जाहिर है कि नैतिकता से उनका आशय भी भिन्न था, कहा जा सकता है कि भिन्न होकर भी अभिन्न था, इसलिए किसी भी रूप में एक दूसरे का विरोधी तो बिल्कुल नहीं था।
भारत के समाज में नैतिकता की एक ‘आध्यात्मिक दृष्टि’ भी सक्रिय थी। वाम-विचार और बाबासाहेब की नैतिक-दृष्टि का इससे सीधा टकराव था, लेकिन महात्मा गांधी की राजनीतिक नैतिकता में उस ‘आध्यात्मिक दृष्टि’ के लिए भी थोड़ी-बहुत जगह तो थी ही।
यह महात्मा गांधी ही कर सकते थे कि आंबेडकर से टकराव में गये बिना सार्वजनिक रूप से आंबेडकर को ‘हिंदुत्व’ के लिए खतरा बता सकते थे। समझना ही होगा कि महात्मा गांधी ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचार को ‘हिंदुत्व’ के लिए खतरा बताया था, देश के लिए उपयुक्त मानने से इनकार नहीं किया था।
आजादी हासिल होने के इतने दिन बाद लोकतंत्र के सामने आजादी के आंदोलन की नैतिक-दृष्टि को विखंडित करती राजनीति के बढ़े वर्चस्व के खतरों को देखकर एक सवाल किसी को भी बेचैन कर सकता है कि ऐसा आखिर कैसे हुआ! ठीक-ठीक कुछ भी कहना आसान नहीं है, लेकिन लगता है कि आदर्शवादी, सही और प्रगतिशील लोगों के साथ एक समस्या होती है।
इस समस्या का संबंध इस प्रवृत्ति से है जिस के चलते आदर्शवादी, सही और प्रगतिशील लोग अपने बाहरी और भीतरी संदर्भों में अपने ‘सही दृष्टि-कोण’ की जांच-परख करना, कम-से-कम ऐसा करते हुए दिखना लगभग बंद कर लेते हैं। वे अपने हर निर्णय-बोध को निर्णायक तौर पर ‘आदर्शवादी, सही और प्रगतिशील’ मान लिया करते हैं।
सामान्य रूप से हर व्यक्ति कहीं-न-कहीं अपने दृष्टि-कोण को सही मान कर ही चलता है। दूसरा कोई व्यक्ति जिसे वह आदर्शवादी, सही और प्रगतिशील मानता है वह भी जब आक्रामक ढंग से उस के दृष्टि-कोण में बदलाव की कोशिश करता है तो उसकी आत्मा संत्रस्त अर्थात अपने प्रति संशय-ग्रस्त हो जाती है।
आदर्शवादी, सही और प्रगतिशील लोगों में अपने मत को दृढ़तापूर्वक निर्णायक मानने-मनवाने की आक्रामक प्रवृत्ति होती है। मनुष्य का ही नहीं, प्राणी मात्र का मूल स्वभाव किसी भी तरह के आक्रमण के विरोध का होता है। भले ही वह जिसे आक्रमण समझ रहा होता है, उसमें आत्यंतिक उसके हित की आकांक्षा ही क्यों न अंतर्निहित हो।
आदर्शवादी, सही और प्रगतिशील दृष्टि-कोणवालों की दृष्टि का आक्रामक कोण दूसरों की दृष्टि में भयानक तरीके से चुभ जाता है। अकसर आदर्शवादी, सही और प्रगतिशील लोगों के मत और विचार के प्रति साधारण लोगों की आंतरिक सहमति और स्वीकृति हासिल करना बहुत मुश्किल होता है।
लोकतंत्र का वास्तविक वैभव इसी साधारण आदमी के मताधिकार की ‘गुदड़ी’ में छिपा होता है।
सृष्टि की संरचना पर गौर किया जाये तो किसी एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व के विरुद्ध जीत का जश्न लगेगा। ‘एक’ और ‘अनेक’ के बीच रिश्ता का यह खुला रहस्य सभ्यता के आवरण में छिपा रहता है। कहने का आशय यह है कि एक के जीत के जश्न से दूसरे के अस्तित्व को हमेशा चुनौती मिलती रहती है।
इसलिए मनुष्य की सामाजिकता के बचाव की दृष्टि से सहिष्णुता और सह-अस्तित्व का स्व-परिभाषित महत्व है। सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की भावना और बुद्धिमत्ता मिलकर ‘जीत के जश्न’ और ‘हार की हताशा’ पर नियंत्रण का हर उपाय करती है।
हर-बार ‘हार की समीक्षा’ की सकारात्मक और विश्वसनीय-सी व्याख्या यही होती है कि अगली बारी, हमारी है। सह-अस्तित्व और सहिष्णुता का दामन छूट जाये तो ‘अस्थाई चुनावी जीत-हार’ बिना किसी देर के दुश्मनी में बदल जाती है।
जिंदगी में जीत-हार यदि दुश्मनी का कारण बन जाये तो जीवन युद्ध में बदल जाता है। युद्ध-काल में जिसकी तिलांजलि सबसे पहले दी जाती है उसे नैतिकता कहते हैं।
चुनावी राजनीति की जीत-हार को दुश्मनी में बदलने से रोकने का सब से कारगर उपाय संविधान में होता है। संविधान की अवहेलना से राजनीतिक जीत-हार अंततः राजनीतिक दुश्मनी में बदल ही जाती है। ऐसे में नागरिक जमात दृश्य-अदृश्य युद्ध में फंस जाता है। ऐसे में कहां की नैतिकता और कैसी नैतिकता!
सार्वजनिक जीवन की हर अभिव्यक्ति आयुध में बदल जाती है। अभिव्यक्ति का आयुधीकरण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक अधिकार के अमृत को विष में बदल देता है। यह सब किसी सिद्धांतिकी से पुष्ट हो, न हो भारत के ताजा अनुभव से जरूर पुष्ट है।
अभिव्यक्ति के आयुध में बदलने के एक तात्कालिक उदाहरण के लिए; अभी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने रामायण के भरत प्रसंग का उल्लेख करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी की बगल में अपने बैठने के लिए एक अन्य कुर्सी का इंतजाम कर लिया।
बस फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी को संविधान के प्रावधानों की याद आ गई! सवाल आतिशी के इस रुख या रवैये के गलत-सही होने का नहीं, संवैधानिकता का भी नहीं है। सवाल इरादे का है।
संवैधानिक दृष्टि से यह सवाल महत्वपूर्ण है तो इस पर कार्रवाई भारत सरकार एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं का संवैधानिक दायित्व है। ‘विषाक्त बयानों’ की क्या जरूरत! अभिव्यक्ति के आयुधीकरण की क्या जरूरत! इस पर अविलंब संविधान सम्मत कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए। लेकिन नहीं, इरादा तो आतिशी के इस फैसला पर हमला करना था और इसके लिए अभिव्यक्ति का आयुधीकरण जरूरी था, सो कर लिया!
भारत का इतिहास ही नहीं इस की पूरी संरचना ही आत्मसातीकरण (Assimilations) की स्व-चालित प्रक्रिया से निर्मित है। जाहिर है कि आत्मसातीकरण की कोई भी प्रक्रिया हो हितों के टकराव को प्रबंधित करते हुए, किये गये सुधार और समन्वय के बिना यह संभव ही नहीं सकता है।
इसलिए भारत नायक का पहला और आखिरी गुण होता है न्याय के प्रति आग्रहशील स्वभाव। न्याय-विमुख व्यक्ति तात्कालिक रूप से चाहे जितना शक्तिशाली हो जाये मिलनसारी संस्कृति से संपन्न भारत का नायक नहीं हो सकता है।
हितों के टकराव को प्रबंधित करने के रास्ते का सबसे बड़ा अवरोधक आयुधीकृत अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति के आयुधीकरण के खतरे को भारत ने बहुत पहले पहचान लिया था।
इतिहास में झांकें तो, ‘न्याय का स्वरूप’ में अमर्त्य सेन उल्लिखित करते हैं, “अशोक इस बात के प्रति बहुत प्रतिबद्ध थे कि सार्वजनिक चर्चा बिना किसी वैमनस्य और हिंसा के संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक चर्चा के लिए प्राथमिक नियमों की रचना कर उन्हें सूत्रबद्ध भी किया था।
इसका तुल्य प्रयास पश्चिम में तो दो हजार वर्ष बाद राबर्ट के व्यवस्था के नियमों में दिखाई पड़ता है। अशोक का आग्रह था कि सभी वक्ता अपनी भाषा पर नियन्त्रण रखेगा, कोई अपने मत को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन बताने की गलत अवसरों पर चेष्टा नहीं करेगा, और उपयुक्त अवसरों पर भी वे नरम या उदारवादी भाषा का ही प्रयोग करेगा।
तीखी बहस के समय भी, सभी अवसरों पर, अन्य मतों एवं उनके अनुयायियों के प्रति सद्भाव और सम्मान की भावना का प्रदर्शन भी अनिवार्य था। सम्राट अशोक के द्वारा जन-संवाद को प्रोत्साहन दिए जाने की एक प्रतिध्वनि लगभग दो हजार वर्ष बाद मुगल बादशाह अकबर द्वारा विभिन्न धर्मानुयायियों के बीच संवाद के आयोजन और प्रश्रय में सुनाई दी थी।
अकबर का आग्रह था कि सामाजिक सद्भाव की समस्याओं का समाधान परम्परा के ‘अनुकरण के द्वारा नहीं, बल्कि तर्क के अनुसरण’ के द्वारा संभव हो सकता है। समाधान की खोज में तर्कशील संवाद का ही बोलबाला होना चाहिए।”
माना जाना चाहिए कि किसी गंभीर समस्या का समाधान आंख बंद कर परंपरा के अनुकरण से नहीं मिलता है, ईमानदार तर्क से ही कोई रास्ता निकल पाता है। पुरखों ने बहुत हद तक अनुकरण से अधिक तर्क को महत्व दिया, न दिया होता तो भारत के संविधान का यह स्वरूप बन ही नहीं पाता।
हां, संविधान में संशोधन हुए हैं, वे संशोधन संविधान में सुझाये गये तौर-तरीकों से ही होते रहे हैं। बहुमत के बल पर संविधान के दुरुपयोग के इरादे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। संविधान में अंतर्निहित ‘शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत’ ने ऐसे मामले में प्रभावी भूमिका भी निभाई है।
बहुमत के बल पर शासन और संविधान के उपयोग-दुरुपयोग तथा बहुसंख्यक की इच्छा के किसी अविवेकी दबाव में संवैधानिक प्रावधानों की मनमानी व्याख्या और बदलाव में बहुत फर्क होता है।
यह नहीं भूलना चाहिए कि ‘हितों के जिस टकराव’ को पुरखों ने प्रबंधित कर लिया था उसे आज फिर से ‘टकराव’ में बदलने पर आज के शासक की आत्मा आमादा दिखती है।
इसके लिए बहुसंख्यक के मन में राजनीतिक और सामाजिक उत्तेजना और उन्माद पैदा कर ‘तर्क’ के बदले ‘अनुकरण’ का महत्व बढ़ाने का उपाय किया जाता रहा है।
उत्तेजना और उन्माद पैदा करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग अभिव्यक्ति के आयुधीकरण में किया जा रहा है।
आश्वासन देकर आश्वासन को पूरा करने से मुंह मोड़ लेनेवाले शासक के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए! महाभारत में क्या उल्लेख है! सभी को अपने जैसा, ‘आत्मवत’ मानने इनकार करने से समाज में हितों का टकराव बढ़ जाता है। ‘आत्मवत’ मानने का निषेध ‘हम’ और ‘अन्य’ के निर्धारण का प्रस्ताव देता है।
‘हम’ और ‘अन्य’ का निर्धारण शत्रु-मित्र के बोध को मिथ्या तत्व से जोड़ देता है। मिथ्या तत्व क्या होता है? मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता है। मिथ्या न झूठ होती है, न सच होती है। किसी भी संदर्भ के वास्तविक पहलू को अप्रत्यक्ष और ओझल करनेवाला और उस की जगह अवास्तविक पहलू को आंख के सामने लानेवाला तत्व उस संदर्भ का मिथ्या तत्व होता है।
अभिव्यक्ति के आयुधीकरण में मिथ्या तत्व का मारक उपयोग होता है। भारत में ‘शत्रु-मित्र’ के संदर्भ में ठसाठस मिथ्या तत्व का सबसे सशक्त उपयोग ‘हिंदू-मुसलमान’ के संदर्भों में होता है।
‘शस्यश्यामलाम’ और ‘सुजलां सुफलाम’ के ‘कवि-कल्पित’ यथार्थ को हासिल करने का मनोरथ खंडित हो जाता है। कम-से-कम अशोक के समय से, अभिव्यक्ति के आयुधीकरण के प्रयोग और पराक्रम की जिस प्रक्रिया के खिलाफ भारत के अस्तित्व का आत्म-बोध सदैव सावधान रहा है, वह सावधानी आज कहां कमजोर पड़ गई है!
‘सशक्त भारत’ के सपनों के यथार्थ में बदलने का जिन्हें इंतजार है, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, अभिव्यक्ति के आयुधीकरण की प्रक्रिया को निष्फल करने के उपायों के बारे में सोचना ही होगा। जन-हित के बारे में सोचना और बोलना अपराध हो तो भी सोचने और बोलने का ‘अपराध’ करना ही होगा।
क्या यही है अभिव्यक्ति का वह खतरा जिसे उठाने की प्रेरणा की अविरल धारा सुकरात से लेकर गजानन माधव मुक्तिबोध तक निरंतर बहती चली आ रही है! सुकरात से लेकर आज तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने और अभिव्यक्ति के आयुधीकरण के चलते असंख्य बलिदानियों का गर्वीला इतिहास है।
मुश्किल यह है कि जरा सी चूक होते ही इतिहास को भी तो मिथ्या तत्व आच्छादित करने लगता है।
नैतिकता की वापसी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आयुधीकरण से बचाव के सवाल पर उदार बुद्धिजीवियों के भरोसा पर बैठे रहना ठीक नहीं है। बचाव के उपाय का दायित्व तो मतदाता समाज को खुद ही उठाना होगा।
चुनौती यह कि अपने मत को अंतिम रूप से निर्णायक और दृढ़तापूर्वक मानने-मनवाने की आक्रामक प्रवृत्ति से बचते हुए यह दायित्व उठाना होगा। अपनी बेचैनियों की भाषा को क्या ठीक से समझ पा रहे हैं, हम!
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)