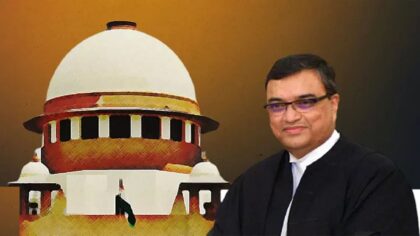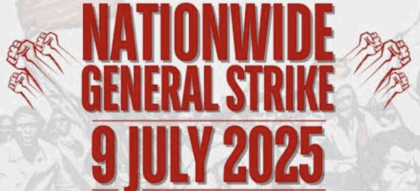दुनिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यापार संगठन के बाद के दौर (post-WTO phage) में प्रवेश कर रही है- या कहा जाए कर चुकी है। वैसे तो डब्लूटीओ गुजरे छह साल से निष्क्रिय अवस्था में है (जब डॉनल्ड ट्रंप ने बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकाल में वहां न्यायाधीशों की नियुक्ति बाधित कर दी और जिस नीति को बाद में जो बाइडन ने भी जारी रखा), मगर अपने दूसरे कार्यकाल में डॉनल्ड ट्रंप ने बाकी पूरी दुनिया के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ कर इस संस्था के तहत स्थापित ‘नियम आधारित व्यापार व्यवस्था’ को छिन्न-भिन्न कर डाला है। नतीजतन, इस दौर में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते फिर से अहम हो गए हैं।
नरेंद्र मोदी के आरंभिक दौर में भारत सरकार की नीति में मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को लेकर एक तरह की हिचक देखने को मिली थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौता है। भारत आरंभ से इस समझौते के लिए चली वार्ता में शामिल था। नवंबर 2019 में बैंकाक में हुए सम्मेलन में इस पर दस्तखत होने थे। प्रधानमंत्री मोदी उस सम्मेलन में गए, लेकिन ऐन वक्त पर भारत ने इस मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया।
तब कहा गया कि उस समझौते में शामिल कुछ ऐसे प्रावधानों पर मोदी सरकार को एतराज था, जिनसे भारत के कृषि एवं दुग्ध (डेयरी) क्षेत्रों को नुकसान होता। हालांकि यह अंतर्कथा भी चर्चित हुई कि उस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य चीन के सस्ते औद्योगिक उत्पादों से भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना था।
अब जो हो रहा है, उससे वो अंतर्कथा अधिक विश्वसनीय मालूम पड़ने लगी है। यानी किसान तब भी मौजूदा सरकार की प्राथमिकता नहीं थे, और ना अब हैं। इन खबरों पर गौर करें:
- हाल में भारत सरकार ने सरकारी खरीद क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना शुरू किया है।
- इस वर्ष छह मई को ब्रिटेन से भारत के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में यह प्रावधान शामिल है कि ब्रिटिश कंपनियां केंद्र सरकार के विभागों में होने वाली खरीदारी के दौरान टेंडर भर सकेंगी।
- हालांकि इसके पहले 2022 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से हुए FTA में भी ऐसा प्रावधान था, लेकिन उद्योग क्षेत्र में UAE की कमजोर स्थिति के कारण तब ये बात उतनी चर्चित नहीं हुई। मगर अब सूरत बदल गई है।
- ताजा खबर है कि अमेरिका के साथ भारत के प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत यह सुविधा अमेरिकी कंपनियों को भी मिल सकती है। इस खबर के मुताबिक संभव है कि यूएई और ब्रिटेन की तरह फिलहाल उन्हें ये सुविधा केंद्र सरकार की खरीदारियों में ही मिले, लेकिन देर-सबेर राज्यों और सार्वजनिक निगमों (PSUs) की खरीदारियों का क्षेत्र भी विदेशी कंपनियों के लिए खुलेगा, यह मानने की ठोस वजहें हैं।
केंद्र सरकार हर वर्ष 50 से 60 बिलियन डॉलर की खरीदारी करती है। तो फिलहाल, यूएई और ब्रिटेन के साथ-साथ अमेरिकी कंपनियों के लिए इस रकम का बाजार खुलेगा। लेकिन भारत की सार्वजनिक खरीदारी का पूरा बाजार खोलने के लिए अमेरिका का दबाव बना हुआ है। भारत सरकार का जो रुख अब तक नजर आया है, आशंका है कि वह इस दबाव को ज्यादा समय तक नहीं टाल पाएगी।
इस घटनाक्रम के दूरगामी परिणामों को समझने के लिए जरूरी है कि इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाएः
- भारत का कुल सालाना सार्वजनिक खरीदारी का बाजार 700 से 750 बिलियन डॉलर तक का है।
- अब तक ये पूरा बाजार देसी कंपनियों के लिए आरक्षित है, जिसमें कम-से-कम 25 प्रतिशत खरीदारी सूक्ष्म एवं लघु (MSME) कंपनियों से करना अनिवार्य है।
- अभी मौजूद प्रावधानों के मुताबिक सिर्फ रक्षा एवं रेलवे के लिए उन स्थितियों में विदेशी कंपनियों से खरीदारी की जा सकती है, अगर देशी विकल्प उपलब्ध ना हों।
- साफ तौर पर इस नीति का मकसद देशी उद्योग-धंधों, खासकर MSME सेक्टर को संरक्षण देना रहा है। समझा जा सकता है कि जब ये सरकारी नीति बदल जाएगी, तो इन क्षेत्रों के लिए कैसी चुनौती खड़ी होगी? विदेशी कंपनियों के सामने ये क्षेत्र कहां तक टिक पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है।
- डब्लूटीओ में भी सरकारी खरीदारी को “मुक्त प्रतिस्पर्धा के लिए” खोलने संबंधी समझौता था। इस संगठन की स्थापना के बाद से भारत पर इस समझौते में शामिल होने का दबाव था। लेकिन लगभग तीन दशक तक भारत उसका मुकाबला करता रहा। मगर post-WTO phage में द्विपक्षीय समझौतों के क्रम में भारत का प्रतिरोध दम तोड़ता नजर आ रहा है। इस क्रम में मोदी सरकार की बहु-प्रचारित योजना मेक इन इंडिया के तकाजे भी बलि चढ़ते नजर आ रहे हैं।
दरअसल, खबर तो यह भी है कि सार्वजनिक खरीदारी के सरकारी प्लैटफॉर्म Government e-Marketplace (G-e-M) पर बाहरी कंपनियों के टेंडर को जगह देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। G-e-M के सीईओ मिहिर कुमार इस बात की पुष्टि कर चुके हैं।
कृषि पर मंडराता खतरा
वैसे, अमेरिका से चल रही व्यापार वार्ता की तलवार सिर्फ MSME सेक्टर पर ही नहीं लटक रही है। बल्कि डॉनल्ड ट्रंप अपनी कंपनियों की पैठ भारत के कृषि क्षेत्र में बनाने के लिए भी उतने ही उतावले हैं। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने हाल में भारतीय बाजार में मौजूद ‘प्रतिबंधों’ की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि भारत अमेरिकी किसानों की राह में रोड़े अटकाए हुए है।
द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के सिलसिले में भी खबरें आई हैं कि अमेरिका भारत के कृषि बाजार को अपनी कंपनियों के लिए खुलवाना चाहता है। यहां ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि अब तक भारत की तमाम सरकारें खाद्य सुरक्षा और करोड़ों की किसानों की आजीविका की दलील देकर भारत के कृषि क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की मांग का प्रतिरोध करती रही हैं।
किसानों के लिए अधिक चिंता का पहलू यह है कि मौजूदा भारत सरकार की नीतियां पहले से ही उनके हित में नहीं हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की सोच कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट्स के हाथ सौंपने की रही है। इसी मकसद से 2020 में तीन विवादास्पद कृषि कानून बनाए गए थे। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के कारण सरकार ने उन कानूनों को वापस तो ले लिया, लेकिन उसके बाद सरकार और उसकी प्रमुख एजेंसी- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि कारोबार से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ऐसे कई सहमति-पत्र (MoU) पर दस्तखत किए हैं, जिनके जरिए बायर, एमेजन और सिन्गेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कृषि संबंधी ठेके मिल गए हैं।
- बायर कंपनी के साथ कम संसाधन खपत के साथ फसल विकास, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से फसलों को बचाने, फसल संरक्षण, मशीनीकरण, और कार्बन क्रेडिट मार्केट के विकास जैसे कार्यों के लिए अनुबंध किए गए हैं। इनके तहत ये कंपनी आईसीएआर को परामर्श देगी।
- अमेजन किसान कंपनी आईसीएआर के साथ मिल कर अपनी आपूर्ति शृंखला (supply chain) और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए “वैज्ञानिक खेती” को बढ़ावा देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि “उच्च गुणवत्ता” के उत्पाद अमेजन फ्रेश के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
- Syngenta Foundation India के साथ आईसीएआर के हुए करार में खेती को जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रखने और खेती में ड्रोन एवं आर्टफिशियल इंटेलीजेंस जैसी तकनीकों के इस्तेमाल की दिशा में काम करने की बात कही गई है।
कनाडा के जर्नल ग्लोबल रिसर्च में छपे एक विश्लेषण में कहा गया है- “ये भागीदारियां कृषि के ‘आधुनिकीकरण’ भर के लिए नहीं हैं। बल्कि इनका संबंध खाद्य व्यवस्था के हर बिंदु पर कॉरपोरेट नियंत्रण को जगह देने से है। डिजिटल कृषि और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम जो किया जा रहा है, उसका असल मतलब बीज, खेती सामग्रियों, डेटा और बाजारों का नियंत्रण किसानों के हाथ से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपना है। इसके परिणामस्वरूप बनने वाली खाद्य प्रणाली खाद्य सुरक्षा या किसानों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि मुनाफा वसूली के लिए होगी।”
उस विश्लेषण में उचित ही इस और ध्यान खींचा गया है कि ये सारे करार बिना सार्वजनिक बहस कराए संपन्न किए गए हैं, जबकि उनका असर राष्ट्रीय संप्रभुता और खासकर छोटे किसानों की स्वायत्तता पर पड़ेगा। एक भारतीय पत्रिका- जनता वीकली- के विश्लेषण में कहा गया है कि सरकार का एक तरफ तीव्र गति से ऐसे समझौते करना और दूसरी तरफ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने से इनकार करना- यह बताता है कि उसकी वफादारी किसके प्रति है।
इसलिए खासकर अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौतों पर चल रही बातचीत को लेकर अगर आशंकाएं गहरा रही हैं, तो उन्हें अकारण नहीं माना जा सकता। अब तक जो संकेत हैं, उनके मुताबिक इस और अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ताओं में भी मोदी सरकार की प्राथमिकता भारत की बड़ी- खासकर मोनोपोली कायम कर चुकी कंपनियों के विदेशी बाजार, वहां उनके निवेश और वहां से उनमें हुए निवेश को सुरक्षित और संरक्षित करने पर अधिक है। इसके लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बलि चढ़ती है, तो इसके उसे अधिक चिंता नहीं है।
जबकि भारत के पक्ष में ऐसे आंकड़े हैं, जिन्हें आधार बना कर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, तो भारत को कोई नई रियायत अमेरिका को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आंकड़े थिंक टैंक- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की ताजा रिपोर्ट से और भी स्पष्ट होकर सामने आए हैं। इस संस्था ने कहा है- ‘ऐसे हर कारण मौजूद हैं, जिनसे भारत को मुक्त व्यापार वार्ता में पूरे आत्म-विश्वास के साथ शामिल होना चाहिए। वह वहां व्यापार घाटे में होने के अमेरिकी तर्क का पुरजोर प्रतिवाद कर सकता है और समग्र आर्थिक संबंध की ओर ध्यान खींच कर संतुलित शर्तों की मांग कर सकता है। उसे अपनी सुविधा से चुने गए कुछ क्षेत्रों के आंकड़ों के संकीर्ण दायरे में सिमटे रहने की जरूरत नहीं है।’
जीटीआरआई के मुताबिक,
- बात व्यापार के समग्र दायरे में हो रही है, तो सिर्फ वस्तु और सेवाओं से संबंधित आंकड़ों के आधार पर समझौता करने का कोई तर्क नहीं बनता।
- इन दो क्षेत्रों में भारत को अमेरिका से 44.4 बिलियन डॉलर का व्यापार लाभ जरूर होता है, लेकिन अगर शिक्षा, डिजिटल सेवाओं, वित्तीय कारोबार, बौद्धिक संपदा पर दी जाने वाली रॉयल्टी, और हथियार बिक्री संबंधी आकंड़ों को भी शामिल किया जाए, तो अमेरिका 40 बिलियन डॉलर तक के फायदे में नजर आता है।
- अमेरिका की तरफ से बनाए कथानक का जिक्र करते हुए जीटीआरआई ने कहा है- ‘अमेरिका के व्यापार घाटे में होने की बात गुमराह करने वाली और अधूरी है। ध्यान देने योग्य यह है कि अमेरिका शिक्षा, डिजिटल सेवाओं, वित्तीय कारोबार, बौद्धिक संपदा संबंधी रॉयल्टी और हथियार बेच कर भारत से हर साल 80 से 85 बिलियन डॉलर कमाता है।’
- जीटीआरआई के प्रमुख अजय श्रीवास्तव के मुताबिक व्यापार घाटे की संकीर्ण चर्चा में जो आंकड़े दिए जाते हैं, उनमें हर साल अमेरिका को होने वाली उपरोक्त कमाई शामिल नहीं होती। अगर उसको भी शामिल किया जाए, तो समग्र रूप से अमेरिका को हर साल भारत से 35 से 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस यानी मुनाफा होता है।
जाहिर है, भारत सरकार के वार्ताकार अपनी रीढ़ को सीधी रखते हुए अमेरिकी अधिकारियों के सामने ठोस तथ्य और उन पर आधारित मजबूत तर्क पेश करें, तो कृषि तो क्या भारत को कोई क्षेत्र अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही भारत को अमेरिकी वस्तु और सेवाओं पर आयात शुल्क में कटौती करने की जरूरत होगी। उलटे भारत अमेरिका से समग्र आर्थिक संबंधों को संतुलित करने की मांग कर सकता है।
मगर ऐसा करने में जोखिम है। डॉनल्ड ट्रंप अपने अस्थिर मूड और कमजोर पर (यानी जिसे वे कमजोर समझते हैं) टूट पड़ने के लिए जाने जाते हैं। जोखिम यह है कि भारत ने प्रतिवाद किया और उस पर उन्होंने जज्बाती प्रतिक्रिया दिखाई, तो थोड़े समय के लिए बड़ी भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजारों में पहुंच अवरुद्ध हो सकती है। जाहिर है, भारत सरकार ये जोखिम नहीं उठाएगी।
अब तक का तुजर्बा यही है कि अमेरिका ने अपने पक्ष में जो तर्क दिए हैं, भारत में सत्ताधारी समूह के इकोसिस्टम ने उन्हें और बढ़ा-चढ़ा कर प्रचारित किया है। इसलिए छोटे कारोबारियों और किसानों के लिए यह जागने का समय है। उन्होंने देर की, तो फिर बहुत देर हो जाएगी; अभी लटक रही तलवार आखिरकार उन पर आ ही गिरेगी।
(यह लेख हालिया खबरों और कुछ विशेषज्ञों के विश्लेषणों पर आधारित है।)
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं।)