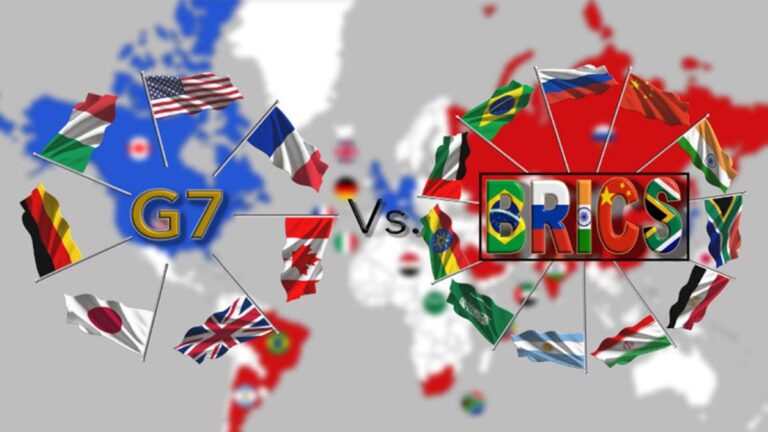रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तीन मई को विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से फोन पर बातचीत के दौरान जो कहा, उसे सीधे और सरल शब्दों में भारत के लिए झटका ही माना जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस समय भारत में भावनाएं उफान पर हैं, रूस ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करते हुए मसला हल करने की सलाह भारत को दी। लावरोव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अपनी असहमतियां शिमला समझौते एवं लाहौर घोषणापत्र के अनुरूप द्विपक्षीय तौर पर हल करनी चाहिए। (https://www.hindustantimes.com/india-news/russia-india-pakistan-pahalgam-attack-s-jaishankar-sergey-lavrov-101746286465938.html)
स्पष्टतः इस रुख से पाकिस्तान की सेना या सरकार को (पहलगाम हमले के लिए) दोषी मानने का संकेत नहीं मिलता। इस रूप में ये नजरिया अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से बहुत अलग नहीं है, जिन्होंने भारत से तुरंत तनाव घटाने को कहा है। जयशंकर- लावरोव फोन वार्ता से एक दिन पहले अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वांस ने टीवी चैनल फॉक्स को दिए इंटरव्यू में कहा था- ‘हमें उम्मीद है कि भारत आतंकवादी हमले का जवाब इस तरह देगा, जिससे बड़ा क्षेत्रीय टकराव शुरू ना हो।’ पाकिस्तान को वांस ने सलाह दी कि वह इसे सुनिश्चित करे कि आतंकवादी पकड़े जाएं और उनके प्रति कार्रवाई हो सके। इस टिप्पणी से संकेत यही मिलता है कि अमेरिका पाकिस्तान सरकार को प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी हमले के लिए दोषी नहीं समझता।
जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार से फोन पर बातचीत के बाद यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने उसी रोज कहा था- ‘भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहा तनाव खतरनाक है। मैं दोनों पक्षों से अपील करती हूं कि वे संयम का परिचय दें और स्थिति को सुधारने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं। तनाव बढ़ने से किसी का भला नहीं होगा।’
(https://x.com/kajakallas/status/1918311802229662164)
इन तीनों प्रतिक्रियाओं में समान पहलू यह है कि इनमें भारत और पाकिस्तान को समान धरातल पर रखा गया है। भारत की ‘मुख्यधारा सोच’ के नजरिए से यह बात चुभने वाली है कि ‘आक्रांता’ और उसके ‘शिकार’ दोनों को समान नजरिए से देखा जाए। उस दौर में यह बात और भी चुभती है, जब देश के अंदर बड़ा जनमत यह मानता है कि यह भारत उदय का युग है, जिसमें देश की इज्जत बढ़ी है और भारतवासियों की भावनाओं का सम्मान बढ़ा है!
खैर, भावनाओं को छोड़ भी दें और गंभीर कूटनीति के नजरिए से ध्यान दें, तब भी रूस की बेरुखी को भारत के लिए चिंताजनक कहा जाएगा। जिस देश के बारे में आम धारणा है कि उसने (सोवियत जमाने से) हर नाजुक मौके पर भारत का साथ दिया है, उससे विशेष प्रतिक्रिया की अपेक्षा लाजिमी रही है। जबकि इस बार ऐसा नहीं है।
- जयशंकर से बातचीत के एक दिन बाद सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार को फोन किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की। (https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Russia-offers-to-act-as-mediator-between-India-and-Pakistan)
अगर यह रिपोर्ट सही है, तो इसे रूस का रुख और स्पष्ट होता है।
इसके एक दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। आधिकारिक रूप से बताया गया कि इस दौरान पुतिन ने पहलगाम के पीड़ितों के प्रति हमदर्दी जताई और दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ समझौताविहीन लड़ाई पर जोर दिया।
रूस की तरफ से ये बात 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के तुरंत बाद भी कही गई थी। घटना के 13 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति ने सिर्फ उसे ही दोहराने के लिए फोन किया, यह बात थोड़ी अजीब-सी लगती है। उसके पहले लावरोव की जयशंकर और इशहाक डार के साथ फोन वार्ताओं के बारे में जो सूचना आ चुकी थी, पुतिन ने उसके विपरीत रुख लिया होगा, इसकी संभावना कम है। बहरहाल, जो बात बताई गई है, वह भी सामान्य किस्म की है। उससे यह संकेत नहीं मिलता कि पाकिस्तान को दंडित करने के मामले में रूस भारत के साथ खड़ा है।
यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी 2019 तक जम्मू-कश्मीर मामले में भारत को रूस का बेलाग समर्थन मिला था। उस वर्ष पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत के फैसले का रूस ने समर्थन किया।
- तब रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये निर्णय भारतीय संविधान के दायरे में लिया गया है
- रूस ने इस फैसले को भारत का संप्रभु और आंतरिक मामला बताया था
- यह कहने के बाद रूस ने भारत और पाकिस्तान से 1972 के शिमला समझौते एवं 1999 के लाहौर घोषणापत्र के अनुरूप राजनीतिक एवं कूटनीतिक माध्यमों से मतभेद दूर करने की अपील की थी।
- तब रूसी कूटनीतिकों ने कहा था- रूस भारत के इस विचार से सौ फीसदी सहमत है कि इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय रूप नहीं दिया जाना चाहिए।
इसके पहले पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत ने फरवरी 2019 में जब बालाकोट में हवाई हमला किया, तब भी रूस ने जोर दिया था कि यह मुद्दा द्विपक्षीय दायरे में ही रहना चाहिए। इस बार भी रूस ने यही कहा है, मगर इस बार की पृष्ठभूमि ऐसी है, जिसमें इसे भारत के पक्ष में झुका हुआ नहीं समझा जा सकता। इस समय भारत सरकार की प्राथमिकता पाकिस्तान को “सबक सिखाने” की है, जबकि रूस भारत को ऐसा कोई कदम न उठाने को कह रहा है!
यहां उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस संबंध में चर्चा हुई। तब चीन की मदद से फिलहाल अस्थायी सदस्य पाकिस्तान यह सुनिश्चित करने में सफल रहा कि प्रस्ताव में उसकी या उसके जमीन से अपनी गतिविधियां चला रहे किसी दहशतगर्द संगठन का नाम लेकर निंदा ना की जाए। पश्चिमी देशों के साथ-साथ रूस ने भी इस पर कोई एतराज नहीं किया। बल्कि वे सभी सर्व-सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को पारित कराने में सहायक बने।
स्पष्टतः यह घटनाक्रम भारत के “आजमाए हुए दोस्त” के रूप में रूस की छवि पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करता है। सवाल है कि आखिर रूस के रुख में क्यों बदलाव आया है?
पहले प्रश्न को समझने के लिए हमें हालिया वर्षों के घटनाक्रम पर गौर करना चाहिए- खासकर 24 फरवरी 2022 के बाद बनते गए हालात पर। उस रोज रूस ने यूक्रेन में विशेष सैनिक कार्रवाई शुरू की थी। भारत ने इसकी निंदा नहीं की। ना ही भारत रूस पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका और यूरोप के अभियान का हिस्सा बना। बल्कि उन प्रतिबंधों से बने हालात का पूरा लाभ उठाने की नीति भारत ने अपनाई। प्रतिबंधों के कारण रूस तब सस्ता तेल बेचने पर मजबूर हुआ, जिसका फायदा भारत सरकार और यहां की निजी कंपनियों ने खूब उठाया।
इसके बावजूद भारत ने यह संकेत देने में कभी कोताही नहीं की है कि उसकी नीतिगत प्राथमिकता पश्चिमी खेमे के साथ जुड़े रहने में है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे all alignment यानी सबसे संबंध रखने की नीति कहा है। हमारे सरकारी रणनीतिकार दावा करते रहे कि जवाहर लाल नेहरू के युग में अपनाई गई non- alignment की नीति से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ, जबकि all alignment की नीति से भारत सभी पक्षों से फायदा उठा रहा है। देश में ऐसा होने का आभास काफी गहरा रहा है।
वैसे दुनिया के बदलते शक्ति-संतुलन एवं समीकरणों से परिचित विश्लेषक आरंभ से आगाह करते रहे हैं कि ये नीति ज्यादा दिन कारगर नहीं रहेगी। दुनिया जिन दो खेमों में बंट रही है, उनके बीच तीखे होते अंतर्विरोधों के साथ असल में यह नीति नुकसान का सौदा बन जाएगी।
यह आकलन इस समझ पर आधारित था कि दुनिया जिन खेमों में बंट रही है, उनमें एक में प्रमुख भूमिका चीन और रूस की है, जिनके बीच उद्देश्य की एकता बनी है। यह उनकी साझा परियोजना है। स्पष्टतः दूसरा खेमा अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम का है, जिसके साथ चीन- रूस की धुरी का टकराव बढ़ना अपरिहार्य है। भारत बड़ा देश है, जिसके पास अपेक्षाकृत मजबूत आर्थिक एवं सैनिक ताकत है और जो भौगोलिक रूप से खासा महत्त्वपूर्ण है। इसलिए लाजिमी था कि दोनों खेमों में उसकी मांग रहे। लेकिन ये स्थिति अनंत काल तक नहीं रह सकती। समझ यह थी कि दोनों खेमों में अंतर्विरोध तीखा होने के साथ हर देश की तरह भारत के लिए भी यह तय करना अनिवार्य हो जाएगा कि नई विश्व व्यवस्था के संबंध में उनकी दृष्टि क्या है?
दोनों खेमों के साथ समान दूरी रखना एक नजरिया हो सकता है। लेकिन दोनों समूहों से लाभ उठाने भर का नजरिया टिकाऊ नहीं हो सकता। और तब तो बिल्कुल ही नहीं, जबकि एक धुरी में चीन की सर्व-प्रमुख भूमिका है। चीन से “असीमित दोस्ती” के एलान को बार-बार दोहराते हुए रूस ने इस भूमिका के साथ सामंजस्य बना रखा है।
दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों की विजय की 80 सालगिरह के मौके पर मास्को में आयोजित हाई प्रोफाइल समारोह में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वहां जाने की पुष्टि करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने जो कहा, वह इस सिलसिले में अहम हैः
“आज की दुनिया में तीव्रतर गति से अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में गहन समायोजन हो रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि के साथ रणनीतिक ऊंचाइयों से, राष्ट्रपति शी और राष्ट्रपति पुतिन ने नए युग में, जटिल बाहरी माहौल के बावजूद चीन-रूस संबंधों का मार्गदर्शन किया है। इससे जाहिर हुआ है कि यह संबंध अच्छे पड़ोसी और दोस्ती, व्यापक रणनीतिक समन्वय, पारस्परिक लाभ, सहयोग और द्विपक्षीय उपलब्धि की भावना पर आधारित है।”
(https://x.com/globaltimesnews/status/1918964184613863704)
स्पष्ट है कि आज के समय में रूस और चीन को एक सीमा तक ही अलग करके देखा जा सकता है। इसे चीन के प्रभाव का ही संकेत माना जाएगा कि रूस की रणनीतिक दृष्टि में आज पाकिस्तान की एक अहम जगह बन गई है। गौरतलब है कि ब्रिक्स समूह में पाकिस्तान को शामिल करने की सबसे जोरदार पैरोकारी रूस ने ही की है। यह अच्छी बात है कि अब इस हकीकत को भारत के रणनीतिक समुदाय में भी समझा और स्वीकार किया जाने लगा है।
(https://x.com/ANI/status/1918571238856765493)
क्या यह स्थिति भारत के हित में है? इस प्रश्न पर अलग-अलग नजरिया संभव है। मुख्यधारा नजरिया यही है कि भारत की अमेरिकी धुरी से अपने रणनीतिक हित जोड़ने की नीति सही है। इसके पीछे एक कारण चीन को लेकर यह समझ है कि भारत नए युग में चीन का प्रतिस्पर्धी देश है, इसलिए उससे या उसके नेतृत्व वाले समूहों से वह एक सीमा से ज्यादा गहरा रिश्ता नहीं बन सकता। उससे रिश्ते की सीमा सिर्फ इतनी है कि सरहद पर टकराव टला रहे। इस बीच पश्चिम से रिश्ते गहरे करते हुए भारत को अपनी ‘राष्ट्रीय शक्ति’ विकसित करनी चाहिए।
नरेंद्र मोदी सरकार इसी समझ के साथ पिछले एक दशक में आगे बढ़ी है। वैसे इस नीति पर राजनीतिक दायरे में कमोबेश आम सहमति है। मगर 2023 में इस रणनीति में पेच उभरने लगे, जब पहले कनाडा और फिर अमेरिका ने आरोप लगाया कि वहां सिख आतंकवादियों की हत्या या हत्या की साजिश में भारतीय एजेंसियां शामिल रही हैं। तब से उन देशों में माहौल बदलता चला गया है।
डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद तो पुराने सारे समीकरण ही उलट-पुलट होते दिखे हैं। ऐसे में पश्चिमी धुरी के साथ रहने की रणनीति फिलहाल डगमगाई नजर आ रही है। पहलगाम कांड के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बीच का रुख अपना कर साफ कर दिया है कि पश्चिम आज उसे अपनी धुरी का हिस्सा नहीं मानता। इस बीच चीन ने खुल कर पाकिस्तान का साथ दिया है, जबकि भारत के पुराने दोस्त रूस का नजरिया बदल गया है।
तो यह बुनियादी सवाल है कि all alignment की नीति का लाभ क्या हुआ? सबसे जुड़ कर लाभ उठाने की इस सोच का परिणाम सबको खो देने के रूप में सामने आ रहा है। चूंकि वर्तमान केंद्र सरकार के कर्ता-धर्ता कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। वे कभी नीतिगत मामलों पर देश में बहस नहीं छेड़ते और दूसरे पक्ष की राय पर ध्यान नहीं देते हैं।
उधर विपक्ष हर समस्या के लिए नरेंद्र मोदी को दोषी ठहरा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। उसके पास गंभीर प्रश्नों पर बहस करने की ना तो दृष्टि है, और ना ही इच्छाशक्ति। इसलिए all alignment जैसी दोषपूर्ण नीति पर देश में कोई चर्चा नहीं है। दरअसल, इस नीति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को कितना अकेला कर दिया है, उसका अहसास होने का संकेत तक यहां नहीं है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं।)