खिरियाबाग, आजमगढ़। आज़मगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के लिए आठ गांवों के लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की रीढ़ दलित महिलाएं हैं। 12 नवंबर के दिन और विशेषकर करीब 1 बजे रात पुलिस से मुठभेड़ भी दलित महिलाओं ने ही किया। हालांकि रात को पुलिस के आने का शोर ब्राह्मण टोले की महिलाओं ने मचाया, लेकिन पुलिस को रोकने के लिए दौड़कर दलित महिलाएं ही गईं। सभी प्रत्यक्षदर्शी और आंदोलन के शीर्ष नेता यह तथ्य एक स्वर से स्वीकार करते हैं। पहले पुलिस ब्राह्मण टोले की तरफ ही आई थी।
ब्राह्मण टोले के सुजाय उपाध्याय इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि “पुलिस के साथ संघर्ष में दलित महिलाएं सबसे आगे थीं।” पुलिस को जब इस तथ्य का पता चला कि जो महिलाएं उन्हें सर्वे करने से रोक रही हैं, जरीब पकड़ रही हैं, उन्हें डंडा बरसाने से रोक रही हैं, वे दलित महिलाएं हैं, तब पुलिस ने जाति सूचक गालियां भी इन महिलाओं को दीं। 80 दिनों से चल रहे इस आंदोलन में धरना स्थल (खिरिया बाग) में हमेशा 70 से 80 प्रतिशत महिलाएं ही रहती हैं, वहां वे पुरुष ही उपस्थित होते हैं, जो आंदोलन के शीर्ष नेता हैं या आंदोलन में बहुत ही सक्रिय हैं या कोई विशेष अवसर होता है या बाहर से आंदोलन में शामिल होने आए हैं।

पहली बार जो जुलूस नवंबर में निकला था, उसमें करीब 250 लोग शामिल थे, जिसमें करीब 200 महिलाएं थीं। इसी तरह दिसंबर में जो जुलूस निकला उसमें 300 लोग शामिल थे, जिसमें 200 से अधिक महिलाएं थीं। अभी हाल में 1 जनवरी को जो जुलूस निकला है, उसमें करीब 600 लोग शामिल थे, उसमें करीब 400 महिलाएं थीं। आंदोलन एक बड़े चेहरे राजीव यादव को पुलिस द्वारा गुपचुप तरीके से उठाए जाने के बाद 26 दिसंबर को पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ ज्ञापन देने और प्रदर्शन करने के लिए करीब जो 250 लोग गए उसमें करीब 200 महिलाएं थीं और उनका पुलिस से संघर्ष भी हुआ।
इसी तरह 30 दिसंबर को डीएम से वार्ता के लिए जो करीब 60 लोग गए थे, उसमें करीब 40 महिलाएं थीं। ये तथ्य इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे संगठन ‘मकान-जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा’ के अध्यक्ष रामनयन यादव ने उपलब्ध कराए। नियमित तौर पर आंदोलन में सक्रिय और इस आंदोलन के संगठनकर्ता राजीव यादव, राजेश आजाद, विरेन्द्र यादव, प्रवेश निषाद, अजय यादव, दुख हरन राम, प्रेमचंद और मुरली आदि भी इसकी पुष्टि करते हैं।

जनचौक की टीम चार दिनों तक इन गांवों में रहते हुए और धरना स्थल पर उपस्थित लोगों से बात करते इस तथ्य की ताकीद की। यहां यह तथ्य एक बार फिर रेखांकित कर लेना चाहिए कि चाहे धरना स्थल हो, चारे जुलूस हो और चाहे प्रशासन के पास जाना जो महिलाएं इसमें शामिल होती हैं, उनका 90 प्रतिशत से अधिक दलित महिलाएं होती हैं। कुछ एक कुम्हार, निषाद, राजभर या यादव परिवार की महिलाएं होती हैं, कुछ गुप्ता परिवार की महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हैं, हालांकि गुप्ता लोगों की संख्या गांव में कम है। आंदोलन के शुरूआती दिनों में दलित महिलाओं के यह सवाल उठाने पर कि, आंदोलन के अगुवा ब्राह्मण लोग हैं ( शुरू में आंदोलन की अगुवाई शशिकांत उपाध्याय कर रहे थे) लेकिन उनकी महिलाएं इस आंदोलन में नहीं आतीं। इसके बाद एक-दो बुजुर्ग ब्राह्मण महिलाएं इस आंदोलन में कुछ एक दिन आईं, लेकिन उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया, हालांकि बाद में तो ब्राह्मण पुरूषों ने भी आना बंद कर दिया। ब्राह्मण परिवारों की महिलाएं क्यों नहीं आतीं, इसका जवाब एक ब्राह्मण महिला ने यह कहते हुए दिया- “ उन्हन ( दलित) के बीच हमन के अब जा के बैंठी ( दलित महिलाओं के बीच हम लोग अब जाकर बैठें)।”
महिलाएं इस आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में क्यों हैं? इसका सीधा उत्तर किसी ने नहीं दिया। आंदोलन के एक बड़े चेहरे ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि “ इस आंदोलन की कवच और ढाल महिलाएं हैं। यदि महिलाएं न होतीं, तो पुलिस कब की धरना स्थल से लोगों को भगा चुकी होती और गांवों का सर्वे कर चुकी होती, आठ गांवों के लोग, उसमें विशेषकर चार गांवों के लोग कब तक शासन-प्रशासन और पुलिस-पीएसी को रोक पाते।” वे आगे कहते हैं कि “पुलिस-पीएसी महिलाओं पर लाठी-डंडा चलाने और उन्हें जेल भेजने से डरती है, क्योंकि ऐसा करने पर यह बड़ा मुद्दा बन जाएगा और पुलिस प्रशासन के साथ सरकार की भी बदनामी होगी।” इस बात की पुष्टि आंदोलन के अन्य सक्रिय नेता और कार्यकर्ता भी करते हैं। डीएम कार्यालय में वार्ता के दिन 30 दिसंबर को बात-चीत में एक पुलिस वाले ने भी कहा, “ये सब ( आंदोलन के नेता) बहुत होशियार हैं, महिलाओं को आगे किए हुए हैं।”

इस सब के बावजूद भी यह प्रश्न किसी के भी मन में उठेगा कि आखिर दलित महिलाएं इस आंदोलन में सबसे बड़ी संख्या में और सबसे आगे क्यों हैं? इसका एक जवाब यह हो सकता है कि इन गांवों की आबादी में सबसे अधिक ( करीब 50 प्रतिशत) दलित हैं और उनके लिए अपना घर और खेती की जमीन ( थोड़ी सी ही सही) अपना अस्तित्व बचाने के बराबर हैं, उन्हें यह भी पता है कि यदि घर और जमीन से उन्हें उजाड़ा जाएगा, तो उन्हें मुआवजा भी बहुत कम मिलेगा। कई के तो घर का भी पक्का कागज नहीं, कुछ का घर ग्राम सभा की जमीन (आबादी) पर बना है, तो कुछ के घर की जमीन पर किसी पुराने जमींदार का नाम बरकरार है। इसके अलावा वह अधिया (बंटाई) लेकर भी खेती करती हैं, जिससे उनका जीविकोपार्जन चलता है। इन जमीनों में इनका कोई मालिकाना नहीं है। इसके अलावा वह गांव में रहते हुए, अन्य लोगों के खेतों में मजदूरी भी कर लेती हैं। इसके अलावा इसी गांव के बाग-बगीचों, ताल-तलैया और खेत-मैदानों में उनके जानवर और बकरियां भी चरती हैं, जो जीविकोपार्जन का एक साधन हैं।
दलित महिलाओं के पति-बेटे भले ही दूर-दराज के शहरों और कुछ एक विदेशों में मजदूरी करते हैं, लेकिन इतना नहीं कमा पाते कि शहर में घर खरीद सकें या बना सकें, उनके लिए गांव का उनका घर ही अंतिम सहारा है। कोविड के दौरान उनको इसका और भी गहरा अहसास हुआ। इस पूरी स्थिति को कुटुरी ( करीब 55 वर्षीय दलित महिला) इन शब्दों में व्यक्त करती हैं, “अगर हम उजाड़ दिए जाएंगे, तो जाएंगे कहां। किसी तरह बेटों ( अखिलेश-कमलेश) ने विदेशों ( खाड़ी के देशों) में मजदूरी करके एक अच्छा घर बनवाया है, यदि उसे छीन लिया जाएगा, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बच्चे पैसा भेजते हैं, थोड़ा-बहुत दूसरों और अपने खेतों में हम काम कर लेते हैं। परिवार अच्छे से चल रहा है, यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे।”

दलित पुरूषों की तुलना में दलित महिलाओं की धरना स्थल और आंदोलन में हिस्सेदारी क्यों है, इसका सतह पर दिखता एक कारण यह है कि करीब सभी दलित पुरूष दिहाड़ी की मजदूरी के लिए गांव से बाहर जाते हैं, कुछ उसी दिन रात को लौटकर आते हैं, कुछ एक सप्ताह या 25 दिन में लौटते हैं, यह काम के स्वरूप पर निर्भर करता है। यही स्थिति अति पिछड़ी जातियों के पुरूष कामगारों की भी है। प्रवेश निषाद खिरिया बाग आंदोलन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, लेकिन वे भी प्रतिदिन धरना स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसका कारण पूछने पर वे कहते हैं, “अगर मैं मजदूरी न करूं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा और मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। गांव में काम है, नहीं इसलिए गांव से बाहर जाना पड़ता। मुझे धरना-आंदोलन और मजदूरी के बीच तालमेल बैठाना पड़ता है, जब बहुत जरूरी होता है, तो काम छोड़कर आंदोलन में शामिल होने आ जाता हूं। हमें अपने मकान-जमीन बचाने की लड़ाई भी लड़नी है और रोज-रोज पेट भी पालना है” कमोबेश इसी तरह की बात प्रेमचंद ( दलित) भी करते हैं, प्रेमचंद की पत्नी किस्मती इस आंदोलन की एक नेता और महत्वपूर्ण चेहरा हैं।
फिर भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि घर-मकान तो सबका जा रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं, फिर धरना स्थल और संघर्ष में अधिक दलित महिलाएं ही क्यों? इसकी कई वजहें दिखती हैं। पहली वजह यह है कि घर-परिवार के संचालन ( विशेषकर आर्थिक जिम्मेवारियों) को उठाने में दलित पुरूषों और दलित महिलाओं की भूमिका कमोवेश बराबर है। वे सिर्फ घर के अंदर के काम करने तक सीमित नहीं हैं। दलित परिवारों के पुरूष और महिला दोनों बाहर मेहनत-मजूरी करते हैं, तभी घर चलता है। मध्यमवर्गीय कुछ दलित परिवारों को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई दलित महिला यह सोचती हो कि घर की आर्थिक जिम्मेवारियां उठाना पुरूष का काम है। वह अपने को करीब-करीब इसके लिए समान तौर पर जिम्मेवार मानती है। यह स्थिति एक हद तक अति पिछड़ी जाति की महिलाओं की भी है, इसके विपरीत पिछड़ी जाति और सवर्णों के घरों की महिलाओं की स्थिति बिलकुल भिन्न हैं।

गांवों में सवर्ण परिवारों की महिलाएं घर के अंदर के कामों तक सीमित हैं। घर को आर्थिक तौर पर चलाने की जिम्मेदारी वह पुरूषों की मानती हैं। सवर्ण पुरूष भी ऐसा ही सोचते हैं। पिछड़ी जातियों की महिलाएं हालांकि घर के बाहर के कामों में थोड़ा सहयोग करती हैं, लेकिन उनका दायरा भी कमोवेश घरेलू कामों और पशुओं की देखभाल करने तक सीमित है। इसके चलते घर-परिवार के अस्तित्व पर जब कोई संकट आता है, तो अलग-अलग सामाजिक समूहों की महिलाओं की भूमिका अलग-अलग होती है, जहां दलित और अति पिछड़ी जाति की महिलाएं और पुरूष घर पर आए संकट के समाधान के लिए खुद को करीब समान रूप से जिम्मेदार मानते हैं, तो सवर्ण और पिछड़ी जाति की महिलाएं समस्या से जूझने और उसका समाधान करने की मुख्य जिम्मेदारी पुरूषों की मानती हैं। यह स्थिति इस आंदोलन के संदर्भ में भी दिखी। जहां दलित पुरूष और महिलाएं अपना घर और जमीन बचाने के लिए खुद को समान रूप से जिम्मेवार मानते हैं, वहीं सवर्ण और पिछड़ों के अगड़ी जाति की महिलाएं इस मुख्य रूप से पुरूषों की जिम्मेवारी मानती हैं।
परिवार संचालन में अलग-अलग भूमिका और इससे पैदा हुए सोच के चलते जहां दलित और अति पिछड़ी जाति की महिलाएं अपने परिवार के सामाजिक-राजनीतिक निर्णयों में करीब समान रूप से हिस्सेदारी करती हैं, वहीं सवर्ण और पिछड़ों की अगड़ी जातियों की महिलाएं खुद को इससे अलग रखती हैं और अपने घर के पुरूषों की पूरी तरह अनुगामिनी होती हैं। इन सारे संदर्भों में अलग-अलग सामाजिक समूहों के पुरूषों की अपने घरों के महिलाओं के प्रति सोच भी धरना, आंदोलन और संघर्ष में महिलाओं की हिस्सेदारी तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। जहां गांवों के मेहनतकश अधिकांश दलित पुरूष अपने घर की महिलाओं का घर से निकलना, सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी करना, उनका अन्य पुरूषों से बात-चीत करना, अन्य पुरूषों के साथ उनके उठने-बैठने और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्षों में हिस्सेदारी करने, उनके साथ कहीं आने-जाने और संघर्ष का नेतृत्व करने करने को, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और मर्दानगी के लिए चुनौती नहीं मानते हैं, स्वाभाविक है कि दलित पुरूषों की यह सोच दलित महिलाओं को यह आजादी प्रदान करती है कि वे इस आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी करें।

इस स्थिति की अभिव्यक्ति इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण चेहरा सुनीता ( दलित, 22 वर्ष) के बड़े भाइयों अखिलेश और कमलेश के इस इस कथन में होती है। जब मैंने पूछा कि सुनीता ( आपकी बहन) इस आंदोलन में इतनी सक्रिय है, आपको कैसा लगता है, उनका उत्तर था कि “ हम तो इसे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारी बहन बहुत तेज है, हमें अच्छा लगता है, जब हम उसे वीडियो में बोलते हुए देखते हैं, आंदोलन का नेतृत्व करते हुए देखते हैं।” इसके कमोवेश विपरीत सोच इन गांवों के पिछड़ों की अगड़ी जातियों और विशेषकर सवर्ण पुरूषों की है। वे पर पुरुष से अपनी महिलाओं का घुलना-मिलना, बतियाना और उनके साथ उठना-बैठना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें यह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मर्दानगी के खिलाफ लगता है। इसकी अभिव्यक्ति विनय उपाध्याय के इस सहज कथन में होती हैं, “हम उनकी तरह (दलित-पिछड़ों) तो अपनी महिलाओं को नहीं भेज सकते हैं,न।”
(आज़मगढ़ से शेखर आजाद के साथ डॉ. सिद्धार्थ की रिपोर्ट।)




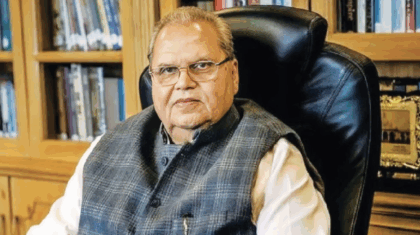









बहुत अच्छा विमर्श खड़ा करते हुए रिपोर्टिंग की गई है।निश्चय ही इसे गम्भीरता से पढ़कर हमें आंदोलन व समाज के बीच वर्गीय और जातिय अंतर्गुथन और अंतर्विरोधों के सवालों को हल करने में बल मिलेगा।धन्यवाद शेखर आज़ाद और सिद्धार्थ जी।