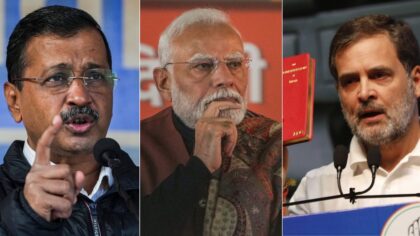वाराणसी। वाराणसी के कमौली, छितौनी और कोटवा गांव में जुलाहा परिवार (बुनकर) की हजारों महिलाओं का जीवन बहुत कठीन दौर से गुजर रहा है। कमर तोड़ती महंगाई और श्रम का उचित मूल्य न मिलने से महिलाएं हासिए पर जा चुकी हैं। पेट पालने की जद्दोजहद में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी चीजें इनसे छूटती जा रही है। सबसे दुखद पहलू यह है कि ये जुलाहा महिलाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हैं, जहां प्रत्येक साल लाखों-करोड़ों रुपए से विकास कार्य किये जा रहे है। ऐसे में बनारस की विरासत बुनकरी पेशे की ‘बैक बोन’ मानी जाने वाली जुलाहा, बुनकर और पसमांदा मुस्लिम महिलाओं के दर्द सभी प्रकार जनसंचार माध्यमों में चर्चा-चिंतन से नदारत है. पेश से पवन कुमार मौर्य की रिपोर्ट।

वाराणसी जिला मुख्यालय से महज 18-20 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में स्थित कमौली की जुलाहा (बुनकर) मोहल्ले में बुधवार की दोपहर में कोई चहल-पहल नहीं थी। कई महिलाएं एक जगह इकठ्ठा होकर रोजमर्रा की बातचीत में समय काट रही थीं। जबकि, पांच-छह साल पहले इन महिलाओं के पास कढ़ाई, बुनाई, जड़ाई, माला-हार व अन्य हाथ से सिलने-टांकने वाले काम होते थे। प्रत्येक माह औसतन 3 से 4 हजार रुपए की आय से कमौली की सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी थीं। हाल के दशक में हजारों बुनकर महिलाएं अपनी पहचान बचाने के लिए मंहगाई और बेरोजगारी से जूझ रही हैं.
महिलाओं ने बताया कि कोरोनाकाल और दोषपूर्ण सरकारी नीतियों के चलते इन महिलाओं का रोजगार चौपट हो गया। ये स्त्रियाँ बुनकर परिवारों से आती हैं जिनके पति हथकरघा अथवा पावरलूम चलाते हैं। हथकरघों की घटती संख्या और साड़ी व्यवसाय पर मंदी का असर इतना ज्यादा पड़ा है कि बुनकरी से परिवार चलाना बहुत कठिन हो गया है। पावरलूम चलानेवाले कारीगर भी महंगी बिजली और दूसरी परेशानियों के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
सोलह साल की गौरी जहां पहले दुल्हन की चुनरी में शीशा और झालर जड़ने का काम करती थीं। वह अब इन दिनों बेला की फूल की माला बनाती हैं। उनके पिता ई-रिक्शा चलाते हैं, जो परिवार के सात सदस्यों के गुजारे के कम पड़ता था। इस वजह से गौरी सिर्फ आठवीं दर्जे तक पढ़ सकी और उसे पढ़ाई छोड़े दो साल हो गया है। गौरी को माला बनाने के एवज में मिलने वाले पैसे से परिवार के आय में सहयोग करती हैं।

गौरी बताती हैं “मैं पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन घर में बहुत मुश्किल से सभी लोगों को दो वक्त का भोजन मिल पाता है। मम्मी पहले बुनाई-कढ़ाई करती थीं, जो बंद हो गया है। अकेले कमाने वाले पापा हैं। उनकी आमदनी बेहद सिमित है। पैसों की तंगी और गरीबी के चलते मैनें पढ़ाई छोड़ दी। मेरे सभी भाई-बहन (दो बहन, दो भाई) सातवीं-आठवीं दर्जे से अधिक न पढ़ सके। मैं 100 माला बनती हूं तो 30 रुपए मिलते हैं। माला बनाने में एक दिन में कई बार सुई उँगलियों में चुभ जाती है।”
मसलन, जटिल आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच असंगति ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये बेहतर जीवन जी सकें। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है, बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती। इसके अलावा, अक्सर बुनकरी से जुड़े कामों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वज़ह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। कमौली की जुलाहा महिलाओं को दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन भी तय नहीं है। इसलिये न्यूनतम मज़दूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये कामगार अपना श्रम करने को विवश हो जाते हैं। वैसे भी हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी की दरें वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम हैं।

बानो निशा “जनचौक” से कहती हैं कि “दुपट्टे, दूल्हन की चुनरी पर शीशा और सजावटी आइटम टांकने का काम कोरोना की महामारी से पहले मिलता रहा है। इसके एवज में एक दुपट्टे पर 30 रुपए, एक दुल्हन चुनरी पर 120 रुपए और एक साड़ी पर 100 रुपए मिलते थे। एक दिन (लगभग पांच घंटे) में दो महिलाएं मिलकर तीन साड़ी या दो दुल्हन चुनरी तैयार कर देती थी। वाराणसी के लल्लापुरा से साड़ी और चंदौली जनपद के पड़ाव से दुपट्टे व चुनरी व्यापारी हमलोगों के यहां भेजते थे। काम पूरा होने पर प्रति सप्ताह मजदूरी का भुगतान कर दिया जाता था। लेकिन, कोरोना के समय यह काम बंद हो गया, तब से लेकर आज तक हमलोग चार पैसे के लिए तरस रहे हैं।”
निशा आगे कहती हैं “अब पहले वाला काम नहीं है, लेकिन मोतियों की माला बनाने के लिए व्यापारी आते हैं, जो बहुत कम मेहनताना देते हैं। मुझे तो अब दिखाई भी कम देता है। इस वजह से साबुन-शैम्पू व चॉकलेट-बिस्किट की दुकान चलाती हूं।”
बनारसी साड़ी उद्योग में गिरावट कोरोना महामारी से पहले भी दर्ज गई गई थी। इसके बाद जो थोड़े-बहुत काम-धंधे बचे भी हुए थे उनकों कोरोना ने तहस-नहस कर दिया। इसके चलते बड़ी संख्या में स्त्री-पुरुष बेरोजगार हुये हैं, जिनके सामने मज़दूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

किशोरवय से हथकरघे पर साड़ी की बुनाई करने वाले सरवर का अबतक बुनकर कार्ड नहीं बन सका है। वह “जनचौक” से कहते हैं “अब बुनकरी में पहले जैसा काम नहीं मिलता है. काम बहुत घट गया है और मजदूरी बेहद सिमित है। आसमान छूती मंहगाई व बढ़ते परिवार को चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। आर्थिक तंगी की वजह से मेरी चार बेटियों की पढ़ाई कक्षा आठ से अधिक नहीं हो सकी, सभी सिलाई-कढ़ाई कर अपना खर्चा चलाती हैं। हमलोग पुश्त-दर-पुश्त बुनकरी ही करते आ रहे हैं, दूसरा कोई काम करने आता ही नहीं है। बुनकरी ही हमारी रोटी, पानी और आक्सीजन है, जो दिनों-दिन मरता जा रहा है। पहले मोहल्ले में बनारसी साड़ी, दुपट्टा और शॉल बनाने के लिए सैकड़ों कारीगरों\बुनकरों की चहल-पहल हुआ करती थी। बुनकरी का काम ख़त्म होने से अधिकांश मजदूरी करने लगे, कोई टोटो, ऑटो रिक्शा चलाने लगा, कोई बैंड पार्टी में बाजा बजाने लगा तो कई बेरोजगार हो गए।”

सलीम सोचते हुए बताते हैं कि तकरीबन 14-15 साल पहले वे हथकरघे पर चमचमाती हुई बनारसी साड़ी बुनते थे। अब अपना और परिवार का पेट पालने के लिए बैंड पार्टी में बाजा बजाते हैं। परिवार का भरण-पोषण मुश्किल से हो रहा है। योजना के नाम पर राशन मिल रहा है। उसे आप विकास कह लीजिये या सरकार का एहसान।”
मोहम्मद अली कहते हैं “बुनकरी के काम-धंधे को पहली चोट अटल जी के सरकार में लगी. उनके बाद के सरकारों ने बुनाई\बुनकरों को मुख्यधारा से जोड़ने का कोई विशेष काम नहीं किया। रही-सही कसर मोदी व योगी ने पूरी कर दी। कोविड-19 (कोरोना महामारी) ने मांग-आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त कर दिया। बनारस शहर की बड़ी-बड़ी गद्दियां (जहां से बनारसी साड़ी, दुपट्टे व शॉल के ऑर्डर लिए जाते थे, फिर बुनकर माल तैयार करते थे. तैयार माल वापस गद्दी पर आता था, जहां से देश-विदेश भेजे जाते थे।) अब हालत ऐसी हो गई है कि एक बुनकर अगर करघे पर 10-11 घंटे तक खटता भी है तो वह परिवार का पेट नहीं भर सकता। और भी जरूरतें है दवाई, फीस, शादी, विवाह, राशन-किराना आदि।”

पिता के निधन के बाद कमौली की किशोरी नाजो ने सतवीं के बाद गरीबी के पढ़ाई छोड़ दी। नाजो ने बताया कि “जीवन के बहुत कठीन दौर से हमारा परिवार गुजर रहा है। सरकारी सुविधा के नाम पर हमलोगों को सिर्फ राशन मिलता है। न आवास मिला और न ही बुनकर कार्ड बनाया गया। मिट्टी का घर बारिश में ढह जाने पर कर्ज लेकर और मजदूरी कर रहने के लिए एक कमरे का घर बन पाया। माला बनाने का काम बहुत मेहनत, ध्यान और ताजा आँखों का है। दिनभर सुई लेकर आंख गड़ाकर बच्चों की कलाई का ब्रासलेट (माला) बनाने पर बहुत कम पैसे मिलते है। एक ब्रासलेट बनाने में 10 से 12 मिनट लगात है। औसतन ढाई घंटे आंख गड़ाकर 12 ब्रासलेट बनाने पर 6 रुपए मिलते हैं। कोई और काम है नहीं तो मजबूरी है, यही करते हैं।”

गौरतलब है कि असंगठित क्षेत्र में रोज़गार गारंटी न होने के कारण रोज़गार का स्वरूप अस्थायी होता है, जो इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हतोत्साहित करता है। अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम करते हैं, जहाँ श्रमिक कानून लागू नहीं होते। इसलिये इनकी कार्य दशा भी सुरक्षित नहीं होती और इनके लिये स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत अधिक होते हैं।
बकरीद्दू सप्ताह के दो से तीन तीन बेकारी में ही गुजर जाते हैं। वे आठ-नौ साल से मजदूर का काम यहां-वहां ढूंढकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। बकरीद्दू पहले साड़ी बुनकरी का काम करते थे, लेकिन अब बुनाई का यह फ़नकार मजदूरी कर गुजारे को विवश है।
शबाना कहती हैं “माला बनाने में मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते है। दो दिन काम करेंगे तब जाकर 15 से 20 रुपए का काम हो पाता है। इसके लिए मेरी सास और देवरानी भी मेरे काम में हाथ बटाती हैं। यानि हफ्ते भर का अधिकतम 150 रुपए हुए। इस कमर तोड़ती महंगाई में, जहां सबकुछ खरीदकर ही खाना है, ऐसे में गुजारा कैसे हो रहा है ? इसका अंदाजा लगाना कठीन नहीं है। ये मजदूरी भी एक-डेढ महीने बाद मिलती है। मजदूरी उचित मिलती तो काम में भी मन लगता, लेकिन बेरोजगारी के चलते बेगारी करनी पड़ती है। बैठे-बैठे घुटने और आँख में दर्द हो जाता है। इस वजह से कई दिनों तक परेशान रहना पड़ता है। हमारे परिवार का एक सदस्य विकलांग है। जिसका विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए चार से पांच बार आवेदन करने के बाद भी नहीं बना।”

जुलाहा समाज की महिलाओं का कोई संगठन या संघ नहीं है जो इनके हक और अधिकार की बात रख सके. हजारों महिलाएं घरेलू स्तर से जुड़ी हुई हैं। इनका कोई संघ नहीं है जो उनके काम का अनुबंध तैयार करें। इन वजहों से यहां काम और काम के घंटे और शोषण अधिक है।
भारत की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 के अनुसार, 2019-20 के दौरान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 43.99 करोड़ है। कमौली, कोटवा, सरायमोहाना और आसपास के गांवों में माला बनाने, कढ़ाई और टंकाई करने वाली महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। इस वजह से ये सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ से भी वंचित हैं।

भारत सरकार मानती है कि कोरोना महामारी ने देश के सभी तरह के उद्योग-धंधे को नुकसान पहुंचाया। श्रमिकों को दुबारा काम और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अक्टूबर 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली करना है, लेकिन बुनकर परिवारों में महिलाएं योजना और सुविधा से कोशो दूर और दो वक्त की रोटी चलाने के लिए जूझ रही हैं।
(पवन कुमार मौर्य स्वतंत्र पत्रकार हैं)