“अबुआ दिशुम, अबुआ राज” मतलब अपना देश, अपना राज। यह नारा था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोही जननायकों का, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत, महाजनी प्रथा और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए सामंतों के शोषण के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। जिसका ही परिणाम है कि आजादी के बाद इस नारे की सार्थकता पर अलग झारखंड राज्य की अवधारणा बनी। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद झारखंड नाम के अलग राज्य का गठन हो पाया।
अलग राज्य गठन के 23 वर्षों बाद भी झारखंड के 86.5 लाख आदिवासी जनसंख्या में से अधिकांश आज शोषण, उत्पीड़न, भय, पलायन, भूख, कुपोषण, एनीमिया जैसी असंख्य समस्याओं के मकड़जाल में जिन्दगी जीने को विवश हैं। जबकि देश के विकास में झारखंड की 40 फीसदी खनिज सम्पदाओं का योगदान है। सिर्फ इतना ही नहीं यहां की कुल भूमि का लगभग 29 प्रतिशत वनभूमि जो मूलत: आदिवासी इलाकों में अवस्थित है, इन जंगलों को बचाकर जलवायु परिवर्तन के संकट से भी देश ही नहीं बल्कि विश्व को बचाने में झारखंड के लोग अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बावजूद इसके हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का हर दूसरा आदिवासी गरीबी की चपेट में है यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर है।
वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भी दुनिया के 121 देशों में से भारत का स्थान शर्मनाक तरीके से 107 वें नम्बर पर है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में 2016 से कोविड काल 2019-20 तक जनसंगठनों द्वारा संधारित आंकड़ों के अनुसार 33 लोगों ने भूख एवं कुपोषण की वजह से असमय दम तोड़ दिए। जिसमें सिमडेगा की 14 वर्षीय संतोषी कुमारी की भूख से हुई मौत की घटना काफी चर्चे में रही। संतोषी की भूख से हुई मौत का दर्दनाक पहलू यह था कि वह “भात दे, भात दे” कहते हुए दम तोड़ दी। क्योंकि वह पेट की आग बुझाने के लिए स्कूल के मध्याह्न भोजन पर ही पूरी तरह आश्रित थी और उसका स्कूल बंद था, उसे चार दिनों से खाना नहीं मिला था। इस घटना ने पूरे सभ्य समाज को विचलित कर दिया था।
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, जो वर्ष 2019-21 में संपन्न की गई, के अनुसार झारखंड में 67.5 प्रतिशत बच्चे एनीमिक हैं। 15 से 49 वर्ष की सामान्य महिलाओं में 65.7% महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम से कम है। इसी उम्र समूह की 56.8% गर्भवती महिलाएं हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 29.6 % ऐसे पुरुष हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम से कम है यानी हर तीसरा पुरुष एनीमिक है।
जब पोषण के इन विभिन्न आयामों को आदिवासी आबादी उसमें भी खासकर विशिष्ट जनजाति समुदायों पर विश्लेषित करते हैं तो स्थिति और भी चिंताजनक होती है। एक स्वस्थ वयस्क की दैनिक खाद्य जरूरतें 1207 ग्राम हैं, जिसमें अनाज, दाल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, सब्जियां और फल शामिल हैं। इसी भांति भारत में गरीबी का मानदण्ड मुख्यतः 1979 में गठित अलघ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2,400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2,100 कैलोरी प्रतिदिन से कम ग्रहण करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है।
अनुशंसित खाद्यान्न अथवा कैलोरी मात्रा के बदले हम जो कुछ भी उपभोग कर पा रहे हैं या जन वितरण प्रणाली के जरिये सरकार हमें चैरिटी भाव से उपलब्ध करा पा रही है, वह हमारी दैनिक खाद्य व पोषण जरूरत का एक तिहाई हिस्सा मात्र है। इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को प्रति माह न्यूनतम 14 किलो खाद्यान्न की जरूरत होती है। लेकिन जन वितरण में लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज देने की बात की गई है। मानव स्वास्थ्य सिर्फ अनाज से सुनिश्चित नहीं हो सकता, बल्कि दाल, तेल, दुग्ध उत्पाद, सब्जियां और फल जैसे पोषण तत्व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक आयाम हैं।
भूमिहीन और दैनिक मजदूरी से वंचित राज्य के 2 लाख 92 हजार विशिष्ट जनजाति परिवार जो पूर्णत: पीडीएस अनाज पर निर्भर हैं, वे सरकार से मिलने वाले राशन से सिर्फ 2 सप्ताह ही खर्चा चल पाते हैं। शेष समय के लिए वे जंगलों से लकड़ी, दतुवन (दातौन), दोना, पत्तल इत्यादि बेचकर खर्चा चलाते हैं।
कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार?
राष्ट्रहित एवं देश के विकास के नाम पर भारत की सरकारों ने 1951 से 1995 तक 15 लाख से अधिक लोगों को बिना किसी समुचित पुनर्वास के उनके व्यवस्थित जीविकोपार्जन के साधनों से बेदखल किया। जिनमें 6 लाख 20 हजार से अधिक आदिवासी, 2 लाख 12 हजार से अधिक दलित और शेष अन्य समुदाय शामिल हैं। आजादी के पूर्व टाटा कारखाना और दूसरे बड़ी परियोजनाओं तथा झारखंड अलग राज्य गठन के बाद भी विस्थापन का दर्द झारखंडियों खासकर आदिवासियों के समक्ष हमेशा मंडराता रहा है और इस दौर में विस्थापितों की संख्या 15 लाख में शामिल नहीं है।
झारखंड में 11 हजार गांव हैं जो वन क्षेत्र में स्थित हैं। इन गांवों की 40 फीसदी यानी 12 महीने में से 7 माह की खाद्य जरूरतें जंगलों से पूरी होती हैं। आदिवासियों ने सदियों से प्रकृति के साथ सुसंगत और जंगली जीव जंतुओं के साथ सहजीविता का सम्बन्ध रखते हुए वनोत्पादों का उपभोग करते रहे हैं। लेकिन सरकारें और वन विभाग, कार्पोरेट घराने वन कानूनों की आड़ में आदिवासियों को अतिक्रमणकारी साबित करने की कोशिश करते रहे हैं।
नक्सल आन्दोलन को नियंत्रित करने और नक्सल उन्मूलन के नाम पर आदिवासी इलाकों में अर्द्ध सैनिक बलों के हजारों कैम्प और पुलिस थाने स्थापित किये जाते रहे हैं। ऐसे हालात में आज उन इलाकों के आदिवासी जंगलों में मिलने वाले खाद्य पदार्थों को स्वच्छंद तरीके से संग्रहित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी नक्सल होने का इल्जाम लगाकर उनके साथ कुछ भी सरकारी प्रताड़ना की जा सकती है। वन विभाग के प्लान्टेशन योजनाओं में कोई भी ऐसे पेड़-पौधे शामिल नहीं करती जो इंसानों या जीव-जंतुओं के खाद्य या स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करता हो।
इस बाबत नरेगा वाच के राज्य संयोजक जेम्स हेरेंज बताते हैं कि ‘हाल के वर्षो में जलवायु परिवर्तन खाद्य असुरक्षा का एक प्रमुख कारण बनकर एक नई चुनौती पैदा कर दी है। इसके कारण लम्बे समय तक चलने वाले हीट वेव्स ने जंगलों में लगने वाली आग के लिए उपयुक्त गर्म और शुष्क परिस्थितियां पैदा की हैं। तापमान में वृद्धि और वनस्पति पैटर्न में बदलाव ने पक्षी प्रजातियों सहित नदियों व समुद्री प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारे खेतों और नदियों से अनेकों प्रकार की मछलियां गायब हो गईं, जो लोगों के लिए प्रोटीन की सहज स्रोत थीं। इसी प्रकार ग्रामीण परिवारों के आर्थिक स्रोत में अहम योगदान देने वाले पशुओं की आज विभिन्न बीमारियों के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों की आर्थिक कमर टूट जाती है’।
वे आगे कहते हैं कि ‘झारखंड के आदिवासियों को यदि उनके इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर आना है तो आज के इस क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर में फिर एक उलगुलान करना ही होगा। उसे राजसत्ता से टकराना होगा। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा ने रिसोर्से पॉलिटिक्स का जो सवाल उठाया था, वह आज भी प्रासंगिक है’।
जेम्स हेरेंज सवाल उठाते हुए कहते हैं कि ‘जब हमारे आदिवासियों के 40 फीसदी संसाधनों से देश संचालित हो रहा है तो उससे प्राप्त होने वाली रॉयल्टी पर आखिर कौन लोग कुण्डली मारे बैठे हैं? हमें भीख नहीं हमारी हिस्सेदारी चाहिए’।
बताते चलें कि भारतीय संविधान में उल्लेखित 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 (1) और (2) में आदिवासियों को पूर्ण स्वशासन व नियंत्रण की शक्ति दी गयी है। झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में राज्यपाल को शासन करना है। लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी किसी राज्यपाल ने इन क्षेत्रों के लिए अलग से कोई कानून नहीं बनाया। परिणामतः गैर अनुसूचित (अर्थात सामान्य) जिले के नियम कानून ही आज तक आदिवासियों के ऊपर लादे जाते रहे हैं।
अनुच्छेद 19 (5) और (6) में आदिवासियों के स्वशासन व नियंत्रण क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र) में गैर-लोगों के मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं। मतलब कि कोई भी गैर-लोग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत निर्बाध गति से निवास, व्यवसाय, जमीन की खरीद आदि नहीं कर सकते। यहां तक कि गैर-लोगों को इन इलाकों में प्रवेश के लिए वहां के परम्परागत प्रधानों से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई काम पिछले 60-70 सालों से चलन में नहीं रहने की वजह से यहां के गैर-लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।
अनुच्छेद 244 (1) कंडिका (5) (क) में विधानसभा या लोकसभा द्वारा बनाया गया कोई भी सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्रों में हू-ब-हू लागू नहीं हो सकते। जैसे आईपीसी एक्ट, सीआरपीसी एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1991, भूमि अधिग्रहण कानून, आबकारी अधिनियम, भू-राजस्व अधिनियम, पंचायत अधिनियम 1993, नगर पंचायत अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, परिवहन अधिनियम, भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1956 आदि।
अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को किसी भी विधान मण्डल या व्यवहार न्यायालय का अनुसरण करने की बात कही गयी है। ‘लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्रामसभा’, वेदांता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 18 अप्रैल 2013 को सुनाया था।
वहीं पेसा कानून-1996 जो आदिवासियों के अपने अधिकारों की लड़ाई का एक सार्थक हथियार माना जाता है, यह 27 वर्षों की एक चौथाई सदी का अन्तराल गुजर जाने के बावजूद इस कानून पर नियमावली नहीं बन पाई है।
इस बावत आदिवासी मामलों के जानकार इमिल वाल्टर केन्डुलना सवाल करते हैं- सरकारें उस पर सही नियमावली बनाने से क्यों कतरा रही हैं? वे कहते हैं कि ‘दुखद यह है कि पेसा कानून -1996 के effects & implications (प्रभाव और निहितार्थ) क्या हैं या क्या होंगे अथवा क्या हो सकते हैं? इसकी सम्पूर्ण जानकारी आदिवासियों को छोड़ कर अन्य सभी लोगों को है। अभी तक पेसा कानून -1996 को लेकर नियमावली नहीं बन पाने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम आदिवासी अभी भी पेसा कानून को सही तौर से समझ नहीं पाये हैं।
दरअसल हमें सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि पेसा कानून के द्वारा आदिवासियों की समूची परंपरागत सामाजिक-आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था तंत्र (traditional socio-economic and administrative system) को संवैधानिक मान्यता दी गई है। दूसरे शब्दों में इस कानून को हम संविधान का अनुच्छेद 13 (3) a और संविधान के पाचवीं अनुसूची का सूक्ष्म स्तर (MICRO-LEVEL) का विस्तारीकरण (Extension) भी मान सकते हैं।
केन्डुलना कहते है कि पेसा कानून आदिवासियों के रीति-रिवाज़ को समर्थन और रेखांकित करता है। मतलब अपने गांव से लेकर जिला स्तर तक के आदिवासी समुदायों के लिए खुद से अपने हित के लिए नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। यह कानून कोई व्यक्तिगत स्तर के अपराधों का कानून नहीं है, बल्कि वैसे किन्हीं भी अपराधों के रोकथाम के लिए नियम और नीतिगत पॉलिसी अथवा सबकी उन्नति के लिए आईन-कानून बनाने की संरचनात्मक व्यवस्था और शक्ति है।
हमें आज यह भी समझना जरूरी है कि आज की लड़ाई तीर-धनुष या तलवार की नहीं बल्कि कानूनों की लड़ाई है, और इस लड़ाई में पेसा कानून एक बहुत बड़ा हथियार है। वे आह्वान करते हैं कि पेसा कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने-कराने लिए हम सबको अपने अन्तर्विरोधों से ऊपर उठकर एकजुट होना ही पड़ेगा।
पूर्व सांसद सालखन मुर्मू विश्व आदिवासी दिवस की प्रासंगिकता पर कहते हैं- दुनिया की लगभग 7,000 भाषाओं में से 40% भाषाएं विलुप्ति के कगार पर हैं, जिसमें सर्वाधिक आदिवासी भाषाएं हैं। अतः उनकी संरक्षण हेतु यूएन ने आदिवासी भाषा दशक (2022 से 2032) घोषित किया है। इन परिस्थितियों के बीच 9 अगस्त को दुनिया के लगभग 90 देशों के 47 करोड़ आदिवासी या इंडीजीनस पीपल जन्मदिन या बर्थडे की तरह इसे मना रहे हैं। मरते-मरते भी थोड़ी खुशी मना लेना है, क्या पता पुनर्जन्म हो जाय।
जैसा कि सर्वविदित है कि विश्व आदिवासी दिवस का अनुपालन 9 अगस्त 1994 से संयुक्त राष्ट्र ने प्रारंभ किया है। चूंकि 9 अगस्त 1982 को जेनेवा में सर्वप्रथम यूएन ने आदिवासियों के मानवीय अधिकारों पर चर्चा की थी। तत्पश्चात 13 सितंबर 2007 को यूएन ने आदिवासी अधिकार घोषणा- पत्र भी जारी किया है।
सालखन कहते हैं- “दुनिया भर के आदिवासी नशापान, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, राजनीतिक कुपोषण और आपसी समन्वय की कमी से टूटते, बिखरते, लड़ते-लड़ते मर रहे हैं। भारत देश में आदिवासियों (एसटी) के आरक्षण कोटे से 47 लोकसभा आदिवासी सांसद और 553 आदिवासी विधायक हैं। मगर देश में कोई आदिवासी नेतृत्व और आदिवासी आवाज नहीं है। संविधान प्रदत्त अनेक अधिकार हैं। मगर किसी राजनीतिक दल और सरकारों ने अब तक इसे तवज्जो नहीं दी है।
अब जबकि देश की राष्ट्रपति और मणिपुर की राज्यपाल भी आदिवासी महिलाएं हैं। मगर मणिपुर में आदिवासी महिलाएं खुलेआम दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। राजनीतिक फायदे और आदिवासी आरक्षण लूटने के लिए अब देशभर के आदिवासी क्षेत्रों में मणिपुर की आग फैलने की आशंका है”।
अनेक समृद्ध और अधिसंख्यक जातियों को राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीतिक लाभ के लिए असली आदिवासियों (संताल, मुंडा, उरांव, गोंड, भील आदि) को बलि का बकरा बना रहे हैं। इसी आलोक में कुर्मी महतो को एसटी बनाने के सवाल पर जेएमएम, टीएमसी, बीजेडी और कांग्रेस ने खुलेआम समर्थन दे दिया है। तब असली आदिवासियों की हालत कुकी-नागा आदिवासियों की तरह होना निश्चित जैसा है।
जातीय संघर्ष के इस नरसंहार को कुछ सरफिरे हिंदू-ईसाई का चोला पहना रहे हैं, जो न्याय और मानवता की दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुचित है। अच्छा होगा नई जातियों को एसटी सूची में शामिल करने के दरवाजे को अभी अगले 30 वर्षों तक बंद कर देना चाहिए। ताकि इस बीच में पहले से एसटी सूची में शामिल आदिवासियों की दशा-दिशा की समीक्षा और भविष्य में उनकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक मजबूत रोड मैप बनाया जा सके।
दूसरी तरफ विकास की अंधी दौड़ ने दुनिया भर में प्रकृति-पर्यावरण को भी नहीं छोड़ा तो आदिवासी किस खेत की मूली हैं। अतः 2023 का विश्व आदिवासी दिवस भारत और झारखंड के आदिवासियों के लिए केवल नाचने-गाने का अवसर ना होकर अपनी अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी के रक्षार्थ एकजुट होकर, दिल थाम कर शपथ और संकल्प लेने का आखरी मौके जैसा है।
आदिवासी समन्वय समिति, झारखंड के लक्ष्मी नारायण मुंडा कहते हैं कि 15 अगस्त को देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। वहीं 9 अगस्त को पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस मना रही है। जबकि आज आदिवासी समुदाय पर चौतरफा हमला तेज हो गया है। एक ओर जहां केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (UCC), वन संरक्षण संशोधन विधेयक जैसे कानूनों को ला रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय को मिले संविधान प्रदत्त कानूनों को समाप्त करने में लगी हुई है।
देश और राज्यों में काबिज सरकारें कॉरपोरेट, पूंजीपतियों, व्यापारिक समूहों के हितों के पक्ष में नतमस्तक हो कर खड़ी हैं। यहां की राजनीतिक पार्टियां, राजनेता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी कॉरपोरेट, पूंजीपति, माफिया, दलाल-बिचौलियों के साथ गठजोड़ करके देश को लूट रही हैं और आम जनता के ज्वलंत सवालों-जनमुद्दों को दरकिनार कर रही हैं।
आज देश के अंदर विभिन्न राज्यों में ब्राह्मणवादी-सवर्ण-सामंती मनुवादी सोच वाली ताकतों द्वारा दबे-कुचले लोगों, आदिवासियों, दलितों-पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को कुचला जा रहा है। इन तबकों के साथ आए दिन हत्या, बलात्कार, शोषण-जुल्म होता आ रहा है। इसमें भी मुख्य निशाना आदिवासी समुदाय ही रहा है। मणिपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में घट रही घटनाएं इसके सशक्त उदाहरण हैं। इसी विषम परिस्थितियों के बीच आज आदिवासी समुदाय के संवैधानिक हक-अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व/ हिस्सेदारी, नौकरी, जमीन को हड़पने के लिए आदिवासी बनने की मांग की जा रही है।
इसमें सबसे आगे कुड़मी/ कुरमी/महतो जाति समुदाय के लोग हैं। इसके लिए लगातार कुड़मी/कुरमी/महतो समुदाय के लोगों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। इस समुदाय के लोगों का मकसद मूल आदिवासियों के हक़ अधिकारों को हड़पना और इनकी संघर्षशील गौरवशाली इतिहास, पहचान, अस्तित्व को मिटाकर अपने जाति-समुदाय को स्थापित करना है। एक तरह से देखें तो कह सकते हैं कि घोषित/अघोषित तौर पर आदिवासी समुदाय के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया है। ऐसे समय में आदिवासी समुदाय को एकजुट होकर इसके विरोध में खड़ा होने का समय है।
मुंडा कहते हैं कि आदिवासी समुदाय कई धड़ों में बंटा हुआ है। विरोधी ताकतों का चौतरफा हमला जारी है, ऐसे में हम सभी आदिवासी समुदाय के लोगों को एकताबद्ध होकर इसका प्रतिरोध करना होगा।
यह लड़ाई सांस्कृतिक और राजनीतिक भी है। आदिवासी समुदाय के विद्वानों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं, आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों, छात्रों- नौजवानों, महिलाओं को इस पर चिंतन-मनन करना होगा। विशेषकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं-कार्यकर्ताओं को अपनी-अपनी राजनीतिक पार्टियों का गुलामी छोड़कर आदिवासी समुदाय के ऊपर हो रहे चौतरफा हमलों के खिलाफ मुंह खोलना होगा। महज़ पद, पावर, रुपये-पैसे के लिए अपना जमीर बेच डालने की आदत से बाहर आना होगा।
(विशद कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं।)






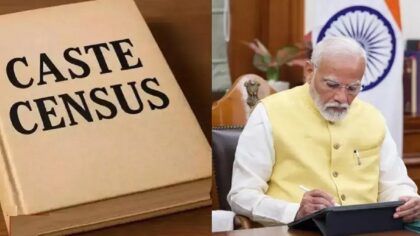











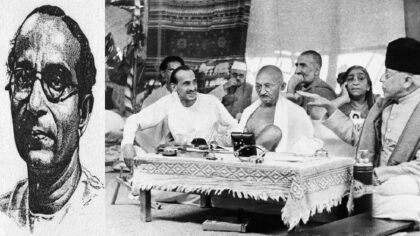







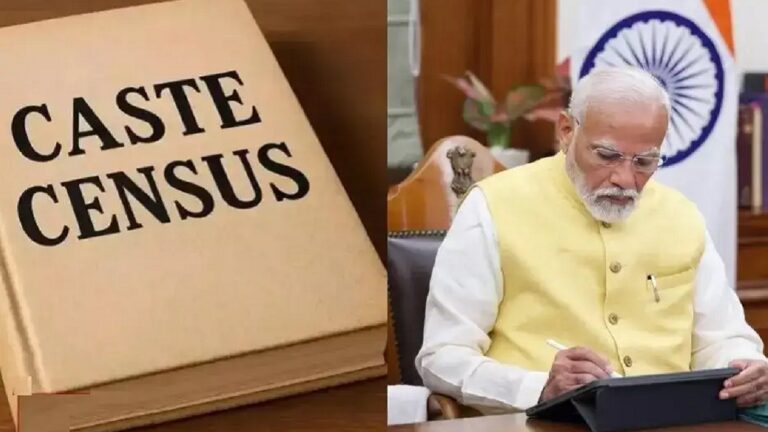

+ There are no comments
Add yours