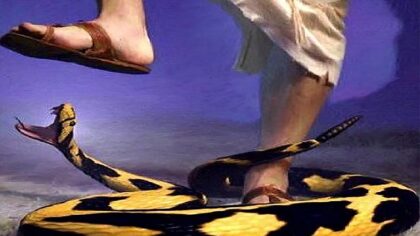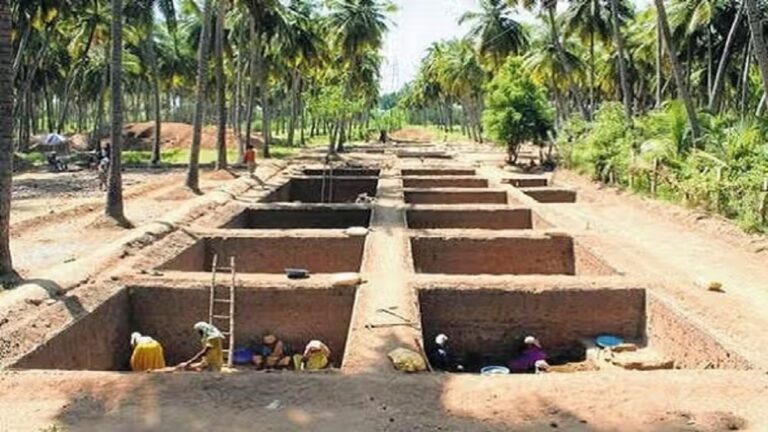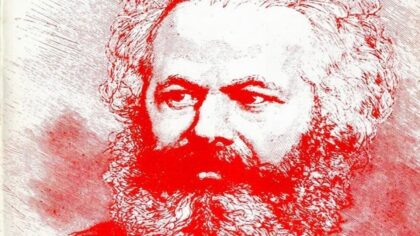प्राचीन काल से लेकर आज तक विश्व के प्रत्येक देश में ऐसे महापुरुष एवं समाज सुधारक, राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, लेखक, वैज्ञानिक, संत, महात्मा, राजनीतिज्ञ एवं क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने मानवता को नई दिशा एवं नया प्रकाश देकर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इन महापुरुषों एवं महिलाओं की आकाशगंगा में डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम ध्रुव तारे की तरह चमकता है और विश्व के अधिकांश देशों में समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। यही कारण है कि 14 अप्रैल को विश्व के लगभग 150 देशों में उनकी जयंती मनाई जाती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने घोषणा की कि अंबेडकर की जयंती हर साल मनाई जाएगी और 14 अप्रैल को ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर दिवस’ के रूप में घोषित किया। सबसे खास बात यह है कि अंबेडकर जयंती उत्तर कोरिया में मनाई गई और इस अवसर पर उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने अंबेडकर के योगदान को मानवता के लिए महत्वपूर्ण माना।
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (14 अप्रैल, 1891- 6 दिसम्बर, 1956) भारतीय संविधान के जनक, उसके निर्माता, शिल्पकार एवं वास्तुकार, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय गणराज्य के निर्माता, भाषाविद्, स्वतंत्र एवं निर्भीक पत्रकार, किताब प्रेमी, राजनीतिज्ञ, सांसद, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, सामाजिक क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक, जाति-पाति एवं छुआछूत उन्मूलन के समर्थक, अन्याय पर आधारित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के कट्टर विरोधी, दार्शनिक एवं विचारक, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों के हमदर्द, अछूतों एवं वंचित वर्ग के पक्षधर एवं मसीहा, असमानता एवं विषमता पर आधारित समाज के विरुद्ध महान आंदोलनकारी एवं संघर्षशील विचारक एवं उच्च वर्ग के समर्थक थे।
समाज सुधारक के रूप में वे मनुवाद-ब्राह्मणवाद पर आधारित जात-पात उन्मूलन के प्रमुख पक्षधर थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण के बिना कोई भी समाज सुधर एवं विकसित नहीं हो सकता। इस अर्थ में वे महिला सशक्तीकरण के अग्रदूत थे। उन्हें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का समर्थक माना जाता है।
> (https://samajweekly।com/dr-b-r-ambedkar-as-a-journalist)
>https://theasianindependent।co।uk/the-indian-constitution-and-dalit-emancipation/ 29।11 23
>डॉ. रामजीलाल ,https://samajweekly।com/objectives-of-the-constitution-of-india/
अंबेडकरवाद की अवधारणा एवं मुख्य विशेषताएं
डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा समय-समय पर समाचार पत्रों, पुस्तकों, भाषणों, ज्ञापनों, संविधान सभा की बहसों आदि में विभिन्न समस्याओं और मुद्दों के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों का व्यवस्थित रूप ही अंबेडकरवाद या अंबेडकर की सोच माना जाता है। अंबेडकरवाद आज एक ऐसी विचारधारा है जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह दुनिया के राजनेताओं से लेकर समाज के हाशिए पर खड़े आम लोगों तक सभी का मार्गदर्शन करती है।
अम्बेडकरवाद विचारों का एक समूह है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, मानव गरिमा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद, और समाज के हाशिए पर पड़े उपेक्षित वर्गों-दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, लघु किसानों और कृषि विहीन कृषि श्रमिकों, संगठित एवं असंगठित श्रमिकों का सशक्तिकरण, उत्थान तथा एक-एक ऐसे समतावादी समाज की स्थापना शामिल है, जहां बुनियादी जरूरतें भोजन, आश्रय, वस्त्र, सार्वभौमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, काम करने का अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार पूरी हों।
अंबेडकरवादी चिंतन इस बात का समर्थन करता है कि महत्वपूर्ण उद्योगों पर सार्वजनिक नियंत्रण (राष्ट्रीयकरण) होना चाहिए। इस दृष्टि से अंबेडकरवादी चिंतन वर्तमान शताब्दी में प्रचलित उदारीकरण, निजीकरण,एवं वैश्वीकरण सहित कॉरपोरेटीकरण के विरुद्ध है। यही कारण है कि अंबेडकर समाजवादी चिंतकों के अग्रिम दस्ते की श्रेणी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
अम्बेडकरवाद एक ऐसे समाज की स्थापना की कल्पना करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य जीवन के हर क्षेत्र में समान हो, न कि जन्म, जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा, लिंग आदि की संकीर्णताओं और सांप्रदायिक अवधारणाओं के आधार पर दूसरे शब्दों में, समाज एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। भारत में जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा और संस्कृति के आधार पर बहुत अधिक विविधताएं हैं। इसलिए, सामाजिक सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए ‘विविधता में एकता के मूल सिद्धांत’ की वकालत करता है।
अम्बेडकरवाद असमानता, सामाजिक अन्याय, अमानवीय व्यवहार, अस्पृश्यता, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, नौकरशाही के जन-विरोधी रवैये, बहुसंख्यकवाद की तानाशाही, हिंसक आंदोलनों, धर्म-आधारित या धर्म-प्रधान राज्यों, द्वि-राष्ट्र सिद्धांत और हिंदू या मुस्लिम राष्ट्रों के खिलाफ है।
अंबेडकरवाद के अनुसार जातिवाद तथा वर्ण व्यवस्था के कारण उत्पन्न अस्पृश्यता संकुचित, विभाजक, अमानवीय ,अनैतिक अवैज्ञानिक एवं संकीर्ण है। अस्पृश्यता एवं चतुर्वर्ण व्यवस्था विभाजक होने के कारण सामाजिक एकता व सामाजिक एकीकरण व राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय एकीकरण व सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में अवरोध है। अंबेडकरवाद के अनुसार अस्पृश्यता के कारण दलित वर्ग को अपमान झेलना पड़ रहा है। अंबेडकर की धारणा है कि ‘सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है।’’
परिणाम स्वरूप अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष करके सम्मानपूर्वक जीवन हेतु वर्ण व्यवस्था को समूल नष्ट करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी धारणा है कि वर्ण व्यवस्था ने भारत को मुर्दा बना दिया तथा भेदभाव ने दलित वर्ग को शक्तिहीन, अयोग्य एवं पंगु कर दिया। यही कारण है कि भारत में यूरोपीय देशों की भांति कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई। सामाजिक क्रांति के बिना सामाजिक गुलामी, शोषण, असमानता, अत्याचार एवं अपमानजनक जीवन समाप्त नहीं होगा। अतः एक समाज सुधारक के रूप में वह मनुवाद, ब्राह्मणवाद पर आधारित जाति प्रथा के उन्मूलन के मुख्य पैरोकार थे।
अंबेडकर स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के बिना किसी भी समाज का सुधार और विकास नहीं हो सकता। इस दृष्टि से वह महिला सशक्तीकरण के अग्रदूत थे।
दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य का उद्भव : आपराधिक मानसिकता
यद्यपि एक ओर भारत में डॉ. अंबेडकर की जयंती पर अनेक समारोह, सेमिनार, परिसंवाद आदि आयोजित किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अंबेडकरवादी विचारधारा के विरोधियों द्वारा उनकी प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने, तोड़ने व नुकसान पहुंचाने, पुतले व चित्र जलाने की खबरें अमृतसर (पंजाब) से, वाराणसी (यूपी) तक, अहमदाबाद (गुजरात) से हरियाणा,(बुड्ढा खेड़ा थाना उकलाना) तक, बिहार से आंध्र प्रदेश तक समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती हैं।

भारतीय समाज में दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य उभर रहा है। वास्तव में यह दो धारी तलवार की तरह है। एक ओर अंबेडकरवाद व अंबेडकर के योगदान के महत्व को कम करना और दूसरी ओर अनुसूचित जातियों का अपमान व दमन करना है। ’जातिगत भेदभाव’ अथवा ‘छिपे हुए रंगभेद’ के कारण अत्याचार, अपराध और हिंसात्मक घटनाओं में निरंतर वृद्धि दलितों के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र और समाज के लिए भी हानिकारक है।
>हिंदू राष्ट्र दलितों वंचितों के लिये नुक़सानदायक होगा? https://www।satyahindi।com/analysis/hindu-rashtra-be-harmful-for-dalits-and-deprived-138450।html
अंबेडकरवाद के समक्ष चुनौतियां
प्रथम-भेदभाव और असमानता – अंबेडकरवाद भारतीय लोकतंत्र व राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में समाज में प्रचलित भेदभाव और असमानता सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। संविधान सभा के आख़िरी दिन डॉ. बी आर अंबेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को, हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं।
राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी”।डॉ. अंबेडकर ने कहा,‘राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र अर्थात जीवन के सिद्धांतों में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता न हो।
समानता के बिना स्वतंत्रता बहुसंख्यक वर्ग पर मुट्ठी भर लोगों का प्रभुत्व स्थापित कर देगी।
बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक सी बातें नहीं लगेगी। भेदभाव और असमानता दूर करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह लोग जो भेदभाव का शिकार होंगे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे जो इस संविधान सभा ने तैयार किया है।’
सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने की आवश्यकता लिए सामाजिक भेदभाव और असमानता को दूर करके ही स्थाई लोकतंत्र की स्थापना और संविधान की सुरक्षा भी की जा सकती है।
परिणाम स्वरूप अंबेडकरवाद के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करके राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया जारी रहती है। और यदि ऐसा नहीं होता तो वास्तव में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण,आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास और शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रियाओं में बाधाएं पैदा होंगी ।
द्वितीय- राजनीति में भक्ति या नायक-पूजा-अंबेडकरवादी चिंतन के अनुसार वर्तमान समय में राजनीति में भक्ति या नायक-पूजा’ एक महत्वपूर्ण चुनौती है। डॉ.अंबेडकर ने सचेत किया था कि लोकतंत्र के निर्माण में ‘राजनीति में भक्ति या नायक-पूजा’ एक महत्वपूर्ण चुनौती है और अंततः तानाशाही का एक निश्चित रास्ता है’।
डॉ. अंबेडकर ने इस संबंध चेतावनी देते हुए लिखा “उन महान व्यक्तियों के प्रति आभारी होने में कुछ भी गलत नहीं है जिन्होंने देश को जीवन भर सेवाएं प्रदान की हैं। लेकिन कृतज्ञता की भी सीमाएं हैं।
जैसा कि आयरिश देशभक्त डेनियल ओ’कोनेल ने ठीक ही कहा है, कोई भी पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। यह सावधानी किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत के मामले में कहीं अधिक आवश्यक है।
भारत में, भक्ति या जिसे भक्ति या नायक पूजा का मार्ग कहा जा सकता है, उसकी राजनीति में दुनिया के किसी भी अन्य देश की राजनीति में निभाई जाने वाली भूमिका के बराबर नहीं है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है।लेकिन राजनीति में, भक्ति या नायक-पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित रास्ता है”
जान स्टुअर्ट मिल को उद्धृत करते हुए अंबेडकर ने कहा था, “अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए…इस नवजात प्रजातंत्र के लिए यह बिल्कुल संभव है कि वह आवरण प्रजातंत्र का बनाए रखे, परंतु वास्तव में वह तानाशाही हो। चुनाव में महाविजय की स्थिति में दूसरी संभावना के यथार्थ बनने का खतरा अधिक है।”
अतः अंबेडकरवादी विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि अंधभक्ति लोकतंत्र के लिए घातक और नुकसानदेह है क्योंकि यह तार्किक सोच को कमजोर करके तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करती है।
तृतीय- खूनी क्रांति, सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह.. डॉ भीमराव अंबेडकर के अनुसार “अगर हम लोकतंत्र को न केवल स्वरूप में, बल्कि वास्तव में भी बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वह है अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को मजबूती से अपनाना। इसका मतलब है कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों को त्यागना होगा।इसका मतलब है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का रास्ता छोड़ देना चाहिए।
जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का कोई रास्ता नहीं बचा था, तब असंवैधानिक तरीकों का औचित्य बहुत अधिक था।
लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके और कुछ नहीं बल्कि अराजकता का व्याकरण हैं और इन्हें जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही बेहतरहोगा।” हमारा सुनिश्चित अभिमत है कि लोकतंत्र में बंदूक तंत्र (खूनी तरीकों) का स्थान नहीं है। क्योंकि शक्ति (सत्ता) बंदूक की नली से पैदा नहीं होती अपितु चुनाव के समय मतदान के दिन के ईवीएम(EVM) का बटन दबाने से पैदा होती है।
परंतु इसके बावजूद भी दो चुनावों के अंतराल में शांतिपूर्ण आंदोलन सरकारों के सर्वसत्तावाद को नियंत्रित करने लिए जरूरी हैं।शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र व राष्ट्र निर्माण की कमजोरी नहीं है अपितु इनके प्रहरी हैं।
शांतिपूर्ण आंदोलनों का त्याग करने के वकालत जो डॉ अंबेडकर ने की है उससे सहमति प्रकट करना बड़ा कठिन है क्योंकि केवल संवैधानिक तरीके से ‘निर्वाचित तानाशाही’ पर नियंतण करना मुश्किल है।
इसलिए सत्याग्रह और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह,धरना, प्रदर्शन, हड़ताल इत्यादि- शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र व राष्ट्र निर्माण की कमजोरी नहीं है क्योंकि केवल संवैधानिक तरीके से निर्वाचित तानाशाही पर नियंत्रण करना मुश्किल है और इसलिए सत्याग्रह और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करता है जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।
डॉ. अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के समापन में ऐतिहासिक भाषण में वर्णनीत यह तीनों चुनौतियां अथवा चेतावनियां -सामाजिक असमानता, राजनीति में भक्ति या नायक-पूजा’ तथा खूनी क्रांति के तरीके (जैसे आतंकवाद, नक्सलबाड़ी आंदोलन व माओवादी हिंसक आंदोलन), आतंकवाद का परित्याग, वर्तमान 21वीं शताब्दी में आज भी पूर्णतया सार्थक और प्रासंगिक हैं।
सारांशत: शांतिपूर्ण जन आंदोलनों में वह शक्ति होती है जिसके द्वारा सर्वसत्तावादी शासकों को घुटने टेकने अपने निर्णयों या कानूनों को वापिस लेने अथवा कुर्सी छोड़ने के लिए मज़बूर किया जा सकता है।
>https://prasarbharati।gov।in/whatsnew/whatsnew_653363।pdf >https://thebasicstructureconlaw।wordpress।com/2022/11/26/remembering-ambedkars-last-speech-in-the-constituent-assembly/
चतुर्थ-जातिवाद और वर्ण व्यवस्था-भारत में जातिवाद का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद के अनुसार भारत में चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं।
शूद्र वर्ण का अर्थ नौकर अथवा अछूत है। शुद्र वर्ण की तुलना व्यक्ति के शरीर के पैरों से की गई है। इन चारों वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ स्थान पर तथा शूद्र को सबसे निम्न स्थान पर रखा गया है।
डॉ. अंबेडकर मनुवादी एवं ब्राह्मणवादी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के घोर विरोधी थे।
(लेखक डॉ. रामजीलाल समाज विज्ञानी एवं दयाल सिंह कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं और करनाल में रहते हैं)