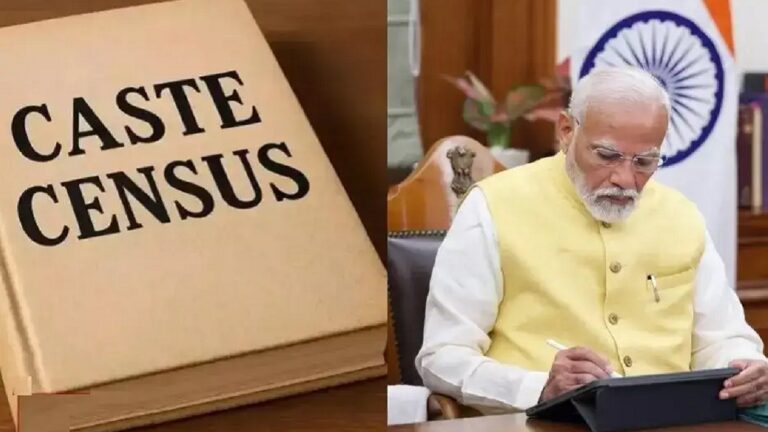हमारे शीर्ष सत्ताधारी नेताओं, बड़े नौकरशाहों और योजनाकारों ने कुछ बेहद सुंदर और सकारात्मक शब्दों के अर्थ बदल दिये हैं। ये सकारात्मक की जगह बेहद नकारात्मक बन चुके हैं। यह सब मौजूदा सत्ताधारियों के दौर की कहानी नहीं है। शुरुआत सन् 1990-91 में ही हो गयी थी। वह सिलसिला आज अपने भयावह रूप में सामने है। आज जब सरकार या प्रशासन का कोई बड़ा ओहदेदार किसी क्षेत्र में ‘सुधार करने’ की बात बोलता है तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि बड़े कारपोरेट घरानों के लिए कुछ बहुत अच्छा और आम जनता व समाज के लिए कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है! प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन और यूपी-पंजाब की चुनावी राजनीति के दबाव में आकर जिन तीन कृषि कानूनों को पिछले दिनों वापस लेने का ऐलान किया, उन कारपोरेट-पक्षी कानूनों को सत्ताधारियों ने ‘महान् सुधार’ ही कहा था। कैसी विडम्बना है! जो सुधार समाज, देश और जनतंत्र के लिए आज बेहद जरूरी हैं, उनकी तरफ हमारे सत्ताधारी बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। पर यहां मैं एक ऐसे जरूरी सुधार की चर्चा कर रहा हूं, जो वर्षों से लंबित है और जिसके लिए देश भर से आवाजें उठती रही हैं। यह है: चुनाव सुधार!
अनेक सुधारों की तरह अपने देश में चुनाव सुधार का मुद्दा लगातार लटकाया जा रहा है। समाज के बीच से इसकी पुरजोर मांग उठती है पर सरकार, मीडिया और न्यायपालिका, कहीं भी चुनाव सुधार को ज्यादा महत्व नहीं मिलता। सुधार के ये दो पहलू हैं: निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर सिस्टम की वापसी! अपने देश में निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 से निर्देशित है। पर इसके तीनों आयुक्तों की नियुक्ति सरकार करती है। राष्ट्रपति के आदेश से नियुक्ति संपन्न होती है। लेकिन वास्तविक फैसला कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री करते हैं। आजकल तो कैबिनेट से ज्यादा ताकतवर पीएमओ(PMO) हो गया है। इस तरह भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था की है, उसकी नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री की इच्छानुसार होती है। संसद या किसी सर्वदलीय समिति की इसमें कोई भूमिका नहीं होती।
एक डेमोक्रेसी के लिए क्या यह संवैधानिक रूप से सुसंगत प्रक्रिया है? वैसे भी हमारा आयोग इतने बड़े मुल्क के लिए एक बेहद केंद्रीकृत व्यवस्था है और उसमें भी सभी आयुक्तों की नियुक्ति का वास्तविक अधिकार सरकार के प्रमुख कार्यकारी यानी प्रधानमंत्री का है!
हमारे संविधान निर्माताओं ने विधान बनाते समय संभवतः आज के राजनीतिक परिदृश्य की कल्पना नहीं की रही होगी कि प्रचंड बहुमत पाकर कुछ सरकारें जनतंत्र के ढांचे को लचर करके निरंकुशता की तरफ भी बढ़ सकती हैं! अपना संविधान पढ़ते हुए मुझे हमेशा लगता है, कुछ अनुच्छेदों में जनता और जनतंत्र के बचाव के प्रावधानों को और पुख़्ता किया जाना चाहिए था। यह बात सिर्फ अनुच्छेद 324 के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं, जिनकी मूल भावना को नोचते हुए हमारे आज के निर्वाचित शासक जनतंत्र की प्रणाली और प्रक्रिया को निष्प्राण कर रहे हैं। कमोबेश यह सिलसिला आजादी के कुछ ही साल बाद शुरू हो गया था।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ‘स्वर्णिम दौर’ में जम्मू-कश्मीर और केरल की सरकारों को असंवैधानिक ढंग से बर्खास्त किया गया था। बाद के दिनों में प्रचंड बहुमत धारी इंदिरा गांधी की सरकार ने इमर्जेंसी लगा दी। यह सब संविधान के सम्बद्ध अनुच्छेदों के नाम पर ही किया गया था। आज फिर एक प्रचंड बहुमत धारी सरकार है, जो संविधान के अनुच्छेद, धारणा और मूल भावना को दरकिनार कर देश को ‘कारपोरेट-हिंदुत्व वर्चस्व के भारत’ में तब्दील करने पर अमादा है! ऐसे दौर में जनतंत्र की बची खुची संरचना की रक्षा के लिए निर्वाचन से सम्बद्ध सुधारों का मसला आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार अगर संसद, संसदीय समिति या कम से कम एक बहुपक्षी समिति, जिसमें सरकार, विपक्ष और न्यायपालिका के प्रतिनिधि हों; को दिया गया होता तो जिस तरह आज भारत के निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठाये जाते हैं, वे नहीं उठाये जाते। सच पूछा जाय तो भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में आयोग के गठन की यह प्रक्रिया अपने मूल रूप में निहायत अजनतांत्रिक है। दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने अपने-अपने निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को बहुत लोकतांत्रिक और पारदर्शी रखा है। इसके अलावा उन देशों की समाज व्यवस्था भी भारत के मुकाबले ज्यादा लोकतांत्रिक और मानवीय है।
ब्रिटेन के निर्वाचन आयोग पर वहां की संसद, खासतौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स की निगरानी रहती है। सर्व दलीय भावना को महत्व मिलता है। कुछ भी एकतरफ़ा नही होता। पिछले कुछ वर्षों से न्यूजीलैंड के निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों की पूरे विश्व में चर्चा होती रहती है। वहां के निर्वाचन आयोग के सदस्यों का चयन देश की पार्लियामेंट करती है। यूरोप के जर्मनी जैसे जिन प्रौढ़ लोकतांत्रिक देशों में चुनाव प्रबंधन समितियों या आयोगों का गठन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करती है, वहां भारत की चुनाव प्रक्रिया जैसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहां चुनाव धांधली एक अकल्पनीय स्थिति है। आस्ट्रेलिया में भी फेडरल कमेटी और संसद की भूमिका होती है।
अपने यहां सन् 1980 के बाद चुनाव आयोग सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशें आती रही हैं पर सिर्फ इतना सा सुधार हुआ कि एक या दो की जगह अब तीन चुनाव आयुक्त होते हैं और इनमें एक मुख्य होता है। लेकिन इससे बेहतर और व्यापक सुधार के लिए सन् 1990 में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी कमेटी ने अपेक्षाकृत कुछ अच्छे सुझाव दिये थे।। इनमें एक बड़ी सिफारिश थी कि नियुक्ति की प्रक्रिया को ज्यादा व्यापक बनाते हुए इसमें दोनों सदनों के पीठासीन प्रमुख(लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति) और विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाय। लेकिन उनकी सिफारिश पर राजनीतिक दलों में सहमति नहीं बन पाई। सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनाव सुधार जैसे मसले पर समय-समय पर याचिकाएं दायर होती रही हैं पर बात आगे नहीं बढ़ पाई।
आज सबसे ज्यादा चर्चा और मांग जिन दो सुधारों पर है, उनमें सबसे पहली मांग है: ईवीएम की जगह बैलेट पेपर सिस्टम की वापसी की मांग और दूसरी है-चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को ज्यादा व्यापक बनाने की मांग। भारतीय चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए अब और देर नहीं की जानी चाहिए। दोनों सुधारों पर ठोस पहल की जानी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक(संसदीय स्तर से) या न्यायिक पहल के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। दुनिया के किसी भी प्रौढ़ या प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश में चुनाव के लिए पूरी तरह ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। फिर भारत जैसे विकासशील देश में ही क्यों?
(उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार और कई किताबों के लेखक हैं।)