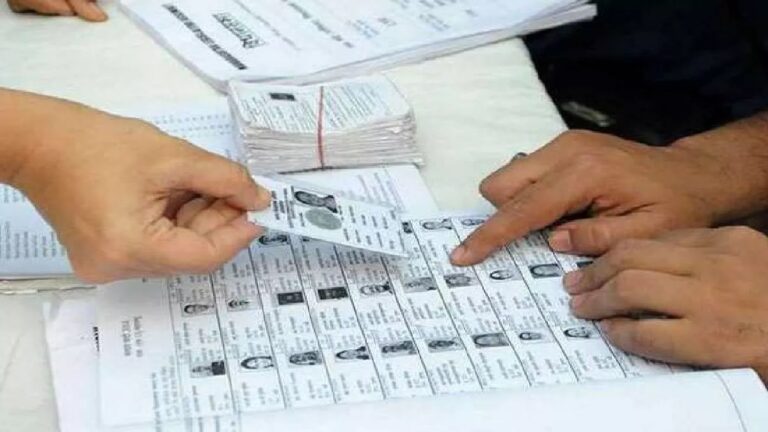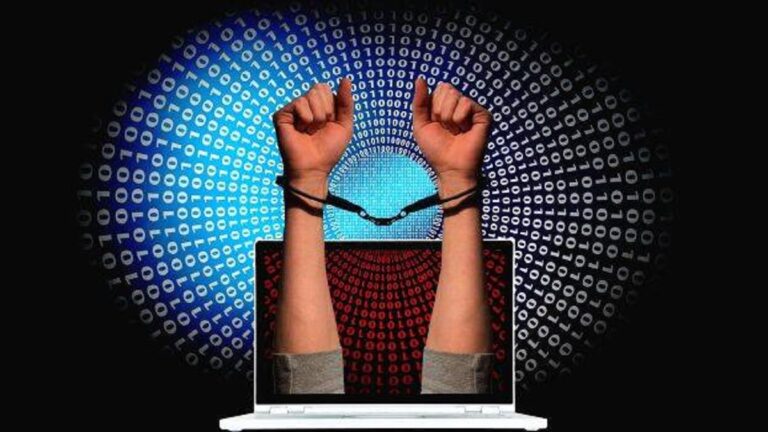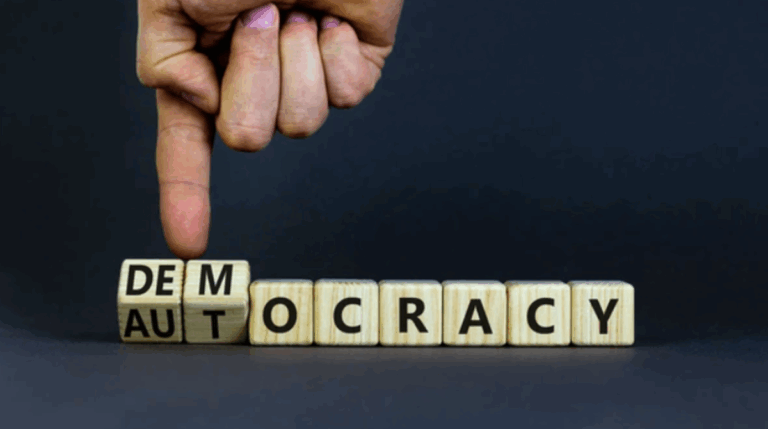खिरियाबाग, आज़मगढ़। आज़मगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रनवे के लिए आठ गांवों को उजाड़ने के विरोध में करीब तीन महीने से चल रहा खिरिया बाग आंदोलन अपनी अंतिम परिणति में सफल होगा या असफल यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हर जनांदोलन की तरह इस जनांदोलन की भी अब तक की कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं, जिन्हें रेखांकित किया जाना जरूरी है। इसकी पहली उपलब्धि है, सामूहिक एकजुटता की ताकत पर भरोसा। सामूहिक एकजुटता पर यह भरोसा गांव वालों में किसी सिद्धांत के अध्ययन या किसी नेता-विचारक की बात से नहीं पैदा हुई, बल्कि तीन महीनों के उनके खुद के अनुभव से हासिल हुई है।
इस सामूहिक एकजुटता का ही नतीजा है कि 13 अक्टूबर से लेकर आज तक शासन-प्रशासन का कोई एक छोटा कारिंदा भी गांव में घुस नहीं पाया है। एक दिन पुलिस के दो सिपाही गांव में आ गए, उन्हें गांव से बाहर सकुशल जाने के लिए आंदोलन के नेताओं का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल शासन-प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वे गांवों का सर्वे करने के लिए गांव वालों की अनुमति के बिना घुस सकें। पहले यह अनुमति एसडीएम ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से मांगी, लेकिन असफल होने पर आज़मगढ़ के डीएम ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से यह मांग (गांवों की जमीन का सर्वे) की कि सर्वे करने दिया जाए, लेकिन गांव वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर धमकियां दी गईं, लेकिन गांव वाले न डरे, न झुके। इसी दौरान आंदोलन को कमजोर करने के लिए आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरे राजीव यादव को अपहरणकर्ता की तरह पुलिस ने उठा लिया।आखिरकार शासन-प्रशासन को यह कहना पड़ा कि उन्होंने ड्रोन से सर्वे कर लिया है। गांव वालों की सामूहिक एकजुटता ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है, इस संदर्भ में इस आंदोलन के नेता रामनयन यादव कहते हैं, “हम जब तक एकजुट हैं, तब तक शासन-प्रशासन और पुलिस हमारे गांव में घुस नहीं सकती है, न हमारे घर-जमीन पर कब्जा कर सकती है।”

वे आगे कहते हैं, “ जिस दिन हमारे में से कुछ लोग शासन-प्रशासन के साथ समझौता करने लगेंगे, उसी दिन हमारी हार की शुरुआत हो जाएगी।” आज़मगढ़ जिला प्रशासन इन गांवों की एकजुटता को तोड़ना चाहता है, इसकी अभिव्यक्ति 30 दिसंबर की वार्ता ( आंदोलन के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के बीच) में डीएम के उस बात से हुई, जिसमें उन्होंने आंदोलन के प्रतिनिधियों से कहा, “हम बिना आप लोगों की अनुमति के आपके घर-जमीन का अधिग्रहण नहीं करेंगे, इसके लिए हम हर परिवार से अलग-अलग बात करेंगे और उनसे उनकी सहमति हासिल करने की कोशिश करेंगे।”
यानी शासन-प्रशासन गांव वालों से सामूहिक बात करने की जगह गांव के एक-एक परिवार से अलग-अलग बात करना चाहता है और उनकी सहमति लेना चाहता है। जबकि आंदोलन के लोगों का कहना है कि सारे गांवों या अलग-अलग गांवों की सभा बुलाकर एक साथ सहमति या असहमति लेना चाहिए। शासन-प्रशासन अलग-अलग परिवारों से अलग-अलग क्यों बात करना चाहता और इस पीछे उनकी मंशा क्या है, इसका जवाब देते हुए आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरे राजीव यादव कहते हैं, “ शासन-प्रशासन सामूहिक तौर पर लोगों को डरा-धमका नहीं सकता है, न ही लालच देकर खरीद सकता है, लेकिन अलग-अलग लोगों को डराया-धमकाया जा सकता है, उन्हें लालच देकर खरीदने की कोशिश की जा सकती है।” डीएम के कथन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि गांव वालों की सामूहिक एकजुटता को तोड़कर ही, उनके घर-दुआर और जमीनों पर कब्जा किया जा सकता है।

गांव वालों की सामूहिक एकजुटता का ही नतीजा है कि शासन-प्रशासन और पुलिस को बार-बार गांव वालों को वार्ता के लिए आमंत्रित करना पड़ रहा है और उनसे धरना-आंदोलन खत्म करने के लिए अनुनय-विनय करना पड़ रहा है, नहीं तो यह वही शासन-प्रशासन और पुलिस है, जो आधी रात को गांवों पर धावा बोल दी थी, गालियों और लाठियों की बौछार कर दी थी।
इस जनांदोलन ने लोगों की पहलकदमी को बहुत आगे बढ़ा दिया है। ऐसे लोगों को नेतृत्वकारी के रूप में सामने लाया है, जो कभी किसी पार्टी या संगठन के सदस्य नहीं रहे हैं, न ही किसी सामूहिक संघर्ष में हिस्सेदार रहे हैं। इसने करीब-करीब निरक्षर कही जाने वाली महिलाओं को इस आंदोलन का रीढ़ और नेता बना दिया है, जैसे कुटुरी, किस्मती, शकुंतला, फूलमती, पुष्पा गुप्ता, मुंजा और तारा यादव आदि। कक्षा तीन तक पढ़ाई करने वाली किस्मती धरना स्थल पर होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करती हैं, डीएम से वार्ता करती हैं, भाषण देती हैं और सावित्रीबाई फुले के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित कराती हैं।

दिहाड़ी मजदूर प्रवेश निषाद इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरते हैं, ऐसे बहुत सारे अन्य चेहरे। तीज-त्यौहार और शादी-ब्याह में परंपरागत गाना गाने वाली महिलाएं क्रांतिकारी बदलाव के गीत गाने लगीं हैं। इस आंदोलन ने कुछ नए गीतों और उनके गाने वालों का जन्म दिया है। इन गावों के जो किशोर और नौजवान पढ़ाई-लिखाई और मजदूरी करने से छुट्टी होने पर इधर-उधर मटरगस्ती में समय बिताते थे, वे अब धरना स्थल के साफ-सफाई करने, मिट्टी डालने और बांस-फूस से स्थायी छांव तैयार करने में लगे हुए हैं। वे बाहर से आए लोगों का स्वागत करते हैं, उनके खाने-सोने का इंतजाम करने में लगे हैं। खुद को कष्ट में डालकर लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हैं।
इस आंदोलन ने वर्ण-जाति और लिंग आधारित बंटवारे और दूरी को पहले की तुलना में कम किया है। इस आंदोलन के एक महत्वपूर्ण चेहरे 75 वर्षीय कॉमरेड दुखहरन राम कहते हैं, “ अपने जीवन में मैंने कभी इन गांवों के लोगों को इतना एकजुट नहीं देखा। इस आंदोलन ने जाति, लिंग और गरीब-अमीर ( गांवों के सापेक्षिक तौर पर गरीब-अमीर) की सीमाओं को तोड़ दिया है। सबको एक साथ ला दिया है।” यह पूछने पर कि सवर्ण आंदोलन से थोड़ा अलग होते दिख रहे हैं, इसका जवाब देते हुए दुखहरन राम कहते हैं, “शुरू में वे साथ थे, थोड़ा भटक गए हैं, वे भी चाहते हैं, आंदोलन चले। आज नहीं तो कल उनको भी आना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अभी उन्हें भूमिहीन मेहनकश दलितों ( स्त्री-पुरूषों) का नेतृत्व स्वीकार करने में हिचक हो रही है, लेकिन यह हिचक देर-सबेर टूट जाएगी।” यह कितना सच होगा या नहीं होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है लेकिन आंदोलन के अगुवा लोग ऐसा ही सोचते हैं।

सवर्णों ( स्त्री-पुरूष) को छोड़ दिया जाए तो इस आंदोलन ने पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों और दलितों को काफी हद तक एक धागे में पिरो दिया है। सब बिना किसी हिचक और भेदभाव के एक दूसरे के साथ उठ-बैठ रहे हैं, बराबरी पर बात कर रहे हैं, बिना जात-पांत और स्त्री-पुरूष के भेदभाव के जो अगुवाई करने लायक है, उसको अगुवा (नेता) मान रहे हैं। पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के बीच की एका के कारणों को रेखांकित करते हुए अजय यादव बताते हैं कि सारे लोगों पर विपत्ति आई हुई है, सब लोग बहुत थोड़ी खेती के मालिक हैं और सबसे बड़ी बात है कि मेहनत-मजूरी करके अपना जीवन चलाते हैं।
कोई भी बैठ कर नहीं खाता है।” अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि हमारे गांव में पहले से भी पिछड़ों और दलितों के बीच में भाई-चारा ( साथ में खाना-पीना, उठना बैठना, दोस्ती-यारी और दुख-सुख में हिस्सेदारी) रहा है। नई पीढ़ी में यह और बढ़ा है। इस आंदोलन ने तो फिलहाल सबको एक साथ खड़ा कर दिया है, क्योंकि हम सब पर विपत्ति ( घर-दुआर और जमीन छीने जाने ) एक साथ टूट पड़ी है।”

सवर्णों के आंदोलन से थोड़ा-थलग होने के सवाल पर अजय यादव कहते हैं, “वे छुआछूत और सामाजिक वर्चस्व की भावना से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी भीतर से वे हमारे साथ हैं, क्योंकि उनका भी हित इसी में है। भले ही वे सामूहिक तौर पर धरना स्थल पर न आ रहे हों और हमारे जुलूसों में शामिल न हो रहे हों।” सवर्णों के एक हद तक के थोड़े से अलगाव को छोड़ दिया जाए तो इस आंदोलन ने पूरे गांव को जोड़ दिया। इस जुड़ाव का सबसे बड़ा कारण इन गांवों के बहुलांश लोगों का उत्पादक और मेहनतकश सामाजिक समूहों का होना है।
आंदोलन ने महिलाओं, विशेषकर मेहनतकश दलित-पिछड़े वर्ग की महिलाओं के भीतर की अपार क्षमताओं को सामने ला दिया है। जैसा कि मैं अपने इस लेख की पिछली किश्तों में चर्चा कर चुका हूं कि इस आंदोलन की रीढ़ दलित-पिछड़ी महिलाएं हैं और फिलहाल यह आंदोलन उनके दम पर टिका हुआ है। ये महिलाएं पुलिस-प्रशासन से संघर्ष में सबसे आगे थीं, धरना स्थल पर सबसे बड़ी संख्या में रहती हैं, जुलूस में इनकी सबसे अधिक हिस्सेदारी होती है और आगे बढ़कर नेतृत्व भी कर रही हैं।
इस आंदोलन के दौरान इन महिलाओं की जितनी और जिस तरह की क्षमताएं सामने आईं हैं, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। खुद उन महिलाओं को भी इसका अहसास नहीं था कि वे यह सब कर सकती हैं। जिन महिलाओं की भूमिका दायरा सीमित कर दिया गया था, इस आंदोलन ने उनके दायरे को बहुत बढ़ा दिया है, जिसका स्वाभाविक परिणाम , उनकी आजादी और आत्मविश्वास में वृद्धि के रूप में सामने आया है। देश-दुनिया के आंदोलन महिलाओं, विशेषकर मेहनतकश महिलाओं की बड़े-बड़े आंदोलन-संघर्षों में भूमिका के साक्षी रहे हैं, खिरिया बाग आंदोलन भी इसका साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है। यह इस आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है।

इस आंदोलन ने इसमें हिस्सेदार लोगों की वैचारिक-राजनीतिक चेतना को भी उन्नत किया है। महिलाएं अपनी रोजी-रोटी और बाल-बच्चों तक सीमित थीं, वे अब अंबानी-अडानी और मोदी-योगी के साठ-गांठ पर बात रही हैं। मोदी सरकार की किसान-मजदूर विरोधी नीतियों पर चर्चा कर रही हैं। किस तरह दुनिया के मेहनत-मजूरी करने वाले एक हैं और कैसे दुनिया के अमीर गरीबों-मेहनतकशों के खिलाफ हैं, इसकी बहस कर रही हैं। वे हवाई अड्डे से संबंधित तथ्यों को जान-समझकर यह राय बना रही हैं कि सरकारें बड़े लोगों के लिए काम करती हैं।
किस्मती देवी कहती हैं, “ यह हवाई अड्डा बड़े-बड़े लोगों के फायदे के लिए बनाया जा रहा है। बड़े लोगों के लिए हमें उजाड़ा जा रहा है।” इस आंदोलन ने महिलाओं के प्रति पुरूषों के नजरिए में भी परिवर्तन लाया है, पुरूषों को महिलाओं की ताकत और क्षमता का अहसास हो रहा है। वे इसकी मुखर अभिव्यक्ति भी करते हैं। गांव के प्रेमचंद कहते हैं, “यदि इस आंदोलन में महिलाएं सक्रिय हिस्सेदारी नहीं करतीं, तो यह आंदोलन अब तक टिका नहीं रहता।” जाने-अनजाने तरीके से इस आंदोलन ने पितृसत्तात्मक मूल्यों ( पुरूषों के महिलाओं के श्रेष्ठ होने) को चोट पहुंचायी है और महिलाओं के प्रति पुरूषों के बीच बराबरी के भाव को बढ़ाया है।

इसके साथ ही आंदोलन ने मेहनतकशों, विशेषकर मेहनतकश दलितों ( स्त्री-पुरूष) को कमतर मानने और उनके प्रति उपेक्षा भाव रखने की भावना एवं सोच को खंडित किया है। पिछड़ी जातियां, यहां तक कि सवर्ण भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों के दम पर यह आंदोलन चल रहा है और टिका हुआ है और भविष्य में इन्हीं के दम पर जीत हासिल की जा सकती है। कामरेड दुखहरन राम इस बात को सूत्रबद्ध करते हुए कहते हैं, “ असल में यही ( भूमिहीन मेहनतकश दलित स्त्री-पुरूष) भारत में मार्क्स के असली सर्वहारा, जो सबकी मुक्ति ( पूरे गांव) के संघर्ष की अगुवाई कर रहे हैं।”
इस आंदोलन ने गांव के लोगों को प्रभावित किया ही है, बदलाव ही है, उन्हें आगे बढ़ाया ही है, उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है, जो बाहर से इस आंदोलन में शामिल होने आए। इसमें देश के कई कोनों से आने वाले लोग आ रहे हैं।। बाहर से आए कुछ लोग तो फिलहाल यहीं के होकर रह गए हैं और दिन-रात आंदोलन को विभिन्न रूपों में मदद पहुंचा रहे हैं। यह आंदोलन और इस आंदोलन के गांवों की आर्थिक और सामाजिक संरचना और वोटर के रूप में यहां के लोगों का राजनीतिक झुकाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन भारतीय समाज को समझने और बदलने में कारगर हथियार साबित हो सकता है।
दुनिया का अब तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अन्याय के विरोध और न्याय के पक्ष में लड़ा जाने वाला हर संघर्ष अपनी परिणति में जीते या हारे लेकिन वह संघर्ष की इस प्रक्रिया में इतिहास के पहिए को कुछ इंच और कुछ कदम आगे बढ़ा देता है और कभी-कभी छलांग लगाकर आगे बढ़ा देता है। खिरिया बाग आंदोलन अपने अंतिम परिणति में सफल होगा या असफल यह भविष्य के गर्भ में है लेकिन तीन महीने के भीतर ही कई-कई सारी उपलब्धियां हासिल कर चुका है, इस आंदोलन में शामिल लोगों को कुछ कदम आगे बढ़ा चुका है।
(आज़मगढ़ से शेखर आजाद के साथ डॉ. सिद्धार्थ की रिपोर्ट।)