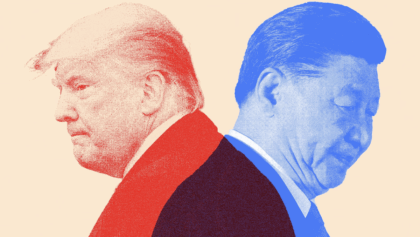1955 में फ़ैज़ ने, जो 1951 से ही मोंटगोमरी जेल में राजद्रोह की गतिविधियों के आरोप में क़ैद थे, नज़्म आ जाओ अफ्रीका लिखी थी। यह नज़्म उस जुमले पर आधारित थी जो उन्होंने अफ्रीका के उपनिवेश-विरोधी बाग़ियों से उनके उत्साहवर्धक नारे के तौर पर सुना था।
आ जाओ ने सुन ली तिरे ढोल की तरंग
आ जाओ मस्त हो गई मेरे लहू की ताल
”आ जाओ अफ़्रीक़ा”
आ जाओ मैं ने धूल से माथा उठा लिया
आ जाओ ने छील दी आँखों से ग़म की छाल
आ जाओ में ने दर्द से बाज़ू छुड़ा लिया
आ जाओ मैं ने नोच दिया बे-कसी का जाल
”आ जाओ अफ़्रीक़ा”
अफ़रीक़ी ख़िदमत पसंदों का नारा
पंजे में हथकड़ी की कड़ी बिन गई है गुर्ज़
गर्दन का तौक़ तोड़ के ढाली है मैं ने ढाल
”आ जाओ अफ़्रीक़ा’‘
चलते हैं हर कछार में भालों के मर्ग नैन
दुश्मन लहू से रात की कालक हुई है लाल
”आ जाओ अफ़्रीक़ा’‘
धरती धड़क रही है मिरे साथ अफ़्रीक़ा
दरिया थिरक रहा है तो बन दे रहा है ताल
मैं अफ़्रीक़ा हूँ धार लिया मैं ने तेरा रूप
मैं तू हूँ मेरी चाल है तेरी बब्बर की चाल
”आ जाओ अफ़्रीक़ा”
आओ बब्बर की चाल
”आ जाओ अफ़्रीक़ा”
इस कविता ने हमेशा हमें जितना आकर्षित किया है उतना ही परेशान भी। जहाँ एक ओर तो इन पंक्तियों में अफ्रीका के प्रति फ़ैज़ की सॉलीडैरिटी ज़ाहिर है, वहीं अफ्रीकी महाद्वीप का बिम्ब आदिम, जंगली, वनों और हिंस्र जानवरों का उपयोग करने वाला है। नए ज़माने की हमारी समझ के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद के प्रति फ़ैज़ की ज़ाहिर प्रतिबद्धता और अफ्रीकी लोगों की आदिम जनों के रूप में उनके मन में रही स्पष्ट प्रतिमा के बीच सामंजस्य बिठाना मुश्किल था। यह तो हमें बहुत बाद में पता चला कि नस्लीकृत स्टीरियोटाइप के उपयोग से बहुत परे फ़ैज़ का बिम्ब विधान नीग्रोत्व आन्दोलन के लेखकों और बुद्धिजीवियों के काव्यात्मक सौंदर्यशास्त्र से प्रेरित था। काले जनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता हेतु कालेपन के रूपकों का उपयोग करना यह नीग्रोत्व आन्दोलन की कोशिश हुआ करती थी। मार्तिनीक देश के एमे शेज़ेयर (Aimé Césaire) जैसे अफ्रीकी कवियों के साथ फ़ैज़ की दोस्ती ने उन्हें इन रूपकों का इस्तेमाल करने की ओर प्रवृत्त किया होगा, जिसे फिर वे उपमहाद्वीप में ले आये। आखिर अली सरदार जाफरी जैसे उर्दू शायरों ने भी अपनी शायरी में ऐसे बिम्ब विधान का प्रयोग विश्व भर के काले क्रांतिकारियों का एहतराम करने के लिए किया।
आ जाओ अफ्रीका की दास्ताँ उर्दू शायरी के तरक्कीपसंद सौंदर्यशास्त्र को अंतर्राष्ट्रीय मिजाज़ अख्तियार करवाने में फ़ैज़ की भूमिका को कई तरीकों से स्थापित करती है। पचास और साठ के दशकों में दुनिया भर में उनकी यात्राएँ उन्हें ऐसी ऐसी जगहों पर ले गईं जो विलायत के द्वीप में लगने वाले उनके समवर्तियों के स्टैंडर्ड डेरों की बनिस्बत कहीं अधिक दिलचस्प थीं। अपने-अपने मुल्कों के मजलूमों के बारे में लिखने वाले बहुतेरे समवर्तियों से उनका रिश्ता बना: चिली के पाब्लो नेरुदा, हार्लम रेनेसांस के लैंग्स्टन ह्यूज, तुर्की के नाज़िम हिकमत (जिनकी कविताओं का फिर उन्होंने उर्दू में तर्जुमा भी किया)। इसके साथ-साथ, उपमहाद्वीप के वामपंथी लेखक जहाँ मायकोवस्की जैसे सोवियत लेखकों से भली-भांति परिचित थे, पर यूरोपीय शैली में लिखने वाले रूसियों का प्रभाव उन पर कम ही था। फ़ैज़ की बदौलत हमारे पास कज़ाकिस्तान के ओल्ज़्हास सुलेमनोव और दागिस्तान के रसूल गम्ज़तोव जैसे ‘कमतर सोवियत’ लेखकों के उर्दू अनुवाद हैं।
राज्य के विरुद्ध
फ़ैज़ कुछ तो अपनी तबीअत से अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे और कुछ परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया था। 15 अगस्त, 1947 को देश के विभाजन के साथ ही राष्ट्र-राज्य के साथ उनका रिश्ता बर्बाद हो गया था। जिस आज़ादी का वादा किया गया था वह आई, पर उसकी रक्तिम छटा उस समाजवादी ‘लाल सुबह’ की सी नहीं थी जिसका इंतज़ार था, बल्कि वह विभाजन की हिंसा में मरे लोगों के खून से आई थी। फ़ैज़ की नज़्म सुबहे-आज़ादी उपनिवेश के ख़त्म होते वक़्त प्रगतिशील राजनीति की हार का तराना है। ये दाग दाग उजाला ये शब-गज़ीदा सहर में विभाजन की त्रासदी की बाबत सारे प्रगतिशीलों की आवाज़ शामिल है। एक अपूर्ण यात्रा को जारी रखने के आवाहन के साथ यह नज़्म ख़त्म होती है।
अभी गिरानी-ए-शब में कमी नहीं आई
नजात-ए-दीदा-ओ-दिल की घड़ी नहीं आई
चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई
राष्ट्र-राज्य के साथ फ़ैज़ का सम्बन्ध और भी डगमग हो गया जब अयूब खान की सरकार ने 1951 में उन्हें रावलपिंडी षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार कर लिया। सरकार का तख्ता पलटने की कार्रवाई के आरोपों ने लंबा कारावास दिलाया, और इत्तेफाक़न 1954 में पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके विभिन्न मोर्चों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की शुरुआत भी हुई। उन दिनों की फैज़ की कविताएँ, जो ज़िन्दांनामा में संकलित हैं, शायद सबसे अच्छी हैं।
निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के जहाँ
चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले
यहीं उनके विशिष्ट काव्य रूपकों का विकास हुआ, जिनमें एक क़ैदी क़फ़स में बंद है, जिसे अपने वतन की खबरें सबा से हासिल होती हैं। नीचे दिए हुए दो शे’र दर्शाते हैं कि फ़ैज़ की शायरी क्लासिक प्रेम कविता की शिद्दत और इंकलाबी मुहावरे को यकसा करती हुई एक विचारमग्न अवस्था में प्रवेश करती प्रतीत होती है, और यही बात उन्हें प्रगतिशीलों के बीच विशिष्ट बनाती है।
चमन में गारत-ए-गुलचीं से जाने क्या गुज़री
क़फ़स से आज सबा बेक़रार गुज़री है
या
क़फ़स है बस में तुम्हारे, तुम्हारे बस में नहीं
चमन में आतिश-ए-गुल के निखार का मौसम
बला से हम ने न देखा तो और देखेंगे
फरोग-ए-गुलशन-ओ-सौत-ए-हज़ार का मौसम
वैश्विक नागरिक
जहाँ फ़ैज़ की कविता तरक्कीपसंद उर्दू शायरी के अंतर्राष्ट्रीयतावादी मिजाज़ की जीवंत मिसाल है, वहीं अंतर्राष्ट्रीयतावाद अपने आप में कोई अपवाद नहीं। प्रगतिशील आन्दोलन की अंतर्राष्ट्रीयतावादी प्रतिबद्धता शुरू से ही स्पष्ट थी। यूरोपीय साहित्यिक हस्तियों के फासीवाद-विरोधी संघर्षों ने प्रगतिशीलों को उत्साहित किया था, और सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद को 1935 में लन्दन में इंटरनेशनल राइटर्स फॉर दि डिफेन्स ऑफ़ कल्चर की कांफ्रेंस में अपने प्रतिनिधियों के तौर पर भेजने का काम नवगठित प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन (पीडब्ल्यूए) के शुरुआती कामों में एक था।
मुहम्मद इक़बाल जैसे शायर कुछ समय से ही दुनिया के साथ उर्दू साहित्य के सम्बन्ध की सीमाओं का विस्तार कर रहे थे। लेकिन फ़ैज़ और अन्य पीडब्ल्यूए शायर अंतर्राष्ट्रीयतावाद को नई ऊंचाइयों पर ले गए। यह संगठन उस समय अस्तित्व में आया जब स्वाधीनता आन्दोलन अपने उरूज पर था और उसके सदस्यों का शुरुआती लेखन ब्रिटिश कब्जे के विरुद्ध के संघर्ष पर केन्द्रित था। अंतर्राष्ट्रीयतावाद की ओर पेशकदमी ने दो स्वरूप धारण किये: उपनिवेशवाद और उससे जुड़े मुद्दों (मसलन द्वितीय विश्व युद्ध) की तहकीकात और प्रत्यालोचना, और सोवियत क्रांति की प्रशंसा की अभिव्यक्ति जिसमें यह उम्मीद शामिल थी कि हिन्दुस्तान की आज़ादी की परिणति वैसे ही समाजवादी समाज में होगी।
बांडुंग, इंडोनेशिया में 1955 (जिस साल आ जाओ अफ्रीका लिखी गई थी) में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के उद्भव ने तीसरी दुनिया की एकजुटता के विचार को मूर्त रूप दिया और तरक्कीपसंद शायरी को अभिव्यक्ति का एक और क्षेत्र प्रदान किया। लेनिन की तारीफ़ में साहिर ने कई नज़्में लिखीं, मखदूम ने पैट्रिस लुमुम्बा और मार्टिन लूथर किंग के लिए मार्मिक गीत लिखे, पॉल रॉब्सन के लिए अली सरदार जाफरी ने ग़ज़लें लिखीं, और कैफ़ी आज़मी ने वियतनाम में अमरीकी दखलंदाज़ी की आलोचना में कविताएँ लिखीं। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और एफ्रो-एशियाई आन्दोलन की हौसला-अफज़ाई से जो सांस्कृतिक विनिमय शुरू हुआ उसमें फ़ैज़ की कई ग़ज़लों/नज़्मों का स्वाहिली, चीनी और वियतनामी भाषाओं में अनुवाद हुआ, उसी समय दुनिया भर के प्रगतिशील कवियों का उर्दू में अनुवाद हुआ।
तीसरी दुनिया की एकजुटता के इस दौर में तरक्कीपसंद शायरों ने 1959 में ईरानी छात्रों के संघर्षों, अमेरिका में असहमति के दमन के मैकार्थी युग, साठ के दशक में यूरोपीय छात्र विद्रोहों, अल्जीरियाई स्वाधीनता संग्राम, फिलिस्तीनी संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद-विरोधी आन्दोलन जैसे मुद्दों पर कविताएँ लिखीं। उस दौर की कई सारी वैश्विक बहसों पर फ़ैज़ ने विचार किया, पर ऐसी तरन्नुम के साथ जिसका कोई सानी नहीं था। जब 1953 में सोवियत गुप्तचर होने के आरोप में अमेरिका ने जूलियस और एथल रोज़नबर्ग को मृत्युदंड दिया तब फ़ैज़ ने एक नज्म लिखी। पर उसे अन्याय की खिलाफत वाले अंदाज़ में लिखने की बजाय उन्होंने उसे रोज़नबर्ग द्वय की मुहब्बत के प्रति काव्यात्मक श्रद्धांजलि के तौर गढ़ा कि प्रलोभनों, धमकियों, कारावासों और अंततः मृत्युदंड के बावजूद दोनों एक दूसरे का दामन थामे रहने पर अड़े रहे। इस श्रद्धांजलि का उन्वान हम जो तारीक राहों में मारे गए बड़ा हृदयविदारक है। यहाँ प्रस्तुत है उस नज़्म का एक अंश।
तेरे होंटों के फूलों की चाहत में हम
दार की ख़ुश्क टहनी पे वारे गए
तेरे हातों की शम्ओं की हसरत में हम
नीम-तारीक राहों में मारे गए
जब घुली तेरी राहों में शाम-ए-सितम
हम चले आए लाए जहाँ तक क़दम
लब पे हर्फ़-ए-ग़ज़ल दिल में क़िंदील-ए-ग़म
अपना ग़म था गवाही तिरे हुस्न की
देख क़ाएम रहे इस गवाही पे हम
हम जो तारीक राहों पे मारे गए
फ़ैज़ की यात्राएँ फिर शुरू हुईं जब ज़िया-उल-हक़ की तानाशाही के दौरान वे आत्म-निर्वासन में लेबनान चले गए। बेरूत में उन्होंने मध्य एशिया के संघर्ष पर कई नज़्में लिखीं: खुद बेरूत पर एक टुकड़ा (इश्क़ अपने मुजरिमों को पाबजौलां ले चला), फिलिस्तीन के स्वतंत्रता-सेनानियों के लिए एक तराना (एक तराना फिलिस्तीनी मुजाहिदीनों के नाम), फिलिस्तीनी मृतकों के लिए एक शोक-गीत (फिलिस्तीनी शोहदा जो परदेस में काम आये) और शायद जो सबसे मशहूर है वह फिलिस्तीनी यतीम के लिए एक लोरी (मत रो बच्चे). फ़ैज़ ने अपनी पुस्तक मेरे दिल,मेरे मुसाफिर फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात को समर्पित की थी। मगर फ़ैज़ की संवेदनशीलता की खासियत फिलिस्तीनी परिस्थितियों को दक्षिण एशिया से जोड़कर देखने में है, जिसमें उन्होंने इस्रायल की जीत के रूपक को भारत और पाकिस्तान में पूंजीवादी उच्च वर्ग की जीत, जिसमें अक्सर धार्मिक उच्च वर्ग की मिलीभगत शामिल होती, के लिए इस्तेमाल किया। 1967 की लड़ाई में अरब ताक़तों की हार के बाद लिखी गई उनकी नज़्म सर-ए-वादी-ए-सीना में दीगर बातों के साथ ही उच्चतावादी इस्लामवादियों की बड़े तीखे ढंग से नालिश की गई है। यह नज़्म लोगों से धर्माधारित राज्य की ज़ंजीरें उखाड़ फेंकने का आवाहन करती है।
फिर बर्क़ फ़रोज़ाँ है सर-ए-वादी-ए-सीना, ऐ दीदा-ए-बीना
फिर दिल को मुसफ़्फ़ा करो, इस लौह पे शायद
माबैन-ए-मन-ओ-तू नया पैमाँ कोई उतरे
अब रस्म-ए-सितम हिकमत-ए-ख़ासान-ए-ज़मीं है
ताईद-ए-सितम मस्लहत-ए-मुफ़्ती-ए-दीं है
अब सदियों के इक़रार-ए-इताअत को बदलने
लाज़िम है कि इंकार का फ़रमाँ कोई उतरे
फ़ैज़ के कुछ समकालीन अपनी कहन में और भी ज्यादा स्पष्ट थे। वैसा ही रूपक कहीं अधिक व्यंगात्मक ढंग से इस्तेमाल करके हबीब जालिब ने एक ग़ज़ल में ज़िया-उल-हक़ पर ताना कसकर उस हुकूमत की आलोचना का समां बाँध दिया जिसने घरेलू ताबेदारी बनाए रखने के लिए इस्लाम को औज़ार बनाया पर जो अमेरिका नाराज़ न हो जाए इस डर से इस्रायली साम्राज्यवाद से टक्कर लेने में कुंद और मंद थी।
जहाँ खतरे में है इस्लाम, उस मैदान में जाओ
हमारी जान के दर पे हो क्यों, लेबनान में जाओ
इजाज़त मांगते हैं हम भी जब बेरूत जाने की
तो अहले-हुक्म ये कहते हैं तुम ज़िन्दां में जाओ
अंततः फ़ैज़ की अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टि और वास्तव में फ़ैज़, मजाज़,मखदूम, कैफ़ी और दीगर पीडब्ल्यूए शायरों की अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टि सीधे तौर पर उस वक़्त की राजनीति और सामान्य चेतना की उपज थी। एक वैश्विक सन्दर्भ और अन्य उपनिवेशीकृत और/या उत्पीड़ित जनों के साथ साझा राजनीतिक संघर्ष का आधार ये दो बातें उपनिवेशवाद और फिर नवउपनिवेशवाद/नवसाम्राज्यवाद की असलियतों की ज़रूरत और उपज दोनों थीं। हालांकि उस दौर का अंतर्राष्ट्रीयतावाद यकसा नहीं था, मसलन फ़ैज़ और प्रगतिशील शायरों का अंतर्राष्ट्रीयतावाद इक़बाल और उनके अनुयायियों के अखिल-इस्लामवाद से बेहद अलग था। दुनिया भर के मुसलमानों की साझा विरासत खोजने की ज़रूरत जहाँ इकबाल की प्रेरणा थी, वहीं फ़ैज़ की समझ उत्पीड़न और संघर्ष की साझा भौतिक परिस्थितियों के ज्ञान से प्रभावित थी और अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा आन्दोलनों और दुनिया भर के उपनिवेशीकृत अवाम के संघर्षों से प्रेरित थी। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मतलब था साम्राज्यवाद के खिलाफ और नयी विश्व व्यवस्था की खातिर साझा लड़ाई।
(अली हुसैन मीर और रज़ा मीर हैदराबाद में तरक्कीपसंद उर्दू शायरी की खुराक पर पले-बढ़े। यह आलेख हिमाल साउथ-एशियन पत्रिका के फ़ैज़ विशेषांक (जनवरी 2011) में मूल अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। किंचित अलग रूप में यह आलेख तरक्कीपसंद उर्दू शायरी पर आधारित उनकी पुस्तक एन्थ्म्स ऑफ़ रेज़िस्टेन्स : अ सेलिब्रेशन ऑफ़ प्रोग्रेसिव उर्दू पोएट्री (रोली बुक्स, 2006) में संकलित है। सम्प्रति दोनों ही एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। ‘नया पथ’ केलिए इसका अनुवाद भारत भूषण तिवारी ने किया था।)