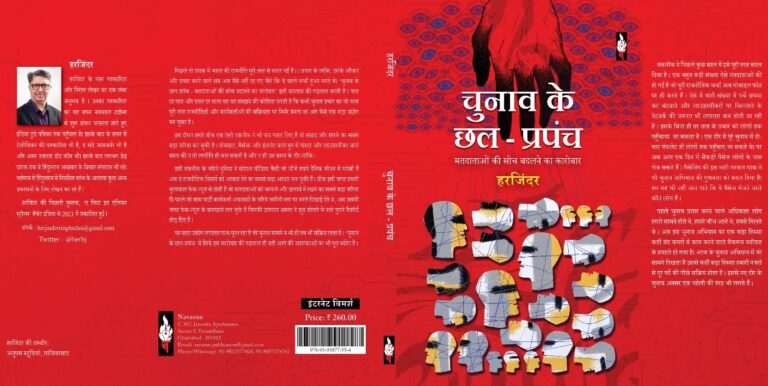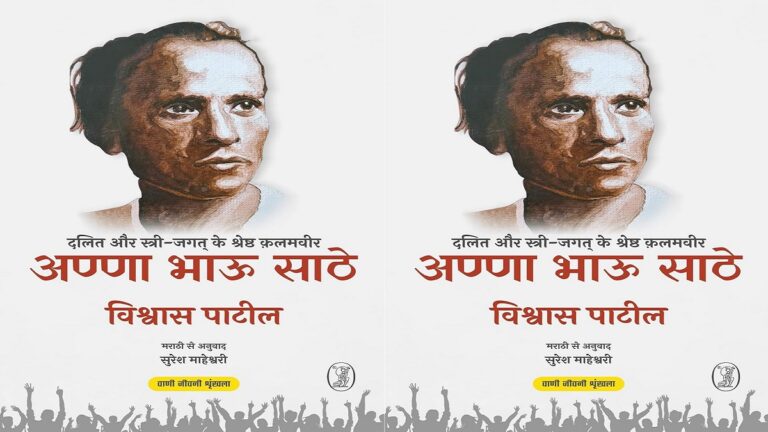अगस्त के महीने को यदि हरिशंकर परसाई का महीना कहा जाए तो कम से कम साहित्य जगत में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। 22 अगस्त 1924 को वे इस दुनिया में आये और 10 अगस्त 1995 को दुनिया से अलविदा कह गये। उनका लेखन काल लगभग भारत की स्वतंत्रता से प्रारंभ हुआ और बाद के लगभग पचास वर्षों तक निरंतर बना रहा। उनका लेखन काल भारत की आजादी के वे वर्ष थे जब 250 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी और लूट-खसोट से मुक्त हुआ भारत न केवल अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था बल्कि स्वयं के निर्माण के लिये उसने निजी और सरकारी पूंजी के जिस मिले-जुले रास्ते पर चलने का निर्णय सत्ता में आये लोगों ने लिया था, उसके दुष्परिणाम भी साफ़-साफ़ देख रहा था।
हरिशंकर परसाई भारत के आम इंसान की अभिलाषाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरी किये जाने के पक्षधर विचारक थे और एक विचारक के रूप में उन्होंने समाज की हर अभिलाषा को स्वर दिया और हर राजनीतिक-सामाजिक विसंगति पर प्रहार किया।
हरिशंकर परसाई के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निडरता है। अपने समय की विसंगतियों और संकीर्णताओं पर उन्होंने बेपरवाह लिखा और इसकी कीमत भी चुकाई। उनकी कलम से तिलमिलाकर लोगों ने उन पर हमले किए। आर्थिक अभाव लगातार बना रहा, फिर भी उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। साहित्य जगत में आज इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि प्रेमचंद होते तो क्या लिख रहे होते? परसाई होते तो क्या लिख रहे होते?
उनके निधन के लगभग 4 वर्ष पूर्व भारत में घोषित रूप से पूंजीपति और कॉरपोरेट परस्त आर्थिक नीतियों और जिस धार्मिक, साम्प्रदायिक राजनीति का उफान हम देख रहे हैं, उस राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जिस प्रहार को आज का स्वतंत्र चिंतन झेल रहा है, उसके बीज दिखाई देने लगे थे। परसाई के लेखन के स्वर्णिम युग में जो सामाजिक विसंगतियां बिल से सर बाहर निकाल रही थी, उनका खुला नृत्य प्रारंभ होना शुरू हो गया था।
परसाई यदि असामयिक मृत्यु को प्राप्त नहीं करते तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे आज के नफरती हालातों पर, राजनीति के धर्म के साथ घालमेल पर, देश में 1991 के बाद आईं तथाकथित उदारवादी नीतियों जो शासन और पूंजीपति के भाईचारे के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, अवश्य ही नियमित और करारी चोट कर रहे होते और न केवल शासन बल्कि समाज के उस हिस्से की भी हिटलिस्ट में होते जो भारत की विविध सभ्यता को हिंदूवादी बनाने के लिये हाथ में तलवार और त्रिशूल लिये सड़कों पर घूम रहा है।
या वे पंसारे-कलबुर्गी या गौरी लंकेश की गति को प्राप्त कर चुके होते। या, फिर शायद हाल यह होता कि उन पर उनकी पहले की लिखी किसी ‘पंच लाइन’ के आधार पर कोई पंचायत स्वत: संज्ञान लेकर उन्हें सजा सुना चुकी होती। या फिर देश के अनेक स्वघोषित बुद्धिजीवी उनके इस वाक्य, ‘इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं’ के आधार पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर चुके होते।
या फिर अंतरात्मा की आवाज या देशहित या अपने क्षेत्र, राज्य की जनता के हित में करोड़ों रुपये लेकर दल-बदल कर सत्ता सुख पाने वाले लोग, ‘अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो फैलाकर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने से टिका दिया’ जैसी लाइन लिखने के लिए परसाई जी को सबक सिखाने का निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दे चुके होते।
प्रश्न वहीं पर है कि परसाई होते तो क्या लिख रहे होते? परसाई जी की छवि एक सशक्त व्यंग्यकार की है। मेरा मानना है कि वे उससे बड़े लोक शिक्षक थे। उनके व्यंग्य जहां हृदय पर चोट करते हैं, करुणा जगाते हैं, वहीं विसंगति को दूर करना चाहिये की सोच को भी पैदा करते हैं। उनके निबंध समाज की गूढ़ बातों के रहस्यों को खोलते हैं।
मैं सिर्फ दो उदाहरण से अपनी बात कहूंगा। जब उन्होंने अपना निबंध ‘युग की पीड़ा का सामना’ लिखा था तब भारत को स्वतंत्र हुए मात्र 17 वर्ष हुए थे। तब उन्हें देश के भूखे-नंगे लोग दिख रहे थे। आज जब देश के राजनेता दम्भ से भरकर ये कहते हैं कि वे देश के 85 करोड़ लोगों को 35 किलो अनाज लगभग मुफ्त दे रहे हैं, तो वे कितने कठोर होकर उस पर प्रहार करते।
उन्होंने अपने निबंध ‘पगडंडियों का ज़माना’ में शिक्षा क्षेत्र में बेईमानी की परतें उधेड़ी थीं। उन्होंने लिखा था “देखता हूं, हर सत्य के हाथ में झूठ का प्रमाणपत्र है। आज जब सत्य का पूर्ण लोप हो गया है और लोकतंत्र के तथाकथित रूप से मंदिर कहे जाने वाले सदनों और विधानसभाओं तक में असत्य तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्थापित किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनकी लेखनी और पैनी होकर प्रहार करती।
परसाई मात्र व्यंग्यकार नहीं थे। वे लोक शिक्षक थे, समाज-निर्देशक थे। परसाई का लेखन केवल सुधार के लिये नहीं होता था। वे बदलाव के लिये लिखते थे। वे बदलाव के लिये केवल लेखन पर नहीं, लेखक की जमीनी जुड़ाव की बात भी करते थे। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। जबलपुर में भड़के दंगे रुकवाने के लिए गली-गली घूमे। मजदूर आंदोलन से जुड़े।
लोक शिक्षण की मंशा से ही वे अखबार में पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। उनके स्तंभ का नाम था, ‘पूछिए परसाई से’ पहले हल्के और फिल्मी सवाल पूछे जाते थे। धीरे-धीरे परसाईजी ने लोगों को गंभीर सामाजिक-राजनीतिक प्रश्नों की ओर प्रवृत्त किया। यह सहज जन शिक्षा थी। लोग उनके सवाल-जवाब पढ़ने के लिए अखबार का इंतजार करते थे।
परसाई अपने बारे में कहते थे, ‘मैं लेखक छोटा हूं, लेकिन संकट बड़ा हूं।’ आज साहित्य में ऐसे बड़े संकटों की घोर आवश्यकता है। जब सत्ता की चोटी पर बैठे लोग बुद्धिजीवियों को राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही के तमगों से नवाज रहे हैं और उनसे खुलकर कह रहे हैं कि या तो हमारी प्रशंसा में लिखो, समर्थन में लिखो या फिर राष्ट्रद्रोही का तमगा गले में लटकवाने के लिये तैयार रहो। ऐसे समय में परसाईजी ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज वे होते तो मौजूदा संकटों पर उनकी चोट भी बहुत बड़ी होती, शायद सबसे बड़ी होती, गहरी होती।
(अरुण कान्त शुक्ला स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)