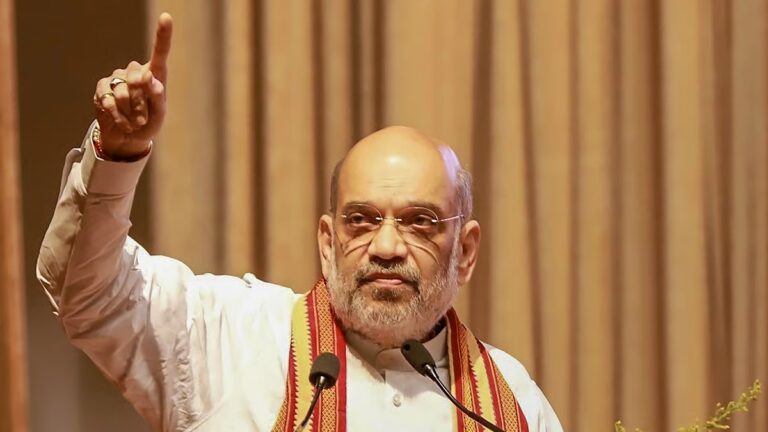पिछले दिनों अंग्रेजी में लिखने-पढ़ने और बोलने वाले बड़े लेखक का एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू सुन रहा था। उन्हें महानगरीय समाज के भद्रलोक में बड़ा लोक-बुद्धिजीवी (पब्लिक-इंटैलेक्चुअल) माना जाता है। यह इंटरव्यू कुछ महीने पहले का था और उस समय के मुद्दों की चर्चा ज्यादा थी, लेकिन इससे राजनीति, समाज और लोकतंत्र के संकट पर उनका नजरिया उभरकर सामने आया। उसे सुनकर गहरी निराशा हुई। उस इंटरव्यू में उन्होंने मौजूदा हालात की अपने ढंग से व्याख्या की और संवैधानिक सहित तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं के सत्ता के आगे नतमस्तक होने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। मुझे समझ में नहीं आया, इसमें उन्होंने नया क्या कहा? यह तो सभी देख रहे हैं।
सेलिब्रेटी-दर्जा पाए उन महाशय की बात से ही हम अपनी बात शुरू करते हैं। जिन संस्थाओं के सत्ताधारियों के समक्ष नतमस्तक होने की बात वह कह रहे हैं, उन्हें चलाता कौन है? ये संस्थाएं इतना कमजोर क्यों रहीं कि राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा का पालन करते हुए उसके आगे आज फौरन नतमस्तक हो गईं? दूसरे लोकतांत्रिक देशों में तो ऐसा नहीं होता? हमारे मौजूदा निर्वाचन आयोग जैसी संस्था के अधीन अगर अमेरिका के चुनाव हुए होते तो वहां चुनाव-नतीजे के विवाद में क्या होता? आखिर हमारी संस्थाओं की समस्या क्या है? कौन लोग संचालित करते हैं इन संस्थाओं को? छह-सात साल में क्या हो गया उन्हें? कायांतरण के साथ उनका हृदयांतरण कैसे हुआ? निर्वाचन आयोग, जांच एजेंसियों और न्यायपालिका आदि के बाहर देखिए- ‘स्वतंत्र’ कहे जाने वाले हमारे मीडिया के साथ क्या हुआ? न्यूज चैनलों का बड़ा हिस्सा इस कदर ‘गोदी’ क्यों बन गया? हिंदी अखबारों का बड़ा हिस्सा ‘पांचजन्य-परिवार’ में कैसे शामिल हो गया? अच्छे समझे जाने वाले अंग्रेजी अखबार भी भक्ति क्यों करने लगे?
भाजपा मार्गदर्शक मंडल के बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इमरजेंसी के दौरान प्रेस/मीडिया की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर एक समय कहा था, “प्रेस को जब झुकने को कहा गया तो वह रेंगने लगा!” आज के हालात पर आडवाणी जी ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बीच, अयोध्या की बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड से भी वह ‘फारिग’ हो चुके हैं। वह बोलें न बोलें, आज पूरा देश देख रहा है कि सिर्फ मेनस्ट्रीम मीडिया ही नहीं, तमाम संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं सत्ता के समक्ष बिछी पड़ी हैं।
जिन ‘पब्लिक इंटैलेक्चुअल’ महाशय के इंटरव्यू के हवाले से मैंने इस टिप्पणी की शुरुआत की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में आज के हालात के ढेर सारे ब्योरे दिए। पर ये नहीं बताया कि आज के ये हालात पैदा क्यों और कैसे हुए? क्या सचमुच हमारे बुद्धिजीवियों को अब तक समझ में नहीं आया कि भारत आज क्यों इस मुकाम पर पहुंचा? ‘लिबरल्स’ कहे जाने वाले विशिष्ट लोगों की सर्किल में शुमार उन महाशय या उनके समानधर्मा लोगों ने सन् 2014 से पहले के दो-तीन दशकों में देश के आम लोगों, खासकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पिछड़े मुसलमानों और अन्य गरीब लोगों के लिए क्या-क्या किया और अपनी पसंदीदा सरकार से क्या-क्या कराया?
यह सवाल इसलिए जायज है कि इन्हीं लिबरल्स और लोक-बुद्धिजीवियों में कुछेक को यूपीए की शीर्ष सलाहकार परिषद (NAC) में भी जगह मिली हुई थी। इनकी सिफारिशों या सलाहों से सरकार चला करती थी। हमारे सवाल का वे लोग जरूर जवाब देना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी पसंदीदा सरकार से नरेगा-मनरेगा जैसी जरूरी योजनाएं चलवाईं। इससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के गरीब हिस्सों को काम के बदले वाजिब मजदूरी मिलती थी। क्या इन हाशिये के समाजों में सिर्फ खेतों में या सड़कों पर काम करते हुए मजदूरी पाने से आगे कोई आकांक्षा नहीं रही होगी?
बीते तीस-चालीस सालों में इन समाजों से जो पढ़े-लिखे युवा उभरे हैं, उनकी आकांक्षाओं और रोजगार सम्बंधी मुश्किलों को ‘लिबरल’ लोगों की इस दुनिया ने समझा? समाज की बमुश्किल पंद्रह-बीस फीसदी आबादी से प्रोफेसर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, वाइस चांसलर, संपादक, एंकर, पद्मश्री, पद्म विभूषण, मंत्री, सलाहकार, राजदूत और गवर्नर बनाए जाते रहे और बाकी का समाज यह सब होते हुए टुकुर-टुकुर देखता रहा। उसके समाजों से बड़े-बड़े क्षेत्रीय नेता तो उभरते रहे पर बहुत जल्दी ही उसी सिस्टम में वे समायोजित भी होते रहे। अपने पंचसितारा दफ्तरों में बैठकर ‘लिबरल्स’ की टीमें ही यूआईडी-आधार जैसी योजनाओं को आकार देती रहीं, जिसका एक मात्र मकसद था- अपने ही देशवासियों के जीवन के हर पहलू की निगरानी कराना, विदेशी सरकारों और निजी कंपनियों के लिए डाटा मुहैय्या कराना।
क्या हमारे इन ‘लिबरल्स’ और ‘पब्लिक इंटलेक्चुअल’ का तमगा लगाए अंग्रेजी लेखकों को याद है, विचार के स्तर पर बीपीसीएल और एचपीसीएल आदि के विनिवेश की गंभीर कोशिशें कब शुरू हुई थीं? कश्मीर के सवाल पर मनमोहन-मुशर्ऱफ संवाद प्रक्रिया को बीच-बीच में बाधित कौन कर रहा था? अर्जुन सिंह ने मानव संसाधन मंत्री के रूप में सन् 2006 में जब उच्च शिक्षा में ‘सकारात्मक कार्रवाई’ (ओबीसी आरक्षण) की पहल की तो शासक पार्टी में एक बड़ा खेमा किन ‘लोक-बुद्धिजीवियों’ की सलाह पर उसके विरोध में मुखर हो गया था?
बंगलुरू में आयोजित कांग्रेस महाधिवेशन में जब एक जमाने के वाम-रूझान वाले बड़े कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री चंद्रजीत यादव ने आर्थिक सुधारों का मानवीय चेहरा तलाशने की बात उठाई तो पार्टी के किन बड़े नेताओं ने उन्हें लानत दी? किन लोगों ने उनसे लगभग माइक छीनकर उन्हें खामोश किया? क्या मंच पर बैठे सारे बड़े कांग्रेसी भूल गए थे कि इंदिरा गांधी शासन के बेहतर-दिनों में चंद्रजीत यादव, मोहन कुमार मंगलम और केआर गणेश की तिकड़ी ही बैंक से लेकर कोयला-खनन क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण जैसे ऐतिहासिक कदम की मुख्य योजनाकार थी?
बाद के दिनों में किन लोगों की सलाह पर कपिल सिब्बल जैसे घोर अमीरपंथी को मानव संसाधन मंत्री बनाया गया? उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र को कितनी गंभीर क्षति पहुंचाई? राजीव गांधी, नरसिंह राव और फिर मनमोहन सिंह के राज में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन-कौन से बड़े कदम उठाए गए? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वादे के बावजूद बजटीय प्रावधान में अपेक्षित बढ़ोत्तरी क्यों नहीं हो पाई? कोयला और खनन क्षेत्र में क्या-क्या खेल खेला गया? और सबसे बढ़कर समाज के उत्पीड़ित और पिछड़े समाजों को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या कुछ किया गया?
विश्वविद्यालयों से लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में दलितों-ओबीसी-आदिवासियों और पसमांदा मुस्लिम प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति रही? मंत्रियों-गवर्नरों की नियुक्ति हो या पद्मा-अवार्ड्स का आवंटन, उस दौर के आंकड़े उठाकर देखिए तो हैरत होगी! ‘सांप्रदायिक-निरंकुश’ भाजपा ने ‘लिबरल’ लोगों की सलाह पर चलने वाली कांग्रेसी या कांग्रेस की अगुवाई वाली तमाम सरकारों की इन नीतियों पर नजर रखी। उसने संघ-भाजपा नेतृत्व में समाज के पिछड़े हिस्सों को बड़े पैमाने पर गोलबंद करना शुरू किया और सन् 2014 में उसका नतीजा सामने था।
घोर हिंदुत्व और नंगे कॉरपोरेटवाद के वैचारिक-गठबंधन ने लिबरल्स की पसंदीदा पार्टियों से दलित-ओबीसी का अच्छा-खासा हिस्सा अपने खाते में जोड़ लिया। इसके लिए उन्होंने ‘सोशल इंजीनियरिंग’ का सहारा लिया। ऐसी ‘सोशल इंजीनियरिंग’ जिसे ‘लिबरल्स’ ने कभी जरूरी नहीं समझा!
आज के हारे-पिटे ऐसे तमाम ‘लिबरल्स’ और उनके बीच से उभारे गए कुछ ‘पब्लिक इंटैलेक्चुअल’ जो बीते छह सालों से यदा-कदा दिल्ली के आईआईसी लौंज, बंगलुरू के किसी बड़े संस्थान या न्यूयार्क, वाशिंगटन, लंदन या पेरिस के शैक्षिक परिसरों या किन्हीं बड़े थिंक-टैंक में सक्रिय दिखते हैं, वे तब क्या कर रहे थे? सच ये है कि उन्हीं तीन दशकों के दौरान आज के इन तमाम ‘पब्लिक इंटैलेक्चुअल्स’ की पैदाइश होती है। इनके बड़े हिस्से ने सबाल्टर्न समूहों की वास्तविक आकांक्षाओं और सत्ता में हिस्सेदारी के आग्रह को ‘पहचान की राजनीति’ या दलित-ओबीसी शीर्ष नेताओं की सत्ता-लिप्सा का पर्यायवाची समझा और उसी रूप में व्याख्यायित किया।
हाशिए के समाजों में अंदर ही अंदर इस उपेक्षा की तीखी प्रतिक्रिया होती रही। उसने अंततः ‘सेक्युलर’ कहे जाने वाले कुछ दलों, उसके नेताओं एवं लिबरल बुद्धिजीवियों के विरुद्ध ठोस आकार धारण कर लिया। इस आकार में बड़ी चतुराई से भाजपा-संघ ने घुसपैठ की थी। टीवी चैनलों का जबर्दस्त इस्तेमाल करते हुए हिन्दुत्व ब्रिगेड ने सबाल्टर्न समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। इस दरमियान, लिबरल्स का बड़ा हिस्सा पढ़े-लिखों की अपनी दुनिया में ही खोया रहा। शायद इसीलिए उसे समझ में भी नहीं आया और आज भी नहीं आ रहा है कि हमारा देश मौजूदा स्थिति में क्यों और कैसे जा पहुंचा?
अंग्रेजी के ऐसे लेखकों को ‘पब्लिक इंटैलेक्टुअल’ कहने वाले- ‘हे महा-बुद्धिजीवियों, मुझे माफ़ करना, आपकी आन-बान और शान बनी रहे, पर आप ‘पब्लिक इंटैलेक्चुअल’ कहलाने के हकदार नहीं हो! अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा कि भारत आज इस स्थिति में पहुंचा क्यों तो आप ‘पब्लिक इंटैलेक्चुअल’ क्या, समझदार नागरिक भी नहीं माने जा सकते!
इस विशाल देश में बुद्धिजीवियों की भारी तादाद है। जटिलताओं और विविधताओं भरे इस देश में दुर्भाग्य ये है कि जो तमिलनाडु, केरल, असम, आंध्र या तेलंगाना में बड़ा बुद्धिजीवी समझा जाता है, उसे यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश में कोई जानता तक नहीं या जानना भी नहीं चाहता! वह लेखक या बुद्धिजीवी अगर अंग्रेजी में लिखता-बोलता है, उसका प्रभामंडल बड़ा है और मीडिया में उसके कई दोस्त संपादक या एडिट-पेज प्रभारी हैं, तो बहुत आराम से उसे दिल्ली-मुंबई की विद्वत-मंडली द्वारा ‘पब्लिक इंटैलेक्चुअल’ घोषित किया जा सकता है।
भारत के अस्सी फीसदी लोगों के आम हितों के विरुद्ध वह अतीत में कभी लिख चुका हो तो भी उसे भारत के श्रेष्ठतम लोक-बुद्धिजीवियों में शुमार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं ऐसे कई ‘पब्लिक इंटैलेक्टुअल्स’, विद्वानों और संपादकों को जानता हूं, जिन्होंने अपने युवा दिनों में एक स्कॉलर के तौर पर मंडल आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ जमकर जहर उगला था। तत्कालीन विपक्षी नेता राजीव गांधी ने 6 सितंबर, 1990 को जब लोकसभा में मंडल-रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराते हुए लंबा भाषण दिया तो इनमें कइयों ने उस विवादास्पद भाषण की तारीफ में कसीदे कढ़े थे।
सकारात्मक कार्रवाई की इस विलंबित पहल को भी इन लोगों ने समाज के व्यापक हितों के विरूद्ध बताया था। पर आज जब ऐसे ही लोगों के नाम के साथ देश के अग्रणी पब्लिक इंटलेक्चुअल का विशेषण नत्थी हो चुका है तो समाज और भारतीय बुद्धिजीवी के बीच की खाई को समझना कठिन नहीं। पर विडंबना देखिए, मोदी-सरकार द्वारा पारित और लागू किए सवर्ण समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आरक्षण के फैसले पर उन बौद्धिकों ने एक भी आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं लिखी। यह भी सवाल नहीं उठाया कि संविधान के किस अनुच्छेद से ऐसे आरक्षण के लिए जगह मिली? उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि इससे वह समाज उनसे नाराज होता, जिससे वह स्वयं आए हैं!
पर राहुल सांकृत्यायन या ईएमएस नंबूदिरिपाद के बौद्धिक चिंतन के रास्ते में तो ऐसी बाधाएं नहीं आईं! फिर आज के लिबरल्स या यहां तक कि अनेक वामपंथियों के समक्ष ऐसे संकट या बाधाएं क्यों और कैसे आ जाती हैं? उन जैसे ऐसे सवालों पर नहीं सोचते। इससे उनके ‘पब्लिक इंटैलेक्चुअल’ तमगे पर क्या असर पड़ता है? आखिर इस तरह के विशेषणों के थोक-वितरक तो वही लोग हैं, जिन्हें इस देश के दलित-ओबीसी सबसे अधिक जातिवादी नजर आते हैं! आदिवासियों की पीड़ा और उपेक्षा से उन्हें कोई परेशानी नहीं। हां, यदाकदा उन पर उनका प्यार जरूर उमड़ पड़ता है कि हाय, वे कितने सहज-सीधे और स्वाभाविक होते हैं! आईआईसी या दिल्ली-मुंबई के ऐसे इलीट अड्डों पर बैठने वालों के लिए अब सब कुछ उलटता-पुलटता नजर आ रहा है।
उनका ‘स्वर्ग’ (जिसकी क्षतिपूर्ति वे लंदन-न्यूयार्क-पेरिस रहकर आसानी से कर लेते हैं) छिनता नजर आ रहा है। अफसोस कि वहां आम जनता ने धावा नहीं बोला। हिंदुत्ववादी नये शासकों के समर्थकों ने धावा बोला है। ऐसे ‘पब्लिक इंटैलेक्चुअल्स’ को लेकर सिर्फ उनकी अल्प-ज्ञात और अल्प-स्वीकार्य शख्सियत ही समस्या नहीं है, समस्या उनके नजरिए या ‘व्यू प्वांइट’ में भी है। कहां और किधर खड़ा होकर वे अपना नज़रिया बना रहे हैं? नये शासकों को मालूम है कि वे रंग-बिरंगे ‘लिबरल्स’ और इलीट पब्लिक इंटैलेक्चुअल्स सिर्फ अंग्रेजी में कुछ लिखते-पढ़ते रहते हैं। उनसे भला क्या समस्या है?
वे सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे, वरवरा राव या फादर स्टैन स्वामी जैसे नहीं हैं! बेशक वे बुद्धिजीवी हैं पर उन्हें लोक-बुद्धिजीवी (पब्लिक इंटैलेक्चुअल) नहीं कहा जा सकता! भारत जैसे देश में सुधा भारद्वाज, नवलखा या तेलतुंबड़े जैसा लोक-बुद्धिजीवी होने के लिए लोक के साथ खड़ा होना बुनियादी शर्त है। भले ही उसका दायरा किसी प्रदेश या क्षेत्र तक ही क्यों न सीमित हो! एक लोक बुद्धिजीवी सिर्फ तमिल में लिखने वाला पेरुमल मुरूगन जैसा भी हो सकता है, इसके लिए किसी आईआईसी जैसे इलीट अड्डे या किसी बड़े अंग्रेजी अखबार की मंजूरी जरूरी नहीं होगी।
गौरी लंकेश अंग्रेजी में भी लिखती थीं। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। पर वह कन्नड़ में लिख-बोल कर पब्लिक इंटैलेक्चुअल बनी थीं। पब्लिक का पक्ष लेने के चलते ही मारी गईं। इसी तरह आजादी से काफी पहले सन् 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अपनी जान दे दी। उन्हें अच्छी अंग्रेजी आती थी। पर वह कानपुर से छपने वाले ‘प्रताप’ जैसे हिंदी अखबार के संपादक थे।
ईमानदारी और समझदारी का अद्भुत समन्वय था उनके व्यक्तित्व में! डॉ. बीआर अंबेडकर भारतीय समाज के सर्वाधिक उत्पीड़ित लोगों की आवाज बनकर उभरे। इसके साथ उन्होंने हमेशा अपने देश-समाज के लिए बड़ा स्वप्न देखा और उसे पूरा करने के लिए वह सब कुछ किया, जो अपनी सीमित शक्ति में वह कर सकते थे। हिंदी भाषी क्षेत्र में एक बड़े पब्लिक इंटैलेक्चुअल के तौर पर राहुल सांकृत्यायन का काम सबके सामने है।
अब तक न जाने कितनी पीढ़ियों को उन्होंने अंध-विश्वास, कूपमंडूकता, कट्टरता, वर्णव्यवस्था और धर्म के राजनीतिक मंसूबों की उग्रता से उबारा। जरूरत पड़ी तो किसानों के लिए पुलिस की लाठियां भी खाईं। पर आज के हमारे स्वघोषित पब्लिक इंटैलेक्चुअल किसानों की बात छोड़िए, समाज के सबसे उत्पीड़ित दलित-आदिवासी, जुलाहा, बुनकर और अंसारी के साथ भी ठीक से नहीं खड़े होते!
आज के दौर में लोक के साथ वही खड़ा हो सकता है, जिसकी प्रतिबद्धता समता, स्वतंत्रता और भाईचारे के महान् मानवीय मूल्यों में हो! समता और स्वतंत्रता के लिए आपको स्वाधीनता आंदोलन की ‘प्रभुत्वशाली-वैचारिकी’ से भी आज आगे बढ़ना होगा। लोकतांत्रिक-सेक्युलरवाद जरूरी है, लेकिन उसे वापस हासिल करने के लिए वर्ण-व्यवस्था के विनाश के पक्ष में जाना होगा। आज के हिंदुत्व-कॉरपोरेट गठबंधन का मुकाबला सत्तर साल पहले की ‘प्रभुत्वशाली वैचारिकी’ से अब नामुमकिन है!
इस घुप्प अंधेरे में भी समय-समय पर नई वैचारिकी की रोशनी झिलमिलाती नजर आती है। इस नयी वैचारिकी के साथ जो खड़ा होगा, इतिहास उसे ही लोक-बुद्धिजीवी के रूप में याद करेगा, बाकी ‘बुद्धिजीवियों’ के लिए रूदाली का विकल्प खुला रहेगा: ‘हाय मेरा वो सेक्युलर-स्वर्ग कहां गया? कब लौटेंगे वे अपने अच्छे दिन? कब हम अंग्रेजी में बोलने-लिखने और जीने वाले ‘श्रेष्ठ लोग’ शासन की सलाहकार-मंडली का हिस्सा होंगे?’ ऐसे लोगों को निराश नहीं कर रहा! पर उन्हें यथार्थवादी होने की सलाह देना नहीं भूलूंगा।
उन्हें समझने के लिए तैयार होना चाहिए कि उनके वो दिन अब नहीं लौटेने वाले हैं! ज्यादा बुरे दिन आएंगे या फिर वाकई सुंदर दिन! उन्हें तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं? किधर खड़े होना चाहते हैं? चाहें तो वे नोट कर लें, लोक-बुद्धिजीवी होने का रास्ता अब किसी लिबरल-कारपोरेट के बाड़े, किसी सुपर-इलीट घराने या किसी द्विजवादी के ‘अग्रहारम्’ से नहीं निकलेगा!
(उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार और कई चर्चित किताबों के लेखक हैं। एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहते राज्यसभा चैनल की शुरुआत करने का श्रेय आपको जाता है।)