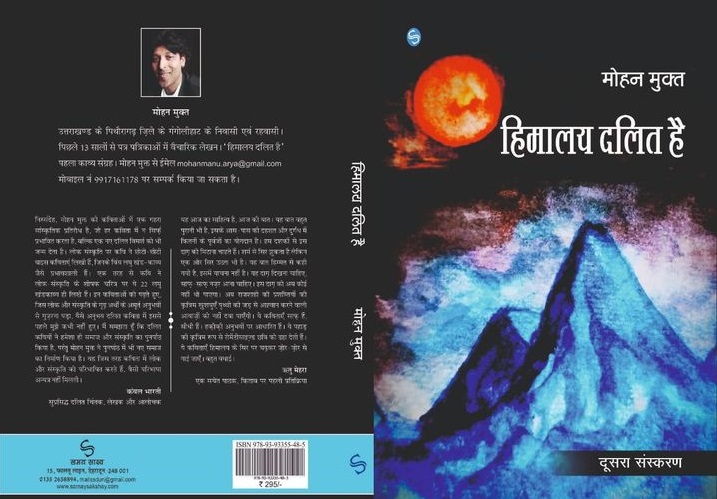इससे पहले कि टीवी समाचार के आसमान पर छाए बादल फटते मैं निकल आया था। या निकलने को विवश हुआ था। लेकिन जाता कहां? ये मेरी ख़ुशफ़हमी थी। अपने इर्दगिर्द ऐसी फुसफुसाहटें, और ऐसी शिकारी आंखें रेंगने लगी थीं जो खुद को भविष्य में आखेट के लिए तैयार कर रही थीं। उनमें मुहावरे की बिल्ली से भी ज्यादा गहरी आध्यात्मिकता और ज़्यादा प्रछन्न झपट थी। लेकिन ये भी कुछ समय की ही बात थी। और कालान्तर में किसी ओट या आड़ की जरूरत भी नहीं रह गयी थी।
1995-96 में टीवी समाचार के उदय, कालान्तर में 24 घंटे के समाचार और लाइव प्रसारणों और मीडिया उद्योग में भीषण प्रतिस्पर्धा का दौर एक भीषण हश्र लेकर आया। टीवी कार्याविधि और टीवी कार्य योजना- ब्रेकिंग न्यूज और टीआरपी की फिसलन से होते हुए एक राजनीतिक हथकंडे से पहले प्रछन्न फिर प्रकट एजेंडे में तब्दील हो गयी। कुछ व्यग्र जानकार मासूमियत में कह देते हैं कि टीआरपी की होड़ ने चैनलों को ग्रस्त कर दिया है। वह दौर चला गया जब बात इतनी वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा वाली थी, अब मामला टीआरपी का नहीं रह गया है। सत्ता राजनीति का उपकरण तो टीवी माध्यम को पहले भी कहा जाता रहा था लेकिन तोहमत सरकार के टीवी पर लगती थी, जिसकी सरकार उसका प्रचार, अब तो इसमें प्रतिस्पर्धा आन पड़ी है!
टीवी समाचार की दुर्दशा पर पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी कुछ लिखा और बोला जा चुका है। लेकिन इस हालात की जिम्मेदारी आज के कारणों में तलाशी जाती है। कोई तात्कालिक जुड़ाव निकाला जाता है। स्वाभाविक है लेकिन अगर 21वीं सदी की शुरुआती तारीखों में जाएं और बिल्कुल हाल के अतीत को भी टटोल आएं तो हम जान पाएंगे कि टीवी के इस अवमूल्यन की एक प्रक्रिया रही है। उन वक्तों को भी याद करें जब टीवी को सनसनीखेज और नंबर वन बनाने के लिए झूठ अंधविश्वास और अपराध कथाओं को भड़कीली सनसनी के साथ पेश किया जा रहा था। टीवी अपनी पुरानी उत्तेजनाओं पर ही सवार होकर आज प्रत्यक्ष है।

टीवी ने मुहावरों से खींचकर वास्तव में आकाश पाताल एक कर दिया था। जाने कैसे कैसे शीर्षकों वाले कार्यक्रम बनाए जाने लगे और मोटे-मोटे टाइप साइज वाले अक्षरों की प्लेट लगाकर और लगभग चीखते हुए और भर्राते हुए वॉयस ओवर और अति नाटकीय और बेहूदे रूपांतरणों के सहारे दर्शकों को लुभाने और थर्राने की कोशिशें की गयीं। लेकिन इस सनसनी से उनके ऐंद्रिक अनुभवों को छलनी किया।
मौलिकता गायब हो चुकी थी और टीवी के स्क्रीन पर समाचार का स्थान अचानक ही एक नये किस्म के विद्रूप ने ले लिया था, भूतप्रेत के किस्से खबरों की तरह और भविष्यफल बताने वाले लोग ऐंकरों की तरह पेश किये जाने लगे थे, उनके विज्ञापनों की भरमार हो चुकी थी। चैनलों का ये बाबा काल कैसे भुलाया जा सकता है। लेकिन इसी में हमें वो प्रक्रिया भी देखनी चाहिए जिसको पूरा होता हुआ आज हम अपने टीवी स्क्रीन पर देखने को विवश हैं। आज के टीवी के स्तर पर आने के लिए कुछ दशकों पहले के टीवी ने तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे इस देश की समाज और राजनीति में आयी फिसलन बहुत समय पहले से जमा काई का नतीजा है वैसा टीवी मीडिया में भी हुआ है। फ़र्क यही है कि राजनीति और उसके विमर्श को यहां तक पहुंचने में एक बहुत लंबा वक्त लगा है जबकि टीवी ने कम समय में ही बड़ी छलांगें लगायी हैं।
सहज, विश्वसनीय, ठोस रिपोर्टें यहां वहां दुबक गयीं। उनके लिए प्राइम टाइम में कोई स्पेस नहीं रह गयी थी। धीरे-धीरे विकरालता बढ़ती और फैलती चली गयी और टीवी समाचार की जगह स्टूडियो की दहाड़ती बहसों ने ले ली। इनके बारे में सब जानते हैं क्या कहा जाए। हरिशंकर परसाई अगर जीवित होते न जाने क्या कहते इस पर। अमेरिकी निजी टीवी चैनलों के ऐंकरों की देखादेखी हिंदी और अंग्रेजी की डिबेटों में गर्जना और अंधड़ टूट पड़े। वैसा गर्जन तर्जन समकालीन समय में याद कीजिए कहां से शुरू हुआ था। आपको 1992 याद आयेगा। उस समय वीडियो पत्रिकाएं आ चुकी थीं और दूरदर्शन तो था ही। एक दशक पूरा होते होते टीवी स्क्रीन के एक कोने से आग उठती रही और ऐंकर सामने देखते हुए जैसे दर्शकों को ही चुनौती देने लगे।

आज की बहस में प्रिंट के, प्रिंट से टीवी में आये और सीधे टीवी में ही पले-बढ़े और फले-फूले उन पुराने प्रधानों की शिनाख़्त भी होनी चाहिए जो अपनी भूतपूर्व प्रधानता के साए में नये शक्ति केंद्रों के कामयाब पुर्जे बन चुके हैं। होड़ है कि कौन कितना रंग जमा पाता है। कौन कितना रौद्र और कितना चित्रकार की उस कल्पना की रेखाओं को साकार कर सकता है जो इधर कुछ वर्षों से कारों के पिछले शीशों पर और सोशल मीडिया नेटवर्किंग के स्टेटस या डीपी पर देखी जाने लगी हैं। क्या हमारे ऐंकरों की पेशानियों पर उभरती गिरती और फिर उभरती जाती वही रेखाएं नहीं हैं।
सौम्यता एक कमजोरी मान ली गयी है। उग्रता एक पॉजिटिव विशेषता। अपनी बात को कहने का सधा हुआ अंदाज़ नहीं हमलावर और हिंसक अंदाज चाहिए। वे क्या सो पाते होंगे या अपने घरों में सामान्य व्यवहार कर पाते होंगे। वे हमारे ऐंकर। इतना चीखते चिल्लाते नथुने फड़काते दौड़ते हाथ उठाते नाखून चबाते हाथ मसलते भृकुटियां तानते कमीज की बांह मरोड़ते, अंगुलियों को नचाते नहीं थे- 2014 ने जैसे उन्हें नया जामा पहना दिया एक नयी टीवी भाषा, एक नयी अग्निवर्षक शब्दावली, एक नया अनुदारवादी सिमैन्टिक्स और सीमिऑटिक्स दोनों। ये जैसे काफ्का का मेटाफॉरफोसिस भी था। कमोबेश धमकियों की तरह बुलेटिन निकाले गये और प्राइम टाइम की बहसें इच्छित और मैनुफैक्चर्ड विषयों और विषयान्तरों पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कोई मलबा गिर पड़ा हो।

लेकिन अपनी गलतियों और नादानियों पर पर्दा डालकर हम कैसे दरकिनार हो सकते हैं, ये जवाबदेही आज की नही है। मेरे टीवी कार्यकाल के एक नौसिखिए युवा सौम्य चेहरे पर आज ये दहला देने वाली क्रूरता की छाप किसने छोड़ी है। क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से मुकर सकते हैं। जब हमारे पास अवसर थे और बोलने की शक्ति और स्पेस थी, अनेकानेक कारणों से हम चुप रह गये, आगे बढ़े या किनारे खड़े हो गये। हमने नयी पीढ़ी को भी नहीं देखा और न ही नयी राजनीतिक परिघटना को जो लोकतंत्र और भरोसे को चबाने निकल आयी थी।
ये विशाल कंटीला जबड़ा हम नहीं देख पाये। हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि हम जो बना रहे थे रात दिन वो दरअसल यही आकार था। हम समझ ही नहीं पाए कि ये हमने क्या बना डाला। और अब एक आमादा टीवी हमें अपनी ओर खींचता जा रहा है। अमेरिकी मीडिया चिंतक नील पोस्टमैन ने दशकों पहले ये सब भांप लिया था अपनी उस विख्यात किताब के ज़रिए जिसका शीर्षक हैः अम्यूज़िंग अवरसेल्व्स टू डेथ।
(शिव प्रसाद जोशी वरिष्ठ पत्रकार, कवि और गद्यकार हैं मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले जोशी आजकल जयपुर में रह रहे हैं।)