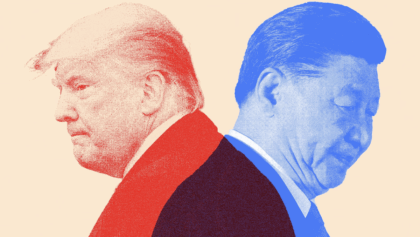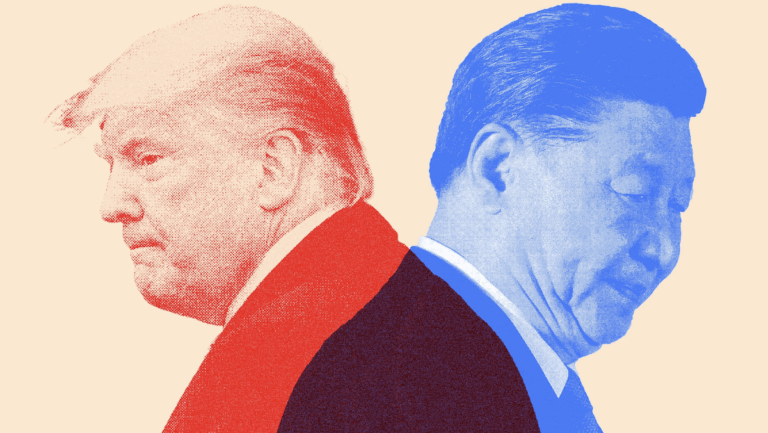लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है, लोकतंत्र का पर्व। लोकतंत्र का पर्व असल में किस का पर्व होता है? लोक का होता है। लोकतंत्र में चुनाव लघुता का पर्व और गर्व होता है, प्रभुता का पर्व और प्रसाद नहीं। लोकतंत्र में चुनाव के पहले सारी ‘लोकतांत्रिक प्रभुताओं’ को विसर्जित हो जाना होता है, बचता है केवल संविधान। संविधान प्रदत्त अधिकार बल पर अपने-अपने मतदान के माध्यम से लघुताएं अपनी सम्मिलित शक्ति से ‘विसर्जित लोकतांत्रिक प्रभुता’ का पुनर्सृजन करती है। लघुता के पर्व की पवित्रता को विसर्जित प्रभुता की दुष्टताओं के सक्रिय रहने या हो जाने पर लोकतंत्र का पवित्र ‘अन्याय के खिलाफ न्याय युद्ध’ में बदल जाता है। फुसलाकर, पैसा देकर, कानूनी कार्रवाई से दंडित करने, फूट डालकर बहुमत का जुगाड़ करनेवाला ‘सिंहासनासीन’ योग का चाहे जितना भी ज्ञान दे लेकिन वह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के खोल और खेल से बाहर निकल कर साम-दाम-दंड-भेद के रास्ते पर ही चलता है। प्रभुता की दुष्टता से लघुता की पवित्रता को बचाना कोई आसान काम नहीं होता है।
चुनाव संघर्ष के लिए समान अवसर (Level Playing Field) का सवाल नेताओं और राजनीतिक दलों से अधिक आम नागरिकों और मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा सवाल है। चुनाव संघर्ष के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने में विवेकाधिकार का ‘सोद्देश्य इस्तेमाल’ करते हुए जानबूझकर नकारात्मक भेद-भाव को बढ़ाना या ऐसे भेद-भाव को रोकने के दायित्व के प्रति उदासीन बने रहना राजनीतिक दलों के प्रति नहीं, आम नागरिकों और मतदाताओं के विश्वास के उल्लंघन (Breach of Trust) का मामला होता है। सारा पेच ‘जानबूझकर’ को लेकर है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के सभी शक्ति प्रसंगों में विवेकाधिकार (Discretionary) का बड़ा महत्व होता है। विवेक का पासंग न्याय को असंतुलन में डाल देता है। विवेकाधिकार के असंतुलन से विषमतामूलक (Discrimination) व्यवहार का जन्म होता है। चुनाव संघर्ष के लिए समान अवसर का अभाव केवल चुनाव को ही नहीं, पूरे लोकतंत्र को असंतुलित कर बैठता है। ऐसे में लोकतंत्र के पर्व में लघुता की पवित्रता को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
पुरा-कथाओं में, प्रवचनों में प्रकट होते हैं। जीवन में कोई देवता नहीं, कोई मसीहा नहीं, कोई नहीं प्रकट होता है, जब गरीबों को सताया जाता है। हमारा सांस्कृतिक अनुभव चेताता है, “शनैः पन्थाः शनैः कन्था शनैः पर्वतमस्तके। शनैः विद्या शनैः वित्तं पञ्चैतानि शनैः शनैः॥” 2024 का आम चुनाव मतदाताओं की समझदारी के साथ-साथ लोकतांत्रिक धीरज की परीक्षा की घड़ी बनकर हाजिर हुआ है। लोकतंत्र का रास्ता लंबा है, धीरे-धीरे तय होगा। संविधान को मजबूती से थामे रहना है। दुख का पहाड़ बहुत ऊंचा है। जिन्हें चार सौ पार जाना है जायें या न जायें, देश के आम लोगों के लिए अधिक जरूरी है बाल-बच्चों और बूढ़े-बीमार मां-बाप को संभालते हुए धीरे-धीरे दुख के दुर्लंघ्य पहाड़ को पार करना होगा। योग-योग चिल्लाते हुए भ्रामक विज्ञापन देकर कोई योगी नहीं बन जाता है! किसी भी योगी-भोगी की पांच-दस ट्रिलियन इकोनॉमी की चकचौंधी बात पर, 2047 की भ्रामक बातों पर आंख मूंदकर यकीन नहीं करना है। रात की रतौंधी और दिन की चकचौंधी से बचते हुए इस चुनाव में प्रभुता के कारनामों से अपनी लघुता की पवित्रता को बचाना भारत के आम नागरिकों और मतदाताओं के अपने हाथ में है। कमजोर-सा दिखनेवाला जो हाथ देश का निर्माण करता है, किसी अन्य का मुनाफा बनाने के काम आता है, यकीनन लोकतंत्र के चुनाव पर्व में लघुता की पवित्रता की भी रक्षा कर सकता है। बस भरोसा न डिगने पाये, ईवीएम (EVM) न कांप जाये।
रात की रतौंधी और दिन की चकचौंधी कैसे नजर को झलफला देती है! तरंगी मीडिया पर सवार होकर कहने-सुनेवाला आता है। कहनेवाला कह रहा होता है। सुननेवाला सुन रहा होता है। बिना किसी बेचैनी के। कहने और सुनने में दोनों रमे रहते हैं। दोनों जानते हैं जो कहा-सुना जा रहा है वह झूठ है। न कहनेवाला पलक झपकाता है, न सुननेवाला कान पटपटाता है। कोई सवाल, पूरक या मूल कोई सवाल नहीं, बस ‘संगत’! संगत दिया जाता है। जैसे एक बाजा बजानेवाले को दूसरा वादक संगत देता है। प्रेस-वार्ता नहीं, प्रेस-संगत! इस तरह, असली सवालों को उलझाने और ओझल करने के लिए भाषा का दुष्ट इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करते हुए नकली सवालों की गहराइयों में जाकर सत्य सरीखा लगनेवाला नकली और निष्प्राण जवाब अर्थहीन अलंकृत भाषा में सजाकर सामने लाया जाता है। यह सफेद झूठ होता है।
सफेद झूठ यानी सफेदपोशों का झूठ। सफेदपोशों का झूठ उन के समूह में स्वीकार किये जाने लायक साझा झूठ होता है। इस साझा झूठ का व्यापक प्रचार प्रसार एवं अन्य समूहों और समुदायों के बीच किया जाता है। सफेद झूठ को लोगों के मन-मस्तिष्क में स्थापित किये जाने लायक बनाकर मीडिया की तरंगी ताकत से जोड़ दिया जाता है। सभ्य, शांत और सुशील वातावरण में ‘खाये-अघाये’ नेताओं के भाषणों में, प्रेस-वार्ता की करुणा विगलित भाषा में अकसर यह ‘महामनोरम’ दृश्य दिख जाता है। इस तरह से वर्चस्वशाली और सशक्त सफेदपोशों का झूठ ‘पूरी दुनिया’ का सच हो जाता है। इस तरह हो जाती है, ‘दुनिया मुट्ठी में’।
इस तरह लोकतंत्र चलता रहता है। झूठ और सच के संघर्ष में तर्कशील चयन की प्रक्रिया इतिहास को गति देती रहती है। इतिहास चलता रहता है, कभी स्वाभाविक गति से तो कभी तेज या मंद गति से। डॉ. राम मनोहर लोहिया हमेशा कहा करते थे, ‘इतिहास कभी चलता है रजामंदी से, कभी चलता है संघर्ष से और अकसर दोनों के मिश्रण से।’ डॉ. राम मनोहर लोहिया की बात को विचार, प्रतिविचार और समविचार (Thesis, Antithesis, Synthesis) के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इसे भारतीय चिंतन परंपरा की ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोधः। बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः’ के संदर्भ से भी समझा जा सकता है। मूल बात यह है कि मनुष्य का जीवन और जीवंत लोकतंत्र में वाद-विवाद-संवाद की अटूट और स्वस्थ परंपरा बहुत गुणकारी होती है।
भारत में जनजीवन और लोकतंत्र का बहुत बड़ा संकट यह है कि यह ‘वाद’ में ही संकुचित होकर रह गया है। ‘विवाद’ की गुंजाइश को समाप्त कर देने से ‘संवाद’ की सारी संभावनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। संकुचित वाद से उत्पन्न होती है, ‘प्रभुता के सफेद झूठ की दहाड़’ और बचता है केवल विपक्षी गठबंधन के बिलखते हुए सच का ‘चिल्ल-पों’! जैसे ‘जंगल में शेर की दहाड़’ और चिड़ियों का चनचुन। जिन में ‘शेर बनने’ की अवांछित आकांक्षा होती है वह देर-सवेर लोकतंत्र को जंजाल में बदलकर ‘एकोअहं’ का रास्ता अख्तियार कर ही लेता है। ‘एकोअहं’ के चरित में ‘चार सौ पार’ का सपना है। सपना में सिद्धांत है। सिद्धांत यह कि सारा वोट मेरा और सारा नोट दोस्तों का; वोट भी मेरा और नोट भी मेरा।
वन नेशन, वन इलेक्शन के पीछे क्या है! वन नेशन, वन इलेक्शन के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ लगता है। खैर रहस्य तो रहस्य है, जब खुलेगा तब खुलेगा। अभी तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि वन नेशन, वन इलेक्शन का इरादा क्या हो सकता है। पहले ‘चार सौ पार’ को समझना होगा। ‘चार सौ पार’ यानी विशेष बहुमत। ‘चार सौ पार’ यानी संविधान में बदलाव या संविधान को बदलने की ताकत। कुछ बदलावों के लिए तो विधान सभाओं में से आधा का समर्थन जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी और उसका पितृ-संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारत के संघात्मक ढांचा के प्रति असम्मान है। वे भारत संविधान की सभी बात को कि “इंडिया, जो भारत है, राज्यों का संघ होगा। (India, that is Bharat, shall be a Union of States.)” से सहमत नहीं हैं। राज्यों को भारत संघ का घटक नहीं मानते हैं, बल्कि वे राज्यों को भारत का अंग मानते हैं। अब संवैधानिक संदर्भ ‘घटक’ और ‘अंग’ का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। भारत का संविधान संघात्मकता पर बल देता है, लेकिन वे एकात्मकता पर जोर देते हैं। इसलिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार-बार किसी-न-किसी बहाने राज्यों पर दबाव बनाती है। इनके हाथ में ताकत हो तो शायद पहला बदलाव इस संघात्मकता ढांचा में ही करना पसंद करेंगे।
इन सब बातों को देखते हुए उनके एक भिन्न इरादे का कयास उभर रहा है। कयास यह कि वे राज्य सभा की तर्ज पर राज्य विधान सभाओं के गठन की संवैधानिक व्यवस्था करें। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की तरकीब यह हो सकती है कि ‘वन नेशन’ भारत में केवल लोकसभा के लिए ‘वन इलेक्शन’ हो। फिर लोकसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर सभी विधान सभाओं के सदस्यों का चयन कर लें। हो सके तो मुख्यमंत्री की हैसियत सूबे (राज्य) के सुबेदार की तरह हो जाये, जो लोकसभा सदस्यों के बहुमत के आधार पर टिके रहें या बदले जा सकें। राजतंत्र के दौर में यह व्यवस्था थी।
ऐसा कयास इसलिए भी लग रहा है कि राजा बनने और राजा जैसा आचरण करने की तीव्र लालसा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार में दिख जाती है। यह भी लगता है कि ‘शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत’ को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए भारत सरकार के किसी भी काम को जांच और संतुलन (Check and Balance) की सभी व्यवस्था से बाहर कर दें। साफ-साफ कहें तो राज्याधिकरण, कार्याधिकरण और न्यायाधिकरण को ‘एकोअहं’ में समाहित करने की कोशिश करें। बहरहाल, कयास तो कयास है। यह पूरी तरह से या आंशिक रूप गलत हो सकता है।
जो हो, कयास गलत हो, सही हो, लेकिन ‘चार सौ पार’ के मनोरथ का कोई-न-कोई कारण तो होगा ही न! यह अलग बात है कि आम नागरिकों और मतदाताओं की ‘रणनीतिक समझदारी’ चुनाव पर्व की पवित्रता को किसी भी तरह की दुष्टता से बचा लेगी। प्रभुता का अपना मनोरथ हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लघुता का पर्व और गर्व होता है, प्रभुता का पर्व और प्रसाद नहीं! हां, सचेत रहने की जरूरत तो है ही।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)