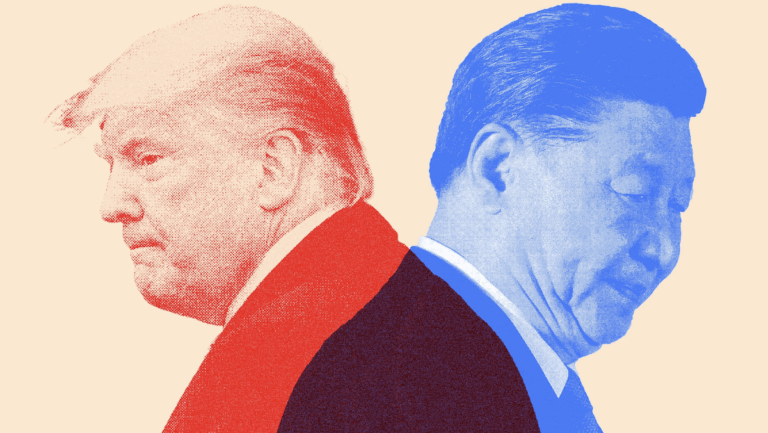उपचुनावों के नतीजों पर हो रही बहस में एक बात पर लगभग सहमति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जादू खो चुके हैं। भले ही गोदी मीडिया और आरएसएस-भाजपा संचालित सोशल मीडिया इसे मानने को तैयार नहीं हों, लेकिन अब लोग यह मानने लगे हैं कि सांप्रदायिक नफरत का जहर पहले जैसा असर नहीं दिखा रहा है। लोग अपनी तकलीफों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार मानने लगे हैं। भाजपा में अब ऐसी स्थिति भी नहीं रह गई है कि उपचुनाव में हार का ठीकरा दूसरे नेताओं के सिर फोड़ दिया जाए। नगर निगम से लेकर संसद के चुनावों तक मोदी ही चेहरा और अमित शाह ही सेनापति हैं। वे पराजय के लिए किसी और को दोषी नहीं करार दे सकते हैं। लेकिन कई सवालों पर बहस नहीं हो रही है।
पिछले सात सालों के मोदी शासन में भारतीय लोकतंत्र को जो नुकसान पहुंचा है उसकी वैचारिक जड़ें कहां हैं और इसके मुकाबले की रणनीति क्या हो? आरएसएस और कारपोरेट मीडिया ने मिल कर विचारधारा की जो शून्यता पैदा की है उससे कैसे लड़ा जाए? अगर लोगों की समस्याओें को दूर करने में नाकामयाबी के कारण मोदी सत्ता गंवा भी देते हैं तो सत्ता जिन लोगों के हाथ में आएगी क्या वे भारतीय राजनीति को सेकुलरिज्म तथा बराबरी के मूल्यों की ओर ले जाएंगे? भाजपा-आरएसएस के विकल्प की दावेदारी कर रही पार्टियों का चरित्र कैसा है? क्या उनके भीतर एक लोकतांत्रिक और विचारधारा आधारित राजनीतिक संस्कृति पैदा करने की जरूरत नहीं है?
विचारधारा की शून्यता का अर्थ समझना हो तो हमें किसान आंदोलन को देखना चाहिए। यह आंदोलन आने वाले 26 नवंबर को अपना एक साल पूरा कर लेगा। आजाद भारत के इतिहास में इतने बड़े जन-समर्थन वाले आंदोलन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं।
इसने अनुशासन का भी बेहतरीन नमूना पेश किया है। सरकार के लाख उकसाने के बावजूद यह अहिंसक बना रहा और हर हिंसा का जवाब इसने लोकतांत्रिक ढंग से दिया। लखीमपुर खीरी इसका ताजा उदाहरण है। काले झंडे दिखाने गए किसानों पर केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी ही चढ़ा दी, लेकिन किसानों ने हिंसा नहीं फैलने दी। सरकार ने सांप्रदायिक और जाति के आधार पर भी आंदोलन को बांटने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी एकता बचाने में कामयाब रहे।
इन सबके बावजूद किसान आंदोलन देश में व्यापक बदलाव का जरिया नहीं बन सका है। इतिहास गवाह है कि चंपारण और बारदोली के किसान आंदोलनों ने एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष की नींव रखी थी और बाद में किसान सभा ने आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। अगर किसानों के हिंसक संघर्षों की बात करें तो तेलांगना और नक्सलबाड़ी के किसान आंदोलनों ने देश के कम्युनिस्ट आंदोलन को गति दी। पश्चिम बंगाल में किसानों के समर्थन और इसके असर में हुए भूमि सुधारों की बदौलत वाम मोर्चा की सरकार ने लगभग साढ़े तीन दशक तक शासन किया। इन आंदोलनों ने न केवल राजनीति बल्कि साहित्य और संस्कृति को भी गहरे प्रभावित किया।
आजाद भारत के दो आंदोलनों के राजनीतिक असर को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक है 1974 का जयप्रकाश आंदोलन जो छात्रों के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और लोकतंत्र बचाने के आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर किया और देश में उन राजनीतिक परिवर्तनों की शुरुआत की जो आगे चल कर एक ओर मंडल की सामाजिक न्याय और दूसरी ओर कमंडल की सांप्रदायिक राजनीति में तब्दील हुई।
ऐसा ही आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में शुरू हुआ था जिसका उद्देश्य देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की संवैधानिक मशीनरी बनाना था। इस आंदोलन के कारण कांग्रेस सरकार की साख बुरी तरह गिरी और भाजपा सत्ता में आई। हालांकि यह आंदोलन लोकतांत्रिक तत्वों के समर्थन से आगे बढ़ा था, लेकिन आरएसएस के समर्थन से अंतत: उन तत्वों के हाथ में चला गया जो हिंदुत्ववादियों के एजेंडे पर ही चल रहे हैं। खुद को हिंदुत्व का समर्थक साबित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह की नौटंकी कर रहे हैं वह सबके सामने है।
कुछ लोग इसे भाजपा को काटने की रणनीति बता सकते हैं। अगर यह सच भी हो तो यह एक गलत और संविधान को कमजोर करने वाली रणनीति ही है। यह संघ की विचारधारा का ही समर्थन है। लेकिन अन्ना आंदोलन के इस राजनीतिक असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसने कांग्रेस के पराभव की जमीन तैयार की। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अन्ना आंदोलन की बुनियाद में यह विचार था कि लोकतंत्र को ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाए। यह आंदोलन लोकपाल कानून के जरिए नौकरशाही तथा राजनीतिक नेतृत्व को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाना चाहता था। केजरीवाल तथा उनके साथियों ने इस लक्ष्य को छोड़ कर इसे दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का जरिया बना लिया।
दोनों ही आंदोलन अंत में नकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने वाले साबित हुए, लेकिन उन्होंने समाज में राजनीतिक परिवर्तन की भूख जगाई। लेकिन मौजूदा किसान आंदोलन देश की राजनीति को बदलने का जरिया बनने को तैयार नहीं दिखाई देता है। यह भाजपा के खिलाफ वोट करने की बात तो करता है, लेकिन देश की राजनीति में व्यापक हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं है। कई वामपंथी संगठनों की मजबूत उपस्थिति के बाद भी वह अपने को गैर-राजनीतिक बनाए है और अपनी इस स्थिति पर गर्व करता है।
लेकिन इसके अराजनीतिक होने के लिए किसान आंदोलन जिम्मेदार नहीं है। देश में लंबे समय से इस लोकतंत्र विरोधी विचार का प्रचार किया जाता रहा है कि राजनीति करना गलत है और राजनीतिक दल बेईमान हैं। इसी तरह का प्रचार विचारधाराओं के खिलाफ भी किया जाता रहा है। आरएसएस और मोदी सरकार ने तो समाज को विचारशून्य बनाने के लिए बाकायदा अभियान ही चला रखा है जिसके तहत उदारवाद और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले बुद्धिजीवियों को ‘‘लिब्रांडु’’ (यह उत्तर भारत की एक भद्दी गाली का रूपांतरण है), सेकुलरिज्म में यकीन करने वालों को ‘‘सिकुलर’’ (बीमार का समानार्थी ) और वामपंथी को ‘‘वामी’’ कहा जाता है। संघ ने बौद्धिक बहस से लोगों को दूर करने के लिए एक और झूठ फैलाया है कि प्रगतिशील बुद्धिजीवी पश्चिम के असर वाले और अंग्रेजीदां हैं। सच्चाई यह है कि हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करने वाले ही अंग्रेज परस्त रहे हैं और अंग्रेजी शासन के लिए काम करने वाले संस्कृत तथा भारत विद्या के विद्वानों के विचारों के समर्थक हैं।
उन्होंने ही अंग्रेजों के गढ़े इस इतिहास को प्रचारित किया है कि प्राचीन काल हिंदू काल, मध्यकाल मुसलमान काल और अंग्रेजों का काल आधुनिक काल है। अंग्रेजों ने उन्हें सिखाया है कि मुसलमान बाहरी और हमलावर हैं। भारत में मुसलमानों के आने के पहले ग्रीक, शक, हूण और कुषाण भी बाहर से आए थे और यहीं के होकर रह गए। एक तो मध्यकाल में सिर्फ मुसलमान ही राज नहीं कर रहे थे, बल्कि कई बड़े हिंदू राजा भी थे।
देश की आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म का पालन करता था और दूसरा मुसलमान भी यहीं के होकर रह गए और यहां की संस्कृति का हिस्सा बन गए। अंग्रेजों ने 1857 में जिन दो शख्सों पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाए वे वाजिद अली शाह और बहादुरशाह जफर थे। दोनों की सोच और उनके रहन-सहन को देखने पर पता चलता है कि वे किस तरह पक्के भारतीय थे। लेकिन संघ उन लोगों को राष्ट्र की प्रेरणा बताने के बदले उनसे प्रेरणा लेता है जो इतिहास की अंग्रेजों की व्याख्या और दुनिया में गोरों के शासन को श्रेष्ठ मानने वाले विचारों के समर्थक रहे हैं। इसमें विनायक दामोदर सावरकर का नाम पहले नंबर पर आएगा जो पश्चिम के उस राष्ट्रवाद के समर्थक थे जो एक धर्म, एक भाषा और एक संस्कृति की वकालत करता है।
बुद्धिजीवियों और विचारधारा पर ऐसा संगठित हमला जैसा आज आरएसएस कर रहा है दूसरे विश्व युद्ध के पहले इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने किया था। उन्होंने उन्हें देशद्रोही करार दिया था और तरह-तरह की यातनाएं दी थी। वह दृश्य भारत में भी दिखाई दे रहा है। अब माहौल बन गया है कि लोग विचारधारा का नाम लेने से घबराने लगे हैं और सेकुलर बताने के बदले अपने को हिंदू साबित करने में लगे हैं।
क्या यह विचारधाराओं की प्रासंगिकता कम होने या संघ की विचारधारा की विजय के कारण है? अगर गौर से देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज विचारधाराओं और विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि देश सबसे बुरे आर्थिक और राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। हमारी आर्थिक व्यवस्था विदेशी कंपनियों और चंद देशी अमीरों के चंगुल में है। लोकतंत्र और संविधान ध्वस्त होने के कगार पर है। सांप्रदायिकता और जातिवाद हमारे सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने में लगा है। ऐसे में विचारधाराओं की सिर्फ जरूरत ही नहीं है बल्कि इन पर जमी काई को भी साफ करने की जरूरत है।
क्या वजह है कि देश का विपक्ष लोकतंत्र पर हमले तथा आर्थिक व्यवस्था को चंद अमीर घरानों के हाथों में जाता देख कर भी उस तरह बेचैन नहीं है जैसा उसे होना चाहिए? असल में वह भी विचारधाराओं पर बहस की वापसी नहीं चाहता है। नई सभ्यता और नई संस्कृति बनाने को लेकर वह कोई बहस नहीं चाहता है। उसके लिए यही सुविधाजनक है कि वह जरूरत पड़ने पर अपने को हिंदू-हितैषी बता दे और फिर सेकुलर बन कर मुसलमानों का वोट मांगे। उसके लिए सुविधाजनक है कि वह महंगाई-बेरोजगारी की बात करे, लेकिन समाधान की बात आने पर लैपटॉप बंटवाने, सड़क बनाने, बिजली सस्ती देने और पीने का पानी पहुंचाने का शॉर्टकट सामने लाए।
उसके लिए यही सुविधाजनक है कि वह इस पर खामोश रहे कि कौन से उद्योग सरकार के पास रहें और कौन से उद्योग निजी क्षेत्र में। इसी तरह वह यह नहीं बताएगा कि सबको शिक्षा और सबको रोजगार देने की उसकी रणनीति क्या है। विपक्ष की पार्टियां यह सब तभी बता सकती हैं जब वे विचारधाराओं पर बात करेंगी। वामपंथी पार्टियां विचारधाराओं पर बात करती हैं, लेकिन उपभोक्तावाद, धार्मिक कट्टरपंथ और आदमी की जगह लेने वाली टेक्नोलॉजी तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों की चुनौती का सामना करने वाली रणनीति बनाने में सफल नहीं हो पा रही हैं। इन मुद्दों ने उनकी राजनीतिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। उन्हें विचारधारा की बहस में खुले मन से भाग लेने की जरूरत है।
(अनिल सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)