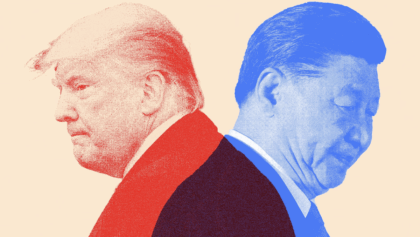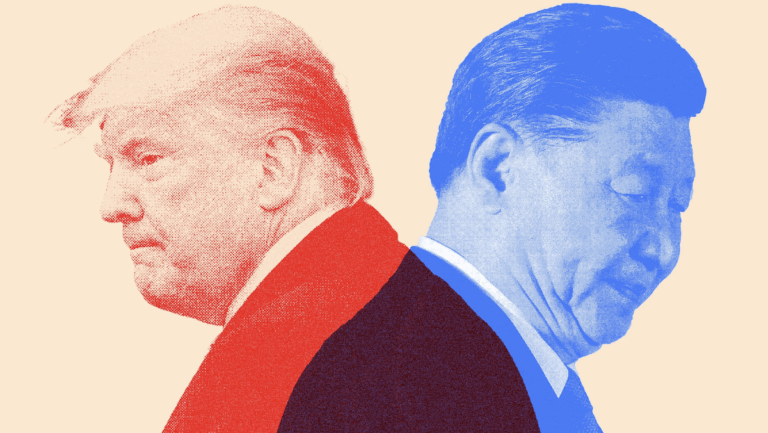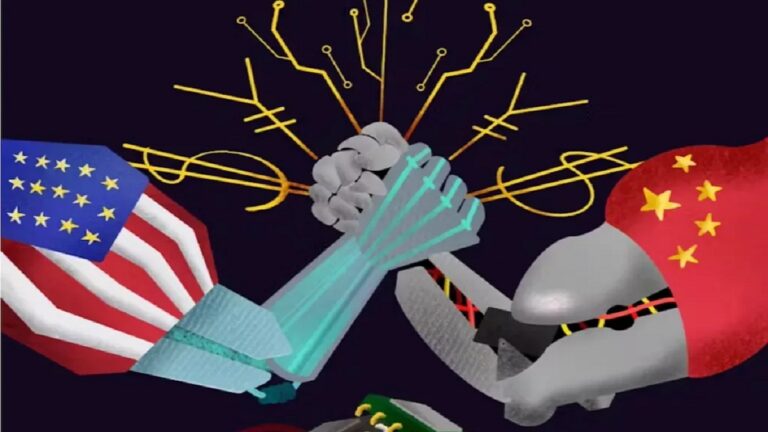(आज बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट आनंद तेलतुंबडे का जन्मदिन है। जन्मदिन के इस मौके पर भी वह भीमा-कोरेगांव मामले में इस समय जेल में हैं। और उनकी तबियत भी ठीक नहीं रह रही है। देश में तमाम बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मानवाधिकार संगठनों द्वारा की गयी उनकी रिहाई की अपील का भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके जन्मदिन के मौके पर यहां उनका एक लेख दिया जा रहा है जिसे उन्होंने एक किताब की भूमिका के तौर पर लिखा था। यह लेख मौजूदा फासीवादी निजाम के साथ-साथ बाबा साहेब डॉ. भीम राव आंबेडकर के आंदोलन और दलितों के प्रति संघ के नजरिये पर केंद्रित है। पेश है पूरा लेख-संपादक)
“यदि हिंदू राज की स्थापना सच में हो जाती है तो निस्संदेह यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चाहे हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मैत्री के लिए एक खतरा है। यह लोकतंत्र के लिए असंगत है। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को स्थापित होने से रोका जाना चाहिए।”
– बाबासाहेब आंबेडकर, थॉट्स ऑन पाकिस्तान (लेख एवं भाषण, खंड-8, पृष्ठ-358)
आज, जब हम पाते हैं कि देश के पास लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ भी था वह पूरी तरह खात्मे की कगार पर पहुंच चुका है और देश औपचारिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ बाबासाहेब आंबेडकर ने बहुत साफ-साफ और दूर-अंदेशी चेतावनी दी थी। हिंदू राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए दलितों को लुभाने की एक अहम रणनीति के बारे में अपनी बेबाक और रोचक शैली में यह किताब लिखने के उनके फैसले की मैं सराहना करता हूं। प्रस्तुत पुस्तक में वे मुख्य रूप से उन आठ किताबों पर चर्चा करते हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) दलितों के बीच वितरित करता आया है और कई सीधे-सादे दलित जिनका शिकार हो जाते हैं।
अब यह महज़ कोई संभावना या कल्पना भर नहीं रह गया है; यह हो चुका है और कुछ वर्षों से होता आ रहा है। 2014 के चुनाव से पहले, दलितों को भरमाने की यह प्रक्रिया चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई थी; ज्यादातर दलित नेता बेशर्मी से भाजपा से जा मिले या आंबेडकर का नाम जपते हुए उसके दल में शामिल हो गए। ईपीडब्ल्यू (इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली) में मेरे स्तंभों में इस प्रक्रिया को दिखाया गया था जिसे ‘थ्री दलित राम्स (राम विलास पासवान, रामदास अठावले एंड रामराज हूरिक्रिस्टेंड हिमसेल्फ़ एज़ उदितराज) प्लेइंग हनुमान्स टू बीजेपी’ आदि में पढ़ा जा सकता है।
हिंदुत्ववादी ताकतों के केंद्र की सत्ता तक पहुंचने की पहली लहर 1996 से 2004 तक चली, जिसकी रहनुमाई वाजपेयी कर रहे थे। उनकी पहली दो कोशिशें बहुत लंबी नहीं चल पाईं। वे मई 1996 में केवल 13 दिन और 1998-99 में 13 महीनों तक सत्ता में रहे। लेकिन, अंतिम अवधि में उन्होंने 1999 से 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि, वाजपेयी अपनी उदारता के लिए मशहूर थे और अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग या एनडीए) के तहत अन्य पार्टियों पर निर्भरता से उनकी स्थिति अनिश्चित बनी रही थी, फिर भी उन्होंने अपने पितृ संगठन आरएसएस के ज़हरीले दांतों की झलक दे ही दी थी।
इसके संकेत मिलने लगे थे कि ब्राह्मणवादी पार्टी के रूप में पहचानी जाने वाली बीजेपी से दूरी बरतने वाले दलित 1990 के दशक से ही उसकी जीत में भूमिका निभाने लगे थे। इसका मतलब था कि दलितों को लुभाने की प्रक्रिया में आरएसएस का प्रचार रंग ला रहा था। मंडराते खतरे को महसूस करते हुए मैंने 2005 में ‘हिंदुत्वएंडदलित्स : पर्स्पेक्टिव्सफ़ॉरअंडस्टेंडिंगकम्युनलप्रैक्सिस’ (साम्य, कोलकाता) किताब प्रकाशित की थी, जिसके पहले भाग में मैंने इस समस्या के सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में लिखा था और दूसरे भाग में दिखाया था कि विभिन्न राज्यों में यह वास्तव में किस रूप में उभरकर सामने आ रहा है।
लेकिन दूसरी लहर, जिसने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाया, बहुत ही भयावह साबित हुई। दर्जन भर वर्षों से भी अधिक समय तक गुजरात में किए जाने वाले लंबे और मासूम लोगों के खून से रंगे हुए प्रयोगों ने, जिसे सही ही हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, उन्हें देश भर में दोहराने के लिए उत्साहित किया। वैश्विक पूंजी के पूरे समर्थन के साथ, वे अगली पारी यानी 2019 के चुनाव के बाद हिंदू राष्ट्र का एक नमूना रचने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि बाबासाहेब आंबेडकर ने आगाह किया था, इसे किसी भी कीमत पर रोकने की जरूरत है।
आरएसएस, अल्पसंख्यकों के इस अनूठे देश में एक हिंदू बहुसंख्यक समुदाय निर्मित करने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। हमारा बुद्धिजीवी वर्ग बिना कुछ सोचे समझे हिंदू बहुसंख्या को लेकर एक उथली और सतही राय अपना लेता है, यह समझे बिना कि ‘हिंदू’ जैसा कुछ भी नहीं है। ‘हिंदू’ शब्द के इतिहास में जाएं तो हम पाएंगे कि बाहरी लोग सिंधु नदी के इस तरफ के बाशिंदों को हिंदू कहकर बुलाते थे, और उसमें भी यह एक अपमान सूचक नाम था।
यहां के लोगों की मूल पहचान यही रही है कि वे जातियों और उनकी उप जातियों और शायद उप-उप जातियों की एक ऊंच-नीच के क्रम वाली व्यवस्था में बंटे हुए हैं और उनकी बहुलता को ध्यान में रखें तो कोई भी बहुसंख्यक होने की हैसियत का दावा नहीं कर सकता है। अतः, एक सुसंगत हिंदू बहुसंख्या का निर्माण इन बंटे हुए जातीय समुदायों के बीच से किया जाना था, जिसे आरएसएस ने लगातार मुसलमानों को प्रभावी रूप से ‘अन्य’ और पराया बनाने की अपनी कोशिशों के जरिए हासिल किया। इसने ब्राह्मणों का संगठन होने की अपनी छवि से छुटकारा पाया, जो यह कई दशकों तक असल में था भी, और इसके लिए इसने ब्राह्मणों के वर्चस्व वाले भारत के एक काल्पनिक गौरवशाली अतीत का कीर्तिगान किया।
जब इसने एक सांस्कृतिक संगठन होने और राजनीति से दूर रहने के दावे के विपरीत जाकर एक राजनीतिक दल, भारतीय जनसंघ की शुरुआत की तो उसे ब्राह्मणों से आगे जाकर एक विशाल जनसमूह को आकर्षित करने की जरूरत पड़ी। विभाजन के दौरान उत्तर भारत में लोगों को पहुंचे सदमे और संविधान में दलितों को मुहैया कराए गए सुरक्षा उपायों के खिलाफ व्यापक असंतोष का फायदा उठाते हुए वह द्विजों के साथ-साथ अन्य लोगों को भी लुभाने में कामयाब रहे और इस तरह बीजेपी की खातिर हिंदू जनाधार जैसी एक चीज खड़ी कर पाए। लेकिन, बीजेपी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई और अस्सी के दशकों तक राजनीतिक अखाड़े के हाशिए पर ही रही।
वास्तव में, हिंदू होने की राजनीतिक पहचान औपनिवेशिक शासकों ने मुसलमानों के बरक्स बनाई थी और पहली बार उन्होंने 1909 में मॉर्ली-मिंटो सुधारों के दौरान ऐसा किया था, जब उन्होंने सत्ता को मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बांटकर राजनीति में सांप्रदायिक अलगाव के बीज बोए और मुस्लिम लीग तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रमशः उनके प्रतिनिधि दलों के रूप में लेने लगे।
गौरतलब है कि इन सुधारों पर विचार-विमर्श करते हुए, मुस्लिम लीग ने पहली बार यह संकेत दिया था कि दलित हिंदुओं का हिस्सा नहीं थे और शायद इस तरह दलितों के लिए एक अलग पहचान के बीज बोए, जिसे बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने संघर्षों द्वारा विकसित किया, जिसका नतीजा उनके द्वारा हिंदू धर्म को त्यागकर बौद्ध धर्म को अपना लेने में सामने आया।
आंबेडकर से प्राप्त इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए, दलित जातियों के बीच सबसे अधिक आबादी वाले और राजनीतिक रूप से सजग आंबेडकर विचारों के अनुयायी दलितों ने वैचारिक तौर पर अपनी गैर-हिंदू पहचान को बनाए रखा और एक दशक से भी अधिक समय तक वे ब्राह्मणवादी जातियों को अपना शत्रु मानते रहे। लेकिन, सबसे पहले 1964-65 में देश-व्यापी भूमि सत्याग्रह द्वारा पैदा किए गए डर के बाद कांग्रेस की उनको अपने में समा लेने की नीति और उसके बाद ग्रामीण भारत में उसकी नीतियों के चलते, जिन्होंने दलितों को एक वोट बैंक बना दिया, वे अपना राजनीतिक और वैचारिक संतुलन खोने लगे। फिर भी, वे गैर-हिंदू के रूप में अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए ब्राह्मणवादी जातियों का विरोध करते रहे।
आंबेडकर के नेतृत्व में चल रहे दलित आंदोलन के प्रति हिंदू महासभा और आरएसएस का रवैया काफी उदासीन था। प्रारंभ में बाबासाहेब आंबेडकर उम्मीद करते थे कि दलितों द्वारा एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लेने से हिंदू समाज के कुछ प्रगतिशील वर्गों को सुधार लाने के लिए संवेदनशील बनाया जा सकता है। लेकिन, सवर्ण हिंदुओं ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। महाड में, जब दलित चवदार तालाब के पानी पर अपना कानूनी अधिकार जताने गए, तब सवर्ण हिंदू गुण्डों ने उन पर हमला किया।
इस घटना से क्षुब्ध आंबेडकर ने महज़ नौ महीनों बाद एक सम्मेलन आयोजित करने और चवदार तालाब पर तब तक सत्याग्रह करने का फैसला किया; जो तब तक चलना था, जब तक उसे दलितों के लिए खोल न दिया जाए। लेकिन, कुछ ब्राह्मणों ने छल से सत्याग्रह के विरुद्ध कोर्ट से आज्ञापत्र हासिल किया और इस योजना को विफल कर दिया। उन्होंने दावा किया कि चवदार तालाब वास्तव में चौधरियों की निजी संपत्ति थी। इसलिए, कोई भी इसमें अनधिकृत प्रवेश नहीं कर सकता। परिणामतः, सभा को केवल मनुस्मृति की एक प्रति जलाकर समाप्त कर दिया गया और 10,000 भागीदारों को (जिन्होंने स्वयं को सत्याग्रहियों के रूप में पंजीकृत किया था) खाली हाथ लौटना पड़ा।
महाड़ में हुई निराशा के बाद, उन्होंने धर्म-परिवर्तन के बारे में बात करनी शुरू की, जिससे हिंदुओं के लिए राजनीतिक तौर पर खतरा था। लेकिन, उन पर लोगों का ध्यान नहीं गया। आंबेडकर का सत्याग्रहों पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने राजनीति की तऱफ रुख किया, जो 1909 में मॉर्ली-मिंटो सुधारों के बाद से ही सांप्रदायिक रंग लेने लगी थी। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और तभी से उनका आभामंडल कांग्रेस पर छाने लगा था; हालांकि, उन्होंने अभी तक कांग्रेस का औपचारिक नेतृत्व नहीं संभाला था। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था।
कांग्रेस ने दलितों पर पहली बार तब ध्यान दिया, जब 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासकों से अधिकतम रियायतें प्राप्त करना था। संधि के बावजूद कांग्रेस का मकसद मुस्लिम लीग पर अपनी राजनीतिक बढ़त को बनाए रखना था, इसीलिए वह दलितों के संभावित महत्व को लेकर सजग हुई थी।
कांग्रेस ने दलितों के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए और लखनऊ समझौते के लिए उनकी स्वीकृति चाही। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए; जिनमें हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और आंग्ल-भारतीयों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। आंबेडकर इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी उत्सुकता से नजर रखे हुए थे, जो साउथबरो कमीशन के आगे अपने बयान के साथ सार्वजनिक जीवन में दबे पांव कदम रख चुके थे और अपने अध्ययन में आए गतिरोध (1917-1920) के दौरान मूकनायक नाम की एक पत्रिका निकालने लगे थे।
यह गतिरोध उनका वजीफा खत्म हो जाने की वजह से आया था। लेकिन, अपने अध्ययन के लिए वित्तीय साधनों की बंदोबस्त करने के बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करने लंदन वापस चले गए और अंततः 1923 में भारत लौटे। तब तक गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाल लिया था और महात्मा के रूप में जनता के बीच अपनी पहचान बना ली थी। इस बीच आरएसएस ने इन घटनाओं के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उदासीन होकर ‘ऊंची’ जाति के हिंदुओं, मुख्यतः ब्राह्मणों को संगठित करने में लगा रहा। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के बाद, माधव सदाशिव गोलवलकर ने उसके सरसंघचालक का पदभार संभाला।
उन्होंने आरएसएस के वैचारिक विज़न को प्रकट करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें स्पष्टतः ब्राह्मणवादी अतीत के पुनरुत्थान की उसकी मंशा तथा इटली और जर्मनी के समकालीन फ़ासीवादी प्रयोगों के साथ समानता की झलक मिलती है। इस प्रकार गोलवलकर ने दलितों और आंबेडकर के नेतृत्व में चलाए गए उनके आंदोलन के साथ कोई सरोकार नहीं जताया। अगर उन्होंने कुछ किया तो बस उसे हिकारत से देखते रहे।
जब 1935 में आंबेडकर ने येवला में आयोजित एक सम्मेलन में अपने धर्म-परिवर्तन की घोषणा करते हुए यह प्रण लिया कि वे हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे, तब जाकर हिंदुत्ववादी दलों के बीच हलचल मची। आरएसएस पर तो तब भी कोई खास असर नहीं हुआ। 12-13 जनवरी 1936 के बीच पुणे में डिप्रेस्ड क्लासेज़ के एक अन्य सम्मेलन में आंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागने के अपने संकल्प को दोहराया। फ़रवरी 1936 में पूर्वी खानदेश के चांभारों ने उनके इस संकल्प का समर्थन किया।
धर्म-परिवर्तन के पीछे तर्क को समझाने तथा इस पर महारों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मई 1936 में मुंबई इलाका महार परिषद नामक एक अन्य सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके कुछ महीनों बाद, देवदासियों की सभा आयोजित की गई, जिसने आंबेडकर के धर्म-परिवर्तन के प्रस्ताव को प्रोत्साहन दिया। उनके निर्णय को दलितों द्वारा मिलता उत्साहपूर्ण समर्थन और उन दिनों उनके भाषणों में इस्लाम के प्रति झलकता आकर्षण हिंदुत्ववादी परियोजना के लिए प्रत्यक्ष खतरा था। इसके भय से हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष तथा हेडगेवार के गुरु, मुंजे ने आंबेडकर से बातचीत करते हुए यह वादा लिया कि वे इस्लाम या ईसाई धर्म जैसे किसी भी गैर-भारतीय धर्म को नहीं अपनाएंगे।
इनके स्थान पर उन्होंने सिख धर्म को अपनाने का सुझाव दिया और साथ ही धर्म-परिवर्तित दलितों को आरक्षण प्रदान करने के लिए हिंदू समर्थन का भी आश्वासन दिया। संभवतः आंबेडकर ने मुंजे के साथ किया हुआ यह समझौता स्वीकार कर लिया था। क्योंकि, उन्होंने 13 प्रतिनिधि सदस्यों को तीन महीनों के अंतराल में सिख धर्म का अध्ययन करने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भेजा था। उसके पश्चात (शायद एक बार फिर) मुंजे के नेतृत्व में ही, हिंदुत्ववादी नेताओं से उनकी भेंट हुई थी। मुंजे ने आंबेडकर को भगवा झंडा देकर ध्वज समिति के सदस्य के तौर पर उनसे अनुरोध किया था कि वे उसे राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर प्रस्तावित करें।
लेकिन, गोलवलकर के संचालन-काल में आरएसएस इन सभी गतिविधियों के प्रति उदासीन ही रहा। गोलवलकर की मृत्यु के बाद, जब मधुकर दत्तात्रेय देवरस ने सरसंघचालक का भार संभाला, तब जाकर आरएसएस हेडगेवार-गोलवलकर के विचारों के घेरे से मुक्त हुआ और उसने एक रणनीतिक विज़न अपनाया। देवरस को आरएसएस के हिंदू राष्ट्र प्रकल्प में दलितों के महत्व का एहसास हुआ। आरएसएस ने अपने ठेठ गोपनीय तरीके से बाबासाहेब आंबेडकर को अपने प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के बीच शामिल किया और 14 अप्रैल 1983 को पुणे में सामाजिक समरसता मंच (सोशल हार्मनी प्लेटफार्म) नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के उद्घाटन का संचालन करने वाले दत्तोपंत ठेंगड़ी ने उस अवसर पर कहा था- ‘समरसता के बिना समता असंभव है।’
यह आंबेडकर के विचारों के ठीक उलट था; वे समता की बात करते थे न कि समरसता की। बल्कि, उन्होंने तो जाति व्यवस्था की झूठी समरसता के खिलाफ विद्रोह किया। उनका मानना था कि समाज में समानता के बिना असली सामाजिक सद्भाव असंभव था। फिर भी, इन दोनों विचारों ने तथाकथित आंबेडकर विचारों के अनुयायियों के बीच पर्याप्त भ्रम पैदा कर दिया था। आंबेडकर का भगवाकरण करने की कोशिश करते हुए ठेंगड़ी ने उनके और हेडगेवार के बीच झूठ-मूठ की वैचारिक समानताएं गढ़ीं। उन्होंने एक व्यापक साहित्य रचा, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की कि आरएसएस ने किस प्रकार दलितों के हित के लिए काम किया, किस प्रकार आंबेडकर आरएसएस की प्रशंसा करते थे। उन्होंने किस प्रकार हिंदुओं के उत्थान में योगदान दिया, किस तरह वे मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे; आदि। इस पुस्तक में कँवल भारती ने जिन आठ किताबों का विश्लेषण किया है, वे इसी प्रचारात्मक साहित्य का हिस्सा हैं।
1920 के दशक के अंतिम वर्षों में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के बीच मुसोलिनी और उसका फ़ासीवादी शासन किस प्रकार लोकप्रिय था, इसकी पूरी कहानी एक इतालवी शोधकर्ता, मार्ज़िया कासोलारी ने लिखी है। उन्होंने मूलतः फ़ासीवाद के तत्कालीन मॉडल में अपनी ब्राह्मणवादी आकांक्षाओं को साकार होते देखा। कुछ निश्चित विशेषताएं फ़ासीवाद को परिभाषित करती हैं और यदि हम उनकी तुलना मोदी के शासन से करें तो इसके फ़ासीवादी चरित्र के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता।
एक शोधकर्ता, स्टेनली पायने ने कुछ ‘न्यूनतम फासीवादी खासियतों’ (फासिस्ट मिनिमम) की रूपरेखा तैयार की है; यानी कुछ ऐसे न्यूनतम लक्षणों का खाका तैयार किया है, जिनसे फासीवाद परिभाषित होता है। इसमें शामिल हैं- (क) फ़ासीवादी विरोध (उदारवाद का विरोध, लोकतंत्र का विरोध और साम्यवाद का विरोध); (ख) सामान्य विचारधारात्मक लक्ष्य और उद्देश्य (एक ‘परम’ संस्था के रूप में राजसत्ता, विस्तारवादी विदेश नीति, व्यक्तिगत स्वायत्तता पर अंकुश, किसी खास समूह को ‘अन्य’ के रूप में दुश्मन मानना, अत्यंत निरंकुश, निष्ठुर राष्ट्रवाद, ‘सभ्यता के संकट’ का एक सर्वनाशपूर्ण नज़रिया; (ग) शैली और संगठन की खास और आम विशेषताएं (करिश्माई नेतृत्व, युवाओं और फ़ासीवादी नेताओं के यौवन की बड़ाई, हिंसा का गुणगान, हमेशा याद दिलाने वाले प्रतीकों के माध्यम से जनभावनाओं को जगाना, तथा मर्दानगी)।
यदि हम इन कसौटियों में से प्रत्येक पर मौजूदा शासन को परखें तो आसानी से देख पाएंगे कि वह काफी हद तक इन पर खरा उतरता है। हालांकि, इस सरलीकृत रूपरेखा में शायद ऐतिहासिक ब्राह्मणवादी धूर्तता के पहलू को शामिल करना अभी बाकी है, जिसके साथ ज्यादातर दलितों का सरोकार हो सकता है।
देखिए कि किस प्रकार इस व्यवस्था ने अपने क्रूर कानून का उपयोग करते हुए चुनिंदा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, जनसाधारण का पक्ष लेने वाले वकीलों और जनवादी बुद्धिजीवियों को कैद करने के लिए भीमा-कोरेगांव स्मरणोत्सव का निर्लज्जतापूर्वक इस्तेमाल किया है, जिसके लिए इसने गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए)- जो किसी भी लोकतंत्र का विरोधाभासी है -और माओवाद के हौवे का सहारा लिया है। दलितों के भीतर कम्युनिज्म के खिलाफ जहर भरा जाता रहा है, इसलिए जब उनके अपने लोगों को सरकार माओवादी बताने लगती है तो दलित उनकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। वे यह समझ नहीं पाते कि यह उन्हें आतंकित करके चुप कराने की रणनीति है।
किसी भी आंबेडकरवादी संगठन ने सामने आकर भीमा-कोरेगांव को माओवाद से जोड़कर उसे बदनाम करने की घटना का विरोध नहीं किया। किसी को भी किसी की हिंसा की अनदेखी करने या उसे माफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, साथ ही इस बात की जरूरत है कि राजसत्ता के आचरण पर ध्यान दिया जाए। चाहे माओवाद जैसे जनांदोलन कितने भी भटके हुए क्यों न हों, उनकी तुलना में राजसत्ता अरबों गुना शक्तिशाली है और उन पर कानून के मुताबिक, आचरण करने की जिम्मेदारी आती है। लेकिन, वह पुलिस की ताकत के बल पर निर्दोष गरीबों के विरुद्ध इस तरह हिंसा पर उतर आई कि अनेक लोग इसे अपराधियों का सबसे बड़े संगठित गिरोह तक कहने पर मजबूर हो गए। राजसत्ता लोगों को आतंकित करके चुप कराने के लिए माओवाद को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करती है। दलितों को यह समझने की जरूरत है कि राजसत्ता द्वारा लोकतंत्र को इस तरह कुचलना बाबासाहेब आंबेडकर का सबसे बड़ा अपमान करना है।