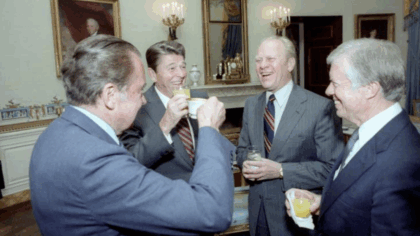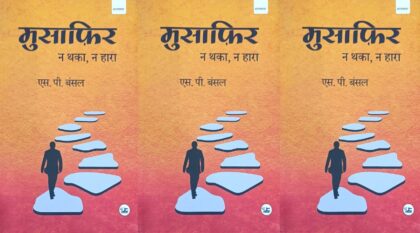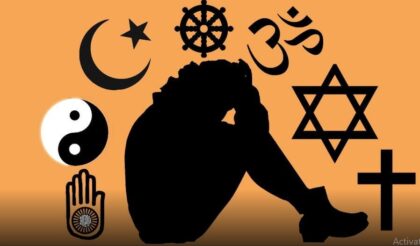हाल ही में कांग्रेस की आलोचना पर एक सज्जन इस कदर तिलमिला गए कि शालीन संवाद छोड़ अपशब्दों की शरण ले बैठे। अफसोस की बात ये है कि ये जनाब मुसलमानों के उस अशराफ वर्ग से हैं जो खुद को शिक्षित, विवेकशील और उदार मानता है। यह घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि आज के सार्वजनिक विमर्श की एक पहचान बन चुकी है। आलोचना और नफ़रत के बीच की रेखा इस कदर धुंधला दी गई है कि जैसे हर सवाल एक साजिश और हर असहमति एक गुनाह बन गई हो।
कांग्रेस पार्टी ने भारत पर सबसे लंबा शासन किया है। यह तथ्य निर्विवाद है कि देश का बुनियादी ढांचा- संस्थाएं, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र, विज्ञान, विदेश नीति और पंचायती लोकतंत्र- कांग्रेस की नीतियों और दूरदर्शिता से ही खड़ा हुआ।
आज एक “महामानव” देश को विश्वगुरु बनाने का सपना बेच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दौर में ज़रूरी विकास न हुआ होता तो आज इन्हें ड्रामा करने के लिए ज़रूरी ज़मीन नहीं मिलती।
इस काम के लिए कांग्रेस की प्रशंसा की जानी चाहिए- लेकिन प्रशंसा और अंधश्रद्धा के बीच भी एक महीन रेखा होती है, जिसे समझना ज़रूरी है।
मैं स्वयं नेहरू जी की प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का कायल हूँ। एक नव स्वतंत्र देश को विश्व की दो महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र से बचाते हुए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखना और भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाना उनके व्यक्तित्व की ताकत को दर्शाता है। वह अपने समकालीन राष्ट्राध्यक्षों के समकक्ष खड़े होते थे- न उन्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत पड़ी, न किसी “जादू की झप्पी” से काम चलाना पड़ा।
परंतु नेहरू जी भी पूर्ण नहीं थे। वे गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेताओं को काबू में नहीं कर पाए, जिनकी सांप्रदायिक सोच ने बाबरी मस्जिद विवाद का बीज बोया। नेहरू की मजबूरी रही होगी कि वे हिंदूवादी दबावों के आगे चुप रहें, परंतु यह चुप्पी आज देश को कितनी महँगी पड़ रही है, यह सब देख रहे हैं।
सावरकर पर डाक टिकट जारी करना, बाबरी मस्जिद का ताला खोलना, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय चुप्पी, और हाल में प्रियंका गांधी द्वारा राम मंदिर शिलान्यास का श्रेय लेने की कोशिश- ये सब कांग्रेस की उस रणनीति को दर्शाते हैं जिसे “सॉफ्ट हिंदुत्व” कहा जाता है। ये फैसले चाहे चुनावी विवशता के तहत लिए गए हों या विचारधारा के तहत, लेकिन जब ये ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो चुके हैं, तो इन पर सवाल उठाने से तिलमिलाना क्यों?
सवाल करने पर अक्सर जवाब मिलता है- “जाओ भाजपा जॉइन कर लो।” यह वही मानसिकता है जो किसी महिला के बुर्क़ा विरोध करने पर कहती है — “तो नंगी घूमो।” यानी दो अतियों के बीच कोई मध्य मार्ग नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तर्क नहीं। यह अतिवाद भक्ति और नफरत दोनों में समान रूप से मौजूद है।
एक मित्र ने कहा, “कांग्रेस के दौर में लिंचिंग नहीं होती थी।” यह एक अधूरा तर्क है। लिंचिंग भी एक प्रकार की भीड़ हिंसा है, जो आज संगठित रूप में हमारे सामने है। परंतु क्या हाशिमपुरा, मलियाना, मेरठ, भागलपुर और नेल्ली के नरसंहार कांग्रेस शासन में नहीं हुए थे? क्या वे मुस्लिम विरोधी हिंसा नहीं थी? क्या इन मामलों में अपराधियों को बचाया नहीं गया? और सबसे बड़ी बात- क्या कांग्रेस ने इन पर कभी माफी मांगी?
इन सवालों के जवाब देने की बजाय जब लोग भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में बह जाते हैं, तो ये साफ़ हो जाता है कि उन्हें पार्टी से मोह है, सच्चाई से नहीं। और यहीं से संवाद की जगह आरोप, और तर्क की जगह गालियाँ ले लेती हैं।
जब आलोचना का जवाब न हो, तब अक्सर कहा जाता है- “तो बताओ विकल्प क्या है?” इस प्रश्न के पीछे अक्सर एक तंज छिपा होता है- “अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो रास्ता दिखाओ!” लेकिन दरअसल विकल्प बताने और विकल्प गढ़ने में फर्क है। भारतीय मानस सदियों से “गुरु” ढूंढता आया है- एक ऐसा व्यक्ति जो चरणामृत दे और मोक्ष दिला दे। लेकिन राजनीति में समस्याओं का हल सामूहिक सोच, संवाद और जनचेतना से निकलता है, न कि किसी मसीहा से।
कोई एक पार्टी या व्यक्ति विकल्प नहीं हो सकता। विकल्प तब बनता है जब हम अपनी समस्याओं की जड़ में जाएं, उनके कारणों को समझें, उनके ऊपर चर्चा करें और सामूहिक संकल्प के साथ समाधान तलाशें। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, न ही इसमें कोई रेडीमेड फार्मूला है। लेकिन क्या कठिन रास्ता अपनाना छोड़ कर आसान जुमलों के पीछे भागते रहना ही बेहतर है?
राजनीति को सुधारने का काम किसी एक वर्ग, पार्टी या व्यक्ति का नहीं — पूरे समाज का है। आलोचना, आत्मालोचना और संवाद ही वह रास्ता है जिससे एक ज़िम्मेदार लोकतंत्र आकार लेता है। जब हम किसी पार्टी की आलोचना को व्यक्तिगत हमले मान लेते हैं, या सवाल पूछने वालों को “गद्दार”, “दलाल” या “भाजपा एजेंट” कहने लगते हैं, तो हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे होते हैं।
मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूँ और न ही मुझे किसी से नफरत है। मैं वही कहूँगा जो मुझे तर्कसंगत और सच लगेगा। जहाँ ग़लत होऊँगा, वहाँ माफ़ी माँग लूँगा, और सुधार करूँगा। ये मेरा नागरिक धर्म है।
आज ज़रूरत इस बात की है कि हम विचारधारा और भावुकता में फर्क करना सीखें। आलोचना और नफरत में, प्रशंसा और भक्ति में, असहमति और देशद्रोह में फर्क करना हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस हो या भाजपा- दोनों से सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता कभी सवालों से ऊपर नहीं होती। यदि आप वाक़ई बेहतर विकल्प चाहते हैं, तो तर्क का रास्ता अपनाइए, संवाद में उतरिए, और समाधान को मिलकर गढ़िए।
तभी इस देश की सियासत और समाज दोनों बेहतर बन पाएंगे।
(डॉ. सलमान अरशद लेखक और टिप्पणीकार हैं।)