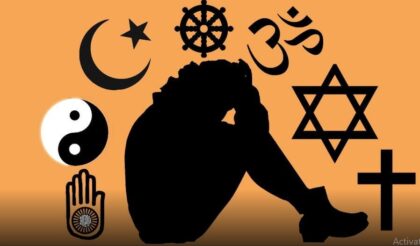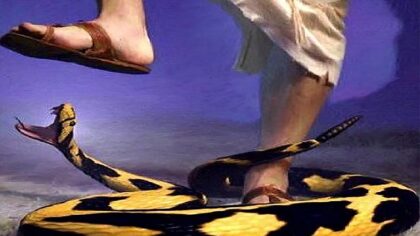जिन लोगों को लगता है यह व्यवस्था पूंजीपतियों के लिए है और इसमें बहुसंख्यक जनता न्यूनतम जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकती, वे इस व्यवस्था को बदलने के लिए लंबे समय से संघर्षशील रहे हैं। पिछले आठ सालों में परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं। सत्ता ही नहीं जनता का एक वर्ग काफी हद तक प्रतिक्रियावादी हो गया है तो बहुसंख्यक जनता का एक वर्ग या तो सीधे तौर पर उसका समर्थन करता है और अगर खुले तौर पर समर्थन नहीं भी करता तो भी उसका रुझान उसकी ओर है। अगर हालत नहीं बदले तो भविष्य कब फासीवाद की गिरफ्त में आ जाएगा कहा नहीं जा सकता।
प्रगतिशील लोगों के लिए जहां परिस्थितियां निराशाजनक हुई हैं वहीं अवसरवादियों के लिए अवसर तलाशने का मौका प्रदान किया है। लेकिन कविता कृष्णन का मामला थोड़ा अलग है। कविता कृष्णन ने 1 सितम्बर को सीपीआई माले के सभी पदों से मुक्त होने की घोषणा फेसबुक पर की। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से मुक्त होने का निवेदन किया उसमें तीन बिंदु शामिल थे।
- भारत ही नहीं विश्व में सर्वसत्तावाद व बहुसंख्यक लोकलुभावनवाद के उत्थान के विरुद्ध उदार लोकतंत्रों के बचाव के महत्व को पहचानने की ज़रूरत।
- इतनी चर्चा काफी नहीं है कि सोवियत रूस में स्तालिन की शासन प्रणाली या चीन असफल समाजवाद थे बल्कि दुनिया के सबसे ख़राब अधिनायकवाद थे ,यह चिह्नित करने की आवश्यकता।
- यह स्वीकारना कि भारत में लोकतंत्र के लिए, फासीवाद और सर्वसत्तावाद के उत्थान के विरुद्ध हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। हमें अवश्य स्वीकारना चाहिए कि पूरे विश्व के लोग, समाजवादी सर्वसत्तावादी शासन प्रणालियों सहित, समान लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के पात्र हैं।
जहां तक भारत का सवाल है तो आज के समय में वे पार्टियां जो बीजेपी के साथ हैं उन्हें छोड़ कर सभी राजनीतिक पार्टियां जिनमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं, दक्षिणपंथियों को छोड़ दें तो स्वतंत्र बुद्धिजीवी तक लोकतंत्र बचाने के महत्व को दोहरा ही रहे हैं। इसलिए पहले बिंदु का कोई मतलब नहीं है। इसे तीसरे बिंदु के साथ मिला कर देखने से स्पष्ट होता है कि वे निरंतर पूंजीवादी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कह रही हैं। बिंदु दो इसे और स्पष्ट करता है। जो पूंजीवादी बुद्धिजीवी कहते थे कि मार्क्सवाद एक यूटोपिया है और वास्तविकता में इसका क्रियान्वयन संभव नहीं है, इसका यही मतलब निकलता है।
कविता कृष्णन अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं – ” खास तरह का बदलाव हिन्दू वर्चस्ववाद चाहता है और हम एक खास तरह का बदलाव चाहते हैं। हमारा बदलाव कैसे होगा क्या होगा उसमें उसकी इमेज कैसे दिखाएं लोगों को यह भी बात आती है उस अर्जेन्सी में लगने लगा हमको बगल में भाई चीन है। कोई पूछेगा हमको तो उनके दिमाग में ये आएगा कि क्या बनाएँगे ये चीन बनाएंगे तो चीन तो दुःस्वप्न है। ”
शायद कविता कृष्णन और उनकी पार्टी ने कार्यभार लिया है कि वे बदलाव चाहते हैं और उनका बदलाव कैसा होगा यह जनता को बताना है। और उस बदलाव की इमेज लोगों को कैसे दिखाएं ? यहीं से उनके अंदर एक अंतर्विरोध पैदा हुआ है। वैसे कोई समाजवादी तो क्या बुर्जुआ बुद्धिजीवी भी नहीं मानते हैं कि चीन में समाजवाद है। वे भी देंग का प्रसिद्ध कथन कोट करते हैं कि बिल्ली चूहे पकड़ रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह काली है या भूरी।
कविता कृष्णन की विचारधारा और राजनीति लगभग स्पष्ट ही है। वे अपने आपको मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बता रही हैं। स्तालिन के समय को वे दुनिया का सबसे ख़राब अधिनायकवाद मानती हैं। उन्होंने अभी विस्तार से अपना पक्ष नहीं रखा है। पार्टी से अपने अंतर्विरोध तीन बिंदुओं के माध्यम से प्रकट किए हैं और साक्षात्कारों के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे रूस और चीन में अभी समाजवाद मानती हैं। थोड़ी सी आड़ लेकर वे यह भी प्रकट करती हैं कि चीन का दुःस्वप्न माओ से ही शुरू हो गया। लेनिन की राजनीति को वे ऑउटडेटेड और आज के समय में अप्रासंगिक मानती हैं। स्तालिन और माओ के सर्वसत्तावाद की चर्चा के बाद जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि यह थ्योरी की प्रॉब्लम है या पर्सन्स की प्रॉब्लम है। इस पर उनका स्पष्ट कहना है कि यह पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब भी वे अपने आप को मार्क्सवादी फेमिनिस्ट मानती हैं। तब इसका मतलब यही हो सकता है कि वे मार्क्सवाद में जितना फेमिनिज्म है, उसे मानती हैं।
सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं है कि उनका मार्क्सवाद या उसके सिद्धांत पर स्थापित हुई सत्ताओं से कोई अंतर्विरोध है। बस चीजों को देखने का उनका नजरिया बदल गया है। स्तालिन या माओ के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा है यह कोई नई बात नहीं है। यह सभी बातें पहले कही जा चुकी हैं। जब वर्गीय हित का मामला हो तो पूंजीवाद इतनी आसानी से तो हार नहीं मानता। वे कहती भी हैं, यह कहने से काम नहीं चलेगा यह पूंजीवादी दुष्प्रचार है। लेकिन यह सच तो है ही। अमेरिका ने कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम जैसी संस्थाएं एंटी कम्युनिस्ट लेखक तैयार करने के लिए खड़ी कीं। उनके प्रचार प्रसार पर बड़ा बजट खर्च किया। उन्होंने अपने वर्ग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काफी काम किया।
आश्चर्य की बात यह है कि कविता कृष्णन तीस साल से पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं और इस समय पोलित ब्यूरो की सदस्य थीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें अब आकर पता चला हो कि समाजवाद के नाम पर जो सत्ताएं स्थापित हुई हैं वे अब तक की सबसे खराब सर्वसत्तावादी सत्ताएं हैं। विचारधारा तो बहुत से लोग जानते हैं लेकिन पार्टियों की राजनीति व रणनीति इसी बात से तय होती है कि वे पूर्ववर्ती पार्टी नेतृत्वों व सिद्धांतों से कितने सहमत हैं और उनसे कितने अंतर्विरोध हैं।
कविता कृष्णन फेसबुक पर लिखती हैं- “स्तालिन 1917 क्रांति के पूरे नेतृत्व को फासीवादी, षड्यंत्रकारी बता दिए। खासकर ट्रॉट्स्की, कामेनेव और जिनोविएव को उन्होंने स्तालिन की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले हिटलर के एजेंट बता दिए और उनको मारने का आदेश दे दिया। ये तीन नेता यहूदी थे। जिस नस्ल के लोगों का कत्लेआम हिटलर कर रहा था।”
24 अप्रैल 1917 को सातवीं कॉन्फ्रेंस में कामेनेव ने लेनिन का विरोध किया था और मेंशेविकों की बात को दोहराया था। इसी कॉन्फ्रेंस में जिनोवियेव ने भी लेनिन का विरोध किया था। विरोध इस बात पर था कि बोल्शेविक पार्टी जिमरवाल्ड मित्र मंडल के साथ रहे या उससे नाता तोड़ ले और नया इंटरनेशनल बनाए। लेनिन ने जिनोवियेव की निंदा की और इस कार्यनीति को अवसरवादी बताया। ट्रॉटस्की की 1917 तक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी और क्रांति से कुछ समय पहले ही वह बोल्शेविक में शामिल हुए थे। क्रांति के ये प्रमुख नेतृत्वकारी क्रांति से पहले लेनिन के साथ तीखे मतभेद रखते थे।
भले उनकी सोच में अवसरवादी भटकाव थे क्रांति के बाद लेनिन की सोच रही जो अब बोल्शेविकों से सहमत हैं उन्हें लेकर क्रांति को स्थाई बनाना है। लेनिन 1924 तक जीवित रहे ये उनके नेतृत्व को चुपचाप स्वीकारते रहे। स्तालिन के सत्ता में आते ही वे अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगे। पूंजीवादी प्रोपेगंडा यही बताता है कि हिटलर की तरह स्तालिन भी यहूदियों की हत्या कर रहा था। कविता कृष्णन इसी थ्योरी को पेश कर रही हैं। अगर वे यह मानती हैं कि स्टालिन और ट्रॉटस्की के बीच जो मतभेद था वह इसलिए था कि ट्रॉटस्की यहूदी था तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि ट्रॉटस्की ने विश्व में एक साथ समाजवाद की थ्योरी को छोड़ दिया था और उनके अनुयायी आज भी इस थ्योरी को नहीं मानते हैं ?
पूंजीवादी राज्य चुपचाप तो नहीं बैठे थे। उन्होंने बाकायदा कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम जैसे संगठन और लेखक तैयार किए। जो उनके मन में आया उन्होंने लिखा। कविता कृष्णन ने जो भी सवाल उठाए हैं वे नए नहीं हैं। वे पहले से उठाए जाते रहे हैं। उन सवालों के जवाब भी दिए जाते रहे हैं। मुख्य बात नज़रिए की और पक्ष चुनने की है। कविता कृष्णन का नजरिया और पक्ष स्पष्ट है। अब माले को अपना पक्ष स्पष्ट कर देना चाहिए। एक ही घटना को अलग-अलग दृष्टिकोण से लोग कैसे देखते हैं इसका अच्छा उदहारण अन्ना लुइस स्ट्रांग हैं। वे अमेरिकी पत्रकार थीं 1920 से सोवियत रूस में पत्रकार रहीं। उनकी पुस्तक टू इयर्स ऑफ़ सोवियत लाइफ 2024 में आई जिसकी भूमिका ट्रॉटस्की ने लिखी। 1949 में वे जासूस होने के शक में गिरफ्तार हुईं और बाद में दोषमुक्त हुईं। स्टालिन के समय को उन्होंने करीब से देखा। 1956 में उनकी पुस्तक आई स्टालिन एरा। उन्होंने बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से स्टालिन के समय को इसमें दर्ज किया है।
कविता कृष्णन तीस साल से पार्टी पॉलिटिक्स से जुडी थीं और पोलित ब्यूरो की सदस्य थीं। आज जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वे पार्टी की विचारधारा और राजनीति दोनों पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि रात को उनके सपने में कृष्ण जी आए और सुबह उठकर उन्होंने ऐसा बोल दिया।
पार्टी ने अब तक इन मुद्दों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यह एक तरह से पार्टी के वैचारिक संकट को व्यक्त करता है। यह वैचारिक संकट पार्टी में हर जगह देखा जा सकता है। तीन साल पहले माले के सांस्कृतिक संगठन जसम के कार्यकारी अध्यक्ष रविभूषण ने अपने लेख में कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का निर्वहन कम्युनिस्ट ही कर रहे हैं। यह लेखक और बुद्धिजीवियों का संगठन है।
(डॉ. राम प्रकाश अनंत पेशे से चिकित्सक हैं और सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर लिखते रहते हैं। ये लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं और इसके जवाब या फिर इससे इतर कोई कुछ लिखना चाहे तो उसका स्वागत है।)