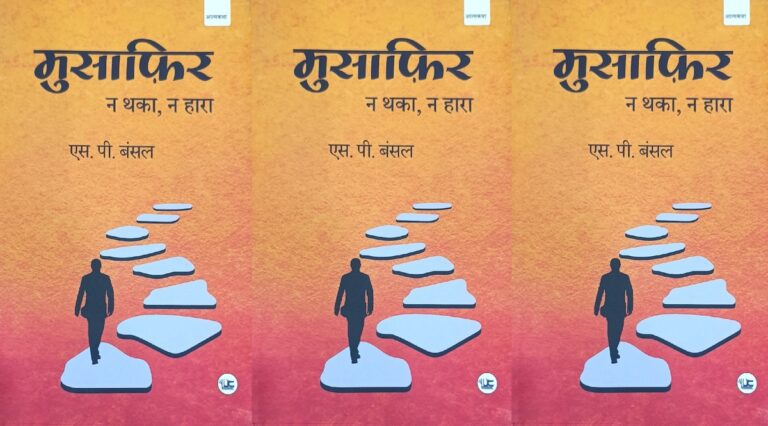करीब पच्चीस-तीस साल की पत्रकारिता से गुजरने के बाद मैंने पाया कि सन् 2014 यानी भाजपा नीत राजग के सत्तारोहण के बाद सब कुछ विध्वंसात्मक और अपमानजनक ढंग से बदल गया। सबसे पहले चैनलों ने घुटने टेके सत्ता के आगे, और फिर जल्द ही प्रिंट मीडिया ने भी सत्ता का दास होना मंजूर कर लिया। अब आठ-नौ साल बाद यह कहना मुश्किल है कि कहीं कोई रीढ़ बची भी है या नहीं। कुछ व्यक्तिगत प्रयासों को छोड़ दें तो संस्थागत पत्रकारिता (जिसमें चैनलों का जुलूस सबसे आगे है) ने इतिहास के आईने में अपनी चेहरे पर बढ़िया कालिख पोत ली है।
अखबारों से सत्ता के नीतियों की (उन नीतियों की भी जो दमनकारी हैं) आलोचना गायब है। खोजी रपटें बीते दिनों की कहानियां हैं। अपने खोजी खबरों के लिए जाना जाने वाला इंडियन एक्सप्रेस समूह भी इक्का-दुक्का रपटें देने के बाद हांफ गया है जैसे। दक्षिण भारत में मुख्यालय होने के कारण ‘द हिंदू’ अपनी थोड़ी-बहुत साख बचाए हुए है, लेकिन हिंदी के विशाल मरुभूमि में इसकी हरियाली का अंशमात्र भी प्रभाव नहीं है। सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है हिंदी के बहुप्रसारित अखबारों ने। वे हिंदी चैनलों से भी ज्यादा सांप्रदायिक और सत्तापेक्षी हो गए हैं। उनमें होड़ यह है कि कौन सत्ता के सामने कितना गिर सकता है। सत्ता के चरणों में वैसे भी बहुत जगह नहीं होती तो बहुत सारे तो नाली और नाबदानों में ही अपना सिर घुसाए हुए हैं।
पत्रकारिता का इतिहास आज नहीं तो कल लिखा जाएगा। तब यह सवाल प्रमुख होगा कि पत्रकारिता की कलम, सेल्फी जर्नलिज्म में क्यों व्यस्त थी। चैनलों का जो हाहाकारी सांप्रदायिक रूप इस समय हमारे सामने है, उसकी भी खोजबीन होगी ही होगी।
लेकिन, आइए जान लेते हैं पत्रकारिता है क्या? सबसे पहले तो हमें इस झूठ से बाहर हो जाना चाहिए कि पत्रकारिता वाकई लोकतंत्र का चौथा खंभा है। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लोकतंत्र के जिन तीन खंभों की चर्चा हम करते हैं उन्हें देखिए कि उनकी आर्थिकी शासकीय धन पर टिकी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का खर्च सरकारी धन या सामूहिक धन या जनता से अर्जित राजस्व पर टिका है। पत्रकारिता का समूचा ढांचा निजी तंत्र या जिसे कह सकते हैं स्वार्जित धन पर टिका है। पूरी पत्रकारिता निजी पूंजीपतियों के हाथ में है। यह उसी तरह का धंधा है, जैसे निजी उद्योगपति गैस या कोयला या सीमेंट का धंधा करता है। निजी पूंजीपति के पास कोई सामाजिक सरोकार नहीं होता, उसके सामने केवल अपना संपत्तिवर्द्धन ही लक्ष्य है।
यानी पत्रकारिता का धंधा करीब-करीब सत्ता से सांठगांठ करके ही चलता है। न्यायपालिका चाहे तो सत्ता के सामने सीना तानकर खड़ी हो सकती है, कार्यपालिका भी कई बार विधायिका के सामने बेमतलब झुकने से इनकार कर सकती है और सही-सलामत रह सकती है। खबरपालिका सत्ता के सामने सबसे पहले घुटने टेकती है। उसकी वजह यह है कि उसके पांव, सत्ता की मेहरबानी से टिके हैं। पत्रकारिता उतनी ही लोकतांत्रिक हो सकती है, जितनी सत्ता होगी। अगर किसी देश की सत्ता निरंकुश है तो खबरपालिका भी वैसी ही हो जाएगी।
सवाल यह है कि सत्ता खबरपालिका को भ्रष्ट करती है या खबरपालिका सत्ता को। उत्तर सीधा है कि सत्ता ही खबरपालिका को भ्रष्ट करती है। हां, यह अलग बात है कि खबरपालिका को इससे बचना चाहिए। आपातकाल में पत्रकारिता के एकमात्र संस्थान इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका ने इंदिरा गांधी से लोहा लिया। अमेरिका के अखबारों ने भी लिखा कि भारत में कोई विपक्ष नहीं बचा, सिवाय एक अखबार के। इस बात को भाजपा के नेता गर्वोक्ति के साथ पेश करते हैं।
लेकिन, यही सत्ताधारी लोग आज कोई ‘रामनाथ गोयनका’ पैदा नहीं होने देना चाहते। अगर कोई सिर उठाने की कोशिश करता है तो सत्ता उसे कुचल देती है। एनडीटीवी के प्रणव राय इसके जीते-जागते सुबूत हैं। ऐसा नहीं था कि 2014 के पहले सत्ता के दलाल नहीं होते थे, लेकिन तब वे छिप कर रहते थे। सार्वजनिक रूप से खुद सत्ता का दलाल कहे जाने पर लज्जित होते थे। वे रात के अंधरे में मत्रियों से मिलते थे। उनसे लाभ लेते थे। लेकिन अब सब कुछ दिन के उजाले में हैं। दफ्तरों में जाइए और देखिए, पत्रकार खुद चीखते हैं कि–हां, मैं..भक्त हूं, हां मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, हां..मेरी पार्टी की सरकार है। और, ज्यादातर लोग इसी मानसिकता के हैं। जो बोलते नहीं, वे भी ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं।
पत्रकारिता निरपेक्ष रूप से कुछ हो भी नहीं सकती। वह निर्वात में पैदा नहीं होती। जैसे सत्ता होती है, वैसे ही अखबारों और मीडिया हाउसों के मालिक हो जाते हैं और फिर वैसे ही पत्रकार पैदा करते हैं।
सत्ता की पूंछ पकड़कर ही पत्रकारिता जब अपना मूंछ सहलाने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि कोई भारी भूल हो चुकी है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी कहते थे कि–अभी पूरा अंधकार नहीं हुआ है। यह एक खुशफहमी है।
हकीकत यह है कि रात गहरी है। और अंधेरा कितना घना है, अगर आप इसे नहीं देख पाते तो यह आपकी आंखों का ही कमाल है। यह वक्तव्य निराश करने वाला है। लेकिन, झूठी आशा से निराशा हमेशा बेहतर होती है। और फिलहाल कहीं कोई कान्हा इस भादों के अंधियारी रात में पैदा होते नहीं दिख रहे हैं।
(राम जन्म पाठक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)