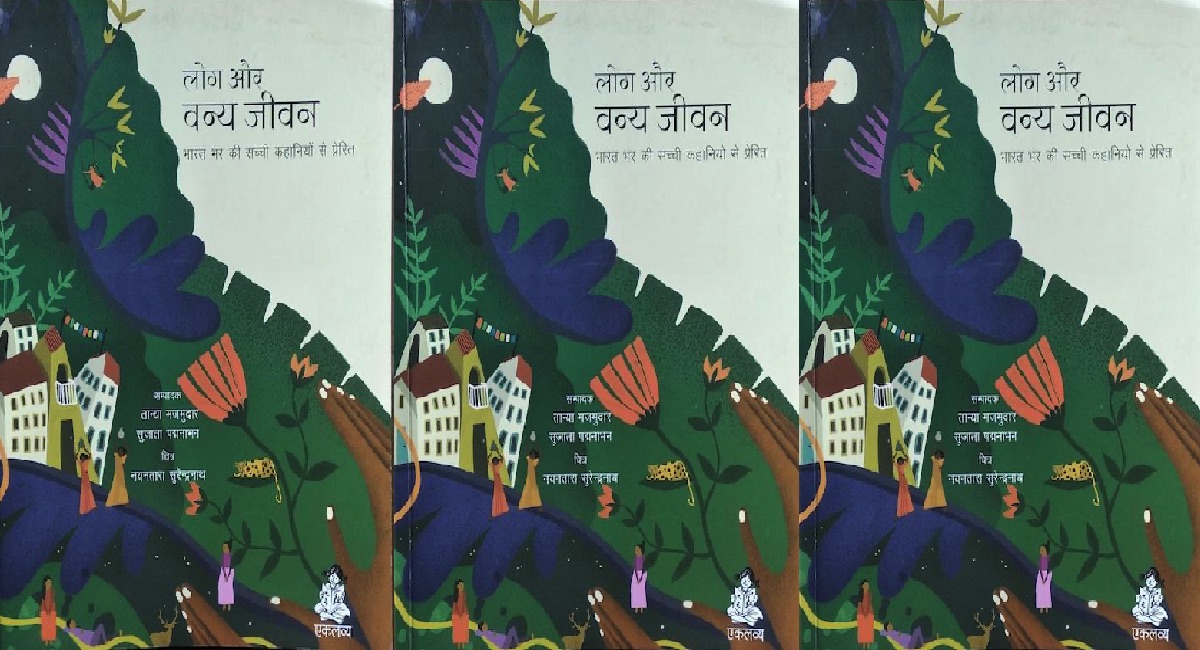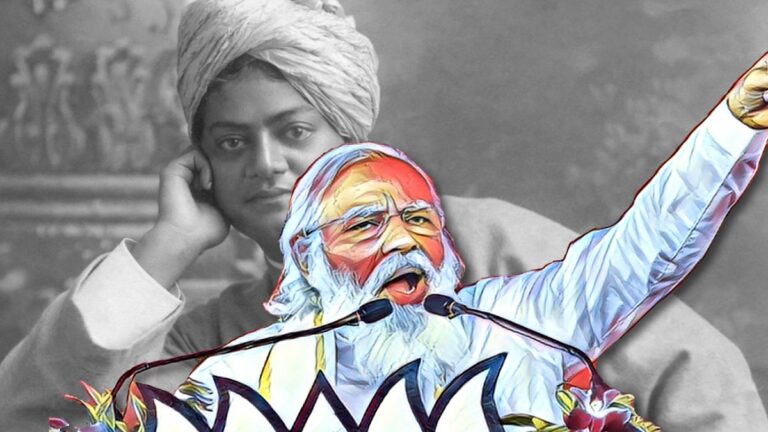मानव-केंद्रिकता। बहुत बड़ा शब्द है। इसका मतलब क्या है? यह विश्वास का द्योतक है कि मनुष्य दुनिया के केंद्र में है और हमारे ग्रह पर मौजूद किसी भी अन्य प्रजाति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस विश्वास ने हम में से कुछ लोगों को यह छूट दे दी कि वे मनुष्यों के फायदे के लिए पेड़-पौधों और जन्तुओं का शोषण करें और कल का सोचे बगैर धरती के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें।
अलबत्ता, दुनिया में और हमारे अपने देश के कई लोग हैं जो इससे ठीक उल्टा सोचते हैं। उनको लगता है कि वन्य जीवों और पेड़-पौधों का संरक्षण करना ज़रूरी है, और उन्हें अपने जीने की जगह मिलनी चाहिए। भारत में कई समुदाय हैं जिनके लिए प्रकृति के बीच जीना रोज़मर्रा की बात है, जीवन का ढंग है। कई पीढ़ियों से उन्होंने अपने आस-पास की प्रकृति और वन्य जीव की सुरक्षा की प्रथाएं बनाई हैं।
ऐसे ही कुछ लोग जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं, भारत भर की सच्ची कहानियों से प्रेरित लोग और वन्य जीवन पुस्तक देश में ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियों का संकलन है। यह पुस्तक मूल अंग्रेजी में पीपुल एंड वाइल्ड लाइफ के नाम से कल्पवृक्ष ने प्रकाशित की थी। हिन्दी में यह पुस्तक एकलव्य संस्था पाठकों के लिए लेकर आई है। इस संकलन में दस सच्ची कहानियां हैं जिसको तान्या मजूमदार और सुजाता पद्मनाभन ने संपादित किया है दोनों को ही प्रकृति से बहुत लगाव है, इस पुस्तक को चित्रों द्वारा नयनतारा सुरेंद्रनाथ ने संवारा है और हिन्दी में अनुवाद सुशील जोशी ने किया है।
तान्या मजूमदार बताती हैं कि नगालैंड के चाखेसांग कबीले का मेदोलो जब शिकार की वकालत करते हैं तो वेते सर उसको समझाते हैं कि चाखेलांग की अपनी व्यवस्थाएं हैं जिनसे वहां का जंगल समृद्ध है, उनके पानी के स्रोत हैं, यदि तुम इस संतुलन को बिगाड़ोगे…मेदोलो अपने दादा से पूछता है कि आजकल लोग कहते हैं कि शिकार करना गलत है, आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि ऐसी बातें हमारी परम्परा के खिलाफ हैं। दादा ने कहा कि पहले गांव के कुछ लोग ही शिकार करते थे, हर दिखाई देने वाली चीज को नहीं मारते थे। तुम शिकार करते हो क्योंकि तुम्हें शिकार करने में आलस आता है, ऐसा शिकार कभी हमारी परम्परा नही था, जंगलों को अपनी पांचों इन्द्रियों से देखना, जानवर जो सिखाते थे उसे सुनना- यह था चाखेसांग का तरीका।
एक कहानी में जानकी मेनन ने लिखा है कि अहमदाबाद के दक्षिण में स्थित चरोतर में मगरमच्छ लोगों के बीच रहते थे, एक बार जब एक औरत देवा तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी, तब मगरमच्छ ने उसका हाथ पकड़ लिया था, शायद उसे अपनी गल्ती का अहसास हो गया क्योंकि उसको जल्दी ही छोड़ दिया। चरोतर के लोग तो मगरमच्छ से भी अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। मगरमच्छ शोधकर्ता अनिरुद्ध वहां हर साल जाता है लेकिन कारण नहीं खोज पाया कि चरोतर के मगरमच्छ इतने सहिष्णु क्यों हैं और मनुष्य और मगरमच्छ की दोनों प्रजातियों के बीच इस विश्वास का आधार क्या था।
सुजाता पद्मनाभन ने काडू पापा! की कहानी में बताया कि कर्नाटक के नागवल्ली शासकीय हाई स्कूल के जीव विज्ञान शिक्षक अपने छात्रों को बताते हैं कि भारत में कई जन्तु हैं जिनकी संख्या कम हो रही है और जिन्हें सुरक्षा की तत्काल जरूरत है, इनमें स्लेंडर लोरिस जिसे कन्नड़ में काडू पापा कहते हैं, भी शामिल हैं। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर लोरिस की गणना की। विद्यार्थियों ने लोरिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर बनाए, लोरिस के बारे में जानकारी का एक बड़ा सा बोर्ड बनाकर स्कूल की दीवार के पास लगाया ताकि सड़क पर चलने वालों की नजर भी उस पर पड़ सके। गुंडप्पा ने कई लोरिसों को बचाया, लेकिन बहुत को नहीं भी बचा सका क्योंकि कुछ को बिजली के तारों से झटका लग जाता था किसी को सड़कों के वाहन कुचल देते थे। गुंडप्पा की बच्चों के लिए सलाह है कि अपनी कक्षा और घरों से बाहर कदम ज़रूर रखो, कौन जाने अपने आंगन में ही तुम्हें क्या कुछ मिल जाए।
गंगाधरन मेनन ने खीचन के पक्षीजन में बताया कि जब मंगोलिया के क्रेन पहली बार खीचन आए थे, तब वे सिर्फ आधा दर्जन थे और छह माह बाद वे अचानक चले गए और वो सितम्बर में फिर लौट आए, इस बार उनकी संख्या 100 के आसपास थी। मंगोलिया में जरूर रतन लालजी और सुंदरबाई की उदारता की बात फैल गई होगी, इन दोनों पति पत्नी द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा के 40 सालों में यह संख्या 15000 तक हो गई थी। जब उन दोनों पति-पत्नी ने पक्षियों को दाना खिलाना शुरू किया था, तब उनको नहीं मालूम था कि वो इतना बड़ा काम शुरू कर रहे हैं।
आशीष मजूमदार की कहानी कंटीली दुम की कथा, जानकी मेनन की असाधारण भाईचारा, तान्या मजूमदार की देवताओं के वन, वी अरुण और अकीला बालू की कछुआ चाल, तेंदुओं के साथ जीवन में निकित सुर्वे और तोडूपुय्या के राक स्टार में सुजाता पद्मनाभन ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से वन्य जीवन की विविधता और रिश्तों को बताया है और यह कि गांवों में और शहरों में भी ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जिनका वन्य जीवन की निर्जनता से गहरा रिश्ता है। प्राणियों के साथ शान्तिपूर्वक रहना, किसी खास प्रजाति या भूदृश्य की सक्रियता से रक्षा करना या प्रकृति के साथ पारम्परिक व टिकाऊ ढंग से जीने के तरीके अपनाना जैसे रिश्तों के कई रूप हैं।
(मनोज निगम की समीक्षा।)