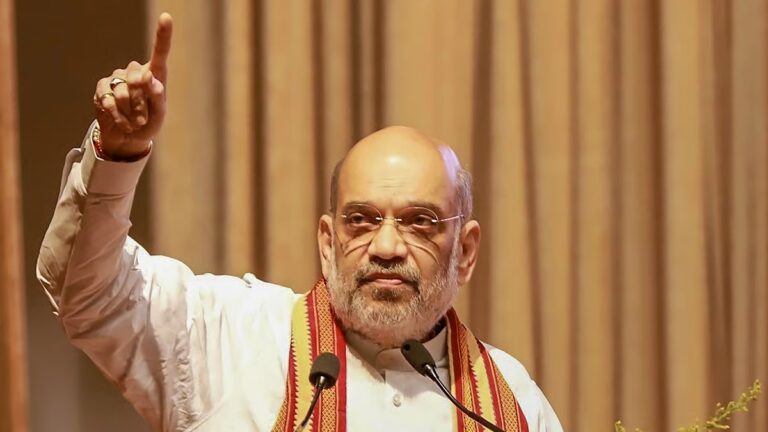एक बनता हुआ राष्ट्र अगर भारत जैसा विशाल, विविधता और इस कदर असमानता-ग्रस्त हो तो उसकी चुनौतियां बड़ी और जटिल हो जाती हैं। आज के भारत में बेरोजगारी-बेहाली-महामारी का संकट सिर्फ प्रशासकीय कारणों से नहीं है। इसके मूल में अर्थनीति और राजनीति है। यह संकट हमारी राष्ट्रीयता और सामाजिकता को लगातार बेध रहा है। ‘आपदा में अवसर’ तलाशते हमारे शासक-समूहों के सामने अपने वर्चस्व के विस्तार के सवाल हैं और अवाम के सामने अपना वजूद बचाने का! इस संकट से देश को बाहर निकालने का शासकों के पास कोई सुसंगत और मानवीय रास्ता नहीं है इसलिए उन्होंने असंगत, अमानवीय और क्रूर कारपोरेट-पक्षी सुधारों का सहारा लिया है। बीते तीन दशकों से कमोबेश सभी सत्ताधारी इसी रास्ते पर चलते रहे हैं। मौजूदा सत्ताधारियों ने सिर्फ इसमें हिंदुत्वा का पहलू जोड़ा है।
इन कथित सुधारों के स्रोत शिकागो स्कूल के नये आर्थिक चिंतन, बिल गेट्स मार्का बिजनेस-गुरुओं, डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक-आईएमएफ आदि के पूंजीवादी प्रारूपों में हैं। हिंदुत्व की वैचारिकी के साथ जोड़कर इन विनाशकारी ‘सुधारों’ का जो रसायन तैयार किया गया है, वह पूरी दुनिया में अपने ढंग का अनोखा है। लातिनी-अमेरिकी या अफ्रीकी देशों ने भी ऐसा मॉडल नहीं देखा! ऐसे दौर में शुरू हुए मौजूदा किसान आंदोलन को सिर्फ एमएसपी या मंडी (एपीएमसी) जैसे मुद्दों के आंदोलन तक सीमित करके न तो देखा जा सकता है और न समझा जा सकता है। बीते कई दशकों बाद यह पहला किसान आंदोलन है, जो किसानों की कुछ बेहद जरूरी मांगों पर केंद्रित होते हुए भी भयानक गतिरोध में फंसी राजनीति को नया रास्ता दिखाता नजर आ रहा है। क्या समाज इस रास्ते को देख और समझ पा रहा है?

इस आंदोलन में कई धाराएं और इसके कई महत्वपूर्ण आयाम हैं। वैचारिकता के अलावा इसकी सामाजिकता और भौगोलिकता के भी कई फलक हैं। इसे लेकर सवाल भी कुछ कम नहीं हैं। एक सवाल लगातार चर्चा का विषय है-क्या यह महज संयोग था कि कृषक और कृषि-विनाशक तीनों कानूनों के विरुद्ध इतना बड़ा जनांदोलन यूपी-बिहार-मध्यप्रदेश आदि से नहीं, पंजाब से शुरू हुआ? कुछ लोग कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ही एमएसपी और मंडी (एपीएमसी व्यवस्था) से जुड़े मसले ज्यादा प्रासंगिक हैं। सरकारी कानूनों का सर्वाधिक असर वहीं पड़ने वाला था। गेहूं, धान और दलहन आदि उपजाने वाले किसानों पर सबसे ज्यादा मार वहीं पड़ रही थी इसलिए किसान-प्रतिरोध की शुरुआत भी वहीं से शुरू हुई। एक हद तक इस जवाब में दम है। पर मामला सिर्फ यही नहीं है। अगर सिर्फ एमएसपी-एपीएमसी के नाम पर ही आंदोलन खड़ा हो गया तो फिर ये हालात तो सन् 2006 में बिहार में भी पैदा हुए थे। वहां क्यों नहीं कोई उल्लेखनीय आंदोलन खड़ा हो पाया? बिहार तो पहले से ही आंदोलनकारी राज्य की उपाधि धारण किये हुए है। क्या हो गया वहां?
दरअसल, पंजाब में इस तरह के आंदोलन की जमीन तैयार होने में वहां की सामाजिकता, आर्थिकी और वैचारिकता, दोनों की अहम् भूमिका नजर आती है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य ऊपरी तौर पर अपेक्षाकृत खुशहाल और समृद्ध समाज नजर आते हैं। पर वहां के समाज के समक्ष ढेर सारे यक्ष प्रश्न हैं। आर्थिकी और मानव संसाधन को लेकर समाज में गतिरोध व्याप्त है। अगर बेरोजगारी के आंकड़े देखें तो वे कई राज्यों से ज्यादा चिंताजनक हैं। इस आंदोलन के पीछे बहुत सारे कारण और कारक हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि समाज और विचार ने इसे टिकाऊ और मजबूत किया है, वरना वह आंदोलन एक-डेढ़ सप्ताह में फुस्स भी हो सकता था। आंदोलन में इतनी व्यापक भागीदारी का राज यही है। पंजाब और हरियाणा आदि के सिर्फ जाट किसान और अन्य खेतिहर समुदाय ही नहीं, दलित और उत्पीड़ित समुदाय के कामगार यानी पूरा कमेरा समाज इसमें शामिल हो गया।
सिंघु बार्डर पर गुरुओं की शिक्षाओं से जुड़े साहित्य के ही स्टाल ही नहीं हैं, वहां के स्टालों पर भगत सिंह, अवतार पाश, सुरजीत पातर, गुरुशरण सिंह, चमन लाल, अवतार सिंह बिलिंग, परगट सिंह सतौज और बलदेव सिंह सडकनामा सहित असंख्य लेखकों-कवियों की किताबें देखी जा सकती हैं। यही नहीं, चंडीगढ़ और जालंधर के अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशनों के वे स्टाल भी लगे हैं, जहां डॉ. बी आर अम्बेडकर, ज्योति बा फुले, पेरियार, आनंद तेलतुंबड़े सहित तमाम बड़े चिंतकों-लेखकों का रचना-साहित्य उपलब्ध है। इस आंदोलन ने संस्कृति के स्तर पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। पंजाब-हरियाणा के तकरीबन सारे बड़े बुद्धिजीवी, लेखक और कवि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। वे सिर्फ समर्थन में बोल और लिख ही नहीं रहे हैं, इसके लिए वे सड़क पर भी आए हैं। एक कारपोरेट-पक्षी आर्थिकी और क्रूर राजनीति की मुखालफत में पूरा समाज आंदोलन के साथ हो गया है।

यूपी-बिहार-मध्य प्रदेश जैसे हिंदी-भाषी क्षेत्रों में किसान और कमेरा वर्ग आज भी जाति-वर्ण की संकीर्णताओं में बुरी तरह बंटा हुआ है। सत्ताधारियों की तरफ से यूपी में सबसे बड़ा सवाल धर्मांतरण को बना दिया गया है। दोनों हिंदी भाषी प्रदेशों का समाज, खासतौर पर हिंदू उच्च वर्णीय बिरादरियों के सामाजिक-बौद्धिक वर्चस्व के चलते बिल्कुल अलग तरह का है। पंजाब से काफी अलग! हमने अपने बचपन में देखा था कि पूर्वी यूपी के प्रवासी श्रमिक किस तरह कलकत्ता(अब कोलकाता) या बंबई(अब मुंबई) में वामपंथी ट्रेडयूनियों से जुड़े रहकर ‘लाल-सलाम’ करते थे लेकिन जब किसी चुनाव में गांव लौटते तो दुबे जी, तिवारी जी, सिंह जी, राय साहब, यादव जी या राम जी बनकर अपनी-अपनी बिरादरी की पसंद वाले नेताओं के लिए मतदान करते थे। गांव-घर लौटकर वे अपने-अपने सामाजिक-राजनीतिक बाड़े में बंद हो जाते थे। लेकिन पंजाब का आदमी कनाडा से लौटकर भी सिंघु बार्डर पर लगी ट्राली में सो जाता है। हिंदी भाषी प्रदेशों में वर्ण-आधारित हिन्दुत्व की वैचारिकी राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हो चुकी है।
इसका एक बड़ा कारण रहा कि यूपी-बिहार में तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों या मजदूरों का वैसा बड़ा आंदोलन नहीं हो सका, जिसमें वर्ण की बाड़ेबंदी तोड़कर लोगों ने अपने पेशागत-आधारों पर बड़ी एकता कायम की हो! मध्य बिहार में हमने बार-बार देखा कि किस तरह खेत-मजदूरों या दलित व पिछड़े समुदाय के छोटे किसानों के आधार वाले आंदोलनों की मुखालफत करने के लिए ब्राह्मण-राजपूत समुदाय के गरीब और छोटे किसान भी अपनी जाति के बड़े भूस्वामियों के पाले में चले जाते थे। पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, नालंदा, नवादा और रोहतास के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की परिघटनाएं और प्रक्रियाएं बहुत आम थीं। वाम-दलीय राजनीति से प्रेरित बहुत सारे महत्वपूर्ण आंदोलन जेनुइन होते हुए भी अपने समर्थन के दायरे को बड़ा नहीं कर पाते थे। हालात आज भी वही हैं। लेकिन गुरुओं की शिक्षाओं से प्रभावित पंजाब-हरियाणा में आज वैसा परिदृश्य नहीं है। हाल के वर्षों में किसी बड़े जन-आंदोलन के बगैर महाराष्ट्र भी पहले से काफी बदला है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में तो वैसे भी यूपी-बिहार से अलग स्थितियां रही हैं।
आज के किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा, पश्चिम यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि के किसान बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। बिहार में वामपंथी दलों से जुड़े किसान संगठन भी साथ खड़े हैं। बहुत दूरी के बावजूद केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान भी सिंघु बार्डर पर डेरा डाले किसानों का अपने-अपने स्तर पर समर्थन कर रहे हैं। अपनी अंतर्वस्तु में यह सचमुच राष्ट्रीय आंदोलन है। पर दो बड़े हिंदी-भाषी प्रदेशों-यूपी-बिहार में समर्थन का भाव है पर आंदोलन नहीं है।

ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है-हिंदी-भाषी राज्यों में ऐसा समावेशी आंदोलन क्यों नहीं उठ पाता, जिसके चेहरे पर जाति-वर्ण का वैशिष्ट्य न हो! किसान आंदोलन के जनाधार और नेतृत्व को बारीकी से देखें तो इसके चरित्र के दो बहुत उल्लेखनीय आयाम हैं। जिन समाजों का आंदोलन है, उन्हीं का नेतृत्व भी है। इसके जितने प्रमुख नेता हैं, वे किसान हों, डॉक्टर हों, छात्र-युवा हों, महिलाएं हों या शिक्षक हों, सभी खेतिहर सामाजिक पृष्ठभूमि से आये हैं। आमतौर पर ये सभी सिख, दलित-सिख, हिन्दू वर्णव्यवस्था के हिसाब से शूद्र या दलित यानी गैर-सवर्ण बिरादरियों से हैं। यानी भारत में जिन्हें सामाजिक-आर्थिक बदलाव की सर्वाधिक जरूरत है, ये उन्हीं समुदायों से आये हैं। किसी आंदोलन का ऐसा नेतृत्व हाल के तीन दशकों में पहली बार उभरता दिखा है। बीते तीन दशक में सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ हिंदी भाषी राज्यों में जो नेतृत्व सामने आया था, आज वह अपनी आभा और असर, दोनों खो चुका है। उसके कथित उत्तराधिकारी राजनीतिक से ज्यादा व्यक्तिवादी, व्यवसायी या अपने परिवारों द्वारा कमायी अकूत संपत्ति के महज रखवाले भर हैं। हिंदी-भाषी सूबों की जड़ता के पीछे ऐसी कई वजहें हैं।
अचरज की बात है कि आपदा या महामारी के बीच जिस तरह कारपोरेट-पक्षी आर्थिक सुधारों को धड़ाधड़ लागू किया जा रहा है, उसे रोकने में संसदीय विपक्ष तो अक्षम है ही, हिंदी भाषी समाज के बौद्धिक प्रतिष्ठानों में भी उदास तटस्थता है। इससे एक बार फिर साबित हो रहा है कि भारत जैसे देश में आपदा में कारपोरेट के लिए अवसर निकालने की राजनीति को सिर्फ कमेरा वर्ग ही चुनौती दे सकता है। लेकिन ऐसे वर्गों के नेतृत्व का मानस हैरान करने वाला है। कल्पना कर सकते हैं कि अपने आपको मंडलवादी और अम्बेडकरवादी बताने वाले नेता और उऩके दल भी सन् 1990-91 से ही कारपोरेट-पक्षी तमाम सुधारों के पक्ष में लगातार मतदान करते आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, मायावती, रामविलास पासवान और अठावले साहब की पार्टियों के ज्यादातर फैसलों को देखें तो वे कारपोरेट-वादी नजर आते हैं। लेकिन इन दलों के समर्थक विचारशील और बौद्धिक मिजाज के लोगों ने भी कभी इन पर सवाल नहीं उठाये।
हिंदी-भाषी क्षेत्रों में वाम आंदोलन भले कमजोर हो पर प्रगतिशील और वाम सोच के लेखकों-बुद्धिजीवियों की भारी सक्रियता दिखती रही है। आश्चर्यजनक है कि इनकी सक्रियता का भी लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। हिंदी के ऐसे अनेक प्रगतिशील, सोशलिस्ट और वाम सोच के लेखकों से मेरा मिलना-जुलना होता रहा है, जिनमें अधिकांश के अपने गांव-घर के लोग या उनके पाठक उसी पार्टी या वैचारिकी के साथ खड़े हैं, जिसने इन तीन कृषि-विनाशक क़ानूनों को लागू किया है। यूपी-बिहार-मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में मौजूदा सत्ताधारी दल या पूरी हिंदुत्व-वैचारिकी का सबसे बड़ा ध्वजवाहक उच्चवर्णीय हिंदू ही है। सबाल्टर्न के उल्लेखनीय हिस्से ने भी हाल के वर्षों में उच्चवर्णीय-हिंदुओं की अगुवाई में इस वैचारिकी की पालकी उठा ली है। हिंदी के नब्बे फीसद से ज्यादा प्रगतिशील लेखक-कवि और आज के चर्चित ‘लिबरल्स’ उच्चवर्णीय समूहों से ही आते हैं। वे सब मिलजुलकर एक-दूसरे को लेखक-कवि, दार्शनिक-चिंतक और विचारक बनाने में लगे रहते हैं। उनमें कई प्रतिभाशाली और ईमानदार भी हैं। पर इससे उनका समाज कितना बदल रहा है, जिसके लिए वे सचेष्ट दिखते हैं? क्या उन्होंने कभी सोचा कि सिर्फ सबाल्टर्न समूहों की बात नहीं, उनकी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के समूहों और समाजों में भी उनका कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है?

मैं ये नहीं कह रहा कि शेष-भारत में बदलाव की बयार चल रही है। पर निश्चय ही, पंजाब, महाराष्ट्र या दक्षिणी प्रदेशों के लेखकों-बौद्धिकों और उनके समाजों के बीच ऐसी संवादहीनता तो नहीं है! आज का संदर्भ ही लें। पंजाबी प्रेस-मीडिया, मराठी प्रेस या दक्षिण के अखबारों को देखें तो किसान-आंदोलन को लेकर वे ज्यादा तथ्यपरक और वस्तुगत हैं। वे सरकार द्वारा लाये गये कानून पर सवाल उठा रहे हैं। पर हिंदी या दिल्ली के कथित राष्ट्रीय मीडिया (इंग्लिश और हिंदी के चैनल व अखबार) को देखें तो कुछेक चैनलों के कुछेक एंकरों को छोड़कर इनका पूरा कवरेज़ किसान-विरोधी, कारपोरेट-पक्षी और सत्ता-पक्षी है। इन चैनलों-अखबारों में काम करने वाले पत्रकारों-संपादकों-एंकरों का तकरीबन नब्बे फीसदी हिस्सा हिंदी-भाषी प्रदेशों के उच्च-वर्णीय हिंदू परिवारों से आता है।
इनमें बड़ी संख्या कृषि से जुड़े परिवारों के भी हैं। पर वे कारपोरेट-मीडिया की धुन आगे बढ़ाते हुए पूरी तरह किसानों के खिलाफ खड़े हैं। वहीं, पंजाब के नये-पुराने, हर स्तर के लेखक-कलाकार किसान और अवाम के साथ खड़े हैं। एक तरफ है-गुरुओं की शिक्षाओं पर आधारित सामाजिक-धार्मिकता और नैतिकता तो दूसरी तरफ है-जाति-वर्ण के कर्कश कोरस के बीच उभरती हिंदुत्वा की कट्टरता! ऐसे में अगर बौद्धिकों की जनपक्षधरता सिर्फ शब्दों तक सीमित रहे तो हिंदी-भाषी क्षेत्र कैसे बदलेगा? मुझे लगता है, इस विरोधाभास को समझे बगैर हिंदी-क्षेत्र की बौद्धिकता और वैचारिकता की सीमा को तोड़ना संभव नहीं होगा। विशाल हिंदी-क्षेत्र अगर इसी तरह जड़ता में मगन रहता है तो ‘आपदा में अवसर की तलाश’ से उभरी आज की नयी चुनौतियों का मुकाबला कैसे संभव होगा? इसी तलाश से निकला है-कारपोरेट-हिंदुत्व का खतरनाक रसायन! किसान आंदोलन इस खतरनाक रसायन से फिलहाल अकेले ही लड़ रहा है! देखिये, आगे क्या होता है?
(उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ कई किताबों के लेखक हैं। आप राज्यसभा टीवी के पूर्व कार्यकारी संपादक हैं।)