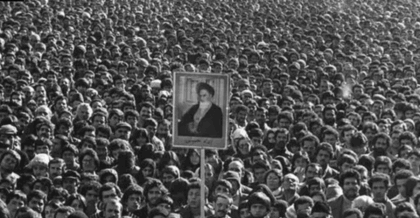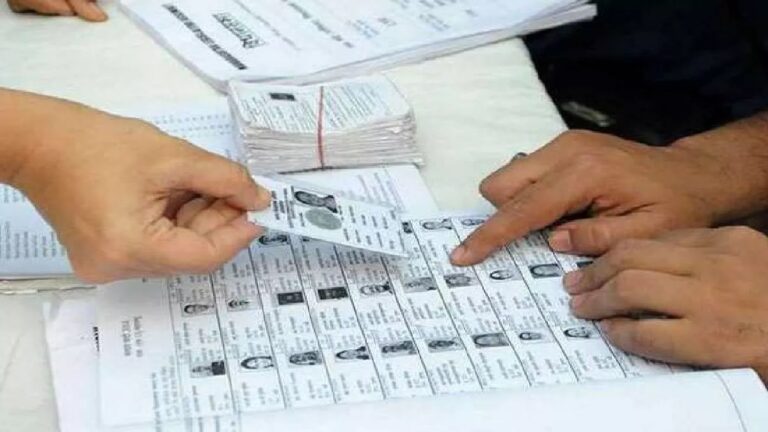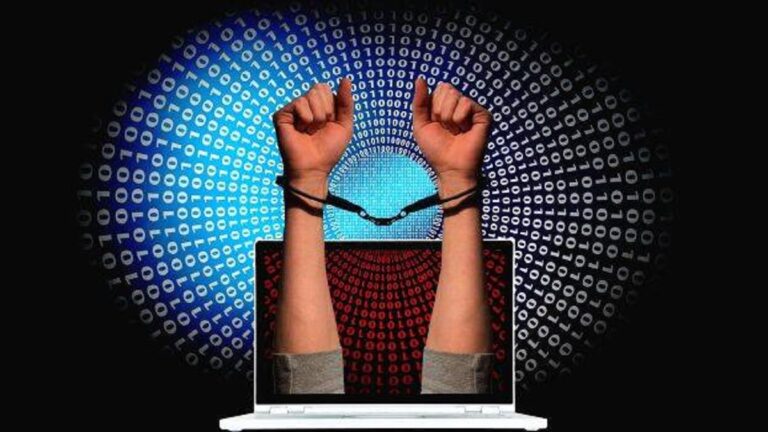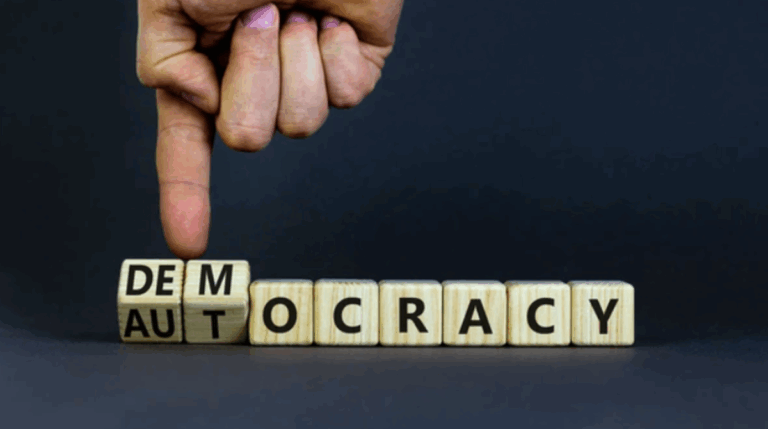खिरियाबाग, आजगमढ़। आज़मगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे बनाने के लिए 670 एकड़ जमीन अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया गया है। इसके दायरे में आठ ग्राम सभाएं आ रही हैं। इन आठ ग्राम सभाओं में से चार ग्राम सभाएं पूरी तरह उजाड़ दी जाएंगी और उन्हें कहीं और विस्थापित किया जाएगा। शेष चार ग्राम सभाएं आंशिक तौर पर प्रभावित होंगी। हालांकि भविष्य में जब रनवे के अलावा एयर पोर्ट के अन्य गतिविधियों के लिए जब जमीन ली जाएगी, तो आंशिक तौर पर प्रभावित ग्राम सभाओं के भी उनकी जद में आ जाने की पूरी संभावना है। इसके चलते इन आठों ग्राम सभाओं के लोग समान रूप से चिंतित और भयभीत दिखाई देते हैं।
जिन आठ ग्राम सभाओं के लोग अपना मकान और जमीन देने के विरोध में पिछले करीब 80 दिनों से आंदोलन चला रहे हैं, जिसका केंद्र खिरिया बाग (धरना-सभा स्थल) है। उन गांवों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का मोटी-मोटा लेखा-जोखा प्रस्तुत किए बिना इस आंदोलन के स्वरूप, इसकी ताकत और कमजोरियों और इसके भविष्य को नहीं समझा जा सकता है। ये गांव आज़मगढ़ जिला मुख्यालय से 13 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास स्थिति हैं। इन गावों से सटा एक बड़ा कस्बा कप्तानगंज है। घरेलू उड़ान के लिए बना मंदूरी हवाई अड्डे के दो किलोमीटर के दायरे में है। अगर उत्पादकता की दृष्टि से देखें, तो यहां की जमीन बहुत ही उपजाऊ और बहुफसली। यहां रवि, खरीफ और जायद तीनों फसलें होती हैं। इस समय ( रवि) पूरे इलाके में फूलों से लदे सरसों की फसल लहलहा रही है, मटर के दाने पक चुके हैं, कुछ खेतों में पकने की तरफ बढ़ रहे हैं।

आलू की फसल जगह-जगह दिखाई दे रही है। गन्ने की पेराई हो रही है, गन्ने का रस, ताजी भेली और कड़ाहे में पकते गुड़ ( राब) की महक आपको अपनी ओर खींच लेती है। लोग गन्ना चूसते हुए भी मिल जाएंगे। गेंहू करीब-करीब बोया जा चुका है, कुछ की सिंचाई भी हो रही है। अरहर में छिम्मियां निकलना शुरू हो गई हैं। इस इलाके में सब्जियां भी खूब होती हैं। यहां फलदार पेड़ भी खूब पाए जाते हैं, आम की यहां अच्छी पैदावार होती है। यहां करीब हर गांव के पास ताल है, अनगिनत पोखरे और पोखरियां हैं, यह कई सारी नदियों और मछलियों का भी इलाका है। यहां अधिकांश लोगों के पास कोई न कोई जानवर है। किसी के पास भैंस है और किसी के पास गाय। बड़े पैमाने पर यहां लोग बकरियां भी पालते हैं।
बैल करीब-करीब खत्म हो चुके हैं। खेतों की जुताई ट्रैक्टर से ही होती है, लेकिन इन गांवों में फसलों की कटाई हार्वेस्टर कंबाइंड से नहीं होती है। हाथ से कटाई होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जानवरों के चारे के लिए भूसा और पुआल की जरूरत होती। जलावन और आग तापने के लिए पुआल और गन्ने की खोइया आदि का इस्तेमाल होता है। दूसरा कारण यह है कि ज्यादातर लोगों के खेत का आकार बहुत छोटा ( औसत पर आधे एकड़ से कम) है। लोग खुद और मजदूर रखकर कटाई करवाते हैं। यह खेत के आकार और सामाजिक स्थिति दोनों पर निर्भर करता है, जैसे जिस सवर्ण के पास आधे एकड़ भी खेत है, वह खुद नहीं काटता, अधिया पर दे देता है या मजदूर से कटवाता है।

उत्पादन के साधन ( विशेषकर खेती की जमीन के मालिकाने) के आधार पर देखें तो यहां बहुलांश परिवार भूमिहीन मजदूर और गरीब किसान हैं। कुछ एक परिवारों को मध्यम किसान कहा जा सकता है। आमतौर पर भूमिहीन मजदूरों की श्रेणी में वे परिवार आते हैं, जिनके पास आधे बीघा से कम जमीन है और वे अपने जीविकोपार्जन का बड़ा हिस्सा मजदूरी करके जुटाते हैं। ये मोटी-मोटा दो तरह की मजदूरी करते हैं, इन परिवारों की महिलाएं गांव के दूसरे लोगों के खेतों या मनरेगा में काम करती हैं। अब इन्हें खेतों में साल के 2 महीने से अधिक काम नहीं मिलता है। अधिकांश पुरूष गांव से बाहर के कस्बों, आज़मगढ़ जिला मुख्यालय और अन्य जगहों पर दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, ज्यादातर अकुशल मजदूर हैं। काम मिलने में इन्हें आमतौर पर तीन सौ रूपए प्रतिदिन की मजदूरी मिल जाती है। आम तौर पर इन्हें साल के पांच-छह महीने काम मिलता है या काम कर पाते हैं। थोड़ा-बहुत जो इनके पास खेत है, उसमें कुछ दिनों काम करते हैं। अधिकांश भूमिहीन मजदूर दलित समुदाय के और अति पिछड़ी जातियों के हैं।
गरीब किसान वे हैं, जिनके पास एक एकड़ के करीब जमीन है, इनके जीविकोपार्जन का स्रोत अपने खेत में काम और शेष समय मजदूरी है। गरीब किसानों का बड़ा हिस्सा पिछड़ी जातियों का है। मध्यम किसान वे हैं, जिनके पास एक से तीन एकड़ तक जमीन है और उनकी आय का मुख्य स्रोत खेती-किसानी है और इसके साथ कुछ कारोबार करते हैं। अधिकांश मध्यम किसान पिछड़ी और सवर्ण जातियों के हैं। हालांकि खेती के मालिक सवर्णों को किस श्रेणी में रखा जाए, यह एक मुश्किल प्रश्न है, खेती की जमीन के मालिकाने के आधार पर ये मध्यम किसान में आते हैं, लेकिन आमतौर ये अपने खेतों में काम नहीं करते हैं। अपनी खेती बटाई पर दे रखें है या मजदूरों से करवाते हैं, हालांकि जुताई के मशीनीकरण के चलते इन्हें अब हरवाहे की जरूरत नहीं रह गई है। इन्हें पूंजीवादी धनी किसान भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि खेती इनके आय का मुख्य स्रोत नहीं है, इनकी आय का बड़ा स्रोत सरकारी या प्राइवेट नौकरी या कोई कारोबार है।

इनके खेतों का आकार और खेती का स्वरूप ऐसा नहीं है कि उन्हें पूंजीवादी किसान कहा जा सके। खेती के मालिकाना और अन्य सामाजिक समूहों के साथ अपने रिश्तों के संदर्भ में ये छोटे सामंत से हैं। सवर्णों के गांव में उनसे आधी खेती के मालिक पिछड़ी जातियों के किसान अपने खेतों में काम करते हैं और वही उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत है। खेती का बंटवारा पूरी तरह वर्णों और जातियों के क्रम में है। अन आठों गांवों में करीब आधी आबादी दलितों की है। सिर्फ दो या तीन परिवार ऐसे हैं, जिनके पास 20 बिस्वा ( एक बीघा) से अधिक जमीन है। अधिकांश के पास 2 बिस्वा से लेकर 10 बिस्वा ( आधा बीघा) तक जमीन है। ये मूलत: मजदूर हैं। दलितों में पासवान लोगों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, जमीन तो उनके पास भी बहुत कम है, लेकिन अन्य कारोबार में उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, क्योंकि उस इलाके के सवर्ण उन्हें उतना ‘अछूत’ नहीं मानते हैं, जितना वे अन्य दलितों को मानते हैं।
आर्थिक तौर अति पिछड़ी जातियों ( निषाद, कुम्हार और राजभर) की स्थिति भी दलितों जैसी ही है। करीब-करीब सभी के पास आधे बीघा ( 10 बिस्वा) से कम जमीन है, सिर्फ एक या दो परिवार हैं, जिनके पास एक बीघा ( 20 बिस्वा) जमीन है। प्रजापति ( कुम्हार) समुदाय भी भूमिहीनों में शामिल है, उनके भी जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत दिहाड़ी की मजदूरी है। किसी के पास भी आधे बीघा से अधिक जमीन नहीं है। सारे पैमानों पर अति पिछड़े ( निषाद, कुम्हार और राजभर आदि) भूमिहीन मजदूरों में शामिल हैं। इनका परंपरागत पेशा कब का खत्म हो चुका है और इन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार का साधन नहीं मिला। दिहाड़ी मजदूरी ही इनके पास विकल्प है।

गरीब किसानों और मध्यम किसानों की श्रेणी में यादव आते हैं, जिनकी इन आठ गांवों में पिछड़ों में सबसे अधिक आबादी है। अधिकांश यादव गरीब किसानों में शामिल हैं। इनके पास 1 बीघा से पांच बीघा ( करीब तीन एकड़) तक जमीन है। ये अपनी खेती में हाड़-तोड़ मेहनत करते दिखते हैं और करीब सबके पास दुधारू पशु ( भैंस या गाय) हैं। इनका एक हिस्सा दिहाड़ी मजदूरी भी करता है। यादवों के कुछ परिवार मध्यम किसान हैं, जो सापेक्षिक तौर पर समृद्ध हैं। अधिकांश ब्राह्मणों के पास एक एकड़ ( डेढ बीघा) से पांच एकड़ ( सात बीघा) तक जमीन है। कुछ एक परिवार हैं, जिनके पास पांच एकड़ से अधिक जमीन है। सिर्फ एक परिवार ऐसा है, जिसके पास 30 बीघा जमीन है। एक गांव में चार-पांच राय परिवार हैं, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है।
एक समान या कम या ज्यादा जमीन होने पर भी उन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या रहा है या कोई अन्य कारोबार और धंधा है। दलितों के उन परिवारों की स्थिति सापेक्षिक तौर पर बेहतर है, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है। अति पिछड़ों और पिछड़ों में कम परिवार हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी है। अधिकांश ब्राह्मण परिवार किसी न किसी नौकरी या अन्य धंधे में हैं यानी पूरी तरह खेती या पशुपालन पर निर्भर नहीं है।
सामाजिक तौर देखें तो आठों गांव दलित-पिछड़ा बहुल गांव हैं। करीब 50 प्रतिशत आबादी दलितों की है। दलित साफ तौर पर सामाजिक रूप में दो हिस्सों में बंटे हैं। सवर्णों के लिए पूरी तरह ‘अछूत’ दलित और कम ‘अछूत’ ( पासी और धोबी)। पिछड़ों के बीच आर्थिक तौर पर पिछड़े और अतिपिछड़े का बंटवारा साफ दिखता है। इन गांवों में अति पिछड़े आर्थिक तौर पर दलितों के करीब हैं, तो सामाजिक तौर पर पिछड़ों के करीब हैं। वर्णों और जातियों के आधार पर टोले अलग-अलग हैं। ब्राह्मण टोला, यादव टोला, निषाद टोला, राजभर टोला, पासी टोला और दलित टोला। लेकिन इन गांवों में विशेष बात यह दिखी कि पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के बीच खाने-पीने और साथ में उठने-बैठने का संबंध है। दलित बहुत ही सहज भाव से यादवों के यहां उठते-बैठते हैं और खाते-पीते हैं, इसी तरह बहुत सारे यादव दलितों के यहां उठते-बैठते और खाते-पीते हैं।

काफी सहज और दोस्ताना रिश्ता दिखा। अति पिछड़ों और दलितों के बीच का रिश्ता और भी सहज और बराबरी का दिखा, इसका एक बड़ा कारण दोनों का साथ-साथ दिहाड़ी मजदूरी करने गांव से जाना है। सामाजिक तौर पर सवर्णों की दुनिया अलग है, वे दलितों ( विशेषकर) को आज भी ‘अछूत’ और अपने से बहुत छोटा मानते हैं। सवर्णों और दलितों के बीच में गांव के भीतर आज भी बराबरी के आधार पर उठने-बैठने और खाने-पीने का संबंध नहीं है और न ही दोनों के बीच दोस्ताना भाव और भाईचारा है। पिछड़े और दलितों के बीच इस तरह के भाईचारे और दोस्ताना रिश्ते के बारे में पूछने पर अजय यादव ( 35 वर्ष, बी.ए.) बताते हैं कि ‘ पिछड़ों और दलितों के बीच कुछ हद तक यह रिश्ता पहले से था, लेकिन यह नई पीढ़ी के बीच और तेजी से बढ़ा है।’ पिछड़े और दलितों के बीच काफी हद तक बराबरी के इस रिश्ते का एक बड़ा कारण यह दिखता है, दोनों मेहनत-मजदूरी करके जीवन-यापन करते हैं, दोनों उत्पादक और मेहनतकश समुदाय हैं, इसके विपरीत सवर्ण शारीरिक श्रम ( विशेषकर खेती में) से भागते हैं और उसे हेय समझते हैं। किसी न किसी स्तर पर वे शारीरिक श्रम करने वालों ( दलितों-पिछड़ों) को भी हेय समझते हैं। धार्मिक-सामाजिक विचार, परंपराएं और मूल्य-मान्यताओं की भूमिका जग-जाहिर है।
इन गांवों में महिलाएं मोटी-मोटा तीन तरह की दिखाई देती हैं। एक तरफ दलित टोले कि महिलाएं हैं, जो मेहनत मजूरी करती हैं, अपने जानवरों ( गाय, बकरी, भैंस) की देखभाल करती हैं। समय-समय पर सवर्णों और कुछ यादवों के खेतों में कटिया आदि का काम करती हैं, कुछ समय मनरेगा की मजदूरी करती हैं और साथ में घरेलू काम करती हैं। जिन दलित परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर ( सरकारी नौकरी या विदेशों में मजदूरी) होने के चलते उनके घरों की नई बहुएं घरों के भीतर, पर्दे में थीं। उनसे कोई बाहरी आदमी के लिए संवाद करना मुश्किल है। ब्राह्मण टोले में अधिकांश महिलाएं घरों में पर्दे के भीतर थीं। कुछ बूढ़ी-बुजुर्ग महिलाएं बाहर दिखीं। उनसे भी बात-चीत करना मुश्किल था, वे पुरुषों से बात करने को कहती थीं। कुछ एक महिलाओं ने बात किया।

हां सवर्ण टोले की भी कुछ एक महिलाएं खेतों में साग-सरसों तोड़ते दिखीं। एक बरसीन ( जानवर का चारा) भी काट रही थीं। दलित टोले की महिलाएं पूरी तरह मुखर और आजाद दिखीं। खिरिया बाग आंदोलन की अधिकांश नेतृत्वकारी महिलाएं ( सुनीता, कुटुरी, किस्मती, फूलमती आदि) दलित हैं, यह एक बड़ा कारण लगता है। अति पिछड़ी जातियों की महिलाओं और दलित महिलाओं की स्थिति कमोवेश एक दिखी। पिछड़ी जातियों ( विशेषकर यादव) के महिलाओं की स्थिति बीच की है। वे आमतौर किसी दूसरे के खेत में काम नहीं करती हैं, न ही दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, लेकिन अपने पशुओं की देखभाल करती हैं, एक हद तक घर के अंदर और पर्दे में भी रहती हैं। उनके यहां भी 40-50 के उम्र की नीचे की महिलाओं से बात करना किसी बाहरी व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल है, हां कुछ बहुत ही गरीब परिवार हैं, उनकी स्थिति भिन्न है।

हम कह सकते हैं कि यादव परिवारों के महिलाओं की स्थिति दलित और सवर्ण महिलाओं के बीच की है। सार्वजनिक श्रम में हिस्सेदार की दृष्टि से देखें तो इन गांवों में सवर्ण महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं के बराबर है, जबकि अधिकांश दलित महिलाएं सार्वजनिक श्रम में हिस्सेदार हैं, यही स्थिति अति पिछड़ी जाति की महिलाओं की भी है। यादव परिवार के महिलाओं की स्थिति सार्वजनिक श्रम में हिस्सेदारी की दृष्टि से दलित और सवर्णों के बीच की है। चूंकि ये आठों गांव दलित-पिछड़ा बहुल गांव हैं, तो समग्रता में देखें तो ज्यादातर महिलाएं मेहनतकश ( घरेलू श्रम से इतर) हैं और यही महिलाएं खिरिया बाग आंदोलन की रीढ़ हैं। मुख्यत: यही शासन-प्रशासन और पुलिस का मुकाबला करती हैं, सच यह है कि इन्हीं के दम पर यह आंदोलन पिछले 80 दिनों से चल रहा है और टिका हुआ है।
इन आठ गांवों की राजनीतिक पक्षधरता साफ तौर पर काफी हद तक वर्ण-जाति के आधार पर बंटी हुई है। सवर्ण भाजपा के वोटर हैं, यादव पूरी ताकत के साथ सपा के साथ खड़े हैं और दलित बसपा के वोटर हैं, लेकिन दलितों में पासवानों का एक बड़ा हिस्सा हाल में भाजपा का वोटर बना है। निषाद, राजभर और कुम्हार ( प्रजापति) का झुकाव इधर भाजपा की ओर या भाजपा की सहयोगी उनकी जातियों की पार्टी की तरफ हुआ है, जैसे संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। लेकिन वोटर या राजनीतिक पक्षधरता के रूप में राजनीतिक झुकाव की अभिव्यक्ति अलग सामाजिक समूहों में अलग-अलग रूप में होती दिखी।

जहां सवर्ण भाजपा, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ और स्थानीय सांसद ( निरहुआ) की आलोचना सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं, वहीं भाजपा के दलित ( पासवान) और अन्य पिछड़े वोटर ( निषाद, राजभर और कुम्हार आदि) इतनी कट्टरता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ नहीं खड़े हैं और न ही खुद को उनके विचारों के वाहक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यादव और दलित अलग-अलग पार्टियों ( सपा-बसपा) के वोटर भले हैं, लेकिन गांव के भीतर इस राजनीतिक पक्षधरता के बावजूद कोई तीखी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं दिखाई देती है, जो दोनों को उस तरह अलगाव में डाल दे, जैसा अलगाव यादवों और सवर्णों या दलितों और सवर्णों के बीच दिखाई देता है।
उपर्युक्त आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की मुखर अभिव्यक्ति खिरिया बाग आंदोलन में दिखाई दे रही है। जहां आठों गांवों के सभी परिवार ( दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और सवर्ण) अपनी अलग-अलग आर्थिक और सामाजिक स्थिति और राजनीतिक पक्षधरता के बावजूद एक स्वर से चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के नाम इनकी एक इंच जमीन न ली जाए। कोई भी समुदाय कितना भी मुआवजा मिले अपना घर और जमीन देने को तैयार नहीं। सवर्णों ने भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में अपनी जमीनें खो कर देख लिया है, उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, भले ही कितना भी मुआवजा क्यों न मिले।

घर-दुआर, जमीन और बाग-बगीचा बचाने की चाह सबसे एकजुट होने की मांग कर रही है, लेकिन सवर्णों की सामाजिक वर्चस्व हर हालात में बचाये रखने की चाहत और भाजपा की विचारधारा और राजनीति के प्रति कट्टर प्रतिबद्धता उन्हें व्यवहारिक तौर पर संघर्ष और आंदोलन से अलग कर चुकी है या अलग रास्ता अपनाने की ओर ले गई है। पूरे आंदोलन में बहुसंख्या दलितों , अति पिछड़ों और पिछड़ों की है। दलितों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दलित महिलाओं की है, आंदोलन के कई महत्वपूर्ण चेहरे ( सुनीता, किस्मती, फूलमती, कुटुरी आदि) दलित महिलाएं हैं। जो संगठन ( घर-जमीन बचाओ संयुक्त मोर्चा) इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, उसके अध्यक्ष रामनयन यादव हैं।
इस आंदोलन में गांवों की जो कमेटियां बनी हैं, उसमें दलितों, अति पिछड़ों और पिछड़ों का वर्चस्व है। इसके दो कारण हैं- पहला इन गांवों की करीब 90 प्रतिशत आबादी इन्हीं समुदायों की है और दूसरा यही समुदाय आंदोलन में सबसे आगे बढ़कर हिस्सेदारी ले रहा है। इन सब में भी आंदोलन में सबसे अधिक संख्या और प्रभाव दलित महिलाओं का है। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के अधिकांश लोगों को अपनी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अवस्थिति के चलते आंदोलन में दलित महिलाओं की बहुलता और उनके नेतृत्व से कोई खास दिक्कत नहीं, वहीं सवर्ण दलित महिलाओं के नेतृत्व वाले किसी धरने और आंदोलन में सीधे हिस्सेदारी करने को तैयार नहीं हैं।
इसकी अभिव्यक्ति एक सवर्ण महिला ने इन शब्दों में किया- “उन्हन ( दलित महिलाएं) के बीच में हम्नन ( सवर्ण) के कैसे बैठीं।” आंदोलन से प्रत्यक्ष तौर पर सवर्णों को जो थोड़ा-बहुत जुड़ाव चल पा रहा है, वह इसलिए कि आंदोलन के शीर्ष पर पिछड़ी जातियों के नेता ( रामनयन यादव-राजीव यादव, विरेन्द्र यादव ) हैं। इसकी अभिव्यक्ति इस आंदोलन के समर्थक दो उपाध्याय लोगों के कथनों से हो जाती है- “ राजीव यादव को चलते हम कभी-कभी चले जाते हैं, नहीं तो वह सब ( दलित महिलाएं) ऐसे व्यवहार करती हैं, वहां कौन जाए।”
सवर्ण अपनी राजनीति वैचारिक-राजनीतिक अवस्थिति के चलते भी इस आंदोलन से अलग-थलग पड़ रहे हैं। जहां आंदोलन के बहुलांश हिस्सा खासकर उसका नेतृत्वकारी समूह विकास के पूरे मॉडल का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि आजमगढ़ में किसी अंतरराष्टीय हवाई अड्डे की कहीं भी कोई जरूरत नहीं। मकान-जमीन बचाओ संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष रामनयन यादव कहते हैं- “ आजमगढ़ में किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कोई जरूरत नहीं है, यह सारा कुछ किसानों की जमीन अंबानी-अडानी को सौंपने की योजना का हिस्सा है।” वे आगे कहते हैं- “कहीं भी किसी गांव के भी लोगों की घर-जमीन हवाई अड्डे के लिए लेने की कोई जरूरत नहीं है।” उनकी बात का समर्थन आंदोलन के एक बड़े समर्थक और सहयोगी राजीव यादव भी करते हैं।

वे बार-बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि “हमारा आंदोलन विकास के इस मॉडल के खिलाफ है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर आदिवासियों और मेहनतकश किसानों की जमीन ली जा रही है। हम सिर्फ इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस हर योजना का विरोध करते हैं, जिसका उद्देश्य इस देश के कार्पोरेट-घरानों और पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। हम किसानों-मजदूरों और आदिवासियों को समृद्ध बनाने वाले और सबको रोजगार देने वाले विकास के मॉडल की मांग करते हैं, न कि उनके घर-जमीन लूटने वाले विकास के मॉडल की।” आंदोलन के इस स्वर के विपरीत सवर्ण तबकों के लोगों का हवाई अड्डे से विरोध नहीं है, उनका कहना है कि उनके गांव की जगह कहीं और बने। वे इसके लिए खाली जगह सुझाते हैं, जहां लोगों के मकान बहुत ही कम हैं और जमीन खेती की हैं या कुछ हिस्सा ऊसर है। इसकी अभिव्यक्ति सुजाय उपाध्याय ने इन शब्दों में की- “ पहले से मौजूद हवाई अड्डे के उत्तर और दक्षिण दिशा में खाली जमीनें उपलब्ध हैं, तो फिर क्यों घनी आबादी वाले इलाके में एयर पोर्ट बनाया जा रहा है।”
विकास के मॉडल के अलावा सवर्णों और अन्य आंदोलनकारियों के बीच मोदी-योगी और स्थानीय सांसद के प्रति रूख को लेकर है। जहां आज़मगढ़ के सभी सपा विधायक इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा सांसद खुलकर इसके समर्थन में खड़े हैं। स्थानीय सपा विधायक नफीस अहमद ने विधान सभा में इस मुद्दे को उठाया था। आंदोलन के सवर्ण चेहरों को यह भरोसा है कि आजमगढ़ के सांसद ( निरहुआ) इन आठ गांवों को उजड़ने नहीं देंगे। ऐसा उन्होंने इन लोगों को भरोसा दिया है, जिस पर इन लोगों को पूरा विश्वास है।
सवर्ण लोग यह भी नहीं चाहते हैं कि सभा स्थल पर मोदी-योगी और निरहुआ विरोधी नारे लगाए जाएं। आंदोलन के शुरुआती नेता शशिकांत उपाध्याय कहते हैं कि “इस आंदोलन को राजनीतिक नहीं बनाना है, हमें अपने मुद्दों तक सीमित रहना चाहिए। हमें स्थानीय सांसद के आश्वासन पर भरोसा करना चाहिए।” हालांकि यह आश्वासन भाजपा सांसद ( निरहुआ) ने व्यक्तिगत स्तर पर इन लोगों को दिया है। आंदोलन के शीर्ष अगुवा के रूप में यादव ( रामनयन यादव, विरेंद्र यादव और राजीव यादव आदि) के उभरकर आने के चलते सवर्णों के एक हिस्से द्वारा कहा जा रहा है कि यह सपा का आंदोलन बन गया है, जिसका मुख्य काम भाजपा का विरोध करना है। हालांकि सवर्णों के अगुवा भी चाहते हैं कि यह धरना और आंदोलन चलता रहे। इस भावना की अभिव्यक्ति करते हुए सुजाय उपाध्याय ने कहा कि “ यह धरना ( आंदोलन) चलता रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा, तभी भाजपा के नेता ( विशेषकर सांसद ) हमारी बात सुनेंगे। इस संघर्ष के चलते ही उन्हें हमसे बात करनी पड़ी। उन पर दबाव बने रहना चाहिए।” शशिकांत उपाध्याय और सुजाय उपाध्याय कहते हैं कि “ हम भले ही आंदोलन से अलग हो गए हैं, लेकिन हम भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अलग चैनल (सांसद के माध्यम से) से।”
आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे इन आठ गांवों के सभी समुदायों के बीच एकता बनाए रखी जाए और एकजुट होकर संघर्ष किया जाए। कोई भी हिस्सा टूट कर शासन-प्रशासन के पाले में न जाए।
(खिरियाबाग से लौटकर आजाद शेखर के साथ डॉ. सिद्धार्थ की रिपोर्ट।)