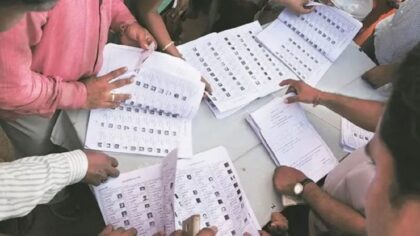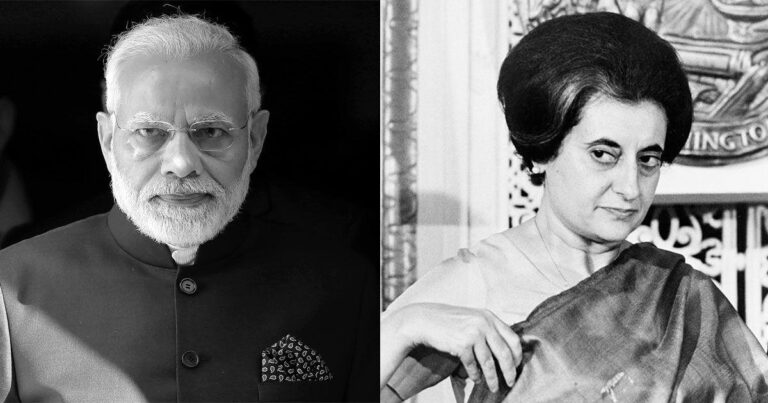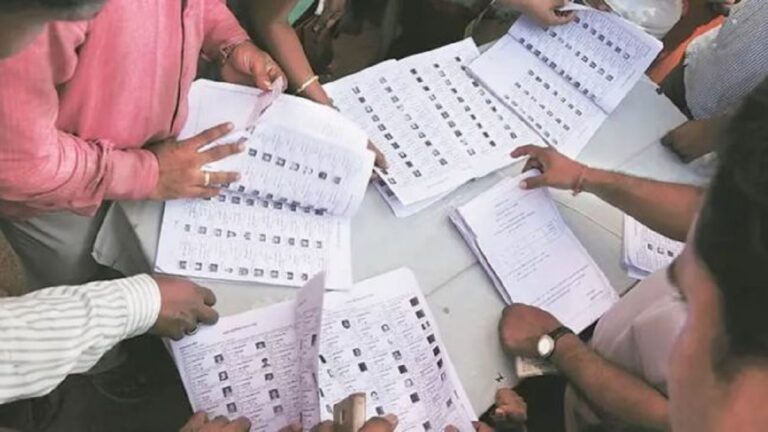2024 का आम चुनाव एक अद्भुत क्षण है। निराशा का माहौल, अधिनायकवाद की दमघोंटू छाया और सांप्रदायिकता की घिनौनी हवाएं, कम से कम फिलहाल के लिए, शांत हो गई हैं। ‘एनडीए’ गठबंधन तीसरी बार सरकार बना सकता है। यह ऐसा मील का पत्थर है जिसका उपहास नहीं किया जा सकता। लेकिन यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। खुद राजनीति के जारी रहने की संभावना ही दांव पर लगी थी। कम से कम, इन परिणामों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राधिकार के बुलबुले में सुई चुभो दिया है। उन्होंने इस पूरे चुनाव को खुद अपना मुद्दा बना लिया था। अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन, अपनी सर्वशक्तिमानता और सर्वज्ञता, और अपनी वैचारिक सनक का मुद्दा बना लिया था। फिलहाल, मोदी न तो इतिहास में शामिल किये जाने वाले अजेय योद्धा रह गये हैं, न ही लोगों के बीच में उनकी कोई देवतुल्य छवि रह गयी है। आज, लोगों ने उनके आकार को काट-छांट कर उन्हें समझा दिया है कि आप भी अन्य सबकी तरह सिर्फ एक साधारण राजनेता ही हैं।
यह चुनाव भारतीय राजनीति के, कई आयामों में, एक क्रांतिकारी पुनर्गठन का पूर्वाभास देता है। सबसे पहले, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का एक बेहतर संतुलन बहाल करता है। अगर चुनाव परिणाम ऐसे नहीं होते तो आज पूरे भारत पर भाजपा के अनियंत्रित प्रभुत्व के ग्रहण का खतरा मंडरा रहा होता। यह एक ऐसा प्रभुत्व था जिससे हर तरह की राजनीति की संभावना के समाप्त हो जाने, सभी विरोधियों को निगल लिये जाने और सारे नागरिक समाज को उपनिवेश बना लिये जाने का खतरा पैदा होने लगा था।
भारत में अब एक बार फिर से एक गहन प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रणाली बहाल हो गयी है। ऐसी राजनीति में ही नियन्त्रण और संतुलन तथा जवाबदेही संभव होती है। यह संतुलन आंशिक रूप से ‘इंडिया’ गठबंधन द्वारा संभव हुआ, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां यह गठबंधन चमत्कारिक रूप से एकजुट रहा। हलांकि भाजपा ने अपना राष्ट्रीय वोट शेयर बरकरार रखा है, लेकिन उसे सीटें नहीं मिली हैं। यदि गठबंधन एकजुट रहता है, तो यह एक स्थायी राजनीतिक ताकत बन सकता है। कम से कम, यह एक विकल्प के रूप में एक गंभीर दावेदार बन चुका है। अब ‘कोई विकल्प नहीं है’ वाली बात नहीं रही।
इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये नतीजे विपक्ष की उस अपराजेय दृढ़ता के लिए एक सम्मान-पत्र हैं, जिसने सरकार द्वारा निशाना बनाए जाने, शत्रुतापूर्ण मीडिया और गहरे संदेह से भरी हुई चुनाव प्रक्रिया के बावजूद पूरी ताकत से संघर्ष किया है।राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, उन पर संदेह करने वालों (जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं), को पूरी तरह गलत साबित करने, गठबंधन बनाने और अपने वोटों को स्थानांतरित करने में सक्षम होने के लिए मैं पूरे अंक देता हूं।
यह चुनाव, आंशिक रूप से, लोकतंत्र पर छाये हुए खतरे, संस्थानों की गरिमा में गिरावट और संविधान पर जोखिम के विषय पर लड़ा गया था। एक बेहतर संतुलित राजनीति ही संस्थानों की गरिमा को फिर से बहाल करने की संभावना भी प्रदान करती है। स्वतंत्र संस्थाएं और नागरिक समाज भी तभी अधिक सशक्त महसूस करते हैं जब वे अधिकाधिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माहौल में रहते हैं। ऐसे माहौल में ऐसी झूठी सामाजिक सहमतियां बनाना कठिन हो जाता है जो व्यक्तियों को शक्तिहीन करती हों। केवल सत्ता के एक के हाथ से दूसरे के हाथों में जाने की संभावना ही भारत के अभिजात वर्ग और स्वतंत्र संस्थाओं में व्याप्त शासकों की गुलामी की प्रवृत्ति के रास्ते की रुकावट बन जाती है।
इससे संसद को दरकिनार करना कठिन हो जाएगा। लेकिन यह तथ्य कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में आधी सीटें खो दी हैं, पार्टी के भीतर और अधिक खींचतान और मतभेद की संभावना को भी खोलता है। खुद पार्टी में अब और अधिक समझौते करने होंगे। क्या मोदी ऐसे समझौतों में सक्षम हैं, यह एक खुला प्रश्न है। यह चुनाव 1989 और 2014 के बीच के दौर की वापसी की संभावना को खोलता है, ऐसे में राजनीति को गठबंधन निर्माण और आम सहमति की आवश्यकता होगी।
यह चुनाव भारतीय राजनीति की सामाजिक कल्पना की पुनर्संरचना है। पिछले दशक में भाजपा ने भारतीय राजनीति की सामाजिक कल्पना को पुनर्संयोजित करके पारंपरिक राजनीतिक बुद्धिमत्ता को उलट दिया था। उसका पहला कदम हिंदुत्व पहचान को मजबूत करना था, जिसने आंशिक रूप से ओबीसी और दलितों को शामिल करने के लिए अपने सामाजिक आधार को व्यापक बनाने की कोशिश की। इसने अल्पसंख्यक वोट को अप्रासंगिक बनाने के लिए खंडित सामाजिक पहचानों की राजनीति का भी इस्तेमाल किया। लेकिन ये रणनीतियां अब अपना काम कर चुकी हैं। कुछ सबूत हैं कि दलित भाजपा से दूर चले गए हैं और, अधिक अविश्वसनीय रूप से, वे इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यकों को आखिरकार कांग्रेस और सपा में ठोस भरोसा मिल गया है।
उनका दूसरा काम था, हिंदी पट्टी में सांस्कृतिक आक्रोश की स्थानीय राजनीति का दोहन करके उसे एक सांस्कृतिक ब्लॉक में तब्दील करना। यह हिंदुओं के एक बड़े हिस्से को कट्टरपंथी बनाने की क्षमता के साथ जुड़ा हुआ था। अगर हम संक्षेप में कहें तो हिंदू समाज के एक तिहाई हिस्से को कट्टरपंथी बनाना संभव था। और एक कमजोर और विभाजित विपक्ष के साथ राजनीतिक लाभ के लिए अक्सर इतना ही पर्याप्त होता था। लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं को स्थायी रूप से कट्टरपंथी बनाना बेहद मुश्किल है।
प्रधानमंत्री ने लगातार आक्रोश और नफरत के मुद्दों का दोहन करते हुए यही कोशिश की। यह इतना सफल रहा था कि भाजपा के आलोचक भी हिंदी पट्टी को एक ऐसे अभेद्य ब्लॉक के रूप में देखने लगे थे, जिसके कारण देश में उत्तर-दक्षिण विभाजन एक विकल्प के रूप में उभरने लगा था। इस चुनाव की धमाकेदार कहानी ने इस मिथक को तोड़ दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा सबक यह है कि राजनीति सामाजिक पहचान से बहुत ज्यादा निर्धारित नहीं होती है, यह अब अलग-अलग तरह के विभिन्न मुद्दों के आधार पर पुनर्गठित होने के लिए तैयार है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत भी एक परेशान करने वाला मुद्दा है। हालांकि यह जनादेश आर्थिक मोर्चे पर भाजपा के प्रदर्शन को पूरी तरह से खारिज नहीं करता। इसके खिलाफ आम गुस्सा तो नहीं दिख रहा था। लेकिन यह इस तथ्य की ओर जरूर इशारा करता है कि कल्याणकारी गठबंधनों की अपनी सीमाएं होती हैं। कांग्रेस को एक दशक पहले पता चल गया था कि कल्याणकारी काम करने और बुनियादी ढांचे में लाभ हासिल करने के बाद वह फंस गई। भाजपा ने भी राजनीतिक श्रेय लेने की अधिक क्षमता के साथ, त्वरित आधार पर यही कोशिश की। लेकिन अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में बदलाव के अभाव में कल्याणकारी गठबंधन एक या दो कार्यकाल के बाद अपना प्रभाव खो देते हैं। बुनियादी ढांचे में बदलाव अभी भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से दूर है। यह स्थिति किसी भी सरकार को कमजोर बना देती है।
अंत में, इस चुनाव ने भाजपा के एक अलग पार्टी होने के मिथक को भी तोड़ दिया। इसका खुला संरचनात्मक भ्रष्टाचार, संस्थानों की शुद्धता के प्रति पूर्ण उपेक्षा, और इसके सार्वजनिक संवाद की असभ्यता ने भाजपा के लिए सद्गुणों का दावा करने की प्रधानमंत्री की इच्छा और इसके ठोस दोषों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी अभी भी लोकप्रिय हैं। लेकिन लोगों ने इस अभियान में एक नेता नहीं, बल्कि एक बेहद आत्म-प्रशंसक व्यक्ति को देखा, जो ईश्वरत्व के अपने भ्रम का कैदी है। और हमेशा की तरह, यह आत्ममुग्धता ही थी जो उनकी कमजोरी का कारण थी।
इस तरह के चुनाव में, सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों के लिए, चुनाव परिणाम और उसके नीतिगत निहितार्थ की व्याख्या करना कठिन है। एक हद तक मोदी के अभिमान को चूर कर दिया गया है। लेकिन सांप्रदायिकता और गैरक़ानूनी निगरानी समितियों की गुंडागर्दी वाले जिस सामाजिक ढांचे को उन्होंने मजबूत किया है, वह आसानी से खत्म नहीं होगा। यह स्वायत्त रूप से मजबूत होता रह सकता है। यह चुनाव इस बात का प्रमाण है कि सत्ता के संकेन्द्रण का रास्ता भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन क्या नया राजनीतिक विन्यास उस तरह की नीतिगत आम सहमति बनाने का माहौल बनाएगा, जो राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए परिस्थितियां पैदा कर सके? यह एक खुला प्रश्न है। लेकिन अभी के लिए, यह स्वतंत्रता के उस मीठे अमृत का स्वाद लेने का क्षण है जो बेहतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लाती है।
(‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से साभार)