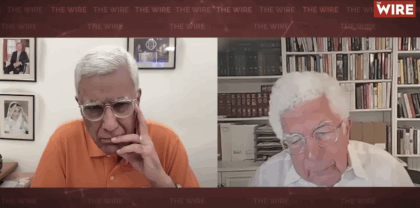आज महान कथा सम्राट और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का 143वां जन्मदिन है। महज 56 वर्ष की उम्र में 15 उपन्यास, 300 के लगभग कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल-पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के समसामयिक आलेख, सम्पादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना करने वाले प्रेमचंद पूरी दुनिया में भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह खेद का विषय है कि ऐसे महान लेखक के जन्मदिन पर हमारे यहां कोई सरकारी आयोजन नहीं हो रहा है।
गांव-गिरांव, बाग-बगीचे, खेत-खलिहान, नदी-नाले और यहां तक कि पूरी प्रकृति के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। उनकी रचनाओं में सम्पूर्ण भारतीय समाज है। उनके कथा साहित्य में माल-मवेशी, हाट-बाजार, सूद-साहूकार, चौपाल की बतकही, अभावों में जीवंतता, धूर्तता, छूआछूत, जातिवाद और पंचायत का वर्ग चरित्र, सब कुछ दिखाई देता है। वहां दलितों के अमानवीय जीवन का अक्स है। ठाकुर की हवेली है। गरीबों का शोषण है और स्त्री का दर्द और बलात्कार है। प्रेमचंद की रचनाओं में गांवों की बजबजाहट और धार्मिक पाखंडों का महावृतांत उपस्थित है। प्रेमचंद का कथा साहित्य, कुलीनतावादी हिन्दी कथा साहित्य में सर्वहारा के प्रवेश का साहित्य है। तत्कालीन समय में गांव, किसान और दलितों की दशा का जो चित्रण प्रेमचंद के कथा साहित्य में मिलता है, अन्य किसी कथाकार की कथा साहित्य में नहीं दिखता। बेचन शर्मा उग्र की एक कहानी ‘अभागा किसान’ उस समयकाल की अपवाद कही जा सकती है।
तत्कालीन समय में देश की आबादी लगभग तीस करोड़ के आसपास थी। इनमें से 90 प्रतिशत गांवों में रहने वाले किसान और मजदूर थे। उनके पास अपनी जमीनें नहीं थी। जमीनों पर सामंतों का अधिकार था। पटवारी और जमींदारों का शोषण चरम पर था। वे लगान, नजराना और बेदखली से गरीब किसान और मजदूरों का शोषण करते थे। इन शोषणों का उल्लेख साहित्य में नहीं किया जाता था। यानी देश की नब्बे प्रतिशत जनता का दर्द, हिन्दी कथा साहित्य का विषय नहीं था। प्रेमचंद ने वर्णवादी समाज व्यवस्था में अमानवीय जीवन जी रही चमरौटी में प्रवेश किया। वहां की अनुभूतियों और यथार्थ को अपने कथा साहित्य में स्थान दिया। तत्कालीन समय में ‘सरस्वती’ पत्रिका की कहानियों पर नजर दौड़ाएं तो पाते हैं कि 1900 से 1960 तक के अंकों में प्रेमचंद को छोड़कर अन्य कहानीकारों की कथा में किसान और जातिदंश की पीड़ा का पूरी तरह अभाव है जबकि प्रेमचंद के कथा साहित्य में तत्कालीन समय के सभी समाज विद्यमान हैं। वहां पंडितों का कर्मकांड है, जो गरीबों की गरदन दबाये हुए, मौज कर रहे हैं। सामंतों की ऐंठ है और हवेलियों का ऐशो-आराम है। मजदूरों का बेगार है। साहूकारों की सूदखोरी है।
प्रेमचंद के यहां किसान बेचारा और उपेक्षित है। किसान आत्महत्याओं का दर्द है। उसके साथ उसके माल-मवेशी और दूसरे जानवर, दुख-सुख के साक्षी हैं। पति-पत्नी, विधवा, बुड्ढों के संबंध हैं। कई कहानियों में स्त्री पात्रों की जीवंतता और जिजीविषा मजबूत है।
प्रेमचंद के कथा साहित्य के कई रूप-रंग हैं। प्रारंभ में वहां भाववादी और आदर्शवादी विचारों के साथ आते हैं। तंत्र-मंत्र, जादू-टोना को कहानियों में स्थान देते हैं। बाद में उन पर 1917 के रूसी बोल्शेविक क्रांति और गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। वह स्वयं गांधीजी के आह्वान पर नौकरी छोड़ देते हैं। स्वयंसेवकों की गतिविधियों को अपनी रचनाओं में शामिल करते हैं। गांधी के बाद आम्बेडकर से वैचारिक विरोध के बावजूद उनके विचारों को प्रेमचंद ग्रहण करते हैं। वह काल मार्क्स और लेनिन के विचारों को भी ग्रहण करते हैं। वह अपनी कहानियों और उपन्यासों में किसान-मजदूर विद्रोहों की आवश्यकता को दर्शाते हैं। कर्मभूमि इसका बेहतर उदाहरण कहा जा सकता है। 1920 से लेकर 1922 तक के अवध किसान विद्रोह की छाप भी प्रेमचंद की कहानियों में दिखती है। उनकी कहानियों में अंग्रेजों द्वारा भारतीय गरीबों को अपने उपनिवेशों में ले जाकर बसाने, उन गिरमिटिया मजदूरों से अमानवीय काम लेने, उनकी स्त्रियों का शोषण करने का दर्द भी रचनाओं में दिखता है।
प्रेमचंद केवल कहानीकार या उपन्यासकार के रूप में ही अपनी भूमिका नहीं निभा रहे थे अपितु वह सजग रचनाकार की तरह, तत्कालीन समय और समाज को गंभीरता से परख रहे थे । विविध प्रसंग के तीनों खंडों में प्रेमचंद के संग्रहित लेख, उनकी वैचारिकी के विकास क्रम को समझने में हमारी मदद करते हैं। वह स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होते हैं और उर्दू के प्रसिद्ध पत्र ‘जमाना’, मौलाना मुहम्मद अली के ‘हमदर्द’ और ‘इम्तयाज अली ताज’ के ‘कहकशां’, जमाना आफिस से ही निकलने वाली साप्ताहिक ‘आजाद’, चकबस्त के मासिक पत्र ‘सुबहे उम्मीद’ में नियमित वैचारिक, साहित्यिक, स्वाधीनता आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, युद्ध और शांति, हिन्दू-मुस्लिम संबंध, छुआ-छूत, किसान-मजदूर की समस्याओं, नागरिक शासन व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और युद्धों आदि पर आलेख लिखते रहे।
यही कारण है कि आज सोशल मीडिया पर प्रेमचंद के चाहने वालों की अभिव्यक्तियां भरी पड़ी हैं। अकादमियों की खामोशी को प्रेमचंद के चाहने वालों ने अपने बल पर झुठला दिया है।
हां, कुछ दलित विमर्शकारों को भी प्रेमचंद से शिकायतें हैं। दूरियां हैं। यह अजीब द्वंद्वात्मकता है कि प्रेमचंद, सत्ता को पसंद नहीं, पुरोहितों, पंडितों को पसंद नहीं, वर्णवादियों को पसंद नहीं और प्रेमचंद कुछ दलित विद्वानों को भी पसन्द नहीं।
तो फिर सवाल उठना स्वभाविक है कि प्रेमचंद को देखने का जो नजरिया हम अपना रहे हैं, कहीं वह खुद संकीर्णता का शिकार तो नहीं है? या कुल मिलाकर अंत तक आते-आते, वर्णवाद को नकारने वाले प्रेमचंद का विरोध, वर्णवाद के पक्ष में खड़ा हो जाना नहीं तो क्या है?
प्रेमचंद को कैसे पढ़ें? समझदारी के विकासक्रम में उन्हें कैसे मापे, उनकी वैचारिकी को परिमार्जित कर नया, प्रगतिशील, समसामयिक कैसे ग्रहण करें, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद ने सजग लेखक की तरह समय के साथ खुद को समझते हुए, परिमार्जित किया है। बदला है। वह एक मंत्र कहानी में झाडफूंक को स्थापित करते हैं जबकि दूसरे मंत्र कहानी में कट्टरपंथी हिन्दू विचारक का हृदयपरिवर्तन कराते हैं। राष्ट्रवादी कट्टरता की आलोचना करते हैं। आदिवासियों की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।
दलितों का यह आरोप कि प्रेमचंद वर्णवादी हैं, निःसंदेह एकहद तक सही है। यह प्रेमचंद की प्रारम्भिक अवस्था है। वह आर्यसमाजी हैं और गांधीवादी भी। वह पूना पैक्ट के समय आंबेडकर पर तीखा व्यंग्य भी करते हैं मगर बाद में वही प्रेमचंद आंबेडकर की महत्ता को स्वीकार करते हैं। वर्णवाद को नकारते हैं। वह लिखते हैं- ‘टके-पंथी पुजारी, पुरोहित और पंडे हिंदू जाति के कलंक हैं।
अगर हममें इतनी शक्ति होती, तो हम अपना सारा जीवन हिंदू-जाति के पुरोहितों, पुजारियों, पंडों और धर्मोपजीवी कीटाणुओं से मुक्त कराने में अर्पण कर देते।
हिन्दू-जाति का सबसे घृणित कोढ़, सबसे लज्जाजनक कलंक यही टके-पंथी दल है, जो एक विशाल जोंक की भांति उसका खून चूस रहा है, और हमारी राष्ट्रीयता के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है।
पुरोहितों के प्रभुत्व के दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं और समाज और राष्ट्र की भलाई इसी में है कि जाति से यह भेद-भाव, यह एकांगी प्रभुत्व, यह खून चूसने की प्रवृत्ति मिटाई जाये, क्योंकि जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्ण- व्यवस्था, ऊंच-नीच के भेद और धार्मिक पाखंड की जड़ खोदना है ।….
और हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें तो जन्मगत वर्णों की गंध तक न होगी, वह हमारे श्रमिकों और किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न कायस्थ, न क्षत्रिय । उसमें सभी भारतवासी होंगे, सभी ब्राह्मण होंगे, या सभी हरिजन होंगे (क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं ? 8 जनवरी, 1934)।
आर्यसमाजी प्रेमचंद आगे चलकर समाजवादी विचारधारा को स्वीकारते हैं। रंगभूमि उपन्यास में दलित सूरदास के संघर्षों और बलिदान को मजबूती से रखते हैं। एक दलित की जमीन हड़पकर, उसकी मूर्ति बनाकर पूजने वालों के चरित्र को नंगा करते हैं। कर्मभूमि में बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित दिखते हैं। मजदूर क्रांति की वकालत करते हैं। विध्वंष कहानी की भुनगी हो या बूढ़ी काकी का विद्रोह या बाबाजी का भोग, जहां वह पाखंडी पुरोहितों का प्रतिकार करते हैं। गोदान का मातादीन-सिलिया प्रसंग, एक साहसिक संकल्प के साथ खत्म होता है जब दलित समुदाय मातादीन के मुंह में हड्डी घुसेड़कर उसे दलित बना लेता है। प्रेमचंद के प्रति नफरत की हद तक विचार व्यक्त करने वाले दलित विचारक आज के समय में ऐसा कुछ कर सकते हैं?
प्रेमचंद का हस्तक्षेप वर्णवादी विचारों से होते हुए, दलित पक्षधरता तक जाता है। कफन कहानी की कुछ सीमाएं हो सकती हैं। वह उनकी आखिरी कहानियों में से एक है। तब प्रेमचंद का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उस कहानी को अगर वह दुबारा पढ़े होते तो जरूर सुधार किए होते। उस कहानी को लेकर आलोचना उतनी बुरी नहीं कही जा सकती जितनी कि उनसे घृणा करना ।
प्रेमचंद सूअरबाड़े में नहीं सोए थे और न अछूत दंश को खुद सहे थे मगर उनकी दृष्टिजीवी रचनात्मकता का अपना योगदान है। तब और भी, जब उस समय कोई अन्य लेखक दलित प्रसंगों से दूर-दूर नाता न रख रहा था। जब स्त्री और दलित विमर्श का दौर न था, प्रेमचंद तब स्त्री और दलित विमर्श को हिन्दी साहित्य के केन्द्र में ला चुके थे। प्रेमचंद को उनके समय और उनकी जमीन से, उनके योगदान की व्यापकता को समझने और सलाम करने की जरूरत है। सोचने की जरूरत है कि वह न होते तो हिन्दी साहित्य का क्या स्वरूप होता? वह कहां सड़-गल रहा होता और कितना बजबजा रहा होता?
(सुभाष चन्द्र कुशवाहा वरिष्ठ साहित्यकार और इतिहासकार हैं।)