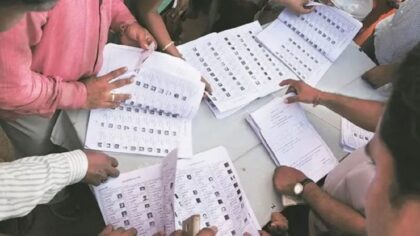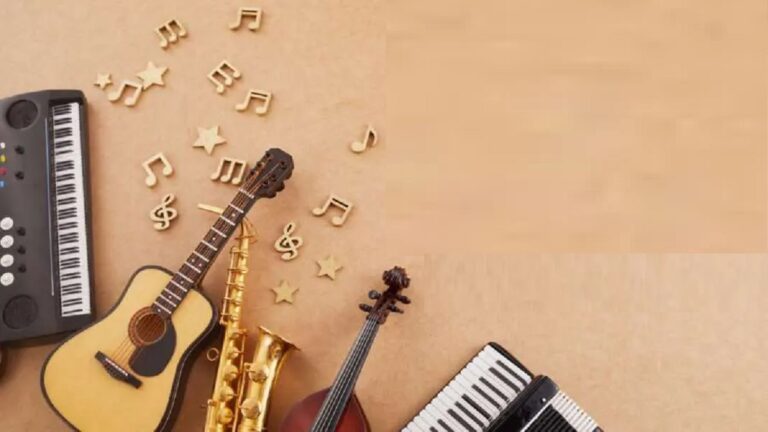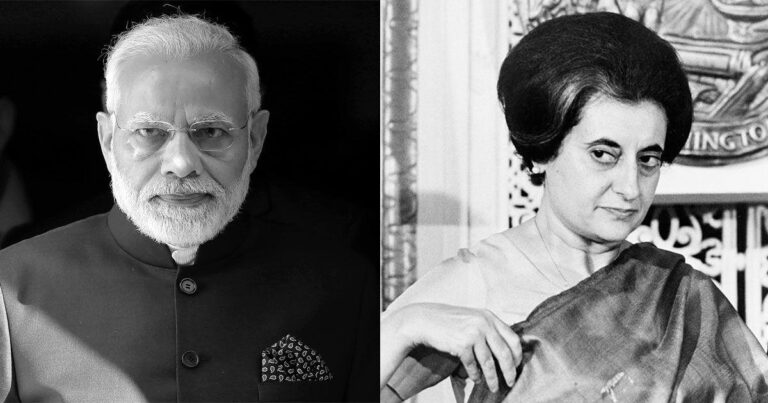जितना पुराना धर्म है, उससे कहीं ज़्यादा पुराना शायद अंधविश्वास है। शुरुआत में हर धर्म सही मायने में उस समय के समाज में फैले अंधविश्वास के ख़िलाफ़ एक चेतनापूर्ण आंदोलन ही था। लेकिन, जैसा कि हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है कि किसी भी आंदोलन के मूल्य सार्वकालिक या सर्वजनीन नहीं होते, उसे पूर्णता प्रदान करने के लिए आंदोलनों की कभी न ख़त्म होने वाली एक श्रृंखला ज़रूरी होती है। यह श्रृंखला जहां ख़त्म हो जाती है, वहां के समाज में एक ठहराव आ जाता है। यह ठहराव कई सामाजिक और सांस्कृतिक समस्यायें पैदा करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अंधविश्वास, धर्म और इन दोनों के जटिल सम्बन्धों को जानने की कोशिश करें।
अंधविश्वास और धर्म का संबंध मानव इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। जहां धर्म एक सुव्यवस्थित आस्था प्रणाली, नैतिक दिशा और जीवन के उद्देश्य को प्रदान करता है, वहीं अंधविश्वास तर्कहीन या बिना किसी ठोस आधार के मान्यताओं से उत्पन्न होता है, जो अक्सर भय, अनिश्चितता या सांस्कृतिक परंपराओं से उपजता है। कई विद्वान और विचारक इस पर बहस करते रहे हैं कि क्या अंधविश्वास धर्म का ही एक उप-उत्पाद (byproduct) है या यह एक स्वतंत्र घटना है।
वहीं आध्यात्मिकता (Spirituality) को एक अलग, लेकिन संबंधित अवधारणा के रूप में देखा जाता है। यह स्वयं की जागरूकता, स्वयं की खोज और आंतरिक शांति के व्यक्तिगत अनुभवों से संबंधित है, जो अक्सर संगठित धर्म की सीमाओं से परे होते हैं। इस लेख में हम अंधविश्वास, धर्म और आध्यात्मिकता के बीच संबंध की पड़ताल करेंगे, उनके उद्गम, परस्पर संबंध और उनके द्वारा मानव समझ को प्रभावित करने के तरीकों को विश्लेषित करेंगे।
अंधविश्वास का बोध
अंधविश्वास को उन मान्यताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी भी तार्किक या वैज्ञानिक समझ पर आधारित नहीं होतीं और अलौकिक शक्तियों, शकुन-अपशकुन या विशेष रीति-रिवाजों में विश्वास पर निर्भर करती हैं। यह अक्सर अनिश्चित परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता से उत्पन्न होता है और विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जैसे कि भाग्यशाली ताबीज रखना, लकड़ी छूना या अशुभ घटनाओं से बचने के लिए विशेष दिनचर्या का पालन करना, काली बिल्ली का रास्ता काटना, टूटा हुआ शीशा देखना या कुछ विशेष संख्याओं को अशुभ मानना, प्राकृतिक घटनाओं जैसे ग्रहण या धूमकेतु को किसी शुभ या अशुभ संकेत के रूप में देखना।
अंधविश्वास हर संस्कृति और समय में मौजूद रहा है और समाज में बदलाव के हिसाब से बदलता रहा है। यह कभी-कभी हानिरहित हो सकता है, लेकिन यह अनुचित भय, भेदभाव या हानिकारक प्रथाओं को भी जन्म दे सकता है।
अंधविश्वास की उत्पत्ति
अंधविश्वास मानव मनोविज्ञान और अस्तित्वगत प्रवृत्तियों में गहराई से निहित है। प्राचीन मनुष्यों को प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और जंगली जानवरों का लगातार सामना करना पड़ता था। वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में उन्होंने इन घटनाओं को अदृश्य शक्तियों या दैवीय हस्तक्षेप से जोड़ा। इस विश्वास ने उन्हें अनुष्ठानों और निषेधों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे इन शक्तियों को शांत कर सकें और सुरक्षा प्राप्त कर सकें।
मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि मानव मस्तिष्क पैटर्न को पहचानने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त होता है, भले ही वे मौजूद हों या न हों। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह (cognitive bias), जिसे एपोफेनिया (Apophenia) कहा जाता है, इसके कारण लोग असंबंधित घटनाओं के बीच कारण-परिणाम संबंध जोड़ लेते हैं, जिससे अंधविश्वास मज़बूत होता है।
धर्म की बनावट, अर्थ और परंपरा
धर्म एक ऐसी आस्था प्रणाली है, जो दिव्य या पवित्र तत्वों के इर्द-गिर्द केंद्रित होती है। इसमें आमतौर पर ग्रंथ, अनुष्ठान, सामूहिक पूजा और नैतिक शिक्षायें शामिल होती हैं। अंधविश्वास के विपरीत, धर्म जीवन, पीड़ा और मृत्यु के बाद के अस्तित्व की संरचित व्याख्या प्रदान करता है।
धर्म और अंधविश्वास में अंतर
हालांकि धर्म और अंधविश्वास दोनों ही अलौकिकता पर विश्वास करते हैं, फिर भी उनमें महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। हालांकि,धर्म और अंधविश्वास भले ही अलग हों, लेकिन वे अक्सर एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। कई धार्मिक परंपरायें अलौकिक मान्यताओं को समाहित करती हैं, जो बाहरी दृष्टिकोण से अंधविश्वास लग सकती हैं। कुछ मामलों में धार्मिक सिद्धांत स्वयं अंधविश्वासी प्रथाओं को जन्म दे सकते हैं।
धार्मिक ढांचे के भीतर अंधविश्वास के कई उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे कि यह मानना कि किसी विशेष वस्तु को छूने या पवित्र जल पीने से चमत्कारी रूप से उपचार हो सकता है, धार्मिक ग्रंथों से भविष्यवाणी निकालना या दिव्य संकेतों की तलाश करना, कुछ विशेष खाद्य पदार्थों, संख्याओं या कार्यों से परहेज करना, प्राकृतिक आपदाओं या व्यक्तिगत दुर्भाग्य को ईश्वरीय क्रोध का परिणाम मानना।
आध्यात्मिकता
आध्यात्मिकता को अक्सर स्वयं की तलाश, स्वयं की जागृति और ब्रह्मांड या दिव्य से जुड़ने की व्यक्तिगत यात्रा के रूप में देखा जाता है। संगठित धर्म के विपरीत, यह संस्थानों, नियमों या अनुष्ठानों पर बिल्कुल निर्भर नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों और आंतरिक परिवर्तन पर केंद्रित होती है। आध्यात्मिकता लोगों को धर्म के पारंपरिक ढांचे से बाहर आस्था की खोज करने और अंधविश्वास से बचने में मदद करती है। शिक्षा अंधविश्वास को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैज्ञानिक साक्षरता, तार्किक सोच और ऐतिहासिक समझ को बढ़ावा देकर समाज लोगों को धर्म और अंधविश्वास के बीच अंतर को समझने में मदद कर सकता है।
अंधविश्वास का मिटना ज़रूरी इसलिए माना जाता है ,क्योंकि सदियों से समाज में गहरे तक फैले हुए ये अंधविश्वास लोगों के रोजमर्रा के जीवन, फैसलों और यहां तक कि शासन पर भी असर डालते रहे हैं। लेकिन विज्ञान, शिक्षा और तर्कशीलता के विकास के साथ दुनिया भर के लोगों ने धीरे-धीरे इन बेबुनियाद मान्यताओं से खुद को बहुत हद तक मुक्त भी किया है। अलग-अलग संस्कृतियों में अंधविश्वास से छुटकारा पाने के अलग-अलग तरीके अपनाए गए, लेकिन इसके मूल कारण हमेशा समान रहे हैं और वे हैं-वैज्ञानिक जागरूकता, शिक्षा, सामाजिक सुधार और तकनीकी प्रगति।
वैज्ञानिक जागरूकता और तर्कशील सोच
अंधविश्वास को दूर करने में यूरोप में आया “एज ऑफ एनलाइटेनमेंट” (17वीं-18वीं शताब्दी) एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वाल्तेयर, रूसो और कांट जैसे विचारकों ने तर्कपूर्ण सोच को बढ़ावा दिया, धार्मिक अंधविश्वासों पर सवाल उठाए और बिना सोचे-समझे मान्यताओं को ख़त्म करने का प्रयास किया। गैलीलियो, न्यूटन और डार्विन जैसे वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक घटनाओं के तार्किक स्पष्टीकरण दिए, जिससे लोगों का झुकाव झूठे विश्वासों से हटकर विज्ञान की ओर हुआ।
भारत में भी चार्वाक जैसे तर्कवादी दार्शनिकों ने अंधविश्वासों को चुनौती दी थी। बाद में स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अनावश्यक रीति-रिवाज़ों के ख़िलाफ़ काम किया और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया।
शिक्षा और साक्षरता अभियान
अंधविश्वास मिटाने में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। जिन देशों ने शिक्षा पर ज़ोर दिया, वहां अंधविश्वास तेजी से घटने लगे। जापान में “मीजी पुनर्जागरण” (1868-1912) के दौरान विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया गया, जिससे पुरानी मान्यतायें पीछे छूट गईं।
अफ्रीका में उपनिवेशवाद और उसके बाद की सरकारों ने शिक्षा पर निवेश किया, जिससे जादू-टोने और काले जादू से जुड़ी भ्रांतियां कम हुईं। इसी तरह, चीन की “सांस्कृतिक क्रांति” (1966-1976) ने पारंपरिक अंधविश्वासों को खत्म करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास किया।
धार्मिक और सामाजिक सुधार
धार्मिक नेताओं और समाज सुधारकों ने भी अंधविश्वास ख़त्म करने में बड़ी भूमिकायें निभायीं। भारत में ज्योतिराव फुले और डॉ. बी. आर. आंबेडकर जैसे सुधारकों ने जातिगत अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष किया। ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे आंदोलनों ने भी धार्मिक विश्वासों को अधिक तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया।
इस्लामी दुनिया में इब्न खल्दून जैसे विद्वानों ने तर्क और इतिहास के माध्यम से मिथकों को चुनौती दी। ईसाई धर्म में “प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन” ने अंधविश्वास-आधारित धार्मिक परंपराओं को अस्वीकार कर दिया।
मीडिया और तकनीक
मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रसार से अंधविश्वास तेज़ी से घटा है। टेलीविज़न, डॉक्यूमेंटरी और सोशल मीडिया अभियानों ने वैज्ञानिक तथ्यों के ज़रिए झूठे विश्वासों को खंडित किया है। भारत में वैज्ञानिक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ने अंधविश्वास-विरोधी आंदोलन चलाया और मीडिया के माध्यम से ढोंगी बाबाओं और चमत्कारी दावों की पोल खोली।
इसी तरह, पश्चिमी देशों में फैक्ट-चेकिंग वेबसाइटें और “स्केप्टिक्स सोसायटी” जैसे संगठन ऑनलाइन माध्यमों से अंधविश्वास और साज़िश के सिद्धांतों को चुनौती देते हैं।
सरकारी नीतियां और क़ानूनी कार्रवाई
कई देशों की सरकारों ने अंधविश्वास के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानून बनाये। भारत में कई राज्यों में जादू-टोना और डायन प्रथा के ख़िलाफ़ क़ानून लागू किए गए हैं। अफ़्रीका के घाना जैसे देशों में “विच कैंप्स” (जहां लोगों को जादूगर बताकर निर्वासित किया जाता था) को बंद कर दिया गया।
चीन और रूस ने भी भाग्य बताने और नकली आध्यात्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया।
अंतत:
हालांकि अंधविश्वास आज भी कुछ जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन दुनिया अब तर्क और विज्ञान की ओर बढ़ रही है। शिक्षा, तकनीक, मीडिया और क़ानून के माध्यम से सदियों पुराने मिथकों पर सवाल उठाये जा रहे हैं, जिससे समाज एक अधिक तार्किक सोच की ओर अग्रसर हो रहा है। धीरे-धीरे लोग अंधविश्वासों की जकड़ से ख़ुद को आज़ाद करने लगे हैं।
अंधविश्वास से मुक्ति एक जागरूक और प्रगतिशील समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। अंधविश्वास तर्क, वैज्ञानिक सोच और स्वतंत्र विचारों को बाधित करता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास में रुकावट आती है। यह डर, भेदभाव और ग़ैर-जरूरी परंपराओं को बढ़ावा देता है, जो समाज को पीछे ले जाते हैं। एक जागरूक समाज शिक्षा, विज्ञान और तर्क पर आधारित होता है, जिससे लोग सही निर्णय ले पाते हैं और अंधविश्वासों के झूठे दावों से बचते हैं। जब लोग तर्कसंगत सोच अपनाते हैं, तो समाज अधिक समानतावादी, उन्नत और आत्मनिर्भर बनता है, जो समग्र विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
(उपेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्यूमेंटरी मेकर हैं।)