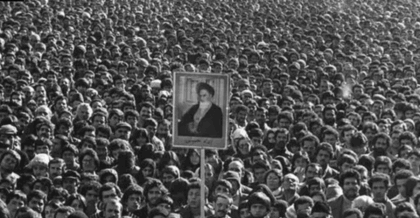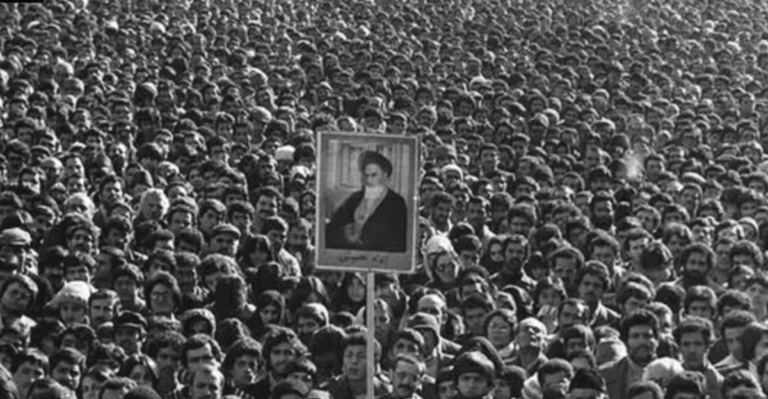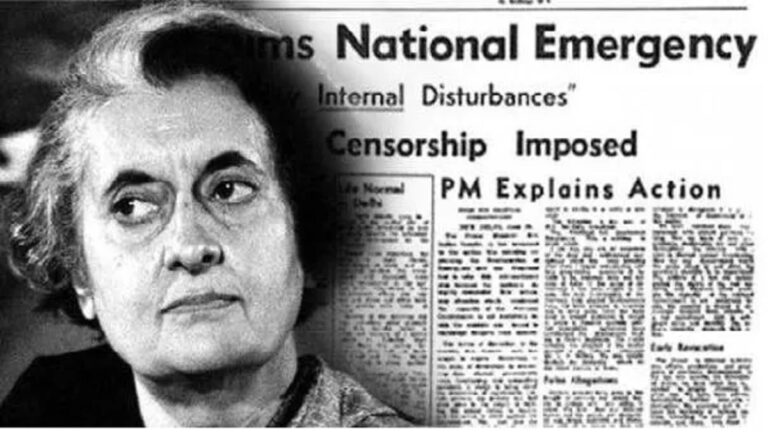इंसान प्रकृति की ही देन है। लेकिन, जब इंसान ने प्रकृति से खुद को अलग करते हुए अपने अनुकूलन कम कर प्रकृति को नियंत्रण में लेने लगा, तब से उसका प्रकृति के साथ एक तरह का झगड़ा शुरू हो गया। महान दार्शनिक एंगेल्स की शब्दावली में इंसान का प्रकृति के साथ यह रिश्ता भौतिक द्वंदवाद में अभिव्यक्त हुआ। इसकी हर कड़ी उसकी भौतिकवादी ऐतिहासिकता में निहित है। इतिहास के विविध चरणों में प्रकृति के साथ इंसान का रिश्ता तनाव से भरता गया है। आज यह सबसे कठिन और जटिल स्थितियों में पहुंच गया है। ऐसे में, चाहे और अनचाहे इन जटिल स्थितियों के कारणों को समझने के लिए आमतौर पर इतिहास में जाने की जरूरत पड़ रही है जिससे अपने समय में प्रकृति के साथ रिश्तों को ठीक कर लिया जाए।
ऐसा ही कुछ दिल्ली में बारिश और भारी जलजमाव की समस्या के संदर्भ में भी हो रहा है। पिछले पखवाड़े में रात के दूसरे पहर में हुई बारिश ने पूरी दिल्ली को जलमग्न कर दिया। दिल्ली का कोई इलाका ऐसा नहीं था जो बरसात से भर न गया हो। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि यह बारिश बादल फटने की वजह से नहीं हुआ था। लेकिन, उसके अनुसार यह उसके करीब ही था। बारिश की वजह से होने वाली परेशानियों को लेकर हर साल की तरह इस साल भी केंद्र बनाम राज्य और गवर्नर बनाम दिल्ली राज्य सरकार के बीच खूब नोक झोंक हुई। लेकिन, इससे समस्या जहां है, वहीं रही। इस दौरान, कुछ लेख सामने आये जिन्होंने दावा किया कि समस्या नई दिल्ली की बनावट में है और इसके लिए लुटियंस को दोषी ठहराया गया। यह कहा गया कि उन्होंने दिल्ली की बारिश को समझा ही नहीं और वास्तुकला को पश्चिम से लाकर दिल्ली पर थोप दिया।
इस संदर्भ में मुख्यतः मिंटो ब्रिज का उदाहरण दिया गया। लेकिन, दिल्ली की बारिश ने दिल्ली के किसी भी हिस्से को तबाही के कगार पर ले जाने से गुरेज नहीं किया था। बारापुला नाला फट पड़ा और संभ्रांत कालोनियों में अपना कचरा लाकर भर दिया था। यही स्थिति हौज खास की थी और आईआईटी में पानी घुसकर छात्रवासों और लैब में घुस गया था। धौला कुंआ से लेकर पूर्वी दिल्ली तक बारिश का पानी उफन रहा था। ऐसे में, संभव है कि लुटियंस की खामियां इसमें एक कारक हों, लेकिन पूरी दिल्ली के लिए उसे दोषी ठहराना उपयुक्त नहीं होगा। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि जब अंग्रेज दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय ले रहे थे, तब उनके सामने दिल्ली का सूखा, गर्म इलाके की चुनौती थी और पानी का मुख्य स्रोत एकमात्र यमुना ही थी जो गर्मियों में पानी की कमी से सिकुड़ जाती थी। उनके पास इस संदर्भ में सिर्फ दिल्ली रेजिडेंट का वह अनुभव था जो मुगलों के अंतिम समय से रहते हुए हासिल किया था।
दिल्ली मुख्यतः अरावली पर बसा हुआ शहर हुआ करता था। वजीराबाद के पास हिमालय की पट्टियां आती हैं। अरावली के इस अंतिम छोर पर आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय के रिज के एक पूरे हिस्से का खत्म कर उस पर मेट्रो का डिपो बना दिया गया है। अभी तक के पुरातत्व की खोजों में सबसे पुरानी बसावट के संकेत फरीदाबाद, गुड़गांव, जेएनयू और संजय वन के रिज में दिखते हैं। यहीं पाषाणकालीन औजार मिले हैं। ये सबसे सूखे इलाके हैं और साथ इन पहाड़ियों में झीलों की एक पूरी श्रृंखला है। किले का पहला अस्तित्व फरीदाबाद में दिखता है। इसी के आसपास में बनाई गई पहली झील सूरजकुंड स्थित है। बाद के समय में अनंगपाल ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया जो वर्तमान समय में राय पिथौरा किला के नाम से प्रसिद्ध है।
आने वाले समय में चहमाणों ने इसे ही केंद्र बनाने का प्रयास किया लेकिन सत्ता का केंद्र तेजी से कन्नौज की ओर खिसक गया। यह गुप्तकाल के अंतिम दौर के समय में घटित हो रहा था और मध्यकाल में सल्तनतों के साथ युद्ध करने तक मजबूती से स्थापित रहा। यह सामंतवाद के मजबूत होने और जाट, गुर्जर आदि समूहों के सामंतों के राजा बनने का दौर था। दिल्ली में राजा अनंगपाल ने एक बड़ी झील का निर्माण किया जिसके ध्वंसावशेष को संजय वन में देखा जा सकता है। संजय वन में आज भी कई कुंए हैं। बावड़ियों के अवशेष दिखते हैं। और, कम से कम दो प्राकृतिक झीलें अब भी बची हुई हैं। इस संदर्भ बी.आर. मणि का अनंगताल पर की गई खुदाई पर पेश की गई रिपोर्ट को देखना उपयुक्त होगा।
मध्यकाल के सल्तनतों का दौर शुरू होने के साथ ही दिल्ली में नई बसावटों ने जोर पकड़ा और देखते-देखते दिल्ली सदा के लिए भारत का केंद्र बन गया। सल्तनतों का प्रवेश और आरम्भिक बसावट इसी राजा अनंग के किले से हुई। आज भी इस किले के चारो ओर सरायों, बेर सराय, कटवरिया सराय, लाडो सराय आदि के अवशेषों को देखा जा सकता है। इन सारे मुहल्लों में पुराने कुंओं को अब भी देखा जा सकता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने मध्यकालीन बावड़ियों के निर्माण में तेजी ला दिया। मेहरौली में इस तरह की बावड़ियों के अवशेष आज भी हैं। कई समय की मार में विलुप्त होने के कगार पर चले गये। आने वाले समय में दिल्ली में पानी की समस्या को हल करने के लिए हम उनके द्वारा कई पुलों का निर्माण होते हुए भी देखते हैं।
दक्षिणी दिल्ली के रिज इलाके का उतार साकेत से होते हुए निजामुद्दीन के यमुना तट की ओर जाता है। दिल्ली की पहाड़ी के इस उतार में प्राकृतिक जल ठहराव की उपस्थिति थी। यह साकेत से लेकर सिरी फोर्ट के उठानों तक दिखती है। पीछे की ओर यह देवली गांव तक जाता है। बारिश के समय में निश्चित ही यह बड़े जलजमाव में बदल जाता होगा। यह एक मैदानी इलाके की तरह था और निश्चित ही मध्यकाल में सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त था। तुगलक के समय में यहां सतपुला का निर्माण हुआ, जिसका मुख्य काम पानी को नियंत्रित करना और उसे उपयोग में लाना था। इसी के दाहिने हिस्से में जहांपनाहनगर बसा। तुगलक काल में ही वजीराबाद के पुल का निर्माण हुआ। फिरोजशाह तुगलक, जिसने कोटला किले का निर्माण किया था, पानी की व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्क रहा। इसने दिल्ली में वजीराबाद पुल का निर्माण किया। यह यमुना पर बनाये गये पुलो में पहला निर्माण था जो उसके बहाव को नियंत्रित करने और शहर के भीतर घुसपैठ को कमतर रखने का प्रयास था।
आने वाले समय में इसी पुल का पुनर्निर्माण और रखरखाव पिछले दशक तक चलता रहा और उपयोग में आता रहा। खिलजी काल में दिल्ली पानी के स्रोत के तौर पर सबसे बड़ा काम हौज खास का निर्माण है और कुछ बावलियों का निर्माण है। मुगलों का आरम्भिक दौर आगरा में गुजरा। सत्ता को मजबूत बनाने और संपन्नता से भरा दौर शाहजहां के समय में चरम पर पहुंचा। उसने नई तकनीक का सहारा लिया और यमुना के तट पर जाकर किले का निर्माण किया और नये शहर शाहजहांनाबाद का निर्माण किया। इसने इसी के तट पर राजशाही से जुड़े लोगों के रहने और बाजार का भी निर्माण किया। लेकिन, यह भी सच् है कि मेहरौली मुगलों के समय में और अंग्रेजों की कंपनी राज के समय तक महत्वपूर्ण बना रहा। दिल्ली में आज भी पुरानी बसावटों में कुंओं और बावलियों, झीलों की एक पूरी श्रृंखला है जो समय की मार में खत्म हो जाने के अभिशप्त होती गईं। शुक्र है कि कुछ का अस्तित्व फिर से वापस लाया जा रहा है।
प्राचीन और मध्ययुगीन दौर में किसी शहर का अर्थ था बाजार। एक राजा को बने रहने के लिए गांव से अन्न और कर की वसूली और सेना के लिए युवाओं की भर्ती जरूरी था। इसके लिए सबसे जरूरी था एक एकीकृत, केंद्रीयकृत प्रशासन और गांव की जरूरतों की आपूर्ति के लिए बाजार। थोड़े से समय में सेना को इकठ्ठा करना, धन की व्यवस्था करना और संचार को दुरूस्त करते हुए बाजार और उसके निवासियों को सुरक्षित करने के लिए किले के साथ-साथ अन्न और जल की भी व्यवस्था उतनी ही जरूरी था। दिल्ली में इस व्यवस्था के अवशेषों को देख सकते हैं। अंग्रेजी राज के समय में ऐसी जरूरत उन्हें नहीं रह गई थी। उनके लिए दिल्ली के बाहरी हिस्सों में कैंटोन्मेंट थे। उन्हें सिर्फ प्रशासकों की जरूरत थी।
वे जब नई दिल्ली बना रहे थे तब उन्हें एक सपाट मैदान की जरूरत थी। अंग्रेजों को 1857 के बाद उजड़ी दिल्ली में बसे रह गये लोगों को पानी की व्यवस्था को उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन, जैसे-जैसे उन्होंने दिल्ली को प्रशासनिक क्षेत्र में ढालते गये, वहां पानी की आपूर्ति को सीधे यमुना से जोड़ा। भूजल का भी प्रयोग शुरू किया। देखते-देखते पंप, पाईप और नल की व्यवस्था दिल्ली के आमजीवन का हिस्सा बन गई। अंग्रेजों ने खुद अपनी ही बनाई गई शुरूआती दौर की नहरों को उनके हाल पर छोड़ दिया। कुंओं और बावड़ियों को खत्म होने के लिए अभिशप्त बना दिया। झीलों और तालाबों को पाटने का काम शुरू हो गया। जो प्राकृतिक नहरें और नाले, नद थे वे सीवेज को बहाने वाली नालों में बदल गये। सतपुला, बारापुला जैसी बनावटें बेसंदर्भ दिखने लगीं। 20वीं सदी तक पुरानी दिल्ली, यहां तक कि आज के कनॉट प्लेस में फैक्ट्रियां, खासकर कपड़ा उद्योग को उभरते हुए देखा जा सकता है। यह आने वाले समय में ये उद्योग लगातार केंद्र से बाहर की ओर अपसरित होते हुए देखे जा सकते हैं। दिल्ली एक ऐसे शहर में बदल रहा था जिसमें पानी की आपूर्ति की जरूरत बढ़ रही थी और कचरे भरे पानी के निस्पादन की जरूरत बढ़ती जा रही थी।
1970 के दशक में साहिबी नदी दम तोड़कर ‘बड़का नाला’ में बदल गई। 1980-90 में बारापुला कचरे की गाद से भरने लगा था। यह कॉमनवेल्थ गेम के समय में विशाल कीचड़ भरे नाले में बदल गई। आईटीओ बैराज जो किसी समय में पानी की आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और बिजली आपूर्ति का केंद्र था, एक बड़े संकट में बदल गया। इस समय तक बुराड़ी से लेकर यमुना पार का विस्तार दिल्ली की सीमा को पार कर गया। ओखला, उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बसावट यमुना और हिंडन नदी के अस्तित्व पर ही खतरा बन गये।
दिल्ली में बारिश का दो ही मौसम है। जाड़े की बारिश आमतौर पर जनवरी के महीने में होती है और कम ही होती है। यह बारिश भूमध्यसागर से चलने वाली पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसका असर मार्च तक रहता है। कई बार यह मई के महीने तक आता है। इस साल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बावजूद जनवरी से मई के बीच के बीच सामान्य से कम बारिश हुई जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी वजह से बारिश और बर्फबारी देर तक होती रही। यह मौसम के लिहाज से दिल्ली के लिए चिंताजनक बात थी। पश्चिमी विक्षोभ जैसे-जैसे गर्म हवा में बदला, दिल्ली का तापमान आसमान छूने लगा। इस साल की गर्मी ऐतिहासिक तौर पर रिकार्ड बनाते हुए गुजरी।
दिल्ली में दूसरी बारिश मानसून से होती है। अरब सागर से उठा मानसून गुजरात और कर्नाटक के तट से होते हुए दिल्ली की ओर रुख करता है। इस साल मानसून में हुई देरी ने इसे जून के अंतिम हफ्तों में यहां पहुंचाया। अमूमन जून के मध्य से बारिश शुरू होती है और जुलाई-अगस्त में खूब बारिश होती है। दिल्ली में पानी के संचार का मुख्य संकट जुलाई और अगस्त के महीने में ही देखी जाती है। इस बार गर्म हवाओं, अलनीनो का देर तक बना प्रभाव और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने मानसून की गति को प्रभावित किया है जिसका नतीजा तेज और पैची बारिश में देखी जा रही है। दिल्ली में जून के अंतिम हफ्तों में हुई बारिश इसी तरह की रही।
दिल्ली में बारिश, जलजमाव की समस्या को लुटियंस के सिर पर डाल देने से न तो सुलझने वाली है और न ही इससे कोई उपयुक्त नतीजा सामने आने वाला है। इस समस्या की जड़ निश्चित ही उपनिवेशिक दौर के शहरी विकास की योजनाओं से गहरे जुड़ा हुआ है। भारत के ज्यादातर आधुनिक शहर प्रशासनिक केंद्र बनकर सामने आये और बाद में ये औद्योगिक और आवासीय शहरों में बदलते गये। इन शहरों के विकास में अराजकता मूल तत्व है। यह अराजकता जनता की कम राज्य और प्रशासन के संस्थानों की अधिक है। अंग्रेजों के दौर में शहर सिर्फ प्रशासकों के आवासीय सुविधा से ही नहीं जुड़ा था, उनके लिए काम करने वालों से लेकर अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी आवास की जरूरत पैदा हुई। ये ब्रिटिश औद्योगिक शहरों में पैदा हुई आवासीय समस्या नहीं थी।
भारत के शहरों में अनौपचारिक बसावट से औपचारिक बसावट का सिलसिला आज तक जारी है। इस सिलसिले में पानी की आपूर्ति और संचार एक महत्पूर्ण पक्ष है। इसमें अधिक गर्मी आपूर्ति और संचार को प्रभावित करती है और अधिक बारिश उसके निकास और संचरण को प्रभावित करती है। यही कारण है नाले, चाहे वे नई दिल्ली से गुजरते हों या सीलमपुर से, वे एक सीमा से अधिक पानी का निर्वहन करने में अक्षम हैं। यह एक ऐसा संकट है जिसे हल करने के लिए जिन प्रयासों की जरूरत है, वह राजनीतिक दांवपेच और अरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाते हैं। यह संकट भी नदियों की सफाई से कम पेचीदा नहीं है। निश्चित ही ये जुमलेबाजी से हल होने से रहा। लुटियंस पर आरोप मढ़ देने से तो कत्तई कोई सबक हाथ नहीं लगेगा।
(अंजनी कुमार लेखक व स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)