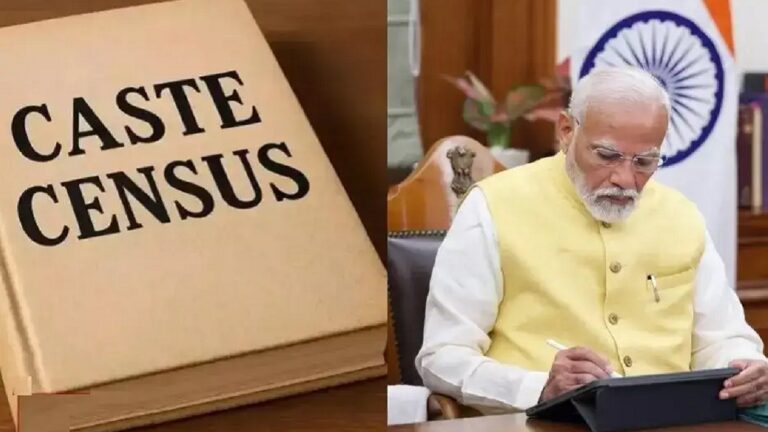सबसे पहले तो इस किताब के शीर्षक में ‘क्रांति’ शब्द पर ध्यान जाता है। अपने देश में सन् 1857 के ब्रिटिश हुकूमत-विरोधी जन-विद्रोह को तरह-तरह की संज्ञाओं और विशेषणों से नवाजा जाता है। तब भारत में ब्रिटिश कंपनी-ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और वह अपने राज का लगातार विस्तार कर रही थी। इसके लिए क्रूरता, धूर्तता और षड्यंत्र, हर तरह के हथकंडे अपना रही थी। कई ब्रिटिश और भारतीय इतिहासकारों ने उसे सिपाही विद्रोह कहा, कइयों ने गदर कहा और कुछ ने स्वाधीनता का संघर्ष कहा। कुछ ने क्रांति भी कहा। निस्संदेह वह एक बड़ा संग्राम था। उस दौर में वह एक तरह की क्रांति ही थी। भले ही वह असफल रही। भारत से बहुत दूर बैठे कार्ल मार्क्स ने उसे ‘नेशनलिस्ट रिवोल्ट’ कहा था।
विदेशी अखबारों में छपी खबरों और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मार्क्स ने इस संग्राम पर लेख लिखे। उन लेखों को मिलाकर बाद में उनकी पुस्तक भी छपी। कार्ल मार्क्स के लेखों को दुनिया भर में पढ़ा गया। उससे स्वाधीनता की भारतीय जनाकांक्षा की जानकारी तमाम महाद्वीपों के लोगों तक पहुंची। अपने देश में रह रहे या बाहर से आये कुछ अन्य विदेशियों ने भी इस बारे में लिखा। इसमें एक उल्लेखनीय नाम है-जार्ज ब्रूस मल्लेसन और क्रिस्टोफर हेबर्ट, जिन्होंने इसे ‘म्यूटिनी’ के तौर पर देखा। ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांगने से काफी पहले वी डी सावरकर ने भी अंग्रेजी और मराठी में 1857 के संग्राम पर किताब लिखी थी।
अपने देश के कुछ उर्दू-हिंदी अखबारों में भी उस संग्राम की खबरें छपती रहीं। उर्दू के बड़े पत्रकार-लेखक मासूम मुरादाबादी की किताबः 1857 की क्रांति और उर्दू पत्रकारिता स्वाधीनता के पहले संग्राम और उर्दू पत्रकारिता के इतिहास व भूमिका पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उनकी किताब का हाल ही में भारतीय प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकार्पण हुआ। मासूम साहब ने सन् 1857 के संग्राम के लिए ‘क्रांति’ शब्द का प्रयोग किया है। किताब बहुत तथ्यात्मक और शोध-परक है। आम हिंदी पाठकों के लिए सन् 1857 और उस दौर की पत्रकारिता पर इसमें बहुत सारी नयी सूचनाएं हैं।
यह बात सही है कि सन् 1857 के संग्राम में विद्रोही सैनिकों के अलावा देश के कुछ हिस्सों के राजा-बादशाह-सामंत-बड़े जमींदारों के एक हिस्से ने भी बगावत की थी। लेकिन इस विद्रोह की आंच जब दूर-दूर के इलाकों में पहुंची तो आम जनता-किसान, मजदूर और साधारण कारीगर भी इसमें शामिल हुए थे या इस संग्राम को उन्होंने अपना समर्थन दिया था। किताब में सन् 1857 के संग्राम के इन तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। मासूम मुरादाबादी अपनी किताब में भारतीय पत्रकारिता के पहले शहीद मौलवी मौहम्मद बाक़र की पूरी कहानी भी सामने लाते हैं। बाकर साहब उन दिनों पत्रकारिता कर रहे थे, जब अवाम के पक्ष की खबरों के लिए अखबारों और उनके पत्रकारों को समय-समय पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। किताब में इसका भी विस्तार से जिक्र आता है। तब अपने मुल्क में अखबारों की संख्या बहुत कम थी। वे बहुत छोटे आधार वाले थे और उनकी बहुत सीमित प्रतियां छपती थीं। हिंदी पत्रकारिता तब अपने शैशव काल में थी। उसके मुकाबले दिल्ली के आसपास के इलाके में उर्दू पत्रकारिता तेजी से विस्तार पा रही थी।
मौलवी बाकर की पत्रकारिता के संदर्भ में मासूम मुरादाबादी ने विभिन्न इतिहासकारों और तब के उर्दू पत्रकारों को उद्धृत किया है। ये तमाम तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय़ पत्रकारिता के पहले शहीद पत्रकार-उर्दू अखबार ‘देहली उर्दू अखबार के संपादक मौलवी मोहम्मद बाक़र ही हैं।
मौलवी बाकर की शहादत सम्बन्धी विवाद के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की भी किताब में चर्चा की गई है। बाकर साहब को पत्रकारिता का पहला शहीद घोषित करने की हड़बड़ाहट में मासूम साहब उन तथ्यों को नजरंदाज नहीं करते, जो बाकर साहब की शहादत पर स्वयं उर्दू लेखकों के बीच सवाल के तौर पर उठाये जाते रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल है कि बाकर साहब को निस्संदेह ब्रिटिश हुकूमत के आदेश पर गोलियों से भून डाला गया था। यह भी सही है कि वह उन दिनों देहली उर्दू अखबार के संपादक थे। लेकिन क्या उन्हें किसी लेख या रिपोर्टिंग के लिए गोलियों से उड़ाया गया या किसी निजी कारण से?
यह किताब इस विवाद पर दोनों पक्षों को सामने लाती है- ‘आमतौर पर यह धारणा है कि मौलवी मोहम्मद बाकर को अंग्रेजों ने इसलिए कत्ल किया कि उन्होंने 1857 के आंदोलन में अपने समाचार पत्र द्वारा लोगों के हृदय को गरमाने और स्वतंत्रता की जोत जगाने का जुर्म किया था। आंदोलन शुरू होने के बाद देहली उर्दू अखबार की रिपोर्टिंग देखकर भी यही अनुमान होता है कि अंग्रेज इनके साहस और निडरता से परेशान थे। इसलिए बहाना मिलते ही उन्हें मार डाला गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि इनकी शहादत का संबंध पत्रकारिता से नहीं बल्कि दिल्ली कालेज (जिसे अब जाकिर हुसैन दिल्ली कालेज कहा जाता है) के प्रिंसिपल मिस्टर टेलर की मौत से था, जिसे उन्होंने अपने घर पर पनाह दी थी। बाद में टेलर उनके घर से निकला। रास्ते में विद्रोहियों का साथ दे रही जनता ने ब्रिटिश प्रिन्सिपल टेलर को देखते ही मार डाला था। हुकूमत ने इसमें बाकर साहब की भूमिका को संदिग्ध समझते हुए उन्हें गोलियों से उड़ाने का हुक्म दे डाला। इस तरह वह खत्म कर दिये गये। इस बारे में उर्दू के कई तत्कालीन लेखकों, समाज के गणमान्य लोगों और स्वयं मौलवी बाकर के परिवार के कुछ लोगों ने भी लिखा है। उनके लेखों से इस प्रकरण पर महत्वपूर्ण रौशनी पड़ती है। पर इन सभी तथ्यों में एक बात साझा है कि बाकर साहब की पत्रकारिता से ईस्ट इंडिया कंपनी और हुकूमत के बड़े ओहदेदार नाराज रहते थे।
मासूम साहब ने अपनी किताब में मौलवी बाकर के बहादुर शाह जफर से घनिष्ठ रिश्तों पर भी रोशनी डाली है। उनके मुताबिक बाकर साहब के उस्ताद ज़ौक से बहुत अच्छे सम्बन्ध थे। ज़ौक के बहादुर शाह जफ़र से रिश्ते जगजाहिर थे। जफ़र के वह उस्ताद थे। जौक साहब के साथ बाकर भी जफर से मिलने अक्सर लाल किले जाया करते थे। ज़फर और बाक़र के बीच परस्पर सम्मान और सद्भाव के रिश्ते थे। यह बात अंग्रेजों के तमाम मुखबिरों को मालूम थी। जीवन लाल नामक मुखबिर की डायरी से भी इसकी पुष्टि होती है। किताब में उसकी डायरी के अंश भी उद्धृत किये गये हैं(पृष्ठ-115)। जीवन लाल जैसे मुखबिर निश्चय ही अफसरों तक यह बात पहुंचाते रहते थे।
11 मई, 1857 को जब दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई तो इसमें मौलवी मोहम्मद बाकर ने अपने अखबार को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी इस लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि सन् 1857 के विद्रोहियों ने अपना नेता बहादुर शाह जफ़र को माना था। अंग्रेजों ने जफ़र और उऩके शाही खानदान पर क्या-क्या जुल्म ढाये, यह सब इतिहास का हिस्सा है। ऐसे में मौलवी बाक़र की शहादत पर किसी तरह का संदेह करना बेमतलब है। वह अपने लेखों के चलते मारे गये या स्वाधीनता की पहली लड़ाई के समर्थन के चलते; दोनों बातों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। ऐसे में मौलवी मौहम्मद बाक़र को निस्संदेह भारतीय पत्रकारिता का पहला शहीद कहा जा सकता है। यह खेदजनक है कि अब तक उन्हें पत्रकारिता के पहले शहीद के तौर पर आधिकारिक या पत्रकारिता के मंचों से याद नहीं किया जाता रहा है।
कुछ साल पहले जब मैं राज्यसभा टीवी(RSTV) के लिए ‘मीडिया मंथन’ नाम से अपना वीकली शो करता था, मौलवी बाकर के बारे में मिले तथ्यों के आधार पर उन्हें भारतीय पत्रकारिता के पहले शहीद के तौर पर याद किया था। उससे पहले हिंदी और उर्दू के कुछ संजीदा पत्रकारों ने 16 सितम्बर, 2007 को मौलवी बाकर के सम्मान में दिल्ली स्थित भारतीय प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम भी किया था। इसमें अरविंद कुमार सिंह, फिरोज नकवी और मासूम मुरादाबादी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने पहल की थी। उन्हीं मासूम साहब ने अब सन् 1857 और उर्दू पत्रकारिता पर यह किताब लिखी है। इसमें मौलवी बाकर पर बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है।
तब और आज के भारत में बहुत फर्क है। सन् 1857 में भारत में साक्षरता की दर महज एक फीसदी थी। पत्रकारिता सिर्फ छोटे-छोटे अखबारों के जरिये होती थी। अखबारों का एक हिस्सा हुकमूत का समर्थक था और दूसरा भारतीय समाज और जनता के साथ था। उन्हीं दिनों भारतीय जनता-समर्थक और समाज-पेक्षी पत्रकारिता को नियंत्रित करने के लिए लार्ड कैनिंग ने एक निरंकुश कानून लाया था। तमाम बंदिशों के बावजूद मौलवी बाक़र का अखबार ‘देहली उर्दू अखबार’ प्रशासनिक खबरों के अलावा समाज और अवाम के पक्ष में भी अपनी बातें लिखता रहता था। कोहिनूर, सादिकुल अखबार, पयामे आजादी, सेहर सामरी सहित कई अखबार अवाम के पक्ष में खड़े रहते थे।
किताब में उर्दू पत्रकारिता के इतिहास पर भी एक अलग अध्याय है। हिंदी का पहला अखबार उदन्त मार्तण्ड को माना जाता है, जो कलकत्ता से सन् 1826 में निकला था। यह हर मंगलवार को छपता था। इसकी भाषा ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण थी। उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा को माना जाता है, जो सन् 1822 में छपना शुरु हुआ था। मजे की बात कि वह भी कलकत्ता से ही निकला। अब तक इसे ही उर्दू का पहला अखबार माना जाता रहा है। लेकिन इस किताब में मासूम साहब बताते हैं कि जामे जहांनुमा से पहले भी एक उर्दू अखबार के छपने का दावा किया जाता है। इसका नाम था-फौजी अखबार । यह पहली बार सन् 1794 में टीपू सुल्तान द्वारा निकाला गया था (पृष्ठ-73-74)। यह अखबार मैसूर के सरकारी प्रेस से छपता था।
इस बारे में मासूम मुरादाबादी उर्दू के कई विद्वानों और इतिहासकारों की पुस्तकों में दर्ज प्रमाण और तथ्यों को उद्धृत करते हैं। लेकिन उर्दू लेखक-इतिहासकार और जामे जहां नुमा पर विस्तार से लिखने वाले गुरुबचन चंदन को उद्धृत करते हुए वह कहते हैं कि फौजी अखबार की उन्हें कोई प्रति नहीं मिली। संभव है, वह मैसूर के सरकारी प्रेस से पर्चे के तौर पर छपता रहा हो। पर उसकी भाषा उर्दू के बजाय फारसी रही होगी क्योंकि उन दिनों मैसूर राज की आधिकारिक भाषा फारसी ही थी।
किताब की एक प्रमुख विशेषता है, घटनाओं और शख्सियतों के बारे में लेखक का वस्तुगत और तथ्यपरक दृष्टिकोण। वह अपनी तरफ से कोई बात थोपते नजर ऩहीं आते। तथ्यों और सूचनाओं की तह में जाते हैं और फिर अलग-अलग पक्षों को रखते हुए बहुत विनम्रता से अपनी बात कहते हैं। मासूम मुरादाबादी की यह किताब उर्दू पत्रकारिता और भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम के इतिहास पर बहुत उल्लेखनीय और पठनीय किताब है।
*1857 की क्रांति और उर्दू पत्रकारिता, लेखक-मासूम मुरादाबादी
प्रकाशकःखबरदार पब्लिकेशन्स, दिल्ली, वर्ष-2021, पृष्ठ-200, मूल्य-250
(उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप आजकल दिल्ली में रहते हैं।)