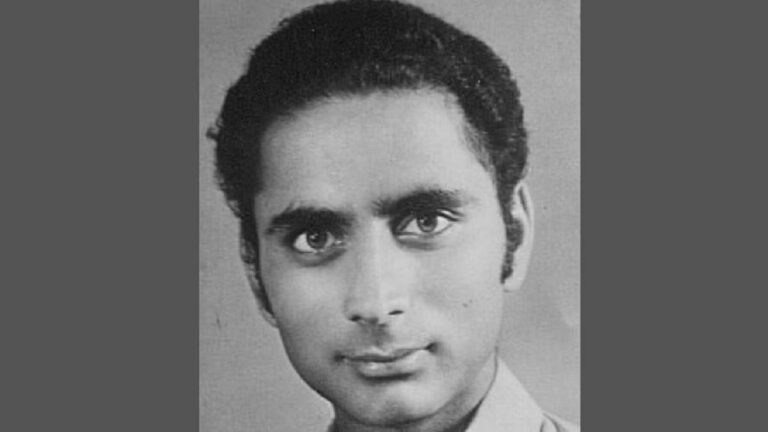बेशक 1947 में देश का खूनी बंटवारा हुआ था और दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान वजूद में आए। बांग्लादेश बाद में बना। इन तीनों देशों में एक त्योहार पुरानी विरासती संस्कृति के साथ अपनी-अपनी सरजमीं पर मनाया जाता है। इसे मनाने की रवायत भी बहुत पुरानी थी।
ज़मीं तो दो (बाद में तीन) हिस्सों में बंट गई लेकिन रवायत को कोई नहीं बदल सका और न आसमान को। मौसम तक वही है। हवा का तो वैसे भी कोई वतन नहीं होता। उसी आसमां और हवा का इस सांझे पर्व में खास महत्व है।
वह पर्व है, ‘बसंत!’ जिसकी शिद्दत की इंतहा जितनी भारतीय पंजाब में है, ठीक उतनी ही पाकिस्तानी पंजाब में और पाकिस्तान से अलहदा हुए बांग्लादेश में। प्रसंगवश, व्यापार के सिलसिले में बहुतेरे भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब के लोग बांग्लादेश में हैं।
जालंधर से थोड़ी दूर बसा लेकिन जीटी रोड से हटकर शहर कपूरथला एक ऐतिहासिक और रियासती शहर है। बसंत कभी यहां का अहम उत्सव हुआ करता था। दिवाली से भी ज्यादा। 1917 में यहां के महाराजा जगजीत सिंह ने बाकायदा बसंत उत्सव की शुरुआत की थी और इसके लिए एक बड़े मैदान को आलीशान बाग में तब्दील किया गया था। महाराजा तो नहीं हैं। लेकिन बसंत का उत्सव अब भी होता है।

जिस बड़े मैदान को बाग में बदला गया था-वह ‘शालीमारबाग’ आज भी वहीं है। उस पर चढ़ा रियासती रंग जरूर बदलते वक्त के साथ उतर गया है लेकिन जब भी बसंत का मेला लगता है तो यहीं लगता है। पुराने लोग बताते हैं कि शालीमार बाग में लगने वाले बसंत मेले की चमक और धमक सुदूर लाहौर और रावलपिंडी तक चर्चा का विषय बना करती थी।
कपूरथला के बसंत मेले में हिंदू, सिख और मुसलमान बड़ी तादाद में शिरकत करते थे। ईसाई भी। (तब इस समुदाय के कई लोग कपूरथला रियासत में बतौर कर्मचारी कार्यरत थे) विरला ही ऐसा कोई परिवार होता था जो बसंत के दिन शालीमार बाग नहीं जाता था।
इस दिन महाराजा जगजीत सिंह सजे हुए हाथी की सवारी करते हुए बाग तक पहुंचते थे और अवाम से रूबरू होते थे। उनके साथ रंग-बिरंगे कई हाथी चलते थे। इस दिन महाराजा परंपरागत पोशाक और जेवर पहने हुए होते थे। शालीमार बाग में कोई भी उन्हें गले से लगाकर बसंत की बधाई दे सकता था। अंग्रेज हुक्मरान भी कपूरथला का बसंत मेला देखने बतौर विशेष मेहमान आते थे।
‘डिवाइड एंड रूल’ की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों के लिए यह नजारा अद्भुत था। सब धर्मों के लोग मिलकर बसंत मनाते थे। गोया पूरा शहर ‘बसंती’ हो जाता था। महाराजा जगजीत सिंह के वंशज शत्रुजीत ने अपनी किताब में लिखा है कि 40-50 हजार लोग, सिर पर पीले रंग के साफे/पगड़ियां बांधकर आते थे। महिलाएं भी बसंती पीले वस्त्रों में होती थीं।
विशेष पीले व्यंजन तैयार किए जाते थे। तमाम लोग बगैर किसी भेदभाव उन्हें खाते थे और महाराज जगजीत सिंह खुद भी। पतंगबाजी के मुकाबले होते थे और पतंगें कपूरथला से बाजरिया हवा में लाहौर तक सैर करती थीं और लाहौर की पतंगे इधर दिखाई देती थीं। रियासत कपूरथला का प्रतिनिधि और सबसे बड़ा त्योहार था ‘बसंत’।
कपूरथला जैसा मंजर पूर्वी पंजाब के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फरीदकोट, पटियाला और बठिंडा में भी दिखाई देता था। लेकिन रियासत कपूरथला का जलवा सबसे अलहदा था। अमृतसर से लाहौर जाकर लोग वहां की पतंगबाजी में शमूलियत करते थे। लाहौर से कई दिनों का सफर तय करके लोग फिरोजपुर का बसंत मेला देखने आते थे। फिरोजपुर का बसंतोत्सव आज भी बेमिसाल है। वक्त के साथ रंग-ढंग बदल गए हैं लेकिन उत्साह में कमी नहीं।
फिरोजपुर और साथ लगते शहर बठिंडा में बसंत महाउत्सव की तरह मनाया जाता है। अमृतसर में भी। इस दिन आपको हर घर में पीले पकवान मिलेंगे और हर छत से उड़ती हुईं पतंगें आकाश पर हावी-सी होती दिखेंगीं। हर तीसरे घर में डीजे पर संगीत बजता और इसकी धुन पर नाचते सभी आयु वर्ग के लोग मिलेंगे।
इन तमाम शहरों में मुस्लिम आबादी भी बड़ी तादाद में है और वह भी बसंत धूमधाम से मनाती है। संगरूर और मलेरकोटला में भी बसंत की धूम रहती है। तमाम समुदायों के लोग इसे मिलकर मनाते हैं।कभी कुछ कट्टरपंथियों का कथन था कि बसंत दरअसल एक मूर्तिपूजक त्योहार है पर इतिहासकारों ने इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया।
हलांकि बसंत एक पूर्व-इस्लामिक दौर का पर्व है लेकिन अपने तमाम मायनों और अर्थों में एक लोक-ऐतिहासिक पर्व। मौखिक और लिखित इतिहास के अनुसार (मरहूम जाने-माने पत्रकार/लेखक और इतिहासकार खुशवंत सिंह भी मानते थे कि) आधुनिक काल में बसंत को व्यापक सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का शासकीय संरक्षण हासिल हुआ।
उसके बाद 1947 तक इसे अघोषित शासकीय पर्व की तरह ही मनाया जाता रहा। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बहुत से पर्व-त्योहार बदले लेकिन ‘बसंत’ में कोई तब्दीली नहीं आई। पंजाबी-अंग्रेजी के महान सिख इतिहासकार और विद्वान भाई काहन सिंह नाभा ने लिखा है कि पहले बसंत सूफी कवि शाह हुसैन के जीवन रंगों से वाबस्ता था।
विभाजन के बाद पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के कई प्रमुख परंपरागत पर्व पाबंदीशुदा कर दिए गए। लेकिन बसंत पर कोई रोक नहीं लगी। उसका उत्साह आज भी वैसे ही बरकरार है। बल्कि इसमें इजाफा ही हुआ। इसकी सांस्कृतिक विरासत भी उसी मांनिद कायम है जैसे हिंदुस्तान में। आज भी लाहौर की पतंग कटकर अमृतसर में गिरती है तो अमृतसर की लाहौर में।

इन पतंगों पर मोहब्बत के संदेश भी लिखे पाए जाते हैं। कट्टरपंथ का थोड़ा ग्रहण इस रवायत पर जरूर लगा लेकिन सांझी संस्कृति की डोर नहीं टूटी।
लाहौर को पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। वहां के कई प्रतिष्ठित लेखकों ने अपनी रचनाओं में बसंत का जिक्र किया है। पाकिस्तानी अदीब इसे सांस्कृतिक संपत्ति के तौर पर भी देखते हैं। ‘इमेजिंग लाहौर’ और ‘वॉकिंग विद नानक’ किताबों के विश्व विख्यात पाकिस्तानी लेखक हारून खालिद के मुताबिक लाहौर में बसंत को ‘सबकी सांझी संस्कृति’ का त्योहार माना और कहा जाता है।
भारतीय पंजाब में भी ऐसा ही है। यहां गुरबानी बसंती रागों में भी गाई जाती है। हारून खालिद के अनुसार पाकिस्तान में बसंत को लेकर जो उत्साह विभाजन से पहले था, वही 1947 के बाद भी बरकरार रहा। यह इस बात का पुख्ता सुबूत है कि कभी महादेश में हिंदू-मुस्लिम-सिख संस्कृति की गंगा-जमुनी रवायत कितनी सशक्त रही होगी।
बाहरहाल, बसंत के लिए दोनों मुल्कों का आकाश खुला और अनंत है। पतंगें हवा में उड़तीं हैं और फिर हवा का कब कोई वतन हुआ? बसंत बखूबी बताता है!
(अमरीक पत्रकार हैं पंजाब में रहते हैं)