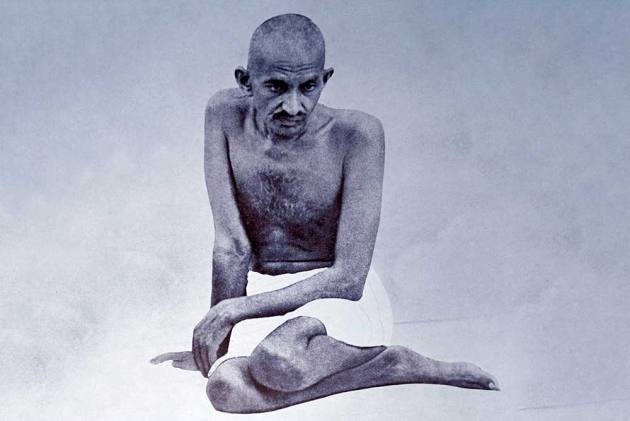सर्व प्रथम यह सपष्ट कर दूं, मैं गांधीवादी या गांधी अनुयाई नहीं हूं। पचास साल पहले जब थोड़ी बहुत राजनीतिक या विचारधारात्मक चेतना मुझमें आयी थी तब मैंने महात्मा गांधी के विचारों और कार्यशैली की आलोचना की थी। तब मैंने समझा था कि गांधी जी पूंजीवाद के एक ईमानदार पक्षधर या नेता हैं। मार्क्सवादी नेता नम्बूदरिपाद ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उन्हें बुर्जुआज़ी व अंग्रेज़ों का हमदर्द समझा जाता था। वह दौर था चरम वामपंथवाद का। उसी दौर की पैदाइश है नक्सलवाद। ज़ाहिर है, इस विचारधारा से प्रभावित था भारतीय किशोर-युवा मन। मैं भी अपवाद कैसे हो सकता था? पिछले पांच दशकों के अनुभवों के आधार पर मैं गांधी जी को समझने की कोशिश में हूं। किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। इस आलेख की यही सीमा है।
इन पांच दशकों में गंगा-यमुना-गोदावरी-साबरमती नदियों में काफी पानी बह चुका है। परिवर्तन- विमर्शों का जल प्लावन हो चुका है। तब वैज्ञानिक मानस से लैस प्रत्येक व्यक्ति से तकाज़ा है कि बीसवीं सदी के इस महान योद्धा पर पुनर्दृष्टि की जाए।हालांकि, किसी एक लेख या पुस्तक के पोखर में महासागर को समेटना सूर्य विजय के समान है। फिर भी, एक किंचित प्रयास तो किया जा सकता है। वैसे गांधी जी की जीवन यात्रा कभी भी निरापद नहीं रही। यहां तक कि उनके जीवन का हिंसात्मक पटाक्षेप भी। यदि गांधी जी एक व्यक्ति, समाजसुधारक, राजनेता या क्रांतिकारी रहे होते तो उनकी कर्म यात्रा पर दृष्टिपात करना सहज-सरल रहा होता। लेकिन, उनकी यात्रा आरम्भ से अंत तक बेहद जटिल, उतार-चढ़ावों से ग्रस्त, सत्य के साथ निरंतर नए नए प्रयोग और अपने विरोधियों के विरुद्ध अथक अहिंसा-सहिषुणता के शस्त्रों के इस्तेमाल से और अधिक पेचीदा बन गयी है।वे एक मौसम के भी हैं, और सभी मौसमों के भी प्रतिनिधि हैं; जहां वे स्वच्छता की बात करते हैं, चरखा चलाते हैं, नमक बनाते हैं, वहीँ वे ‘अंग्रेज़ों भारत छोड़ो’ का नारा भी देते हैं। किसी एक सांचे, वर्ग या विचारधारा में क़ैद नहीं किया जा सकता है। सारांश में, सरहद मुक्त मानव हैं गांधी जी।
आज हम महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मना रहे हैं। ऐसे समय उनकी विवेचनात्मक प्रासंगिकता को समझना और भी ज़रूरी है। आज ‘अतिवादियों‘ का ज़माना है; चरम भौतिकवाद, पूंजीवाद, उपभोगवाद, व्यक्तिवाद, आत्ममोहग्रस्ततावाद, असहिष्णुतावाद, कट्टरतावाद, ध्रुवीकरण, उग्रराष्ट्रवाद-युद्धोन्मादवाद जैसी प्रवृतियां चारों तरफ फैली हुयी हैं। भारत ही नहीं, पूरा विश्व इसकी चपेट में है।
जनवरी 1948 में उनके हिंसात्मक अंत से लेकर अक्टूबर 2019 तक नेताओं और आमजन की चार-पांच पीढ़ियां आई और जा चुकी हैं; जब उनकी मृत्यु हुई थी तब स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य, नैतिकता और राज्य का कल्याणकारी चरित्र जीवित था; मिश्रित अर्थव्यवस्था थी; विषमतामुक्त भारत के नवनिर्माण का विराट स्वप्न था; संवेदनशीलता का वातावरण था और युवा पीढ़ी कुछ करना चाहती थी। आज 21 वीं सदी की बयार दूसरी है। इस समय की समकालीन पीढ़ी हाई टेक है। उसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। अब भारत का ज्ञान-विज्ञान अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है। अगले दो-तीन सालों में किसी भारतीय को चांद की ज़मीन पर उतारने की हमारी तैयारी है। अब भारत का स्वप्न ‘ विश्व की महाशक्ति‘ बनने का है। दूसरे शब्दों में आज के शासक भारत के राष्ट्र राज्य को सुदृढ़ से सुदृढ़तम बना देना चाहते हैं। (जनता कितनी होगी, कहना कठिन है।)
अतः सपनों के इस मायाजाल के बीच वर्तमान पीढ़ी बापू को क्यों याद करे? क्यों याद करे गांधीजी के ‘ राज्यहीन समाज ‘ को; क्यों याद करना चाहिए ‘ अंतिम जन‘ को? गांधीजी मंथर गति के पक्षधर थे, आज का भारत ‘ बुलेट रफ़्तार’ का है। गांधी जी मशीनीकरण या मशीनों पर निर्भरता के विरुद्ध थे, आज का समय है ‘आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस‘ या रोबोट का। अब अति विकसित राष्ट्रों में ‘मशीन का आदमी‘ ( रोबोट) के निर्माण की प्रतिस्पर्द्धा मची हुयी है, जबकि गांधी जी मशीनों पर मनुष्यों के नियंत्रण के हिमायती थे। मनुष्य द्वारा निर्मित मशीन की स्वायत्ता के पक्षधर नहीं थे, लेकिन अब मशीन की स्वायत्ता या सम्प्रभुता ही सब कुछ है। अर्थात ‘मशीन का आदमी बनाम आदमी की मशीन‘ की जंग छिड़ी हुयी है। इस जंग को गांधीजी किस तरह से लेते, इसे समझना इतना सरल नहीं है।
ऐसा नहीं है, गांधी जी के जीवनकाल में उनके साथियों के साथ असहमतियां नहीं थीं।उद्योगीकरण व पश्चिमीकरण को लेकर गांधी और नेहरू के बीच मतभेद जगज़ाहिर हैं। यहां तक की सामाजिक सुधार के मामले में वे काफी संयमित थे; जातिप्रथा के तीव्र समूल नाश के पक्षधर नहीं थे, बाबा साहब आंबेडकर के साथ उनका विवाद व समझौता भी जग जाहिर है; सामंती ज़मींदारों या सामंती शक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के प्रति संकोची थे, यही दृष्टि पूंजीपतियों के मामले में थी; श्रमिक यूनियनों के प्रति भी बहुत उदार नहीं थे; सैन्य विद्रोह के पक्ष में भी नहीं थे इसलिए उन्होंने विद्रोही सैनिक चंद्रसिंह गढ़वाली को भी प्रोत्साहित नहीं किया और न ही 1946 में मुंबई में नेवल विद्रोह का समर्थन किया और न ही सशत्र क्रांतिकारियों (भगतसिंह, चंद्रशेखर आदि) की गतिविधियों का समर्थन किया, सुभाषचंद्र बोस के साथ उनके मतभेदों से सभी परिचित हैं। वे शुद्ध अहिंसावादी थे, इसलिए उन्होंने साम्यवादी क्रांतिकारियों (एमएन रॉय, डांगे, पीसी जोशी, मुज़फ्फर अहमद, राजेश्वर राव, रणदिवे आदि) का कभी समर्थन नहीं किया।
वे मुसलमानों के प्रतिनरम रहे। मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर ‘खिलाफत आंदोलन’ से जुड़े, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया जबकि कांग्रेस के अन्य नेता इसके पक्ष में नहीं थे। गांधीजी को भारत विभाजन के लिए भी ज़िम्मेदार माना जाता है। एक दफा उन्होंने घोषणा की थी कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा, लेकिन वे अपने परम शिष्यों (नेहरू व पटेल) को अपनी बात मनवाने में असफल रहे। किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और 1947 में देश का विभाजन हो गया। कातर दृष्टि से बापू विभाजन और तद्जनित विभीषिका को देखते रह गए ; कोलकाता में उनका आमरण अनशन और नौआखाली आंदोलन की तपस्या निरर्थक रही। उन पर अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण के आरोप जड़े जाते रहे जिसकी कीमत उन्हें अपने प्राणों की आहुति से चुकानी पड़ी।
गांधी जी पर अधिनायकवादी, ज़िद्दी, अराजकतावादी, पाखंडी, दकियानूसी होने के आरोप भी मढ़े जाते रहे; बुनियादी मतभेद होने के कारण सुभाष बाबू को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया; 1942 में चौरी-चौरा में हिंसा के कारण गांधीजी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जिसका तत्कालीन क्रांतिकारियों ने कड़ा विरोध किया; गांधी जी के इस फैसले की वजह से कांग्रेस में विभाजन भी हो गया- नरम दल और गरम दल (या उदारपंथी और अनुदारपंथी) बन गए। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे उनकी हठधर्मिता जाहिर होती है। उन पर व्यंग्य भी कसे जाते हैं; मज़बूरी का नाम महात्मा गांधी, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी सामने कर दो, लेकिन हिंसा से उसका प्रतिवाद न करो; गांधी जी बुजदिल-कायर -पराजित योद्धा थे।
अतः बापू को आज की बुलेट गतिमान पीढ़ी क्यों स्वीकार करे? इस पीढ़ी का आइकॉन वही हो सकता है जो लच्छेदार भाषा में अपनी हथेली पर सरसों लहलहाने और पल में अंतरिक्ष को नापने का चमत्कार दिखाने की क्षमता रखता हो। सारांश में, वर्तमान आख्यान के नायक-महानायक की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। महात्मा गांधी पूर्व और आरम्भिक औद्योगिक काल के महानायकों में से थे, अब ज़माना है उत्तर औद्योगिक व आधुनिक कालों का जिसमें उत्तर सत्य राजनीति का वर्चस्व है यानी सत्य का असत्य, असत्य का सत्य में सुविधापूर्वक रूपांतरण! इस फ्रेम में गांधीजी कभी फिट नहीं हो सकेंगे।
(जारी…)