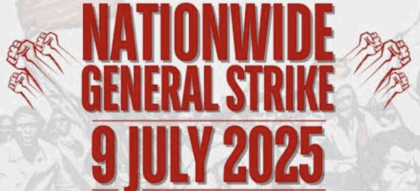अर्णब मामले में ताजी खबर यह है कि 9 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की उनकी अर्जी खारिज कर दी है, और उन्होंने सत्र न्यायालय में भी जमानत के लिए अपनी अर्जी लगाई है, जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। भले ही अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी उनके निजी व्यावसायिक लेनदेन के कारण महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस द्वारा की गई हो, पर इस गिरफ्तारी का सबसे प्रबल विरोध भाजपा द्वारा किया गया और चूंकि अर्णब गोस्वामी एक बड़े और महत्वपूर्ण पत्रकार हैं और उनकी पत्रकारिता की लाइन सत्ता समर्थक है तो, इस गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आज़ादी या प्रेस की आज़ादी पर महाराष्ट्र सरकार का हमला कह कर प्रचारित किया जा रहा है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहे वह किसी व्यक्ति की हो या समाज की या प्रेस की, यह किसी भी लोकतंत्र का बुनियादी उसूल है और इसके बिना न तो लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है और न ही लोक कल्याणकारी राज्य की तो, राज्य का उद्देश्य और दायित्व है कि वह इसे बनाए रखे और जनता का कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे। सच तो यह है कि जन अभिव्यक्ति की आज़ादी की राह, प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी के ही भरोसे सुरक्षित रह सकती है। पर इसके लिए आवश्यक है कि प्रेस जनपक्षधर पत्रकारिता की ओर हो। अर्णब के इस मुकदमे के ज़रिए अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस छिड़ती है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए, पर यह बहस सेलेक्टिव न हो और दलगत स्वार्थ से परे हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
अब यह सवाल उठता है कि आज जो लोग अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी की बात उठा रहे हैं, वह केवल अर्णब गोस्वामी के पक्ष में उठा रहे हैं या भारत के विभिन्न राज्यों में प्रेस और पत्रकारों के जो उत्पीड़न पिछले सालों में हुए हैं या अब भी हो रहे हैं, के प्रति भी उनका आक्रोश है? कम से कम 20 घटनाएं तो सरकार विरोधी खबर छापने पर यूपी में पत्रकारों के खिलाफ ही हुई हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात आदि अन्य राज्यों से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। सरकार कोई भी हो अपनी आलोचना से तिलमिलाती ज़रूर है। बस सरकार इन सब पर रिएक्ट कितना, कैसे और कब करती है यह तो सरकार की सहनशक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उसके कमिटमेंट पर निर्भर करता है।
अर्णब गोस्वामी का यह मामला, प्रथम दृष्टया, न तो पत्रकारिता के मूल्यों से जुड़ा है और न ही अभिव्यक्ति की आज़ादी का है। यह मामला, काम कराकर, किसी का पैसा दबा लेने से जुड़ा है। यह दबंगई और अपनी हैसियत के दुरुपयोग का मामला है। जब आदमी सत्ता से जुड़ जाता है तो वह अक्सर बेअंदाज़ भी हो जाता है, और यह बेअंदाज़ी, एक प्रकार की कमजरफियत भी होती है। अर्णब भी सत्ता के इसी हनक के शिकार हैं। ऐसे बेअंदाज़ लोग, यह सोच भी नहीं पाते कि धरती घूमती रहती है और सूरज डूबता भी है। वे अपने और अपने सरपरस्तों के आभा मंडल में इतने इतराये रहते हैं कि उनकी आंखे चुंधिया सी जाती हैं और रोशनी के पार जो अंधकार है, उसे देख भी नहीं पाते हैं।
आज अर्णब एक महत्वपूर्ण पत्रकार है। पर वे अपनी पत्रकारिता की एक विचित्र शैली के कारण खबरों में हैं, न कि पत्रकारिता के मूल उद्देश्य और चरित्र के कारण। उनकी शैली व्यक्तिगत हमले और वह भी तथ्यों पर कम, निजी बातों पर अधिक करने की है। रिपब्लिक टीवी हिंदी, जिसके वे चीफ एडिटर हैं, का पहला ही एपिसोड शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मृत्यु के बारे में था। इसी प्रकार जब वे पालघर भीड़ हिंसा मामले में, सोनिया गांधी पर निजी टिप्पणी कर के, सत्तारूढ़ दल से शाबाशी बटोर रहे थे, तब उसी क्रम में उनके खिलाफ विभिन्न स्थानों पर मुक़दमे दर्ज हुए। तब भी प्रेस की आज़ादी पर बहस उठी थी। इस मामले में उन्हें राहत भी सुप्रीम कोर्ट से मिली। अर्णब के इस संकट काल में जिस तरह से भारत सरकार उनके पक्ष में खड़ी है, यही इस बात का प्रमाण है कि, वे सत्ता के बेहद नज़दीक हैं।
पालघर भीड़ हिंसा रिपोर्टिंग के बाद ही उनके संबंध महाराष्ट्र राज्य सरकार से असहज हो गए। तभी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या की घटना हो गई। यह एक संदिग्ध मृत्यु की घटना थी, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, तभी पटना में सुशांत के पिता ने उनकी हत्या की आशंका को लेकर एक मुकदमा दर्ज करा दिया जो विवेचना के लिए सीबीआई को बाद में भेज दिया गया। सीबीआई ने जांच की, और अब यह निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है कि घटना आत्महत्या की ही थी। इसी में सुशांत की मित्र रिया चक्रवर्ती जो एक अभिनेत्री हैं, पर अर्णब गोस्वामी ने अपनी रिपोर्टिंग का पूरा फोकस कर दिया और लगभग रोज ही वे यह साबित करते रहे कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या हुई है और इसमें रिया का हाथ है। रिया इस मामले में महीने भर जेल में भी रहीं।
यह खबर सीरीज यदि आपने देखी होगी तो आप को स्वतः लगा होगा कि यह खबर सुशांत की आत्महत्या के बारे में कम, बल्कि हर तरह से रिया को उनकी हत्या का दोषी ठहराने के लिए जानबूझ कर कर किसी अन्य उद्देश्य की आड़ में चलाई जा रही है। इसी बीच इस मामले में उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे का भी नाम आया। जब यह नाम आया तो अर्णब की खटास महाराष्ट्र सरकार से और बढ़ गई और यह मामला अब प्रेस और सरकार के आपसी संबंधों तक ही सीमित नहीं रहा। उधर केंद्र सरकार और उद्धव सरकार के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। राजनीतिक रस्साकशी तो है ही, पर अर्णब इस रस्साकशी में एक मोहरा बन कर सामने आ गए। अब यह भूमिका उन्होंने, सायास चुनी या अनायास ही परिस्थितियां ऐसी बनती गईं कि वे और महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल आमने-सामने हो गए, यह तो अर्णब ही बता पाएंगे।
अर्णब ने यह खबर चलाई कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मुंबई पुलिस में असंतोष है। पुलिस बल में असंतोष पैदा करने के संबंध में 1922 से एक कानून है कि जो कोई भी जानबूझकर पुलिस बल में असंतोष फैलाने की कोशिश करेगा वह दंडित किया जाएगा। यह कानून, द पुलिस (इंसाइटमेंट टू दिसफ़ेक्शन) एक्ट 1922 कहलाता है। इस कानून में महाराष्ट्र सरकार ने 1983 में संशोधन कर इसे और प्रभावी बनाया है। दोषी पाए जाने पर तीन साल की अधिकतम और छह माह के कारावास की न्यूनतम सज़ा तथा अर्थदंड का प्राविधान है। अर्णब पर इसी कानून की धारा 3 के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज है। अभी इस मुकदमे की तफ्तीश चल रही है। पुलिस या किसी भी सुरक्षा बल, सेना सहित सभी बलों में असंतोष को कोई भी सरकार बेहद गंभीरता से लेती है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं।
अर्णब गोस्वामी के इस मामले में, पत्रकारिता के तमाम नैतिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस तो हो रही है पर इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि अन्वय नाइक के बिल का भुगतान हुआ था या नहीं? 2018 में पुलिस ने इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। हो सकता है तब सबूत न मिले हों या सबूतों को ढूंढा ही नहीं गया हो, या सबूतों की अनदेखी कर दी गई हो, या हर हालत में अर्णब गोस्वामी के पक्ष में ही इस मुकदमे को खत्म करने का कोई दबाव रहा हो। महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े मामलों में, समय, परिस्थितियों और उनके संपर्कों के अनुसार, मामले को निपटाने का दबाव पुलिस पर पड़ता रहता है और यह असामान्य भी नहीं है। अर्णब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ही, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है। तो क्या कल जब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी तो, सरकार का दबाव, पुलिस पर, अर्णब के पक्ष में, मुकदमा निपटाने और फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए नहीं पड़ा होगा? अब इस मामले की भी जांच चल रही है कि केस बंद कैसे किया गया।
अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें तो हमे यह भी जान लेना चाहिए कि, भीमा कोरेगांव मामले में, नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत रहने वाली सुधा भारद्वाज, कवि वरवर राव सहित कई प्रतिष्ठित नागरिक सामान्य कैदियों की तरह उसी जेल में बंद हैं, जिसमें 8 नवंबर को अर्णब को भेजा गया है। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार 83 साल के स्टेन स्वामी पार्किंसन रोग से ग्रस्त हैं, और अपनी बीमारी के कारण खुले बर्तन से तरल पदार्थ नहीं पी सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्ट्रॉ या सिपर की जरूरत होती है और अपने साथ ले गए बैग में उनका यह जरूरी सामान भी था। एक तरफ तो उन्हें उनका बैग नहीं दिया गया और इतने दिनों बाद उन्हें इसके लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी और एनआईए ने इसके लिए कई दिन का समय मांग लिया।
ऐसा ही एक मामला है गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट का। संजीव, 30 अक्तूबर 1990 में हुई, हिरासत में मृत्यु के एक मामले में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। इस समय वे नशा रखने के एक अलग मामले में भी जेल में हैं जो 1996 का है। दोनों मामले तब खुले जब संजीव भट्ट ने 2011 में गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया। इसके बाद अगस्त 2015 में उन्हें आईपीएस से निकाल दिया गया था। कार्रवाई 2011 में ही शुरू हुई थी।
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को तीन अन्य के साथ दिल्ली से हाथरस गैंगरेप मामला कवर करने जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। उसे अभी तक जमानत नहीं मिली है। बाद में उन पर यूएपीए लगा दिया गया। फिर उन्हें हाथरस साजिश मामले में भी अभियुक्त बना दिया गया। वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। इन पत्रकारों के परिवार को इनकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। केरल के पत्रकारों की यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर मांग की है कि उनकी जमानत याचिका पर जल्दी सुनवाई की जाए। इस पर शुक्रवार छह नवंबर को सुनवाई होनी थी। अब 16 नवंबर की तारीख पड़ी है।
यह सब उदाहरण यह साबित करते हैं कि सरकारें अपने विरोध और आलोचना पर असहज होती हैं और जब वे प्रतिशोध लेने पर आ जाती हैं तो लेती भी हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात पर, केंद्र सरकार के मंत्री विरोध करेंगे तो वे सारे ट्वीट अर्णब के पक्ष में करेंगे न कि इन महानुभावों के लिए। जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से ही पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। वहां के नागरिकों की कई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं जेके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। पर इनके बारे में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए सचेत रहने वाला मीडिया और पत्रकारों के संगठन न तो बोलेंगे और न ही इनकी व्यथा पर कोई चर्चा अपने कार्यक्रमों में करेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी राजनीतिक दलों के लिए एक सेलेक्टिव दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि वे पक्ष और विपक्ष, अपने एजेंडे के अनुसार तय करते हैं, पर यह दृष्टिकोण मीडिया का तो नहीं ही होना चाहिए।
अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस और पुलिस के आपसी तालमेल का। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या पत्रकारों के संगठनो को अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाए रखने का पूरा अधिकार है और यह उनका दायित्व भी है। इन संगठनों को चाहिए कि केवल खबर छापने पर कितने पत्रकार सरकारों द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, का आंकड़ा भी जारी करें। आज अर्णब की गिरफ्तारी की वे भी निंदा कर रहे हैं जिनकी सरकार ने खबर छापने पर छोटे-छोटे पत्रकारों को उत्पीड़ित किया है और उन्हें मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा है।
अभिव्यक्ति की आजादी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से एक है। दुनिया भर के कई देश अपने नागरिकों को उनके विचारों और सोच को साझा करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी की अनुमति देते हैं। भारत सरकार और अन्य कई देश अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करते हैं। ऐसा विशेष रूप से जहां-जहां लोकतांत्रिक सरकार है उन देशों में है। दुनिया भर के अधिकांश देशों के नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है। यह अधिकार उन देशों में रहने वाले लोगों को कानून द्वारा दंडित होने के डर के बिना अपने मन की बात करने के लिए सक्षम बनाता है।
अभिव्यक्ति की आजादी की अवधारणा बहुत पहले ही उत्पन्न हुई थी। इंग्लैंड ने 1689 में संवैधानिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी को अपनाया था और हमारे संविधान में यह अवधारणा वहीं से आई है। 1789 की फ्रांस क्रांति ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को एक मजबूत वैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की घोषणा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कथन यह है,
“सोच और विचारों का नि:शुल्क संचार मनुष्य के अधिकारों में सबसे अधिक मूल्यवान है। हर नागरिक तदनुसार स्वतंत्रता के साथ बोल सकता है, लिख सकता है तथा अपने शब्द छाप सकता है, लेकिन इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के लिए भी वह उसी तरह जिम्मेदार होगा जैसा कि कानून द्वारा परिभाषित किया गया है।”
मानवाधिकार, नागरिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे शब्द जितने मोहक और आशा बंधाते हैं उतनी ही दुनिया भर की सरकारों को असहज भी करते हैं, लेकिन इन सारी असहजता के बीच जनहित के मुद्दे क्यों और किस तरह उठाए जाएं, इसे भी देखना पत्रकार जमात का ही दायित्व है।
2014 के बाद भारतीय मीडिया के लिए एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है गोदी मीडिया। यानी ऐसा मीडिया जो सत्ता या सरकार की गोद में बैठा हो और ‘जो तुमको हो पसंद, वही बात करेंगे: की तर्ज पर पत्रकारिता करता हो। जब सरकार अनुकूल संगीत सुनने के नशे में आ जाती है तो वह आपनी सारी आलोचना और निंदा के प्रति, ऐसा ही दृष्टिकोण अपना लेती है जैसा कि एक प्रसिद्ध फ़िल्मी गीत में कहा गया है, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। यह मुश्किल भी ऐसी नहीं है कि केवल केंद्र की मोदी सरकार को हो रही है, बल्कि यह, रवैया देश की हर सरकारों में कमोबेश मिलेगा।
क्राइम रिपोर्टिंग को लेकर पुलिस का प्रेस से टकराव अक्सर होता रहता है। पर जिस तरह से सुशांत केस में, हमें चाहिए 302, बोलो भंडारी 302 और रिया के ड्रग मामले में ड्रग दो ड्रग दो, और मुम्बई पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कहां हो परमवीर, और मुख्यमंत्री को ललकारते हुए, कहां हो उद्धव आदि-आदि बातें कही गईं, यह किस तरह की क्राइम रिपोर्टिंग है यह मैं बिल्कुल भी नही समझ पा रहा हूं। अर्णब गोस्वामी की प्रलाप भरी पत्रकारिता और ऐंकरिंग पर मुंबई हाईकोर्ट को यह तक कहना पड़ा कि आप ही, पुलिस, जज सब बन जाएंगे तो हम यहां किस लिए बैठे है। यह एक गंभीर टिप्पणी है न केवल अर्णब गोस्वामी के लिए बल्कि उन सब के लिए भी जो ऐसी प्रलाप भरी पत्रकारिता और चीख पुकार भरी एंकरिंग के आदी हो रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को पत्रकारिता के इस बदले स्वरूप पर भी ध्यान देना चाहिए।
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर, 1948 को की गई थी। इस घोषणा के अंतर्गत यह बताया गया है कि हर किसी को अपने विचारों और राय को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के आधार के रूप में जानी जाती है। अगर निर्वाचित सरकार शुरू में स्थापित मानकों के अनुसार अपना दायित्व नहीं निभा रही हैं और नागरिकों को इससे सम्बंधित मुद्दों पर अपनी राय देने का अधिकार नहीं है तो, ऐसी सरकार और कुछ भले ही हो, वह लोकतांत्रिक सरकार तो नहीं ही है। इसीलिए, लोकतांत्रिक राष्ट्रों में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार एक अनिवार्य अधिकार है जो लोकतंत्र का मूल आधार है। अभिव्यक्ति की आजादी लोगों को अपने विचारों को साझा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन पत्रकार हो या कोई भी नागरिक, वह देश के कानून के ऊपर नहीं है। उसके किसी कृत्य से कोई अपराध हुआ है तो उससे निपटने के क़ानून के जो कायदे कानून हैं, वह सब पर लागू है।
(विजय शंकर सिंह रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं और आजकल कानपुर में रहते हैं।)