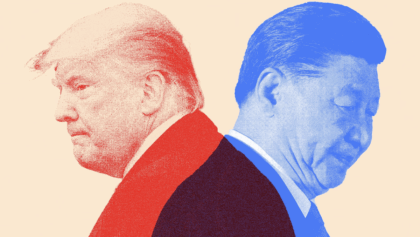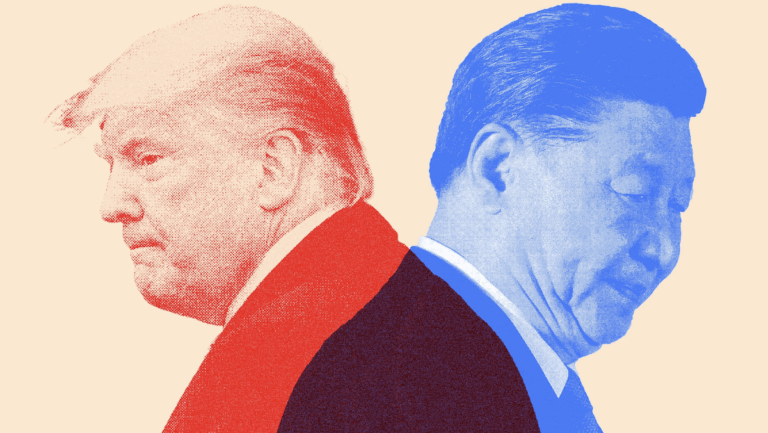केरल के कन्नूर शहर में सीपीआई (एम) की 23वीं कांग्रेस (6-10 अप्रैल 2022) पूरी भव्यता के साथ संपन्न हो गई। फिर से सीताराम येचुरी का महासचिव पद पर चुनाव और कुछ पुराने, जमे-जमाये नेताओं की विदाई और पोलित ब्यूरो में पहली बार एक दलित नेता को शामिल किया जाना इतने सरल और सीधे ढंग से हुआ कि सीताराम येचुरी ने इस कांग्रेस को पार्टी के ‘एकजुट संकल्प’ (united resolve) की कांग्रेस की संज्ञा दी। इस कांग्रेस से कुछ पुरानी दुविधाओं, बल्कि राजनीतिक कार्यनीति की ‘इसे हराओ, उसे अलग-थलग करो और वाम को जिताओ’ की द्वंद्वों की त्रिकोणीय निष्पत्ति की अजीबो-गरीब दुविधाओं से भी शायद मुक्ति पाई गई।
अब इस कांग्रेस के जरिए यह साफ कह दिया गया है कि सभी धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक शक्तियों को एक साथ इकट्ठा करके फासिस्ट आरएसएस-भाजपा की पराजय को सुनिश्चित करने और भारत के जनतंत्र और संघीय ढांचे की रक्षा करने के लिए ही आगे सभी जरूरी राजनीतिक कदम उठाने होंगे।
बहरहाल, सबसे पहले हम केरल में संपन्न हुई इस कांग्रेस के भव्य आयोजन पर ही आते हैं ।
राजनीति के जगत का यह एक मूलभूत सत्य है कि इसका एक प्रमुख लक्ष्य अनिवार्य रूप से राजसत्ता को प्राप्त करना होता है। भारत एक बहुजातीय राष्ट्र है। राजसत्ता संबंधी बारीक सैद्धांतिक तर्क के आधार पर हम भले कहें कि किसी भी राज्य सरकार में होने का अर्थ राजसत्ता पाना नहीं होता है। पर जब हम देश के संविधान और राज्य के संघीय ढांचे के प्रति आस्था रखते हैं और उनकी रक्षा को अपना कर्तव्य मानते हैं, तो इससे यह भी जाहिर होता है कि प्रकारांतर से हम यह भी मानते हैं कि किसी भी राज्य सरकार में होने का अर्थ एक हद तक राजसत्ता की शक्ति को हासिल करना भी होता है। अपनी राजनीतिक सुविधा-असुविधा की वजह से भले हम इस सच को न पूरी तरह से मानते हों, और न ही इसे पूरी तरह से अस्वीकारते हों, पर राजनीति के दैनंदिन अनुभवों में इसके प्रयोग से बखूबी परिचित होते हैं । राज्य सरकारों के जरिये भी राजनीतिक दल सामाजिक परिवर्तनों, और जनजीवन में सुधार के अपने कई अभिप्सित कामों को क्रमिक रूप में किया करते हैं ।
यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भले पार्टी कांग्रेस की तरह के अनुष्ठानों का अपने आप में कोई मायने न होता हो, पर पार्टी कार्यकर्ता के लिए ऐसे अनुष्ठानादि पार्टी की राजनीतिक लाइन से अपने को उन्नत करने के साधन हुआ करते हैं । ये एक प्रकार से ऐसे वैदिक कर्मकांड की तरह हैं जो निष्काम भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को उपनिषदों के अध्ययन का सुपात्र बनाते हैं। इनके लिए ही इन आयोजनों की प्रभावशाली भव्यता भारी महत्व रखती है। और कहना न होगा, इसमें राजसत्ता का योगदान, वह कितनी ही सीमित क्यों न हो, बहुत मायने रखता है ।
हमारी दृष्टि में केरल की यह कांग्रेस इस अर्थ में भी भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए अभी की कठिन घड़ी में बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसने आज के समय में कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति का परिचय दे कर देश भर के वामपंथियों को जरूर उत्साहित किया है।
पार्टी कांग्रेस के सुचारु और भव्य संचालन, तथा इस कांग्रेस के जरिए कुछ खास प्रकार की ‘ऐतिहासिक उलझनों’ से उबरने के लक्षणों की पहचान के साथ ही जरूरी है कि इस मौके पर ही हम अधिक ठोस रूप में इस बात को समझें कि वास्तव में आज के राजनीतिक जगत में सीपीआई(एम) खड़ी कहां है? क्या वह आज भी ऐसी जगह पर बनी हुई है कि इस जगत के उस सत्य से स्पंदित हो सके जो उसे तेज या धीमी गति से ही आगे की ओर बढ़ा सकता है, या दुनिया के दूसरे कई वामपंथी समूहों की तरह ही वह किसी ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां से अब वर्तमान राजनीतिक जगत की संरचना का सच उसे स्पर्श ही नहीं कर सकता है ! अर्थात् अब उसमें उर्ध्वगामी गति की संभावनाएँ ही नहीं बची हैं!
सीपीआई(एम) की तरह की भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन की एक सबसे प्रमुख पार्टी के संदर्भ में भी हम ऐसी चिंता इसलिए जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अतीत में इस पार्टी के इतिहास में कुछ ऐसी भयंकर अघटन की तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, जिनसे स्वाभाविक रूप में ही एक झटके में इसके राजनीति के जगत के सत्य से बहुत दूर चले जाने का खतरा पैदा हो सकता था।
सीपीआई(एम) में ऐसे खतरे का पहला संकेत सन् 1996 में देखने को मिला था जब 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पतन के बाद ज्योति बसु को विपक्ष के संयुक्त मोर्चा का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया था और उसे सीपीआई(एम) की केंद्रीय कमेटी में मामूली बहुमत के प्रयोग से ठुकरा दिया गया ।
वह एक ऐसा अवसर था जब सीपीआई(एम) को एक झटके में पूरे भारत की राजनीति के केंद्र में आ जाने का अवसर मिला था। कोई भी साधारण राजनीतिक विश्लेषक ही उससे पैदा होने वाली उन ‘असंभव संभावनाओं’ का अनुमान लगा सकता है, जिन्हें साधना ही वास्तव में राजनीति मात्र की सबसे प्रमुख विशेषता हुआ करती है । उस अवसर को गंवा कर सीपीआई(एम) ने अपने को उस भारतीय राजनीति के उस सत्य से काफी दूर कर दिया था जो उसके लिए एकबारगी, तेजी के साथ अखिल भारतीय स्तर पर फैल जाने के नए अवसर खोल सकती थी । सीपीआई(एम) के अंदर के बहुमत ने उस निर्णय के पीछे शुद्ध गैर-राजनीतिक, नौकरशाही किस्म का तर्क दिया था कि ‘पार्टी की अपनी ताकत से इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी की कोई संगति नहीं बैठती है’ । तब ज्योति बसु ने अपने नपे-तुले अंदाज में पार्टी के उस अराजनीतिक फैसले को ‘ऐतिहासिक भूल’ कहा और साथ ही यह भी कहा कि ‘अब बस छूट गई है’ । ‘बस छूटने’ का मतलब होता है, उस गति से अपने को काट लेना जो आपके लिए तेजी से आगे बढ़ने का अवसर बनाती है। जाहिर था कि आगे ऐसे मौके जब आएंगें, तब तक के समय के फासले को पाटना कहीं ज्यादा कठिन और जटिल काम हो जाएगा ।
इसके साथ ही, पार्टी अपने परंपरागत प्रभाव के तीन राज्यों, पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में, शुद्ध रूप से अपनी सांगठनिक शक्ति के बूते सीमित हो गई । गतानुगतिक सांगठनिक कामों के अलावा उसके विस्तार में राजनीतिक छलांग की भूमिका सीमित हो गई । शुद्ध सांगठनिक दैनंदिन क्रियाकलापों से पार्टी में कैसे-कैसे, मठाधीशों वाले व्यक्तिवादी वर्चस्व के रोग पैदा हो सकते हैं, इसे जानने के लिए भी बहुत गहरी विश्लेषण क्षमता की जरूरत नहीं है । सीपीआई(एम) के सर्वोच्च नेतृत्व में यहीं से बहुमतवादी तिकड़मी राजनीति का जो बीज पड़ा, उसके हाल तक के परिणामों से हम सभी परिचित हैं। उसे सीपीआई(एम) का ‘प्रकाश करातवादी दौर’ कहना गलत नहीं होगा, और उसकी छाया से आज भी सीपीआई(एम) कहां तक मुक्त हो पाई है, कहना मुश्किल है!
बहरहाल, उसके बाद, सन् 2004 में, जब लोकसभा में वामपंथियों को उनके इतिहास में सबसे अधिक सीटें मिली थीं, सीपीआई(एम) के समर्थन से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए-1 की सरकार बनी। पार्टी भारत की राजनीति के केंद्र में फिर से एक बार आई । वह सरकार भी बमुश्किल चार साल ही चल पाई कि 2008 में, अमेरिका के साथ पारमाणविक संधि के सवाल पर सीपीआई(एम) की केंद्रीय कमेटी में प्रकाश करात के नेतृत्व को हमारी राजनीति के ठोस जगत से दूर, अमेरिकी साम्राज्यवाद के विश्व-वर्चस्व की सैद्धांतिक समझ का भूत बुरी तरह से सताने लगा । दलीलें दी जाने लगीं कि यदि यह समझौता हो जाता है, तो भारत सीधे अमेरिका का पिछलग्गू एक ऐसा देश बन जायेगा जहां वामपंथ की कभी कोई संभावना शेष नहीं रहेगी । इस संधि को मानना वामपंथ के लिए आत्म-हत्या के समान होगा ।
गौर करने की बात है कि तब भी ऐतराज परमाणु संधि मात्र से नहीं था, इस बात से था कि यह संधि अमेरिका के साथ नहीं होनी चाहिए । मनमोहन सिंह ने वाम के इस दबाव को एक बेजा दबाव माना, उसे मानने से इंकार कर दिया और इसके प्रत्युत्तर में प्रकाश करात ने भी चाणक्य की तरह चुटिया बांध कर मनमोहन सरकार का सर्वनाश करने का घोषित फैसला कर लिया । वाम ने मनमोहन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और प्रकाश करात तो उसके खिलाफ सभी ताकतों को एकजुट करने की भद्दी कवायद में भी जुट गए । लेकिन उनका दुर्भाग्य कि अपनी नाक कटा कर भी वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हुए । उल्टे, स्पीकर सोमनाथ चटर्जी पर ज्योति बसु वाला फार्मूला भी नहीं चल पाया ।
आज इस दूसरे प्रकरण का सबसे मजेदार पहलू यह लगता है कि मनमोहन सिंह ने अमेरिका सहित और भी कई देशों से परमाणु संधियां कर लीं और तब से अब तक लगभग एक युग बीत गया है, लेकिन उस संधि का कोई राजनीतिक परिणाम आज तक किसी के सामने नहीं आया है। अभी तो वह संधि लगभग बेकार सी, इतिहास के कूड़े के ढेर पर पड़ी दिखाई देती है ।
पर सीपीआई(एम) के साथ इस पूरे प्रकरण का अघटन यह हुआ कि उस संधि के भूत ने सीपीआई(एम) को काट कर भारत के राजनीतिक जगत के केंद्र से निकाल कर इतनी दूर फेंक दिया कि तब से भारत के राजनीतिक जगत में सीपीआई(एम) और वामपंथ की लगातार अवनति की कहानियां ही लिखी जा रही हैं.। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे अपने शक्तिशाली राज्यों में वह अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है । केरल में उसे जरूर इस बार दुबारा जीत मिली है, पर इसका कारण कांग्रेस की दुर्दशा है, जिसके सामने सीपीआई(एम) अपने संगठन के बल पर ही भारी साबित हुई है । संगठन मात्र की जीत को राजनीति की जीत कहना हमेशा सही नहीं होता है ।
इस प्रकरण के बाद, कुल मिला कर ऐसा लगने लगा था कि जैसे भारत की राजनीति का सत्य सीपीआई(एम) से कोसों दूर चला गया है । प्रकाश करात की भाजपा-आरएसएस के फासीवादी चरित्र के प्रति दुविधा से उपजी ‘इसे हराओ, उसे अलग-थलग करो और हमें जिताओ’ वाली गड़बड़झाले वाली बहुमुखी राजनीति हवा में दफ्ती की तलवार भांजने की हास्यास्पद हरकतों से अधिक कुछ भी प्रेषित नहीं करती थी ।
बहरहाल, सीपीआई(एम) की इस सफल 23वीं कांग्रेस के सिलसिले में इसके अब तक के इतिहास के कुछ ऐसे दुखांतकारी क्षणों का स्मरण करना हमें इसलिए जरूरी लगा क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर भी आदतें अक्सर आसानी से नहीं बदला करती हैं । पार्टी कांग्रेस की तरह के गहन विश्लेषण के अनुष्ठानों का मतलब तो यही होता है कि इनसे अब तक के तमाम विषयों को खंगाल कर पार्टी के पुराने रोगों का निदान किया जाता है ।
पार्टी की इस 23वीं कांग्रेस में फिर से सीताराम येचुरी का चुना जाना और देश को बचाने के लिए निर्द्वंद्व भाव से भाजपा-आरएसएस के खिलाफ ही अपनी पूरी शक्ति को नियोजित करने का एकजुट होकर संकल्प लेना इस बात के संकेत देता है कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा बदलाव आया है जिससे पार्टी के रोग के निदान की ओर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। आज भी सीपीआई(एम) के पास केरल की सरकार है और पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में वह निःसंदेह दूसरे स्थान की बड़ी पार्टी है । इन तीन राज्यों के बल पर ही वह कांग्रेस सहित देश की सभी धर्म-निरपेक्ष और जनतांत्रिक ताकतों की पाँत में एक सम्मानजनक स्थान की हकदार हो सकती है । पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कांग्रेस के साथ उसका खुले मन से मजबूत गठबंधन उसकी पूरे देश की भाजपा-विरोधी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का आधार तैयार कर सकता है। केरल में ऐसे गठबंधन की जरूरत नहीं है क्योंकि भाजपा वहां के दृश्य से गायब है।
हमें आशा है कि इस कांग्रेस के बाद अब आगे क्रमशः एक ऐसी नई पार्टी के उभार का संकेत मिलेगा जो पार्टी को हमारे राजनीतिक जगत के केन्द्र में लाकर धर्म-निरपेक्ष और समतापूर्ण भारत के सत्य से स्पंदित होते हुए वामपंथी सोच के क्षितिज के विस्तार का कारक बनायेगी।
(अरुण माहेश्वरी लेखक और स्तंभकार हैं आप आजकल कोलकाता में रहते हैं।)