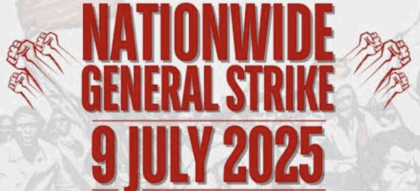15 को दलित आन्दोलन की बड़ी नेता पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन होता है। आज 2021 में अपनी आयु के 64 वर्षों को पूर्ण कर लेंगी। इस दौरान जैसा कि हम सब जानते हैं उन्होनें राजनैतिक रूप से कई उतार-चढ़ाव, सफलताएं-असफलताएं देखीं। यह राजनीति की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हर तरह की विचारधारा, राजनैतिक दल, आन्दोलन को सफलताओं-असफलताओं के उतार-चढ़ाव वाले दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब हम दलित आन्दोलन की या उसकी एक मजबूत और सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो इसका सामान्यीकरण करके नहीं छोड़ना होगा। क्योंकि दलित आन्दोलन और मायावती या उनकी बसपा जिस समुदाय का नेतृत्व करते हैं वह अन्यों की अपेक्षा अलग है।
क्योंकि दलित भारतीय समाज का वह हिस्सा है जो आज भी 21वी सदीं में तमाम तरह के सामाजिक उत्पीड़नों का शिकार होता रहता है। इसकी बानगी रोज ही अखबार की ख़बरों में मिलती रहती है। लेकिन फिर भी मायावती ने अपने गुरु कांशीराम के साथ मिलकर इस समुदाय को वह राजनैतिक पहचान दी, जिसका वह हकदार था। लेकिन 21वीं सदी में ऐसा लगता है कि दलितों ने जो अपने आंदोलनों के माध्यम से लक्ष्य 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में हासिल किये थे वह सब 21 वीं सदी की दहाई तक जाते-जाते धूमिल से होते जा रहे हैं। अगर दलित आन्दोलन की राजनैतिक सफलताओं के सन्दर्भ में बात करें तो इस दौरान दलित अन्दोलन बिखराव और जनसमर्थन जुटा पाने में असमर्थ सा हो गया है।
एक दलित आधारित दल के रूप में बसपा को ही देखें तो बिहार के विधानसभा चुनावों में चुनावी पराजय और लगातार घटते वोट बैंक में देखा जा सकता है। लेकिन यह स्थिति ऐसे ही नहीं बनी है। बल्कि इसके पीछे कई तरह के कारण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दलित आन्दोलन अपनी इस स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार है। एक आन्दोलन की मजबूत ताकत और विचारधारा के तौर पर देखें तो जहाँ एक समय में दलित आन्दोलन के मुख्य मुद्दों में दलित मुक्ति के सवालों के साथ ही रोजगार के सवाल, कृषि और किसानों के सवाल भी शामिल रहते थे लेकिन आज यह सभी सवाल दलित आन्दोलन से गायब से हो गए हैं।
इस सन्दर्भ में यदि गंभीरता के साथ देखें तो पिछली कांग्रेस और भाजपा की सरकार के दौर में रोजगार के सवाल, कृषि और किसानों के संकट के सवालों का मुद्दा एक केन्द्रीय मुद्दा बना हुआ है और सभी राजनैतिक दल इस पर कोई न कोई रुख पेश तो कर रहे हैं लेकिन वे इसे व्यापक रूप से अपने राजनैतिक सवालों से जोड़ने में नाकामयाब रहे हैं। वे यह भी नहीं बता रहे हैं कि भीषण बेरोजगारी और कृषि संकट की मार से सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? और इस समय सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हो रहा है? अलग-अलग सरकारी रिपोर्टों में रोजगार और कृषि संकट को लेकर अलग-अलग दावा किया जा रहा है। इधर, कोरोना के दौर में यह खबर भी आकर चली गयी है कि लाखों कर्मचारी और कामगार लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए।
अभी केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आन्दोलन से रोज ही खबर आ रही है कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह से इस पूरे राजनीतिक वृतांत की जो प्रक्रिया है, उसमें मजदूरों, कृषि संकट और किसानों के आधारभूत मुद्दे खत्म कर दिए गए हैं और उनकी सामजिक पहचान भी गायब कर दी गयी है। इसके साथ ही आज भारत नाम का राष्ट्र-राज्य अपनी कल्पनाओं से मजदूरों और किसानों को भुला चुका है या इसका ढोंग कर रहा है। बढ़ते हुए मध्य वर्ग और उसके हित वेतन और वेतन आयोगों तक सिमट गए हैं। भारत का नया मजदूर अब यही मध्य वर्ग हो गया है।
इधर हाल के दिनों में किसानों के जो आंदोलन हुए वो फसलों के उचित मूल्य को लेकर केंद्रित रहे। इनमें भी जमीन सुधार, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के सवाल नहीं उठाए गए हैं। तीसरे आंदोलन जो अस्मितावादी आंदोलन हैं जो समाज के कमजोर वर्गों – दलित, पिछड़े और आदिवासी- की मांगों को आगे बढ़ाते हैं। इसमें भी मुस्लिम, महिला और विमुक्त-घुमंतू समुदायों के जीवन दशाओं को सुधारने वाले आन्दोलन गायब हैं।
तो कहना यही है कि अभी एक बड़ी आबादी के जीवन को इन आंदोलनों से गायब किया गया है। यह इसलिए भी जरुरी है कि इन हिस्सों से ही भारत का मजदूर वर्ग बनता है जो फैक्ट्री से लेकर सड़क के किनारे काम करता है। मजदूरों के जो आन्दोलन हैं भी वे संगठित क्षेत्र में हैं जो संगठित रूप से ट्रेड यूनियनों द्वारा आगे बढ़ाये जाते हैं। इनमें सरकारी कर्मचारियों के संगठन, आद्योगिक मजदूर और कर्मचारी, वामपंथी ट्रेड यूनियन संगठन शामिल रहते हैं।
जबकि इधर देखा जाए तो समकालीन भारत के मजदूर वर्ग में काफी बढ़ोतरी हुई है। काम की अनिश्चितता काफी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में अनुबंध आधारित नौकरियों की बढ़ोत्तरी हुई है, जिनमें रोजगार की अनिश्चितता हमेशा ही बनी रहती है। इनमें गाँव देहात के भूमिहीन मजदूरों से लेकर निर्माण उद्योग में लगे मजदूरों के साथ ही साथ पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय नौजवान भी शामिल हैं। इस तरह से आज मजदूर वर्ग का चरित्र भी बदला है। इसमें नए समूह और लोग भी शामिल हुए हैं। लेकिन इन सबके बावजूद यह मजदूर वर्ग वामपंथी संगठनों को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में शामिल नहीं है। राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों, संकल्पपत्रों, दृष्टि दस्तावेजों को देखकर तो ऐसा ही लगता है।
लेकिन केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे आन्दोलन को देखें तो दिनों दिन अब यह व्यापक होता जा रहा है। इस आन्दोलन को सूक्ष्म तरीके से देखें तो इस आन्दोलन में कृषि और किसान सवालों के केन्द्रीय मुद्दे के साथ ही साथ ही छात्रों, नौजवानों, मजदूरों, जनता के अन्य सवाल भी शामिल किये गए हैं।
तो आज का मजदूर और किसान क्या करे, किसको देखे कहाँ जाएँ? क्या आज का मजदूर और किसान और उनके मुद्दे किसी के सवालों में हैं? किसी के संकल्पों में हैं? किसी की अपीलों में हैं? कहीं मजदूरों और किसानों की अपील करता कोई दिखता है? किसी के दृष्टि दस्तावेजों में मजदूरों किसानों के प्रति दृष्टि नजर आ रही है क्या? आज भी मजदूरों और किसानों के सवाल उन्हीं लोगों की चिंताओं में हैं जो सही मायनों में अब तक मजदूर हकों की लड़ाई लड़ते आये हैं। कम से कम वामपंथी दलों सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआई(एमएल) ने मजदूरों के सवालों को अभी भी नहीं छोड़ा है।
डॉ. अंबेडकर और दलित मुक्ति का सवाल
दलित-बहुजनों का मुक्ति आंदोलन तभी व्यापक होगा जब वह दुनिया के मुक्ति आंदोलनों के साथ अपने को जोड़ने का काम करेगा। लेकिन पिछले अनुभवों को देखकर तो यही लगता है कि इस आंदोलन ने अपने आपको व्यापक बनाने की बजाय संकुचित अधिक किया है।
दलित-बहुजनों द्वारा यह संकुचन कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है, मसलन विचार के स्तर पर, लेखन के स्तर पर और आन्दोलन के स्तर पर। कविता-कहानी उपन्यास के लेखन से ये लड़ाई लड़ी तो जा सकती है। ये सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम ही हो सकते हैं, इससे न्याय और हक की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और यह ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। इसके लिए आधारभूत स्तर पर जनांदोलन के साथ क्रियात्मक भागीदारी भी करनी होगी। लेकिन मौजूदा दौर में दलित आंदोलन और पिछड़ी राजनीति जिस तरह की राजनैतिक लाइन ले रही है वह दलित-बहुजन आन्दोलन के खिलाफ जाती है। यह उन सब समूहों के खिलाफ जाती है, जो तमाम तरह के शोषण को झेलते हैं।
इस तरह से मौजूदा किसान आन्दोलन के अवसर पर दलित और बहुजन, मुस्लिम और स्त्रियों, विमुक्त-घुमंतू और बेघरों को एक व्यापक एका लाने का संकल्प लेना चाहिए। इसे हम डॉक्टर अंबेडकर के 18 मार्च 1956 को आगरा में दिए गए एक भाषण से समझ सकते हैं। उन्होंने भूमिहीन मजदूरों के लिए कहा था कि मैं गाँव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मैं उनकी दुख तकलीफों को नजरन्दाज नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण उनका भूमिहीन होना है। इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते रहते हैं और वे अपना उत्थान नहीं कर पाते। मैं किसी भी हालात में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाले का प्रयास करूंगा।
अंबेडकर के रेडिकल पक्ष से कौन डरता है
अंबेडकर हर समय इस चिंता में रहते हैं कि लोगों के लिए कितना बेहतर कर दें, इसको पूरा करने की कोशिशों में कई बार वह समझौते करते हुये भी दिखते हैं। लेकिन अंबेडकर की बुनियादी सोच सत्ता पाने की ललक से आज के दलित नेताओं से बिल्कुल भिन्न है और बहुत दूर भी। अंबेडकर एक परिवर्तन के आकांक्षी हैं। उस परिवर्तन में जो भी मदद कर सकता है उसको वह एक उम्मीद के साथ देखते हैं। उस पर सवाल भी खड़े करते हैं। जो वह नहीं कर पाये उस पर वह चिंता भी व्यक्त करते हैं। आज के राजनेता, लेखक, बुद्धिजीवी यदि जनता के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर दें, तो यह कहते फिरते हैं कि हमने यह कर दिया वह कर दिया। लेकिन अंबेडकर हर समय उम्र के अलग-अलग पड़ाव पर ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद के साथ ही वह अपने पर ही सवाल खड़े करते है कि हम ये नहीं कर पाये जबकि आज के दौर में सिर्फ पहचान आधारित, प्रतीक आधारित, आरक्षण, संविधान लिए अंबेडकर की मूर्ति के साथ प्रतीक की राजनीति करते हुये दिखते हैं।
अंबेडकर जो नहीं कर पाये उनको उसका भी अफसोस रहता है। दलित राजनीति और परिवर्तनकामी राजनीति की दिशा होनी चाहिए थी कि ‘अंबेडकर क्या नहीं कर पाये’ वो दिशा दलित नेतृत्व, दलित आंदोलन और दलित राजनीति के साथ ही वह लोग जो परिवर्तनकामी हैं भटक गए हैं। अंबेडकर अपने अंतिम समय में यह बात कहते हैं कि खेत मजदूरों के लिए मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया तो सवाल ये है कि अंबेडकर के बाद जो लोग दलित राजनीति में आए हैं जो नेता दलित मसीहा अपने आपको कहते हैं क्या उनको इन मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए था, उन्होनें यह नहीं किया। जबकि यह सारे सवाल वामपंथी लगातार उठा रहे हैं लेकिन दलित राजनीति उनके साथ किसी प्रकार से सहयोग करना नहीं चाहती क्योंकि वामपंथी इस पहचान की प्रतीक की राजनीति से दूर हैं।
सवाल यह है कि खेत-मजदूर, भूमिहीन कौन है इनमें अधिकतम संख्या दलितों की, अति पिछड़े समुदायों की है। अंबेडकर की बुनियादी सोच जो लोग परिवर्तन की बात करते हैं उनके साथ वह सहमति जताते हैं और उनसे आशा भी करते हैं उनसे सवाल भी करते हैं। इस तरह से अंबेडकर हर समय कुछ ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अंबेडकर जो नहीं कर पाये उस पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। खेत-मजदूरों, भूमिहीनों की बात वो करते हैं। क्या अंबेडकर के बाद की राजनीति और दलित नेताओं ने इन सवालों को ठीक से एड्रेस किया है? आज अंबेडकर को आज सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें संविधान की एक किताब पकड़ाकर उनकी मूर्ति लगाकर उम्मीद यह की जा रही है की सारी समस्याएँ उनकी यह मूर्ति हल कर देगी।
आज दलित-बहुजन राजनीति के नुमाइंदों को अपने आप से सवाल पूछना होगा कि उन्होंने यह मांगें क्यों छोड़ दीं ? बात-बात में डाक्टर अंबेडकर को उद्धृत करने वाले राजनेता क्या डाक्टर अंबेडकर की उस बात को आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में कही थी। कम से कम मायावती जी के 65 वें जन्मदिन के अवसर पर यह समय उनके बारे में गुणगान और अभिनन्दन का नहीं बल्कि जिस आन्दोलन और विचारधारा का वह नेतृत्व करती हैं इस बहाने यदि इस आन्दोलन को व्यापक करना है तो उन्हें अपने को मौजूदा जन-आंदोलनों के साथ जोड़ना होगा क्योंकि इतिहास आपको जनता के मुद्दों के प्रति निभाई गई सार्थक प्रगतिशील भूमिका के साथ ही याद करेगा। न कि आपने अपना जन्मदिन किस तरह से मनाया।
(डॉ. अजय कुमार, शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में (2017-2019) फेलो रहे हैं। वह यहाँ पर समाज विज्ञानों में दलित अध्ययनों की निर्मिति परियोजना पर एक फ़ेलोशिप के तहत काम कर चुके है।)