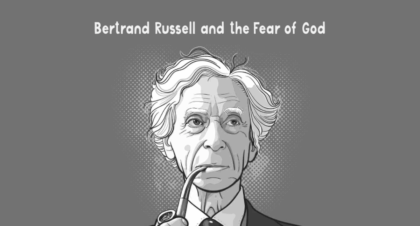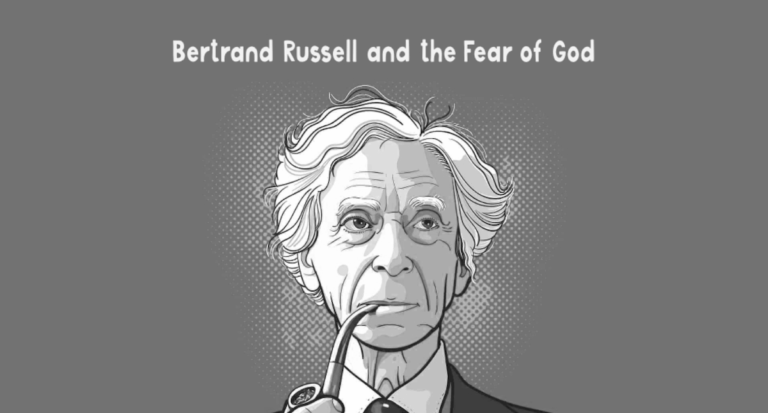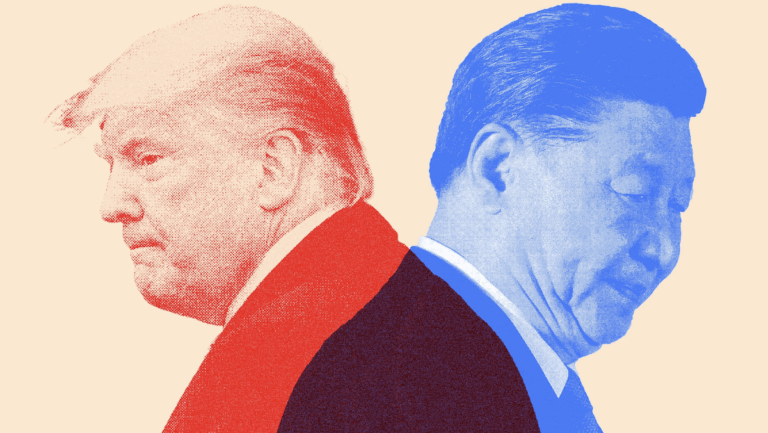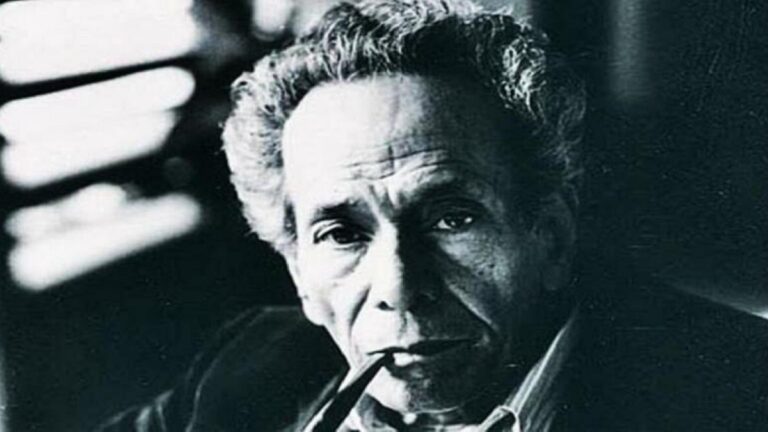जाति की तरह धर्म का मसला भी ऐसा ही उलझा है। मेरा तात्पर्य रिलीजन से है, कर्त्तव्य से नहीं। हमें हमारा धर्म जन्म से मिल जाता है। हमारे माता-पिता हमें बताते हैं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, और हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा धर्म है, वह हमारी पहचान है। हमारा अस्तित्व हमारे धर्म से है। अगर धर्म हम से छीन लिया गया तो, हमारा वजूद खतरे में पड़ जायेगा। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। यानी धर्म हमारी रक्षा करेगा और हम धर्म की रक्षा करें।
हमारे माता-पिता और हमारे वे रिश्तेदार जिनका वही धर्म है, जो हमारे माता-पिता का है, तो हम देखते हैं कि वे कुछ खास तरह की प्रार्थना और उपासना पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। जैसे-जैसे बड़े होते हैं, हम भी उनका अनुसरण करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे माता-पिता करते हैं तो सही करते होंगे। थोड़े अरसे बाद हमें यह भी समझ आ जाता है कि हमारे माता-पिता भी वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माता-पिता वैसा करते थे। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बिना सोचे-विचारे, बिना किसी तरह का सवाल उठाये धार्मिक परंपरा का पालन करते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ तर्क भी इनके पक्ष में विरासत में मिल जाते हैं। हम धार्मिक हैं क्योंकि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं।
ईश्वर में विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। ईश्वर का निर्माण किसने किया। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर सृष्टि के पहले से मौजूद था और जब सृष्टि नहीं रहेगी, तब भी ईश्वर रहेगा। प्रतिप्रश्न: आपको कैसे मालूम? उत्तर : हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है? प्रतिप्रश्न : धार्मिक ग्रंथों को किसने लिखा? उत्तर : ईश्वर ने। प्रतिप्रश्न : आपको कैसे मालूम? उत्तर : हमारे पूर्वजों ने बताया है। प्रतिप्रश्न : उन्हें किसने बताया? उत्तर : तुम कुतर्क कर रहे हो, नास्तिक हो। पापी हो। प्रतिप्रश्न : नास्तिक होना पापी होना कैसे है? उत्तर : (कुछ भी हो सकता है, डांटने से लेकर, थप्पड़ मारने तक)।इस तरह के सवाल जवाब आमतौर पर घरों में नहीं होते क्योंकि प्रश्न पूछने की परंपरा अपवाद रूप में ही मिलती है।
हमारे घर में दो धर्मों का पालन होता था। पुरुष वैष्णव धर्म का पालन करते थे और स्त्रियां जैन धर्म का इसकी वजह यह थी कि मेरे दादा-परदादा के घर की परंपरा वैष्णव धर्म की पालन की थी जबकि हमारे घर में जो बहुएं बनकर आयीं वे सब उन परिवारों से थीं जो जैन धर्म के अनुयायी थे। हालांकि सबकी जाति एक ही थी, ओसवाल। विवाह के लिए धर्म नहीं जाति महत्वपूर्ण होती है और वैसे भी जैन धर्म मानने वालों का काफी हद तक हिंदुइकरण हो चुका था। वे अपनी पहचान हिंदू धर्म में विलीन कर चुके थे और उसीके अनुरूप वर्णव्यवस्था और जातिवाद को पूरी तरह स्वीकार कर चुके थे। इसलिए एक ही घर में जैन और वैष्णव धर्म का सहअस्तित्व हिंदू धर्म की छत्रछाया में ही संभव हो रहा था। इसलिए अपनी-अपनी पूजा-पद्धतियों का पालन भी बिना किसी टकराव के संभव हो रहा था।
मेरे पिता सुबह नहा-धोकर कृष्ण के बाल रूप की कांस्य की छोटी-सी मूर्ति के सामने पूजा करते थे। पहले मूर्ति को नहला-धुलाकर उन्हें वस्त्र पहनाते थे। फिर उनके पास अगरबत्ती लगाते थे। इस पूरे समय में गीता-रामचरितमानस के अंश का पाठ करते रहते थे, जो उन्हें कंठस्थ थे। उस समय कटोरी में दूध रखकर भगवान को भोग लगाते थे और फिर उसे पी लेते थे। यह उनका नाश्ता होता था। फिर घर के सामने बने मंदिर में जाते थे। पाठ उनका चलता रहता था। गीता का एक अध्याय का पाठ वे रोजाना करते थे। मंदिर में ही थोड़ी देर अखबार भी पढ़ते थे। कभी-कभार महंत जी या और किसी परिचित से बातचीत करते थे। फिर घर आते। तब तक हमारी माताजी भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन तैयार कर चुकी होती थी।
एक थाली में भोजन रखकर भगवान के सामने भोग लगाया जाता था। भोग लगाने की विधि यह थी कि थाली में रखी भोजन सामग्री में तुलसी के एक-एक पत्ते डाल दिये जाते थे। फिर पर्दा लगाया जाता था, ताकि भगवान को भोग अरोगते वक्त कोई देखे नहीं। बाद में थाली हटा ली जाती थी। और उसके बाद पिताजी आरती करते थे। ‘ओम जय जगदीश हरे’। लगाया गया भोग ही पिताजी का भोजन होता था। उसी में भूख के अनुसार और रोटी और सब्जी ले लेते थे। दिलचस्प यह था कि रोजाना होने वाली इस आरती के समय परिवार का कोई सदस्य खड़ा नहीं होता था। दिलचस्प यह भी था कि भगवान को भोग एक ही बार लगाया जाता था। दोपहर और शाम को बालगोपाल को भूखा ही रहना पड़ता था।
जिस समय पिताजी पूजा-अर्चना करते थे, उसी समय मेरे तीनों चाचा भी नहा-धोकर हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और गीता के कुछ अंशों या कुछ भजनों का पाठ अपने-अपने टाइम टेबल के अनुसार करते थे। मेरे दादा थोड़ी देर माला फेरते थे और मंदिर जाते थे। उन्हें रोजाना नहाना पसंद नहीं था, इसलिए वे थोड़े में ही काम निपटा लेते थे। दादा-दादी और छोटे बच्चों को छोड़कर घर के सभी सदस्य पूनम का व्रत रखते थे। पूनम के दिन दोपहर को तीन चार बजे हमारे पिताजी सत्यनारायण की एक तस्वीर के सामने सत्यनारायण की कथा बांचते थे। उस समय जो भी मौजूद होता, वह बैठकर शांति से कथा सुनता था। फिर बाज़ार से लायी गयी थोड़ी सी मिठाई का भोग लगाया जाता था और सत्यनारायण की आरती की जाती थी।
इसके बाद प्रसाद सभी में बांट दिया जाता था। कथा खत्म होने के बाद एक बात पिताजी हमेशा कहते थे कि स्कंद पुराणे रेवाखंडे से शुरू होने वाली इस सत्यनारायण की कथा में कथा कहां है? यह तो कथा का महात्म्य है। यह पता नहीं लगता था कि वे हमसे पूछ रहे हैं, या खुद से। लेकिन कथा बांचने का यह क्रम सालों-साल चलता रहा। मूल प्रश्न वहीं का वहीं बना रहा। सत्यनारायण का व्रत और कथा पिताजी ने बुढ़ापे में बंद कर दी। सत्यनारायण की कथा सुनकर धीरे-धीरे मुझे पूरी कथा बड़ी विचित्र लगने लगी। मैंने कई बार कहा भी कि सत्यनारायण भगवान कम दारोगा ज्यादा लगते हैं। हर समय डराते-धमकाते रहते हैं, सजा देते हैं। दिलचस्प यह भी था कि मेरी इस बात पर कोई टोकता नहीं था।
पिताजी को रोजाना पूजा-पाठ करने के संस्कार अपने पिता से नहीं दादा से मिला था। दादा जी यानी मेरे परदादा जी अपने पुत्र यानी मेरे दादाजी में वे संस्कार नहीं डाल पाये। पिताजी ने अपने दादा के प्रभाव में आकर गैर ब्राह्मण होकर भी जनेऊ धारण कर ली थी और सिर पर चोटी भी रखते थे। लेकिन घर में किसी और ने उनका अनुकरण नहीं किया। उन्होंने ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं किया। लेकिन पूरी ज़िंदगी वे इन दोनों को धारण किये रहे। हम देखते थे कि पिताजी जब जब भी शौच (लघु शंका और दीर्घ शंका निवारण) से निवृत्त होने के लिए जाते थे, तब जनेऊ को कान पर लपेट लेते थे। मैंने उनसे पूछा भी कान पर लपेटने से क्या होता है? उन्होंने कहा, पता नहीं। तब लपेटते क्यों हैं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन वे जनेऊ से जुड़ी परंपराओं का पालन करते रहे। जीवन के अंतिम क्षण तक।
मेरी दादी, मां, चाची सुबह ही सुबह नहीं नहाती थी। जैन धर्म में स्नान करना धर्म का अंग नहीं है। मां और सभी चाची पूनम का व्रत जरूर करती थीं। बाकी सब-कुछ जैन धर्म के अनुसार करती थीं और लगभग रोज अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार 50-50 मिनट की एक या दो सामयिकी करती थीं जो किसी भी समय की जा सकती थीं। लेकिन आमतौर पर सुबह ही सुबह एक सामयिकी करने का चलन था। सामयिकी में मुंह पर (आजकल प्रचलित मास्क की तरह) कपड़ा बांधकर जिसे मुहंपट्टी कह सकते हैं, एक आसन पर बैठकर नवकार मंत्र का जाप करना होता है। कपड़ा इसलिए बांधा जाता है कि मुहं में कीड़ा न घूसे और वह मर न जाये। उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हम होंगे और उसकी हत्या का दोष हमें लगेगा।
जैन साधु इसीलिए नंगे पांव चलते हैं क्योंकि नंगे पांव चलने से उनके पैरों के नीचे आकर कीड़े-मकोड़े कम मरेंगे और जीवहत्या का दोष कम लगेगा। सामयिकी करने के लिए नियमित रूप से सुबह नहाना जरूरी नहीं था। इसलिए दादी, मां, चाची आमतौर पर दोपहर या रात को नहाती थी। महीने के कुछ दिन रात को नहीं खाती थीं। पूरे चतुर्मास में रात को नहीं खाती थीं। उन दिनों जैन साधु जिनका चतुर्मास शहर में होता था, जैन स्थानकों में सुबह के समय व्याख्यान देते। जिसे सुनने के लिए जैन स्त्री-पुरुष बड़ी संख्या में पहुंचते। मेरी दादी, मां और चाचियां जाती थीं, लेकिन तब जब बच्चे बड़े हो चुके होते थे। कभी हमने अपने परिवार के किसी पुरुष को, लड़कों को या लड़कियों को व्याख्यान सुनने जाते नहीं देखा।
जब मैं बहुत छोटा था, तब मुझे याद है कि मैं अपनी दादी और मां के साथ दोपहर को होने वाले व्याख्यान को सुनने जाया करता था। दोपहर को जैन साधु (या साध्वियां) उपदेश नहीं देते थे, बल्कि कथावाचक की तरह कथा बांचते थे। प्राकृत, अपभ्रंश में लिखे गये काव्य का हिंदी अनुवाद बहुत रोचक ढंग से सुनाते थे। जब मैं सुनने गया तब ‘भविष्यत्तकहा’ (भविष्यदत्तकथा) सुनायी जा रही थी, जो दो भाइयों बंधुदत्त और भविष्यदत्त की कहानी थी। वह बहुत ही रोचक कहानी थी। अब भी उस सुने हुए के मन में बने कुछ बिंब याद है। जहाज से लौटते हुए बंधुदत्त अपने भाई को एक द्वीप पर छोड़ देता है। वह द्वीप बहुत ही धनधान्य से भरा है लेकिन वहां कोई इंसान नज़र नहीं आता।सड़कें सुनसान पड़ी है। दुकानें खुली हैं, लेकिन न कोई खरीदने वाला है और न बेचने वाला। सारे घर भी बंद है। भविष्यदत्त की यह कहानी बाद में इच्छा होते हुए भी पढ़ नहीं पाया।
हम लड़के अपने पिता और चाचा का अनुकरण करते थे और लड़कियों से अपेक्षा की जाती थीं कि वे अपनी माताओं का अनुकरण करेंगी। लेकिन बच्चों पर कोई दबाव नहीं था। मैंने किशोर अवस्था में अपने पिता और चाचा का अनुकरण करते हुए नियमित रूप से नहाना और हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना शुरू कर दिया। मंदिर जाने लगा। शायद कॉलेज जाने तक यह सब किया। फिर धीरे-धीरे ऊब होने लगी। बंधन महसूस होने लगा। शुरू में नहा-धोकर और कपड़े बदलकर पाठ करता था। बाद में, नहाना शुरू करते ही पाठ शुरू कर देता था और कई बार पूरी तरह तैयार होने तक पाठ खत्म हो जाता था।
पाठ्यपुस्तकों से अलग पुस्तकें पढ़ने की आदत के कारण धर्म और ईश्वर को लेकर जो मंथन चल रहा था, उसका नतीजा निकला कॉलेज पहुंचते-पहुंचते नियमित पूजा-पाठ करना बंद कर दिया। मंदिर जाना भी धीरे-धीरे बंद हो गया। पूनम का उपवास भी छूट गया। नियमित पाठ के लिए जो नियमित नहाना आरंभ किया वही जारी रहा और आज भी जारी है जिसमें दसवीं के बाद नियमित शेविंग जुड़ गयी थी। आज भी पढ़ना-लिखना नहाने के बाद ही आरंभ करता हूं। अखबार भी तैयार होकर ही पढ़ता हूं। चाय जरूर सुबह उठते ही पीता हूं। हां, मोबाइल भी अपवाद है जो कभी भी और कहीं भी देखा जा सकता है।
आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह साफ हो जाता है कि धर्म संबंधी जो भी पूजा-पाठ, व्रत-उपवास करता था, वह घर वालों का अनुकरण करते हुए करता था। मैं स्वत: ही मानता चला गया कि मैं हिंदू (और शायद जैन भी) हूं और आस्तिक भी हूं। मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं। हिंदू हूं क्योंकि ईसाई नहीं हूं। मैं हिंदू हूं क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बताया जाता रहा कि हम हिंदू हैं। लेकिन क्यों? अगर मैं हिंदू या जैन नहीं होता तो मुसलमान होता। अगर मुसलमान भी नहीं होता, तो ईसाई होता, ईसाई नहीं तो, बौद्ध होता। यानी कि मैं इंसान हूं तो मेरा कोई धर्म तो होगा ही। क्यों होगा ही? क्या इंसान होना पर्याप्त नहीं है। मैंने तय नहीं किया था कि मैं ऐसे जैन परिवार में पैदा होऊंगा, जहां के पुरुष हिंदू धर्म का पालन करते हैं। जोधपुर में ऐसे बहुत से परिवार थे जिनमें हिंदू और जैन दोनों धर्मों का पालन होता था।
परिवार के लगभग सभी सदस्यों की धर्म के प्रति निष्ठा काफी मजबूत थी। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर धर्म बहुत सीमित अर्थ में लिया गया था। धर्म का अर्थ था, पूजा-पाठ, कुछ विशेष अवसरों पर व्रत और उपवास, शाकाहारी भोजन, नियमित मंदिर जाना। परदादा ने 1930 के आसपास किसी समय ‘कल्याण’ पत्रिका मंगानी शुरु की थी जो पिता और चाचा लगातार मंगाते रहे। पिता, चाचा कभी-कभार उलट-पलट कर देख लेते थे, लेकिन पढ़ता कोई नहीं था। परदादा ने इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा हो तो मालूम नहीं। लेकिन बाद की पीढ़ी में तो मैंने ही सबसे ज्यादा अध्ययन किया।
अच्छी बात यह थी कि जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनकी आस्था बनी रही। धार्मिक पत्रिका होने के कारण बेचा भी नहीं जाता था। साल में एकबार निकलने वाले विशेषांक में ज्यादातर पुराणादि के हिंदी अनुवाद प्रकाशित होते थे। मैंने उन्हीं में वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रामचरित मानस, बहुत से उपनिषद और पुराण पढ़े। ‘कल्याण’ पत्रिका पढ़ने वाले ज्यादातर सवर्ण हिंदू होते हैं। ‘कल्याण’ का पाठक सांप्रदायिक हो या न हो, लेकिन घोर रूढ़िवादी, जातिवादी, धार्मिक तत्ववादी होता है। वह छुआछूत में यकीन करता है। दलितों और स्त्रियां की समानता और स्वतंत्रता का विरोधी होता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर अंधश्रद्धा रखता है। गीताप्रेस से प्रकाशित कुछ पुस्तकें भी थीं, उन्हें भी मैंने पढ़ा था।
उसमें एक स्वामी करपात्रीजी की पुस्तक ‘मार्क्सवाद और रामराज्य’ भी थी। करपात्री जी घोर ब्राह्मणवादी थे और स्वतंत्र भारत में मनु स्मृति को लागू करने के पक्ष में थे। उन्होंने रामराज्य परिषद नामक राजनीतिक दल भी बनाया था। मैंने उनकी यह पुस्तक पूरी पढ़ी थी। तब तक मैं धार्मिक पुस्तकों के प्रभाव में भी था। किताब दिलचस्प थी। मार्क्सवाद का जवाब तर्क से नहीं बल्कि हिंदू धर्मशास्त्रों से दिया गया था। यह मानकर चला गया था कि शास्त्रों में जो लिखा है, उसके गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए यह कह देना काफी है कि हिंदू धर्म ग्रंथ में जो लिखा है, वह शाश्वत सत्य है क्योंकि वह स्वयं ईश्वर की वाणी है। बाद में मैंने इस पुस्तक की राहुल सांकृत्यायन की लिखी विस्तृत समीक्षा पढ़ी थी, जिसे पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया था।
नवरात्रि में घर में रामचरितमानस का नौ दिन पाठ होता था। ज्यादातर मेरे पिताजी नहा-धोकर सुबह दो-ढाई घंटे पाठ करते थे। गीताप्रेस ने रामचरितमानस का इस तरह आंतरिक विभाजन कर रखा था कि अगर नौ दिन पढना हो तो उसमें यह प्रकाशित होता था कि पहले दिन कहां तक पढ़ना है और दूसरे दिन कहां तक। इसी तरह एक महीने तक पढ़ना है, तो विभाजन तीस दिन के हिसाब से होता था। पाठ की शुरुआत और अंत के समय धार्मिक विधि का पालन किया जाता था। मानस की जिस प्रति से पाठ किया जाता था, उसके लगभग हर पृष्ठ पर चंदन के छींटे और तुलसी के पत्ते होते थे। हर दिन पाठ समाप्त होने पर ‘मानस’ की आरती उतारी जाती थी। रामचरितमानस भले ही कुछ लोगों के लिए साहित्यिक रचना हो, हमारे यहां तो वह धार्मिक पुस्तक थी, जिसका विधि-विधानानुसार पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मेरा मानान है कि ज्यादातर सवर्ण हिंदुओं के लिए धार्मिक पुस्तक थी, एक तरह की पुराण।
धर्म परिवार के प्रत्येक परंपरागत क्रियाकलापों में मौजूद था। पिताजी या चाचाओं को शहर से बाहर जाना होता था, तब यह ध्यान रखा जाता था कि यात्रा निषेध वाले दिन न की जाये। मसलन, बुधवार को यात्रा करना अशुभ माना जाता था, इसलिए बुधवार के दिन घर नहीं छोड़ते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि बुधवार के दिन जाना ज़रूरी होता था, तब एक दिन पहले यात्रा में साथ ले जाने वाले कपड़े किसी पड़ोसी के घर पर रखे जाते थे और यात्रा के दिन उन्हीं कपड़ों को साथ ले जाते थे। यह मान लिया जाता था कि इस तरह अशुभ दिन यात्रा के प्रकोप से बचा जा सकेगा। मालूम नहीं यह अपने आपको धोखा देना होता था या उस देवता को जिस के प्रकोप से बचने के लिए बुधवार को यात्रा नहीं की जाती थी। इस अंधविश्वास का रोचक पहलू यह था कि जब मैं अमरोहा में था, तब जोधपुर जाने-आने का रेल आरक्षण बुधवार को कराता था क्योंकि बुधवार के दिन आरक्षण आसानी से मिल जाता था। भीड़ कम होती थी।
परिवार के लगभग सभी बड़ों में यह विश्वास गहरे तक धंसा हुआ था कि अगर कोई संकट आये या भगवान से किसी विशेष पक्षपात की जरूरत हो और भगवान को प्रसाद चढ़ाने, मंदिर में जाकर दर्शन करने या व्रत-उपवास रखने का आश्वासन पहले से दे दिया जाये यानी बोलवा बोल दी जाये तो, निश्चय ही वह संकट दूर हो जाता है या आपका काम आपके पक्ष में हो जाता है। परीक्षा में अच्छे नंबंरों से पास होने से लेकर नौकरी लगने तक, घर की कोई चीज इधर-उधर रखकर भूल जाने, छोटी-बड़ी बीमारी हो जाने या कोई भी मामूली से लेकर गैरमामूली संकट या लाभ पर घर के ठाकुर जी से लेकर घर के सामने वाले मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की घोषणा कर दी जाती थी।
यह सवा रुपये से लेकर सवा सौ रुपये तक या उससे भी ज्यादा की बोलवा बोली जाती थी। यह इस पर निर्भर करता था कि संकट दूर न होने पर कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर नुकसान दस रुपये के बराबर है, तो बोलवा सवा रूपये के बराबर काफी समझी जाती थी। अगर लाभ बहुत बड़ा है, तो प्रसाद भी उसी अनुपात में बड़ा होगा। अगर जीवन-मरण का सवाल होता तो फिर नुकसान की कीमत नहीं आंकी जाती थी बल्कि अपनी हैसियत देखी जाती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। ऐसे में व्रत उपवास से लेकर ब्राह्मणों को भोज खिलाने या तीर्थयात्रा करने की बोलवा बोली जाती थीं। बोलवा बोलने से आपका काम हो जायेगा और आप संकट मुक्त हो जायेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। यह विश्वास था और ईश्वर, देवी-देवता आपकी नहीं सुनता तो भी विश्वास बना ही रहता था। मेरे जैसों के साथ यह था कि जब ईश्वर पर ही विश्वास नहीं रहा, तो उनकी इस शक्ति पर कैसे विश्वास बनाये रखता। हां, ईश्वर की इस शक्ति और दया पर अब भी विस्तृत परिवार में बहुतों का विश्वास बचा हुआ है, इसलिए बोलवा बोलने का चलन अब भी कायम है।
बचपन में घर से निकलते हुए इस बात पर बहुत टोका-टोकी होती थी कि सामने से कौन आ रहा है। अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है, कोई दूध लेकर आ रहा है, या कोई छींक देता है, तो ऐसे समय कुछ देर रुककर घर से निकलना शुभ रहता है। इसी तरह दही या गुड़ खाकर निकलना या सामने से गाय का आना शुभ रहता है। ये तो कुछ उदाहरण है। ऐसी बहुत सी शुभ और अशुभ चीजें हैं जो घर से निकलने पर आपका काम बना या बिगाड़ सकती है। ये सब बातें इतनी ज्यादा हमारे दिमागों में भर दी गयी थी कि वे ज़िंदगी का सहज हिस्सा हो गया था। बिना कोई प्रश्न उठाये उनका पालन करते रहते थे। बिल्ली देखते ही पांव अपने-आप रुक जाते थे। छींक आते ही या सुनते ही वापस लौट आते और कुछ देर बाद ही वापस निकलते थे।
मेरी मां अपने गले में छींक माता लिखा एक सोने का एक सेंटीमीटर नाप का गोल सिक्का पहनती है जिसे मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। जब इन बातों पर यकीन खत्म हुआ उसके बाद भी बिल्ली के रास्ता काटने पर पैर एक बार रुक जाते थे और अंदर से साहस बटोर कर आगे बढ़ना पड़ता था। धीरे-धीरे यह समझ आया कि जिसे बिल्ली का रास्ता काटना कहते हैं, वह दरअसल बिल्ली के खुद के डर की अभिव्यक्ति है। बिल्ली सड़क पर या गली में जब गुजरती है, तो कुत्तों से डरी रहती है और वह तब तक एक ही तरफ चलती रहती है, जब तक उसे दूसरी तरफ नहीं जाना होता, ताकि अगर कुत्ते नज़र आये तो वह जल्दी से किसी न किसी घर में घुस कर अपनी जान बचाले। और जब बिल्ली को दूसरी तरफ जाना होता तो वह बहुत चौकन्नी होकर चारों तरफ देखकर सड़क पार करती है।
एक बार ठीक ऐसा ही हुआ। घर के सामने के मंदिर के महंत जी ने एक बिल्ली पाल रखी थी। वह न केवल महंत जी से बल्कि मंदिर में आने वाले सभी लोगों से घुली-मिली थी। लेकिन एक बार सर्दी की रात में न जाने कैसे वह मंदिर से बाहर रह गयी। महंत जी ने समझा वह मंदिर में अपनी कोठरी में ही है। जब वह रात को मंदिर की तरफ जाने लगी तो गली के कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। मंदिर और आसपास के घरों के दरवाजे बंद थे। कुत्तों की तेज-तेज भौंकने की आवाज़ में बिल्ली की डरी-सहमी म्याउं म्याउं किसी ने नहीं सुनी।वह अपने को बचा नहीं सकी और कुत्तों ने उसे तभी छोड़ा जब वह बुरी तरह घायल हो गयी। घायल अवस्था में वह मंदिर के दरवाजे के पास बेहोश सी पड़ी थी।
महंत जी ने जब सुबह उसे इस अवस्था में देखा तो बहुत दुखी हुए। उसे बचाने की हर संभव कोशिश की लेकिन वह एक-दो दिन में मर गयी। उस बिल्ली के रास्ते काटने से किसी का नुकसान हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन मंदिर और घरों के दरवाजे बंद होने ने उसकी जान जरूर ले ली। मंदिर में, सीधे भगवान की शरण में रहने वाली उस बिल्ली को कोई नहीं बचा सका। भगवान भी नहीं।
भारत में धर्म लोगों को दार्शनिक भी बना देता है। मसलन, हिंदू यह मानकर चलता है कि जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए वह यह मानकर चलता है कि इस जन्म में मैं जो दुख उठा रहा हूं, वह इसलिए कि मैंने पिछले जन्म में पाप किये थे। और जो आज सुख भोग रहे हैं, वह इसलिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किये थे।यही नहीं यह भी विश्वास करते हैं कि शुभ कर्म करने पर अगले जन्म में उच्च जाति में पैदा होंगे और अशुभ कर्म करने पर निम्नजाति में। नतीजा यह होता है कि कर्मफल और जन्म-जन्मांतर में विश्वास उन्हें ऐसा भाग्यवादी बना देता है जो किसी तरह के बदलाव के लिए प्रयत्न करने की इच्छा को ही समाप्त कर देता है।
लेकिन उनका यह विश्वास भी आधा-अधूरा होता है। अगर वह इन दो सिद्धांतों में विश्वास करे तो फिर उसे किसी और बात में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जीवन में जो कुछ होता जाये उसे अपने कर्मों का फल मानकर सहता जाये और कोशिश करे कि कम से कम इस जन्म में कोई ऐसा काम न करे जो पाप की श्रेणी में आता हो। लेकिन हिंदू इसके साथ उन बातों में भी यकीन करता है, जो उपर्युक्त सिद्धांतों के विपरीत हैं। वह इस बात में भी यकीन करता है कि जिस घड़ी जन्म हुआ है, उस घड़ी ने उसका भाग्य निश्चित कर दिया है। उस घड़ी ने राशि तय कर दी और उससे जन्मपत्री बन जाती है।
अब जन्मपत्री समय-समय पर बताती रहती है कि जीवन में कौन से सुख आयेंगे, कौन से दुख आयेंगे। कौन सा काम कब करना होगा। किस लड़के या लड़की से शादी करनी होगी। कितनी लंबी उम्र होगी। इस तरह जन्म की घड़ी आपके भाग्य की निर्णायक हो जाती है। जन्म की इस घड़ी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए समृद्ध हिंदू परिवारों में यह चलन बढ़ता जा रहा है कि बच्चे का जन्म ठीक उसी मुहूर्त में हो जो ज्योतिष के अनुसार सर्वाधिक शुभ हो। डॉक्टर को पहले ही बता दिया जाता है कि ठीक इस तारीख को, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सैकंड में हमारे घर की बहू को बच्चा होना चाहिए। जाहिर है कि इस हद तक नियंत्रित बच्चा तो सिजेरियन ही होगा और इसका नकारात्मक असर बहू के स्वास्थ्य पर भी पड़े तो इसकी कैन परवाह करता है, शायद खुद बहू भी नहीं।
भविष्य जानने की ललक का नतीजा है कि भविष्य बताना एक बहुधंधी व्यवसाय हो गया है। हाथ की रेखायें दिखायी जाती है और लोग बड़े भोलेपन से इस बात में यकीन कर लेते हैं कि हाथ की रेखाओं में हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य लिखा हुआ है। भविष्य बताने के ऐसे कई धंधे बड़े मजे से फल-फूल रहे हैं। अभी एक विज्ञापन देखा जिसमें ज्योतिषी ने दावा किया था कि वह केवल अंगूठा देखकर बता सकता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। भविष्यवक्ता जो भी बताता है, वह अगर सही नहीं निकलता है तो भी, लोगों का यकीन नहीं डगमगाता। भविष्य जानने की ललक में लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं। जिसके जीवन में जितनी ज्यादा अनिश्चितता होती है, वह उतना ही ज्योतिषियों के पीछे दौड़ता है। इन सबके बीच भाग्यवादी इस बात में भी यकीन करते हैं कि गंगा नहाने, व्रत-उपवास करने, पूजा-पाठ करने, तीर्थयात्रा करने, किसी खास मुहुर्त या दिन में कोई खास काम करने से पुण्य मिलता है, मोक्ष प्राप्त होता है और संकट दूर होता है।
इन सबमें विश्वास के बावजूद भी धार्मिक आस्था कुछ सावधानियों के साथ ही पालन की जाती है। अगर किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आपकी उम्र अस्सी साल होगी, तब भी कोई सड़क के बीच में नहीं चलने का खतरा नहीं उठाता। या बीमार पड़ने पर इलाज कराने से इन्कार करता है। परीक्षा में प्रथम श्रेणी की भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिष विद्यार्थी को यह सलाह कभी नहीं देता कि पढ़ाई छोड़कर आराम करो या परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। भाग्य तुम्हें अपने आप पास करायेगा। मेरा मानना है कि इन सब अंधविश्वासों से अपने आप को मुक्त करना आसान काम नहीं है।
धर्म के नाम पर ये अंधविश्वास हमारे अंदर इतनी गहराई तक धंसे हुए हैं कि विश्चविद्यालय में विज्ञान पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी अपनी बेटे-बेटी का विवाह जन्मपत्री मिलाकर तय करते हैं। धर्म की इस जकड़न के कारण वह अपने सवर्ण होने पर गर्व करता है, दलित से नफ़रत करता है और मुसलमान से घृणा। जिसे वैज्ञानिक मानसिकता कहते हैं, उसे वे अपने नज़दीक भी नहीं फटकने देते। विडंबना यह है कि यह धर्मांधता पिछड़ों में भी है, दलितों में भी है और धार्मिक अल्पसंख्यकों में भी। क्योंकि सामाजिक श्रेणीबद्धता में जो जहां है, उसे नफरत और घृणा करने के लिए अपने से नीचे लोग नज़र आ ही जाते हैं। गैरबराबरी को कायम रखना जिन राजसत्ताओं के हित में होता है, उनके लिए धर्म सबसे उपयोगी अवधारणा भी है और संस्थान भी।
(जवरीमल्ल पारख सेवानिवृत प्रोफेसर हैं।)