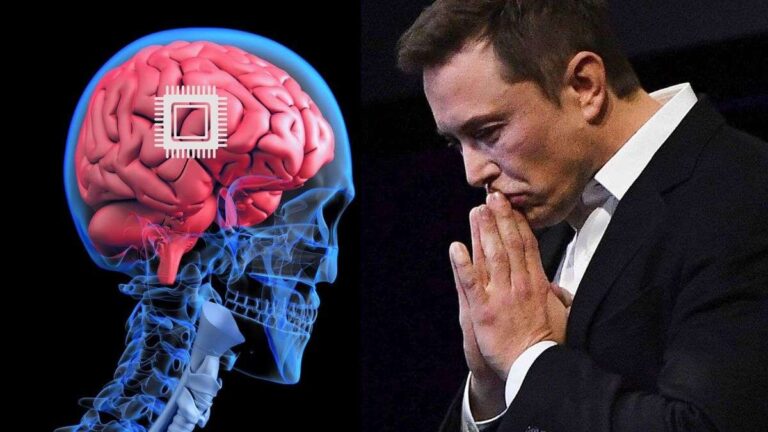(गुरु पूर्णिमा के मौके पर चैतन्य नागर का आया यह लेख किन्हीं कारणों से प्रकाशित होने से रह गया था। लेकिन लेख अच्छा है इसलिए मौका बीत जाने के बाद इसे प्रकाशित किया जा रहा है-संपादक)
दो दिन पहले गुरु पूर्णिमा मनाई गयी। गुरु की महिमा गाने में सभी प्रमुख धर्मों के बीच एक तरह की होड़ सी लगी हुई है। तकरीबन हर धर्म यह कहता है कि गुरु में भरोसा रख कर एक साधारण आदमी अपने सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सनातन धर्म को मानने वाले गुरु को कहीं-कहीं ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, तो ईसाइयत भी यह मानती है कि उनके संस्थापक में पूरा भरोसा हो तो मन का अंधकार हमेशा के लिए दूर हो सकता है। इस्लाम के हिसाब से तो पैगम्बर ने जो कह दिया, 1400 साल पहले, उसके बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल ही करने की जरूरत ही नहीं! बौद्ध धर्म ने तो हद कर दी भाई! अपनी रोशनी खुद बनने की सलाह देने वाले बुद्ध की पूजा तो करते ही हैं, कई लामा भी रॉक स्टार जैसे बन गए हैं। दलाई लामा के दर्शन के लिए, उनके पूजा पाठ में हिस्सा लेने के लिए अनुयायी हाहाकार मचा देते हैं। राजनीति, खेल, संगीत-ऐसा कोई इलाका नहीं जहां गुरुबाजी की तबाही न मची हुई हो।
इन दिनों टीवी पर भी तथाकथित धर्म से जुड़े न जाने कितने चैनल सक्रिय हैं। अलग-अलग धर्मों, सिद्धान्तों, मतों, विचारों, सम्प्रदायों के कई रंगरूप और मुद्राओं वाले गुरु चौबीसों घंटे अपनी बातें दोहराते आपको दिख जाएंगे। धर्म में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति यदि इन सभी गुरुओं की बातों पर गौर करे तो उसके मन में शंका, भ्रम और प्रश्नों का जो बवंडर उठ खड़ा होगा उसे सम्भाल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहां किसी विशेष संप्रदाय, धर्म या मत से जुड़े किसी गुरु, व्यक्ति या अनुयायी के बारे कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। सिर्फ धर्म के वर्तमान स्वरूप, उसके अर्थ और उससे जुड़े लोगों की मानसिकता के बारे में कुछ सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे सवाल जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और धार्मिक जीवन से जुड़े हैं।
कई प्रश्न हैं: गुरु और शिष्य के बीच विभाजन और दूरी का आधार क्या है? शास्त्रों का ज्ञान? कोई अतीन्द्रिय ताकत? कोई चमत्कार? क्या शास्त्रों को पढ़कर और उनकी व्याख्या करके कोई व्यक्ति गुरु बन सकता है? क्या किसी धर्मग्रन्थ के कुछ अंशों को रट कर और उन्हें बार बार दोहरा कर कोई गुरु बन सकता है? आप कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति वास्तव में गुरु बनने के योग्य है? उसके अनुयायियों की संख्या के आधार पर या फिर इस उम्मीद से कि शायद उसके पास सत्य की कुंजी होगी? यदि आप यह जानते हैं कि किसी व्यक्ति के पास सत्य है तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि आपको भी पता है कि सत्य क्या है। और जब आप यह जानते ही हैं कि सत्य क्या है तो फिर किसी गुरु शरण में जाने की आपको जरूरत ही क्या है। मैंने कई सुप्रसिद्ध गुरुओं को देखा है। जिस तरह पॉप गायकों के कार्यक्रमों मे युवतियां चीखती चिल्लाती हैं, ठीक उसी तरह इन गुरुओं की सभाओं में मैंने सामूहिक हिस्टीरिया का हमला देखा है। इस तरह की अनियंत्रित विक्षिप्तता का धर्म/आध्यात्मिकता से क्या संबंध?
कहीं जीवन में ऐसे मित्र की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है जो उन प्रश्नों की तह तक ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा गहराई के साथ गया हो जो आपको भी छूते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति, यदि वह विनम्र और स्नेहपूर्ण है, तो वह आपको अपना मित्र समझेगा, न कि गुरु बनकर आपके सिर पर सवार हो जाएगा। वह सिर्फ इशारे करेगा, यदि वह खुद उन चीजों से बाहर हो चुका है जिससे आप अभी पीड़ित हैं। वह भ्रम में नहीं डालेगा। इस बारे में गौतम बुद्ध की एक बात याद आती है, ‘मेरी बातें चांद की ओर इशारा करने वाली एक अंगुली की तरह हैं। आप मेरी अंगुली को चांद न समझ लें।
गुरु पूजा की बड़ी महिमा गाई जाती है। यदि मान भी लिया जाए कि किसी ने जीवन की गुत्थियां सुलझा ली हैं और मानवीय अवस्था से परे जा चुका है, तो भी क्या आप उसकी पूजा करके कुछ समझ पाएंगे? क्या आइंस्टीन की पूजा करके सापेक्षता के सिद्धान्त को समझा जा सकता है या सचिन की पूजा करके अच्छा क्रिकेट खेलने के गुर सीखे जा सकते हैं?
गुरु शब्द का मूल अर्थ है ‘गु’ यानी अंधकार और ‘रु’ यानी हटाने वाले। अर्थात अंधकार को हटाने वाला गुरु होता है। ऐसा मानते हैं कि बुद्ध के आखिरी शब्द थे ‘अत्त दीपो भव’ यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार कोई सुनार सोने को घिसकर, परखकर उसकी शुद्धता के बारे में निर्णय लेता है उसी तरह मेरी शिक्षाओं को पहले परख लो तब अपनाओ। योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता एक तरह के संवाद हैं, जिनमें दो व्यक्ति अपने-अपने विचारों, प्रश्नों, अंतर्दृष्टियों को आपस में साझा करते हैं। राम एवं वशिष्ठ, जनक और अष्टावक्र, कृष्ण और अर्जुन से संबंधित ये ग्रंथ अस्तित्वगत विषयों पर हुए गंभीर संवादों का परिणाम हैं। धर्म का एक गहरा अर्थ है आत्मज्ञान, यानी स्वयं को जानना। खुद को, अपनी भावनाओं, विचारों एवं परेशानियों को समझने के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु, मैनेजमेंट गुरु एवं मनोचिकित्सकों से सलाह मशविरा करना एक तरह का फैशन हो चुका है। यह कहां तक तर्कसंगत है? अध्यात्म, धर्म और आत्मज्ञान के क्षेत्र में किसी गुरु या विशेषज्ञ की सत्ता मान लेने, उनके अनुयायी बनने, उनके नाम पर संगठनों का निर्माण करने और कई तरह के धार्मिक सर्कस आयोजित करने के प्रवृत्ति के बारे में सवाल उठाने चाहिए। यह आम बात है और जटिल भी, कि हमें स्वयं को या ईश्वर को, यदि ऐसी कोई सत्ता है, जानने के लिए तथाकथित गुरुओं और विशेषज्ञों की भीड़ की जरूरत पड़ती है। हमारी इस प्रवृत्ति का शोषण करने वाले कई लोग हैं जो हमारे और सत्य के बीच एजेंट होने का दावा करते हैं। हम सीधे खुद को समझने की कोशिश करने के बजाए किसी आसान शॉर्टकट में ज्यादा रुचि रखते हैं। मनोविज्ञान कई अर्थों में मानव मन को धर्म की तुलना में अधिक समझता है, और लगातार अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश में भी लगा है।
मेरे विचार से सही गुरु वह है जो दोस्त की तरह आपका हाथ थामे आपसे बातचीत करे और आपके भीतर छिपी हुई समझ को जगाने की कोशिश करे। आत्मबोध या खुद को समझने की यात्रा पूरी तरह से एक ऐसी यात्रा है जो हमारे मन की गहराइयों में घटित होती है। जहां आप अकेले होते हैं अपनी खामोशी के साथ, जिन्दगी से जुड़े अपने सवालों के साथ। जीवन के दूसरे क्षेत्रों जैसे किसी शैक्षिक विषय, खेल-कूद या संगीत आदि में तो किसी शिक्षक, मार्ग दर्शक की जरूरत समझ में आती है, किन्तु स्वयं खुद के बारे में कोई दूसरा कुछ बताए, ये समझ में आने वाली बात नहीं। मनोविज्ञान की कोई किताब आपको अपने क्रोध के बारे मे बहुत कुछ बता सकती है। एक मनोविश्लेषक आपकी भावनाओं और विचारों की चीर-फाड़ करके आपकी मेज पर रख सकता है, लेकिन इस तरह का ज्ञान और विश्लेषण हमें मुक्त नहीं कर सकता है।
स्कूल कॉलेजों में भी आज शिक्षक अपनी चरण चम्पी करवाने से बाज नहीं आते। पता नहीं क्यों, छात्रों से पैर छुआ कर, अपने अहंकार की मालिश करवा कर ही वे खुश क्यों होते हैं? क्या छात्रों के वे मित्र नहीं बन सकते? खुद को मात्र एक प्रशिक्षक या किसी खास विषय का जानकार नहीं मान सकते? यदि ज्ञान और सूचना के भंडार को एक तरफ रख दिया जाए, तो ऐसे कौन से गुण हैं, जिनके आधार पर एक शिक्षक खुद को किसी शिष्य से बेहतर बता सकता है? स्कूल और कॉलेजों में शिक्षक या इंस्ट्रक्टर शब्द का इस्तेमाल बेहतर रहेगा। गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए शिक्षा के संसार में।
यह बहुत संवेदनशील प्रश्न है और इसकी जड़ में सदियों पुरानी गहरी परंपराएं हैं। गुरुओं की तादाद एक ओर बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर आदमी का दुःख भी बढ़ता जा रहा है। यह दुःख किसी बाहरी एजेंसी की मदद से दूर नहीं हो सकता है। इसका कारण और निदान दोनों ही हमारे भीतर ही कहीं है। दूसरा कोई क्या करेगा। इनपर खुद हमें ही काम करना होगा। एक गहरी बौद्धिक अकर्मण्यता भी है और गहरा मानसिक आलस्य भी जो हमें खुद की समस्या को समझने और उन पर श्रम करने से रोकता है। ऐसे में गुरु सरीखा कोई हमें आसान रास्ते बताकर बहला ले जाता है पर वह हमारा उपकार कम और अपना भला ज्यादा करता है।
(चैतन्य नागर लेखक और पत्रकार हैं आप आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)