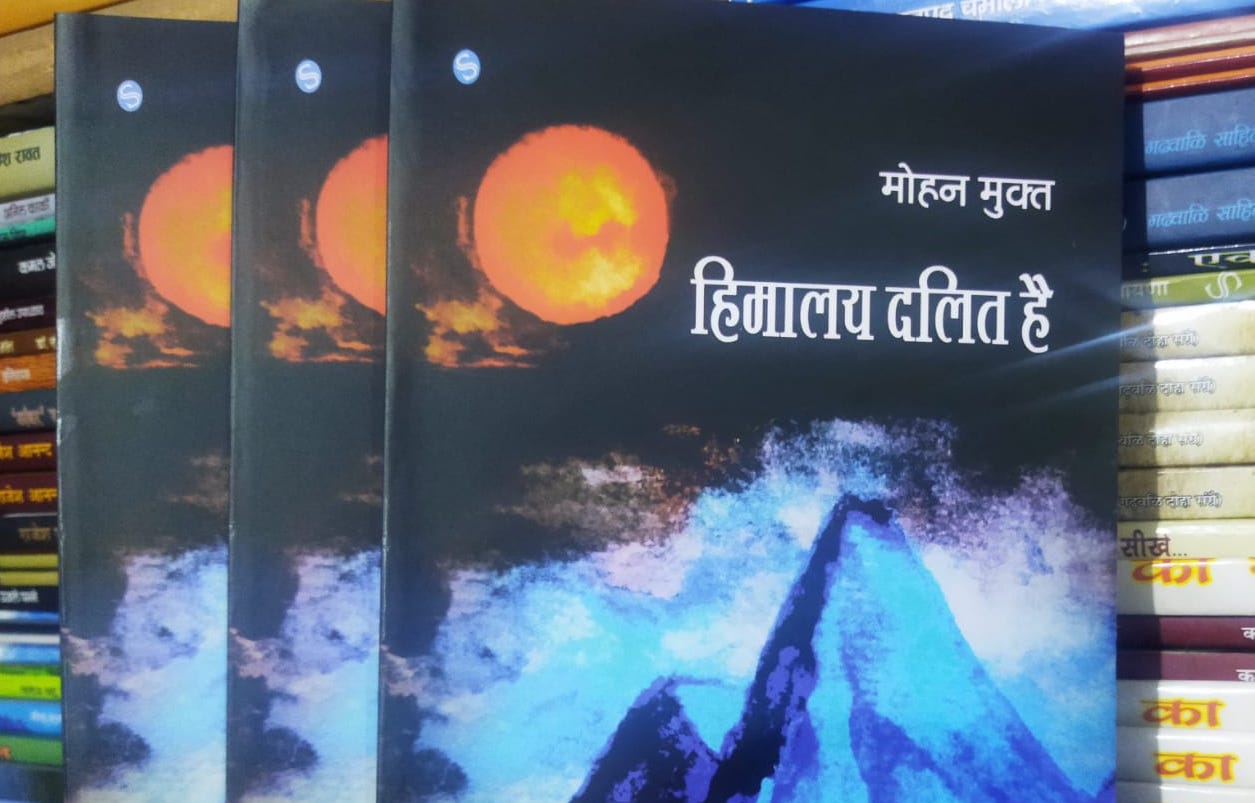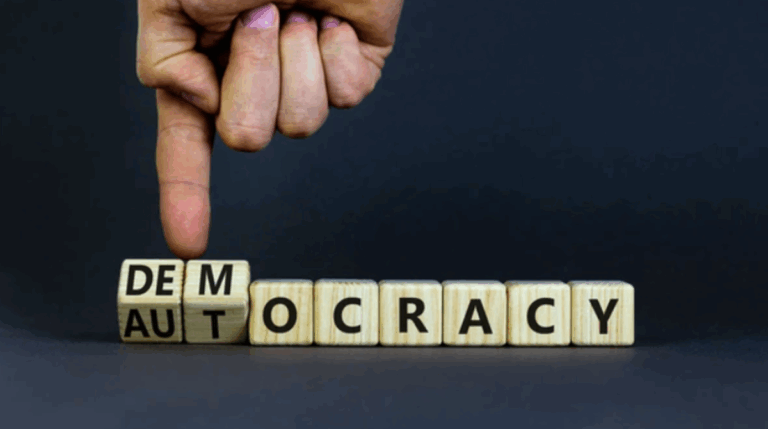‘हिमालय दलित है’ मोहन मुक्त का पहला कविता संग्रह है। संग्रह की कविताएं धधकते लावे की तरह हैं। यहां तक कि कवि की प्रेम कविताओं से भी एक आंच निकलती है। ऐसे लगता है कि कवि किसी ज्वालामुखी के दहाने पर बैठा है और खुद उसके भीतर भी एक ज्वालामुखी धधक रहा है। जो कोई भी इन कविताओं से गुजरेगा इस ज्वालामुखी की धधकती आंच और ताप को महसूस करेगा। ये कविताएं हिंदी कविता की अब तक की परंपरागत संवेदना से भिन्न संवेदना, चीजों को देखने का बिल्कुल ही नया विश्व दृष्टिकोण और इस सब को प्रस्तुत करने के लिए नए शिल्प और नई भाषा के लिए कवि की जद्दोजहद को सामने लाती हैं।
कवि हिंदी कविता के अब तक के मुहावरों को उलट देता है, बिल्कुल नई संवेदना, नई दृष्टि और नए प्रतीक एवं बिम्ब लेकर उपस्थित होता है, जिसके चलते इन कविताओं को हिंदी कविता की अब तक प्रचलित किसी धारा में समाहित कर पाना मुश्किल है, क्योंकि सभी धाराओं की संवेदना, वैचारिकी और शिल्प के रूप काफी हद तक समय के साथ रूढ़ हो गए हैं। इस संग्रह के कवि की संवेदना और वैचारिकी के जो आयाम हैं, वह किसी परंपरागत काव्य प्रतिमानों में खुद को अभिव्यक्त कर पाने में असमर्थ हैं, जिसके चलते परंपरागत काव्य प्रतिमानों को सचेतन-अचेतन और जाने-अनजाने तौर पर ध्वस्त करना कवि की जरूरत और विवशता दोनों बन जाती है। सच यह है कि जिस तरह हर गांव का दलित टोला सवर्णों का उपनिवेश रहा है , उनकी जमींदारी रही है और उन पर उनकी कब्जेदारी रही है, उसी तरह हिंदी कविता भी कमोवेश, कुछ एक अपवादों को छोड़कर आभिजात्य वर्गीय कवियों का उपनिवेश रही है, उसकी जमींदारी रही और उसकी भाषा और मुहावरे पर इस आभिजात्य वर्ग की संवेदना और वैचारिकी का कब्जा रहा है। कवि हिंदी कविता के कब्जेदारों-जमींदारों को इन शब्दों में चुनौती देता है-
तुम कविता के कब्ज़ेदार
तुम भाषा के ज़मींदार
बिम्ब को पलटो सुनो सलाह
अपने श्रेष्ठ को करो तबाह
करता हूँ तुमको आगाह
कविता के नाज़ी तानाशाह
भाषा के नाज़ी तानाशाह……
कविता के कब्जेदारों-जमींदारों को चुनौती देता कवि इस संग्रह में नए प्रतीक एवं बिम्ब गढ़ता है और कविता का नया मुहावरा ईजाद करता है। यहीं कवि की असल चुनौती भी शुरू होती है। यह सच है कि यदि कोई कवि लंबी काव्य परंपरा से प्राप्त विरासत की अगली कड़ी के रूप में खुद को अभिव्यक्त करता है, तो वह सहज संप्रेषणीय हो जाता है, क्योंकि उसके ज्यादातर प्रतीक और बिंब जाने-पहचाने होते हैं, थोड़े अपने बदले रूपों के साथ, लेकिन यदि कोई कवि ऐसा सच लेकर आ रहा है, जो उस भाषा की काव्य परंपरा में अभिव्यक्त नहीं हो सकता है, तो कवि के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसकी काव्य वस्तु नई होती है, दूसरी तरफ अभिव्यक्ति का रूप भी बिलकुल नया होता है, ऐसे में कविताओं को सहज-संप्रेषणीय बनाना एक मुश्किल प्रक्रिया हो जाती है और कवि कई सारी कविताएं अपने पाठ के लिए पाठकों के सामने चुनौती प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि कवि आभिजात्य कवियों की कविता की विरासत से अपनी संवेदना और वैचारिकी के लिए उपकरण नहीं ले सकता, वह उसके किसी काम की नहीं है। वह नई दृष्टि और नई भाषा ईजाद कर रहा है। यह उसके काव्य अंतर्वस्तु की जरूरत है और कवि का संकल्प भी है-
मैं एक शब्द नहीं लूंगा तुम्हारी भाषा से
मैं किसी लैंगिक या जाति सूचक गाली को नहीं बनाऊंगा अपना हथियार
मैं कोई वाक्य नहीं उलटूंगा
मैं सीधा वाक्य भी तुम्हारी भाषा का नहीं करुँगा इस्तेमाल
मैं तुम्हारी भाषा संस्कृति सभ्यता और धर्म को देखूंगा
अपनी तीख़ी स्पष्ट और बेखौफ़ निगाह से
और तुम बिल्कुल चुप हो जाओगे…..एकदम चुप…
यह स्थिति कविता के पुराने मुहावरे के अभ्यस्त पाठकों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है। इस संग्रह की कविताओं को कविता के परंपरागत मुहावरे में समझा ही नहीं जा सकता।
इस सब का निहितार्थ यह नहीं है कि यह संग्रह किसी किसी वायवयी दुनिया को अमूर्त तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जिस जीवन-यथार्थ को कवि अभिव्यक्त देता है, पूरी तरह ठोस है। अगर स्थान के अर्थ में कहें, तो इस कविता की दुनिया उत्तराखंड का पहाड़ी समाज और उसके नाभि का क्रूर यथार्थ है। पहाड़ और पहाड़ी समाज को देखने के आभिजात्य वर्गीय कवियों के जातिवादी, रोमांटिक और सतही नजरिए को कवि जोरदार ठोकर मारता है और बताता है कि पहाड़ का कोई गांव एक साझी ईकाई नहीं है, न उनकी कोई साझी संस्कृति और न ही उनका आपस में कोई भाई-चारा है, हर गांव में जाति की एक विशाल दीवार खड़ी है, जो सवर्णों और दलितों के बीच एक अनुल्लंघनीय सीमा खड़ी करती है। हर गांव में दलितों का एक टोला है, जिस पर सवर्णों का साम्राज्य है-
गांव अकेला दिखता है जो
उसके भीतर होते हैं दो
दोनों के बीच रहती सीमा
दुश्मन देशों जैसी सीमा
क्या एक गांव के भीतर रहते हैं दो देश ?
गाँव में साथ रहते है साम्राज्य उपनिवेश
कवि सवर्णों के इस उपनिवेश का निवासी है, उस उपनिवेश में जन्मा है, पला-बढ़ा है, सवर्णों के साम्राज्यवाद के बूटे तले वह खुद भी रौंदा गया है, उसके बालमन में अंकुरित होते मानवीय मनोभावों को कुचला गया है, उसके व्यक्तित्व, उसकी गरिमा को रौंदा गया है, उसे पल-पल पग-पग पर अपमानित किया गया है, इसका साक्ष्य कविताएं प्रस्तुत करती हैं-
;उस बच्चे के लिए कौन सा वक़्त होगा कठिन
जिसके कान को कागज़ से पकड़कर
मास्टरनी ने शब्द उमेठे थे
“तूने अपने नाम के आगे चंद्र क्यों लगाया रे “
यह बच्चा कोई और नहीं है, स्वयं कवि है।लेकिन यह अपमान उसका अकेले का नहीं है, न ही वह अकेले के अपमान को अभिव्यक्त कर रहा है। वह सवर्णों के उपनिवेश के निवासियों के सामूहिक अपमान और प्रतिरोध को जुबान दे रहा है-
मैं केवल अपनी बात नहीं बोलता
मैं जितने लोगों की जितनी बातें बोलता हूँ
उनके वज़न के नीचे तो
कोई भी नाम दबकर मर जायेगा
कवि ऐसी जगह की तलाश कर रहा है, जहां जाति जैसी स्थायी तौर बांटने वाला कोई अवरोध न हो। जाति सर्वव्यापी है, ‘देवभूमि’ उत्तराखंड इस जाति के पंक में आकंठ डूबी हुई है, इस संग्रह की कविताएं इसका साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। कवि बेचैनी के साथ ऐसी जगह की तलाश कर रहा है, जहां जाति की स्थायी बाधा और जाति जनित घुटन न हो-
मेरी प्यारी बताओ तो
वो कौन सी जगह है
इस धरती पर
जहाँ कुछ न हो
जात जैसा
कृत्रिम अनश्वर और स्थायी निरोध ………
यह सच है संग्रह की कविताओं की संवेदना और वैचारिकी की एक केंद्रीय विषय-वस्तु भारतीय समाज, विशेषकर उत्तराखंड के समाज का वर्ण-जाति जनित ढांचा है और उस ढांचे से पैदा हुए विद्रूपताएं और विरूपताएं है, लेकिन कवि की काव्य संवेदना यही तक सीमित नहीं, कवि की संवेदना और वैचारिकी का दायरा और फलक बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। कवि आंबेडकर और मार्क्स की तरह हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ है और भारत सहित पूरी दुनिया में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का स्वप्न देखता है। कवि मनुष्य-मनुष्य के बीच खड़े की गई सारी दीवारों को तोड़कर सारी दुनिया के इंसानों को सिर्फ इंसान के रूप में अपनाना चाहता है, उन्हें प्यार करना चाहता है-
सारे देश
सब भाषाएं
सभी संस्कृतियां
समूचा इतिहास
और धर्म सब के सब
ये सभी मिलकर भी मुझसे छीन नहीं सकते
इंसानों से प्यार करने का मेरा मूल अधिकार………
कवि भारतीय समााज के उस उपनिवेश का निवासी है, जो हर तरह के शोषण-उत्पीड़न और अन्याय का शिकार रहा है। इसके चलते कवि की काव्य संवेदना में हर तरह के शोषण-उत्पीड़न और अन्याय का प्रतिवाद दिखाई देता है, कवि को वर्चस्व और प्रभुत्व का कोई रूप स्वीकार्य नहीं है, वह सिर्फ उस साम्राज्य से मुक्ति नहीं चाहता, जिसके प्रभुत्व में उसे और उसके जैसे लोगों को जीना पड़ रहा है, वह दुनिया से हर तरह के साम्राज्य और उपनिवेशों का खात्मा चाहता है। कवि दुनिया की उस वैचारिकी का वाहक है, जो अन्याय के हर रूप का खात्मा चाहती है। कवि सार्वभौमिक न्याय का पक्षधर है। वह ऐसी दुनिया की कल्पना करता है, जिसमें एक दिन-
राजवंशों के वंशज
छुपायेंगे पहचान अपनी
सारे विश्वविजेता
लुटेरे कहे जायेंगे
पुरोहित और धर्माधिकारी अगर होंगे
तो मनोचिकित्सक के सामने होंगे
सारे झंडों के कपड़े उधेड़ दिये जायेंगे
महिलाएं इस संग्रह की काव्य संवेदना का एक बड़ा दायरा घेरती हैं। मर्द के रूप में इंसान ने अपने ही इंसानी समुदाय की महिलाओं पर इतिहास में सबसे पहले वर्चस्व और प्रभुत्व कायम किया और वह किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में आज भी जारी है। कवि महिलाओं के माध्यम पूरी मानव सभ्यता और संस्कृति को कटघरे में खड़ा करता है और मर्दों के नायकत्व के हर रूप को प्रश्नांकित करता है-
क्योंकि औरत अगर सवाल करे
तो सारे नायक धूल हो जायेंगे
संस्कृतियां नायक विहीन हो जाएंगी
तथाकथित महान सभ्यताओं ने और महान भाषाओं ने औरत होना ही एक गाली बना दिया। इस संग्रह में कवि बार-बार औरतों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के आधार पर सभ्यताओं, संस्कृतियों और भाषा का आकलन करता है और उन्हें औरत विरोधी पाता है-
सभी संस्कृतियों में
सभी सभ्यताओं में
सभी भाषाओं में
सभी औरतों को
दी जाती है एक ही गाली
वो गाली एक औरत का नाम है
किसी कवि का इतिहासबोध उसकी काव्य संवेदना और वैचारिकी के निर्धारण में एक अहम भूमिका निभाता है। मानव इतिहास और भारत के इतिहास की दो परंपराएं रही हैं, एक आक्रामणकारी, वर्चस्वशाली और प्रभुत्व की पंरपरा और दूसरी इस आक्रमण को झेलने वालों, आक्रामणकारियों के वर्चस्व और प्रभुत्व में जीने वालों और उसका प्रतिवाद एवं प्रतिरोध करने वालों की परंपरा। कवि मोहन मुक्त इतिहास के इस तथ्य पर खुश है कि वह जिसका वंशज है, जो उसके पूर्वज हैं, जिनका वह वारिस है, वे आक्रामणकारी नहीं थे, बलात्कारी नहीं थे, उन्होंने गांव नहीं जलाए। कवि इतिहास के हर उस व्यक्तित्व को खारिज करता है, जो अन्यायी रहा हो, आक्रामणकारी रहा हो। कवि स्वयं को सिर्फ और सिर्फ न्याय की परंपरा के साथ जोड़ता है-
मैं ख़ुश हूँ
कि मैं अपने पुरखों के बारे में नहीं जानता
मैं नहीं जानता
क्योंकि वो इतिहास में नहीं हैं
वो इतिहास में नहीं हैं
क्योंकि वो आक्रमणकारी नहीं थे
उन्होंने कोई नगर नहीं जीते
कोई गांव नहीं जलाये
उन्होंने औरतों के बलात्कार नहीं किये
उन्होंने अबोध बच्चों के सर नहीं काटे
वो धर्माधिकारी नहीं थे
वो जमींदार नहीं थे
निश्चित ही वो लुटेरे नहीं थे
X X X X
मैं ख़ुश हूँ कि मेरे पुरखों ने गाय और भैंस दोनों को खाया था
मैं ख़ुश हूँ कि मेरे पुरखे आदमखोर नहीं थे
कवि इस तथ्य से भी खुश है कि उसे इतिहास की विरासत में ईश्वर भी नहीं मिला है, उसके पुरखों से ईश्वर भी छीन लिया गया था। कवि की विरासत ईश्वविहीनों की विरासत है और उस विरासत पर उसे प्रसन्नता भी है-
मैं नास्तिक पैदा हुआ था
मेरा ईश्वर मेरे पुरखों से लूट लिया गया था
हालांकि लुटेरों ने बेकार चीज लूटी थी
लेकिन अब उनका डुप्लीकेट ईश्वर मुझे नहीं चाहिए
कवि मोहन मुक्त को मेहनतकश वर्ग और उसकी मानवीय संस्कृति बार-बार अपनी ओर खींचती है, कवि को इसका गहरा अहसास है कि जो कुछ दुनिया में रचा गया है, सृजित किया गया है, गढ़ा गया है और जिससे दुनिया खूबसूरत है, उसका केंद्रीय रचयिता और मूल सृजनकर्ता मेहनतकश वर्ग है, जिसने अकेले-अकेले नहीं, सामूहिक तौर सब कुछ रचा है, सृजित किया है और उसकी कृति सबसे सुंदर तब होती है, जब वह स्वतंत्रता के साथ सामूहिक तौर उसको सृजित करता है-
पाषाण काल के बेडौल औजारों में था सौंदर्य
श्रम का सौंदर्य
इसलिये नहीं कि उन बेडौल औजारों से पहले
कोई औजार नहीं थे
इसलिये भी नहीं कि उनके बाद औजार बेडौल नहीं रहे
उनमें सौंदर्य था क्योंकि वो जिन हाथों में थे अब तक
वो हाथ जंजीर नहीं जानते थे
वो बेडौल हथियार सुन्दर थे
क्योंकि उन्हें थामने वाले हाथ स्वतंत्र थे
कवि मोहन मुक्त गहरे और ठोस रूप में स्थानीय हैं, उतने ही सार्वभौमिक भी हैं, वे गहन संवेदना के साथ भौतिकवादी वैज्ञानिक वैचारिकी से लैश हैं, उन्हें पता है कि जिस दुनिया में हम रहे हैं, वह एक साम्राज्यवादी दुनिया है, कुछ चंद साम्राज्यवादी देश दुनिया के अधिकांश देशों की नियति तय करते हैं। क्रांति और क्रांतिकारियों की नियति भी-
सीआईए ईश्वर से कम नहीं
वो सब जानती है
सीआईए को पता था
कि चेग्वेरा को कहाँ और कब मारना है
कल ही तो मारा गया था वो भी
एडगर हूवर को पता था
कि मार्टिन लूथर किंग का मरना ज़रूरी है
संग्रह की कई कविताओं में क्रांति और क्रांतिकारी बदलाव के प्रति कवि की खुली पक्षधरता दिखाई देती है, लेकिन भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की गंभीर समस्याओं और सीमाओं से भी कवि अच्छी तरह अवगत है। भारतीय क्रांति की केंद्रीय समस्या को कवि ने सिर्फ दो पंक्तियों सशक्त तरीके से अभिव्यक्त कर दिया है। भारतीय में क्रांति न संपन्न हो पाने की मुख्य समस्या यह रही है कि क्रांति की वैचारिकी से जो आभिजात्य वर्ग लैस था, क्रांति उसकी जरूरत नहीं थी और जिस मेहनतकश वर्ग, बहुलांश दलितों-पिछड़ों की क्रांति जरूरत थी, उसके पास क्रांतिकारी विचारधारा पहुंची ही नहीं, यह पहुंचने ही नहीं दी गई-
क्रांति तुम्हारी समझ थी
और मेरी ज़रूरत
लेकिन वैज्ञानिक इतिहास चेतना से लैस कवि को इस तथ्य का गहरा अहसास है कि चाहे भारत में क्रांतिकारी बदलाव का प्रश्न हो या दुनिया के किसी कोने में, इसकी अगुवाई करने वाले वे लोग होंगे, जो अब इतिहास से बहिष्कृत रहे हैं और सभ्यता द्वारा तिरस्कृत। ऐसे लोग सबसे लिए न्यायपूर्ण नई दुनिया गढ़ेंगे-
और मैं एकदम स्पष्ट कि
इतिहास से बहिष्कृत
और सभ्यताओं में तिरस्कृत लोग ही
बनायेंगे नया इतिहास
गढ़ेंगे नई सभ्यता
सबके लिए
सभी के लिए ..
(वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉ. सिद्धार्थ की समीक्षा।)